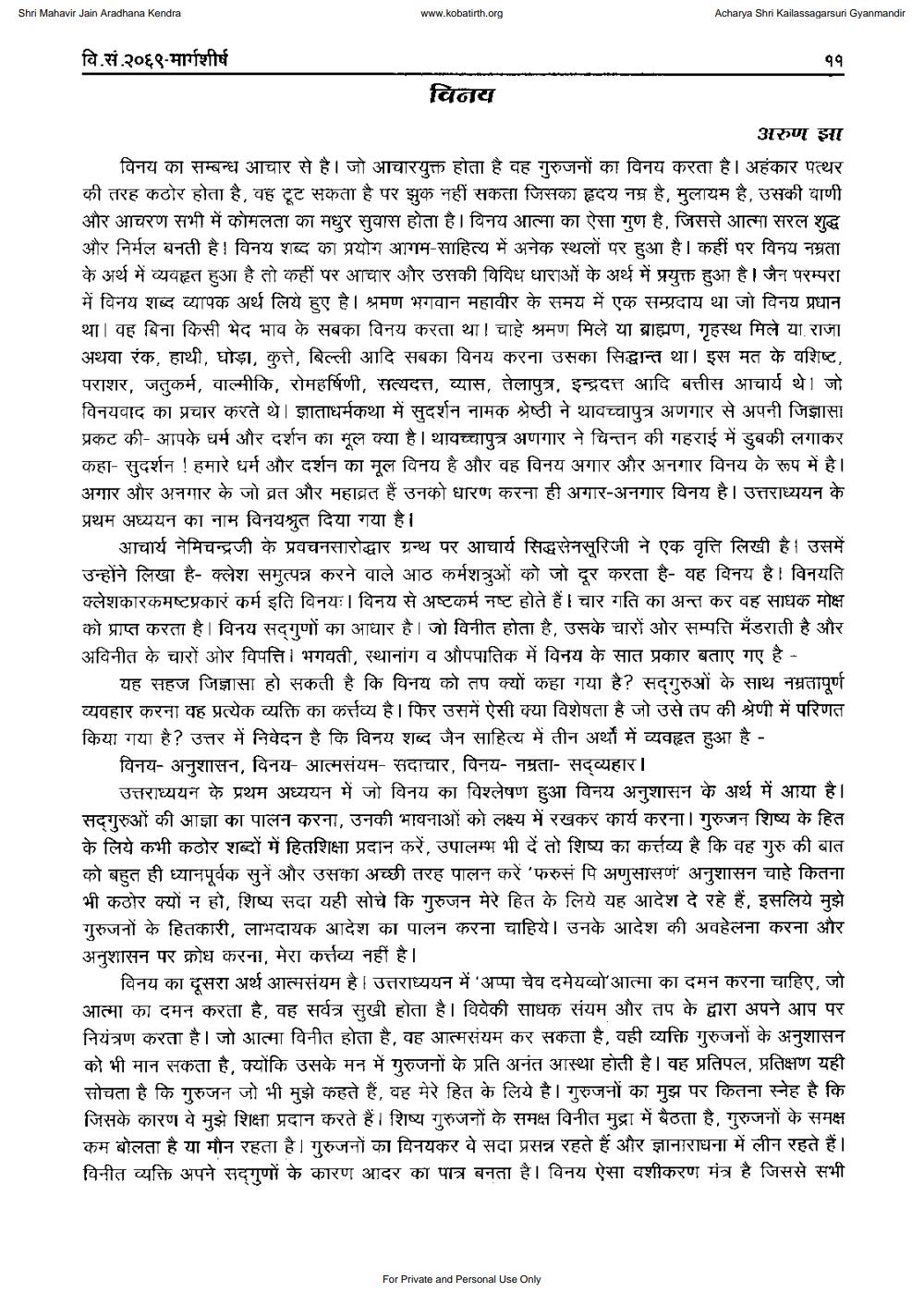________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
वि.सं. २०६९ - मार्गशीर्ष
www.kobatirth.org
विनय
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
For Private and Personal Use Only
११
अरुण झा
विनय का सम्बन्ध आचार से है। जो आचारयुक्त होता है वह गुरुजनों का विनय करता है। अहंकार पत्थर की तरह कठोर होता है, वह टूट सकता है पर झुक नहीं सकता जिसका हृदय नम्र है, मुलायम है, उसकी याणी और आचरण सभी में कोमलता का मधुर सुवास होता है। विनय आत्मा का ऐसा गुण है, जिससे आत्मा सरल शुद्ध और निर्मल बनती है। विनय शब्द का प्रयोग आगम साहित्य में अनेक स्थलों पर हुआ है। कहीं पर विनय नम्रता के अर्थ में व्यवहृत हुआ है तो कहीं पर आधार और उसकी विविध धाराओं के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैन परम्परा में विनय शब्द व्यापक अर्थ लिये हुए है। श्रमण भगवान महावीर के समय में एक सम्प्रदाय था जो विनय प्रधान था। वह बिना किसी भेद भाव के सबका विनय करता था। चाहे श्रमण मिले या ब्राह्मण, गृहस्थ मिले या राजा अथवा रंक, हाथी, घोड़ा, कुत्ते, बिल्ली आदि सबका विनय करना उसका सिद्धान्त था। इस मत के वशिष्ट, पराशर, जतुकर्म, वाल्मीकि, रोमहर्षिणी, सत्यदत्त, व्यास, तेलापुत्र इन्द्रदत्त आदि बत्तीस आचार्य थे जो विनयवाद का प्रचार करते थे। ज्ञाताधर्मकथा में सुदर्शन नामक श्रेष्ठी ने थावच्चापुत्र अणगार से अपनी जिज्ञासा प्रकट की- आपके धर्म और दर्शन का मूल क्या है । थावच्चापुत्र अणगार ने चिन्तन की गहराई में डुबकी लगाकर कहा- सुदर्शन ! हमारे धर्म और दर्शन का मूल विनय है और वह विनय अगार और अनगार विनय के रूप में है । अगार और अनगार के जो व्रत और महाव्रत हैं उनको धारण करना ही अगार अनगार विनय है। उत्तराध्ययन के प्रथम अध्ययन का नाम विनयश्रुत दिया गया है।
आचार्य नेमिचन्द्रजी के प्रवचनसारोद्धार ग्रन्थ पर आचार्य सिद्धसेनसूरिजी ने एक वृत्ति लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है- क्लेश समुत्पन्न करने वाले आठ कर्मशत्रुओं को जो दूर करता है- वह विनय है । विनयति क्लेशकारकमष्टप्रकारं कर्म इति विनयः । विनय से अष्टकर्म नष्ट होते हैं। चार गति का अन्त कर वह साधक मोक्ष को प्राप्त करता है । विनय सद्गुणों का आधार है। जो विनीत होता है, उसके चारों ओर सम्पत्ति मँडराती है और अविनीत के चारों ओर विपत्ति भगवती, स्थानांग व औपपातिक में विनय के सात प्रकार बताए गए है
यह सहज जिज्ञासा हो सकती है कि विनय को तप क्यों कहा गया है? सद्गुरुओं के साथ नम्रतापूर्ण व्यवहार करना वह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। फिर उसमें ऐसी क्या विशेषता है जो उसे तप की श्रेणी में परिणत किया गया है ? उत्तर में निवेदन है कि विनय शब्द जैन साहित्य में तीन अर्थों में व्यवहृत हुआ है -
विनय अनुशासन, विनय आत्मसंयम सदाचार, विनय नम्रता सद्व्यहार |
उत्तराध्ययन के प्रथम अध्ययन में जो विनय का विश्लेषण हुआ विनय अनुशासन के अर्थ में आया है। सद्गुरुओं की आज्ञा का पालन करना, उनकी भावनाओं को लक्ष्य में रखकर कार्य करना । गुरुजन शिष्य के हित के लिये कभी कठोर शब्दों में हितशिक्षा प्रदान करें, उपालम्भ भी दें तो शिष्य का कर्त्तव्य है कि वह गुरु की बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनें और उसका अच्छी तरह पालन करें फरुसं पि अणुसासन अनुशासन चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, शिष्य सदा यही सोचे कि गुरुजन मेरे हित के लिये यह आदेश दे रहे हैं. इसलिये मुझे गुरुजनों के हितकारी लाभदायक आदेश का पालन करना चाहिये। उनके आदेश की अवहेलना करना और अनुशासन पर क्रोध करना मेरा कर्त्तव्य नहीं है।
विनय का दूसरा अर्थ आत्मसंयम है। उत्तराध्ययन में 'अप्पा चेच दमेयव्वो आत्मा का दमन करना चाहिए, जो आत्मा का दमन करता है, वह सर्वत्र सुखी होता है। विवेकी साधक संयम और तप के द्वारा अपने आप पर नियंत्रण करता है। जो आत्मा विनीत होता है, वह आत्मसंयम कर सकता है, यही व्यक्ति गुरुजनों के अनुशासन को भी मान सकता है, क्योंकि उसके मन में गुरुजनों के प्रति अनंत आस्था होती है। वह प्रतिपल, प्रतिक्षण यही सोचता है कि गुरुजन जो भी मुझे कहते हैं, यह मेरे हित के लिये है। गुरुजनों का मुझ पर कितना स्नेह है कि जिसके कारण वे मुझे शिक्षा प्रदान करते हैं। शिष्य गुरुजनों के समक्ष विनीत मुद्रा में बैठता है, गुरुजनों के समक्ष कम बोलता है या मौन रहता है। गुरुजनों का विनयकर वे सदा प्रसन्न रहते हैं और ज्ञानाराधना में लीन रहते हैं। विनीत व्यक्ति अपने सद्गुणों के कारण आदर का पात्र बनता है। विनय ऐसा वशीकरण मंत्र है जिससे सभी