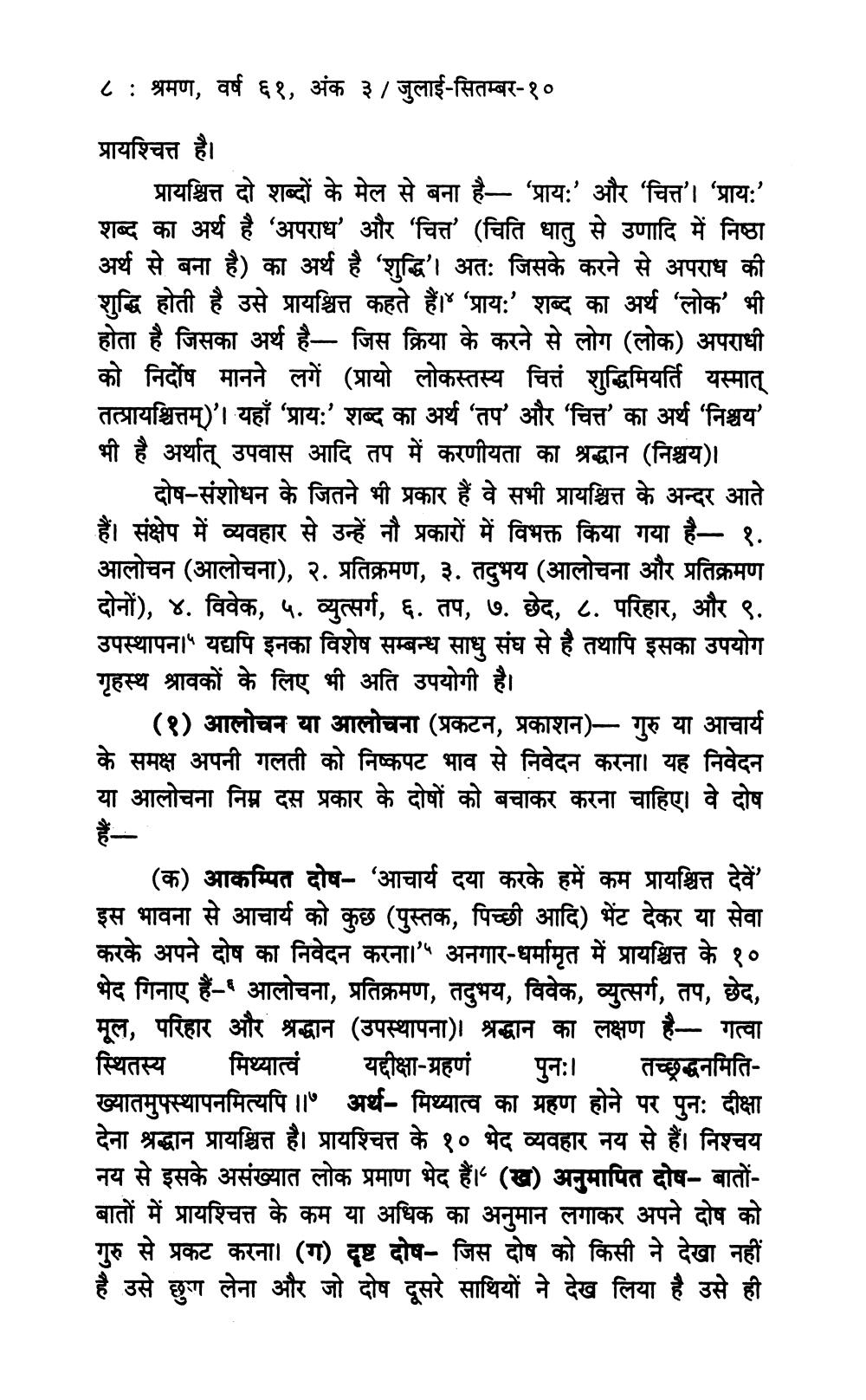________________
८ : श्रमण, वर्ष ६१, अंक ३ / जुलाई-सितम्बर - १०
प्रायश्चित्त है।
प्रायश्चित्त दो शब्दों के मेल से बना है- 'प्रायः' और 'चित्त' । 'प्रायः ' शब्द का अर्थ है 'अपराध' और 'चित्त' (चिति धातु से उणादि में निष्ठा अर्थ से बना है) का अर्थ है 'शुद्धि' । अतः जिसके करने से अपराध की शुद्धि होती है उसे प्रायश्चित्त कहते हैं।' 'प्रायः' शब्द का अर्थ 'लोक' भी होता है जिसका अर्थ है- जिस क्रिया के करने से लोग (लोक) अपराधी को निर्दोष मानने लगें (प्रायो लोकस्तस्य चित्तं शुद्धिमियर्ति यस्मात् तत्प्रायश्चित्तम्)’। यहाँ ‘प्रायः' शब्द का अर्थ 'तप' और 'चित्त' का अर्थ 'निश्चय' भी है अर्थात् उपवास आदि तप में करणीयता का श्रद्धान ( निश्चय ) ।
दोष- संशोधन के जितने भी प्रकार हैं वे सभी प्रायश्चित्त के अन्दर आते हैं। संक्षेप में व्यवहार से उन्हें नौ प्रकारों में विभक्त किया गया है— १. आलोचन (आलोचना), २. प्रतिक्रमण, ३. तदुभय (आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों), ४. विवेक, ५. व्युत्सर्ग, ६. तप, ७. छेद, ८. परिहार, और ९. उपस्थापन।' यद्यपि इनका विशेष सम्बन्ध साधु संघ से है तथापि इसका उपयोग गृहस्थ श्रावकों के लिए भी अति उपयोगी है।
(१) आलोचन या आलोचना (प्रकटन, प्रकाशन ) - गुरु या आचार्य के समक्ष अपनी गलती को निष्कपट भाव से निवेदन करना। यह निवेदन या आलोचना निम्न दस प्रकार के दोषों को बचाकर करना चाहिए। वे दोष हैं
(क) आकम्पित दोष- 'आचार्य दया करके हमें कम प्रायश्चित्त देवें' इस भावना से आचार्य को कुछ ( पुस्तक, पिच्छी आदि) भेंट देकर या सेवा करके अपने दोष का निवेदन करना । ५ अनगार - धर्मामृत में प्रायश्चित्त के १० भेद गिनाए हैं - आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार और श्रद्धान ( उपस्थापना ) । श्रद्धान का लक्षण है- गत्वा स्थितस्य मिथ्यात्वं यद्दीक्षा ग्रहणं पुनः । तच्छ्रद्धनमिति - ख्यातमुपस्थापनमित्यपि ।। अर्थ- मिथ्यात्व का ग्रहण होने पर पुनः दीक्षा देना श्रद्धान प्रायश्चित्त है। प्रायश्चित्त के १० भेद व्यवहार नय से हैं। निश्चय नय से इसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं।' (ख) अनुमापित दोष- बातोंबातों में प्रायश्चित्त के कम या अधिक का अनुमान लगाकर अपने दोष को गुरु से प्रकट करना । (ग) दृष्ट दोष- जिस दोष को किसी ने देखा नहीं है उसे छु लेना और जो दोष दूसरे साथियों ने देख लिया है उसे ही