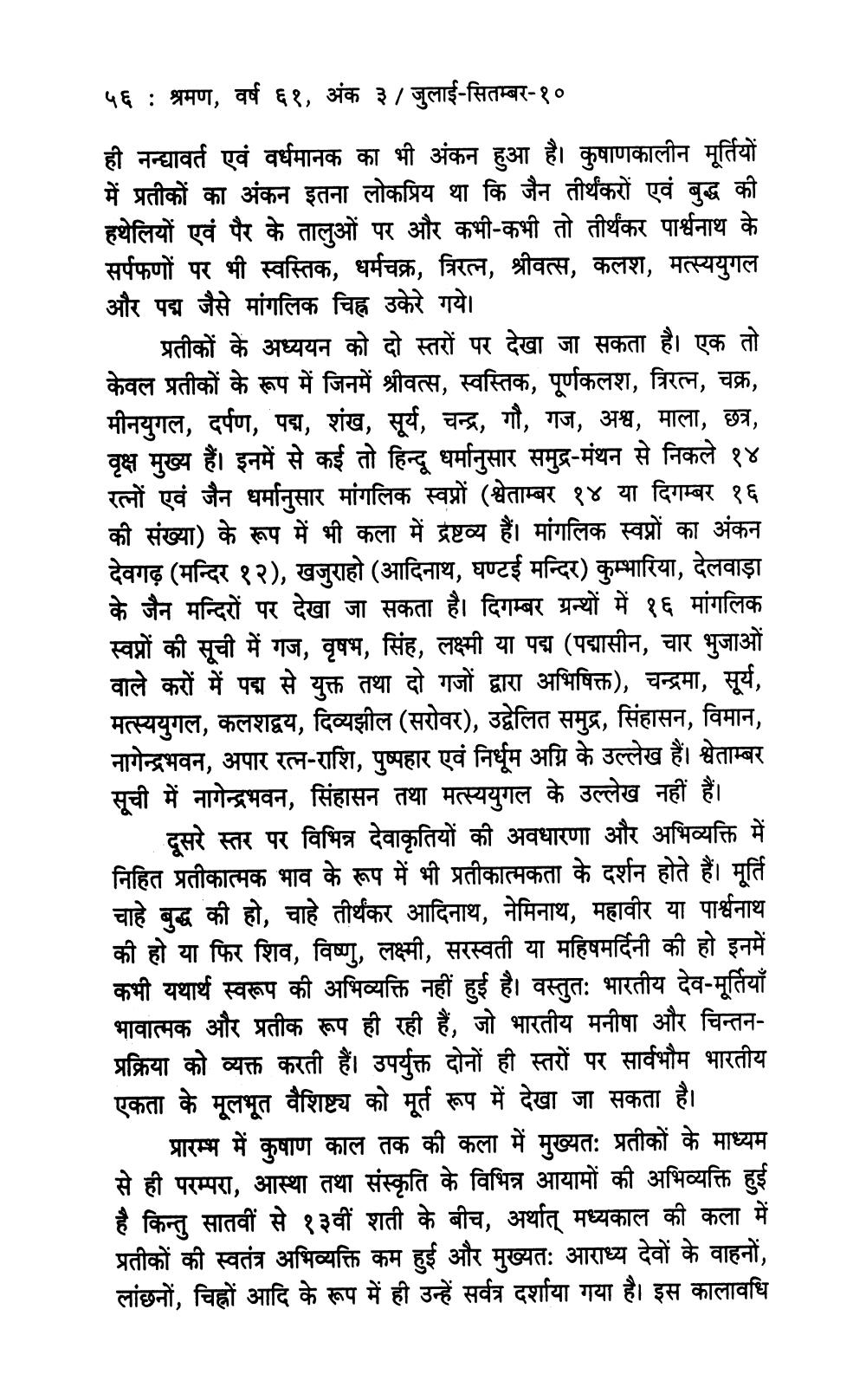________________
५६ : श्रमण, वर्ष ६१, अंक ३ / जुलाई-सितम्बर-१०
ही नन्द्यावर्त एवं वर्धमानक का भी अंकन हुआ है। कुषाणकालीन मूर्तियों में प्रतीकों का अंकन इतना लोकप्रिय था कि जैन तीर्थंकरों एवं बुद्ध की हथेलियों एवं पैर के तालुओं पर और कभी-कभी तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ के सर्पफणों पर भी स्वस्तिक, धर्मचक्र, त्रिरत्न, श्रीवत्स, कलश, मत्स्ययुगल और पद्म जैसे मांगलिक चिह्न उकेरे गये।
प्रतीकों के अध्ययन को दो स्तरों पर देखा जा सकता है। एक तो केवल प्रतीकों के रूप में जिनमें श्रीवत्स, स्वस्तिक, पूर्णकलश, त्रिरत्न, चक्र, मीनयुगल, दर्पण, पद्म, शंख, सूर्य, चन्द्र, गौ, गज, अश्व, माला, छत्र, वृक्ष मुख्य हैं। इनमें से कई तो हिन्दू धर्मानुसार समुद्र-मंथन से निकले १४ रत्नों एवं जैन धर्मानुसार मांगलिक स्वप्नों (श्वेताम्बर १४ या दिगम्बर १६ की संख्या) के रूप में भी कला में द्रष्टव्य हैं। मांगलिक स्वप्नों का अंकन देवगढ़ (मन्दिर १२), खजुराहो (आदिनाथ, घण्टई मन्दिर) कुम्भारिया, देलवाड़ा के जैन मन्दिरों पर देखा जा सकता है। दिगम्बर ग्रन्थों में १६ मांगलिक स्वप्नों की सूची में गज, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी या पद्म (पद्मासीन, चार भुजाओं वाले करों में पद्म से युक्त तथा दो गजों द्वारा अभिषिक्त), चन्द्रमा, सूर्य, मत्स्ययुगल, कलशद्वय, दिव्यझील (सरोवर), उद्वेलित समुद्र, सिंहासन, विमान, नागेन्द्रभवन, अपार रत्न-राशि, पुष्पहार एवं निर्धूम अग्नि के उल्लेख हैं। श्वेताम्बर सूची में नागेन्द्रभवन, सिंहासन तथा मत्स्ययुगल के उल्लेख नहीं हैं।
दूसरे स्तर पर विभिन्न देवाकृतियों की अवधारणा और अभिव्यक्ति में निहित प्रतीकात्मक भाव के रूप में भी प्रतीकात्मकता के दर्शन होते हैं। मूर्ति चाहे बुद्ध की हो, चाहे तीर्थंकर आदिनाथ, नेमिनाथ, महावीर या पार्श्वनाथ की हो या फिर शिव, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती या महिषमर्दिनी की हो इनमें कभी यथार्थ स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं हुई है। वस्तुतः भारतीय देव-मूर्तियाँ भावात्मक और प्रतीक रूप ही रही हैं, जो भारतीय मनीषा और चिन्तनप्रक्रिया को व्यक्त करती हैं। उपर्युक्त दोनों ही स्तरों पर सार्वभौम भारतीय एकता के मूलभूत वैशिष्ट्य को मूर्त रूप में देखा जा सकता है।
प्रारम्भ में कुषाण काल तक की कला में मुख्यतः प्रतीकों के माध्यम से ही परम्परा, आस्था तथा संस्कृति के विभिन्न आयामों की अभिव्यक्ति हुई है किन्तु सातवीं से १३वीं शती के बीच, अर्थात् मध्यकाल की कला में प्रतीकों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति कम हुई और मुख्यतः आराध्य देवों के वाहनों, लांछनों, चिह्नों आदि के रूप में ही उन्हें सर्वत्र दर्शाया गया है। इस कालावधि