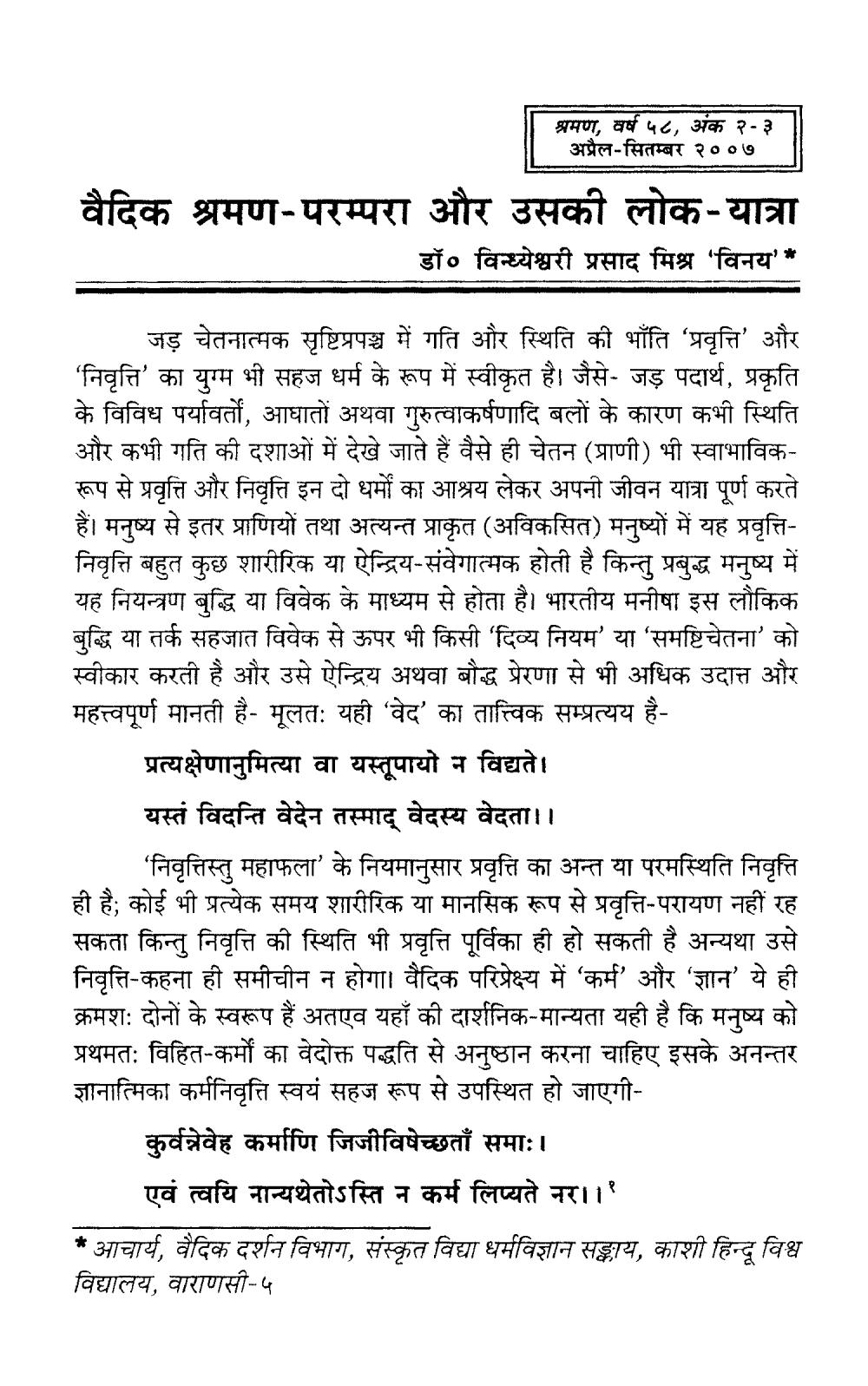________________
श्रमण, वर्ष ५८, अंक २-३ अप्रैल-सितम्बर २००७
वैदिक श्रमण परम्परा और उसकी लोक- यात्रा
डॉ० विन्ध्येश्वरी प्रसाद मिश्र 'विनय' *
जड़ चेतनात्मक सृष्टिप्रपञ्च में गति और स्थिति की भाँति 'प्रवृत्ति' और 'निवृत्ति' का युग्म भी सहज धर्म के रूप में स्वीकृत है। जैसे- जड़ पदार्थ, प्रकृति के विविध पर्यावर्तो, आघातों अथवा गुरुत्वाकर्षणादि बलों के कारण कभी स्थिति और कभी गति की दशाओं में देखे जाते हैं वैसे ही चेतन (प्राणी) भी स्वाभाविकरूप से प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दो धर्मों का आश्रय लेकर अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करते हैं। मनुष्य से इतर प्राणियों तथा अत्यन्त प्राकृत (अविकसित) मनुष्यों में यह प्रवृत्ति - निवृत्ति बहुत कुछ शारीरिक या ऐन्द्रिय संवेगात्मक होती है किन्तु प्रबुद्ध मनुष्य में यह नियन्त्रण बुद्धि या विवेक के माध्यम से होता है। भारतीय मनीषा इस लौकिक बुद्धि या तर्क सहजात विवेक से ऊपर भी किसी 'दिव्य नियम' या 'समष्टिचेतना' को स्वीकार करती हैं और उसे ऐन्द्रिय अथवा बौद्ध प्रेरणा से भी अधिक उदात्त और महत्त्वपूर्ण मानती है - मूलतः यही 'वेद' का तात्त्विक सम्प्रत्यय है
प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न विद्यते ।
यस्तं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता । ।
'निवृत्तिस्तु महाफला' के नियमानुसार प्रवृत्ति का अन्त या परमस्थिति निवृत्ति ही है; कोई भी प्रत्येक समय शारीरिक या मानसिक रूप से प्रवृत्ति परायण नहीं रह सकता किन्तु निवृत्ति की स्थिति भी प्रवृत्ति पूर्विका ही हो सकती है अन्यथा उसे निवृत्ति - कहना ही समीचीन न होगा। वैदिक परिप्रेक्ष्य में 'कर्म' और 'ज्ञान' ये ही क्रमशः दोनों के स्वरूप हैं अतएव यहाँ की दार्शनिक मान्यता यही है कि मनुष्य को प्रथमतः विहित-कर्मों का वेदोक्त पद्धति से अनुष्ठान करना चाहिए इसके अनन्तर ज्ञानात्मिका कर्मनिवृत्ति स्वयं सहज रूप से उपस्थित हो जाएगी -
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छताँ समाः ।
१
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नर । । '
* आचार्य, वैदिक दर्शन विभाग, संस्कृत विद्या धर्मविज्ञान सङ्काय, काशी हिन्दू विश्व विद्यालय, वाराणसी-५