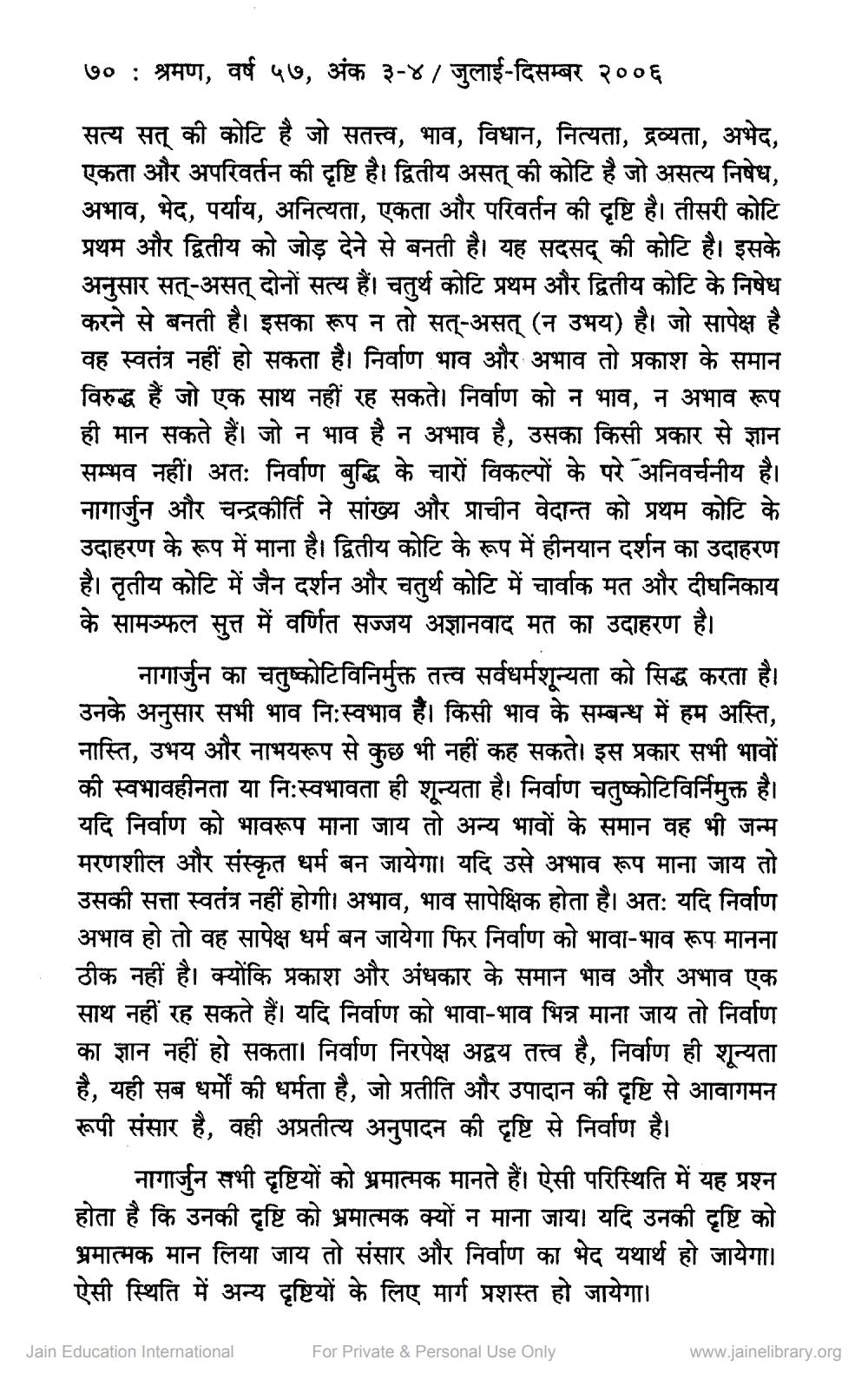________________
७० : श्रमण, वर्ष ५७, अंक ३-४ / जुलाई-दिसम्बर २००६ सत्य सत् की कोटि है जो सतत्त्व, भाव, विधान, नित्यता, द्रव्यता, अभेद, एकता और अपरिवर्तन की दृष्टि है। द्वितीय असत् की कोटि है जो असत्य निषेध, अभाव, भेद, पर्याय, अनित्यता, एकता और परिवर्तन की दृष्टि है। तीसरी कोटि प्रथम और द्वितीय को जोड़ देने से बनती है। यह सदसद् की कोटि है। इसके अनुसार सत्-असत् दोनों सत्य हैं। चतुर्थ कोटि प्रथम और द्वितीय कोटि के निषेध करने से बनती है। इसका रूप न तो सत्-असत् (न उभय) है। जो सापेक्ष है वह स्वतंत्र नहीं हो सकता है। निर्वाण भाव और अभाव तो प्रकाश के समान विरुद्ध हैं जो एक साथ नहीं रह सकते। निर्वाण को न भाव, न अभाव रूप ही मान सकते हैं। जो न भाव है न अभाव है, उसका किसी प्रकार से ज्ञान सम्भव नहीं। अत: निर्वाण बुद्धि के चारों विकल्पों के परे अनिवर्चनीय है। नागार्जुन और चन्द्रकीर्ति ने सांख्य और प्राचीन वेदान्त को प्रथम कोटि के उदाहरण के रूप में माना है। द्वितीय कोटि के रूप में हीनयान दर्शन का उदाहरण है। तृतीय कोटि में जैन दर्शन और चतुर्थ कोटि में चार्वाक मत और दीघनिकाय के सामफल सुत्त में वर्णित सज्जय अज्ञानवाद मत का उदाहरण है।
नागार्जुन का चतुष्कोटिविनिर्मुक्त तत्त्व सर्वधर्मशून्यता को सिद्ध करता है। उनके अनुसार सभी भाव नि:स्वभाव है। किसी भाव के सम्बन्ध में हम अस्ति, नास्ति, उभय और नाभयरूप से कुछ भी नहीं कह सकते। इस प्रकार सभी भावों की स्वभावहीनता या नि:स्वभावता ही शून्यता है। निर्वाण चतुष्कोटिविनिमुक्त है। यदि निर्वाण को भावरूप माना जाय तो अन्य भावों के समान वह भी जन्म मरणशील और संस्कृत धर्म बन जायेगा। यदि उसे अभाव रूप माना जाय तो उसकी सत्ता स्वतंत्र नहीं होगी। अभाव, भाव सापेक्षिक होता है। अत: यदि निर्वाण अभाव हो तो वह सापेक्ष धर्म बन जायेगा फिर निर्वाण को भावा-भाव रूप मानना ठीक नहीं है। क्योंकि प्रकाश और अंधकार के समान भाव और अभाव एक साथ नहीं रह सकते हैं। यदि निर्वाण को भावा-भाव भिन्न माना जाय तो निर्वाण का ज्ञान नहीं हो सकता। निर्वाण निरपेक्ष अद्वय तत्त्व है, निर्वाण ही शून्यता है, यही सब धर्मों की धर्मता है, जो प्रतीति और उपादान की दृष्टि से आवागमन रूपी संसार है, वही अप्रतीत्य अनुपादन की दृष्टि से निर्वाण है।
नागार्जुन सभी दृष्टियों को भ्रमात्मक मानते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह प्रश्न होता है कि उनकी दृष्टि को भ्रमात्मक क्यों न माना जाय। यदि उनकी दृष्टि को भ्रमात्मक मान लिया जाय तो संसार और निर्वाण का भेद यथार्थ हो जायेगा। ऐसी स्थिति में अन्य दृष्टियों के लिए मार्ग प्रशस्त हो जायेगा।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org