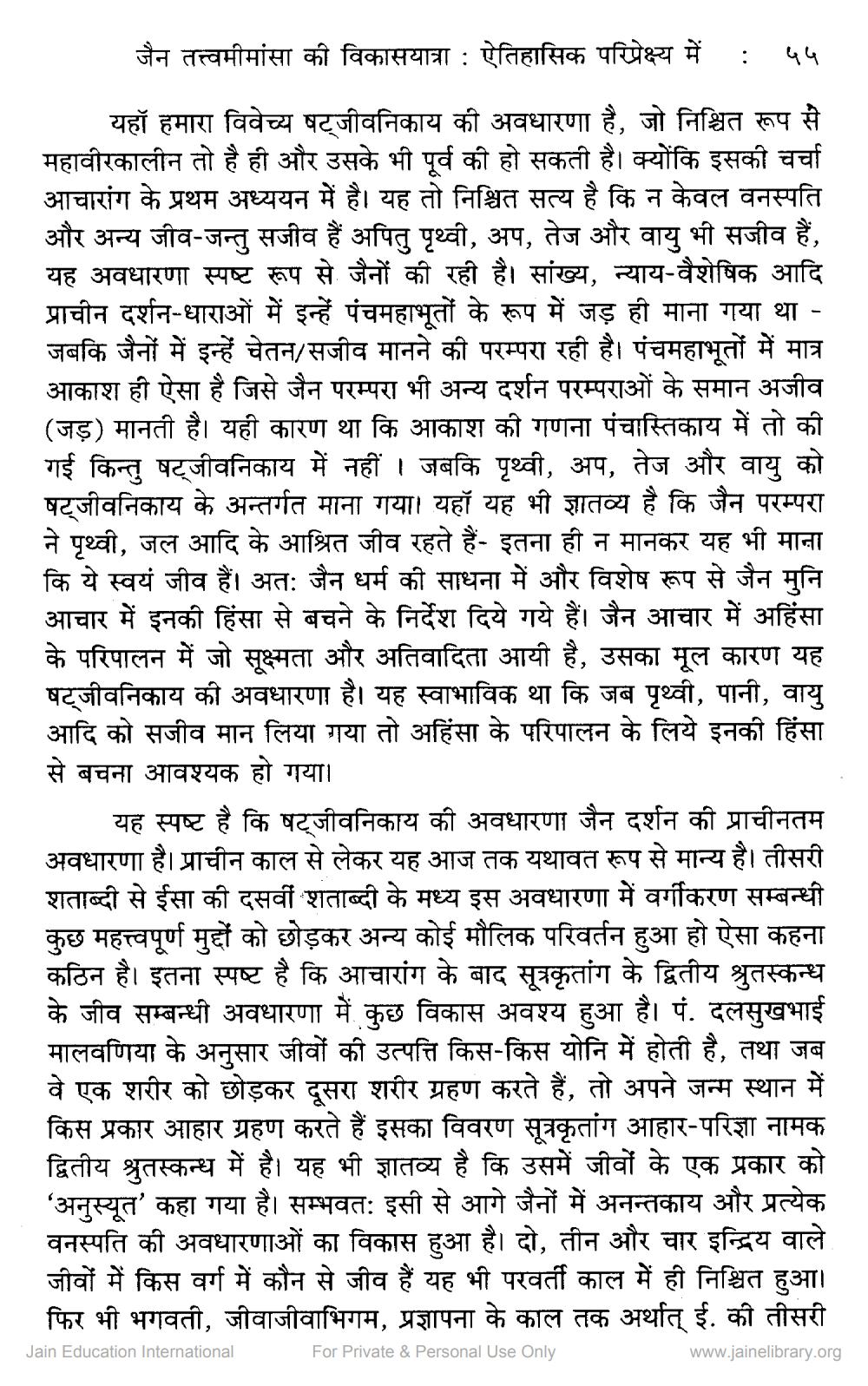________________
जैन तत्त्वमीमांसा की विकासयात्रा : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में :
यहाॅ हमारा विवेच्य षट्जीवनिकाय की अवधारणा है, जो निश्चित रूप से महावीरकालीन तो है ही और उसके भी पूर्व की हो सकती है। क्योंकि इसकी चर्चा आचारांग के प्रथम अध्ययन में है। यह तो निश्चित सत्य है कि न केवल वनस्पति और अन्य जीव-जन्तु सजीव हैं अपितु पृथ्वी, अप, तेज और वायु भी सजीव हैं, यह अवधारणा स्पष्ट रूप से जैनों की रही है। सांख्य, न्याय-वैशेषिक आदि प्राचीन दर्शन-धाराओं में इन्हें पंचमहाभूतों के रूप में जड़ ही माना गया था जबकि जैनों में इन्हें चेतन / सजीव मानने की परम्परा रही है। पंचमहाभूतों में मात्र आकाश ही ऐसा है जिसे जैन परम्परा भी अन्य दर्शन परम्पराओं के समान अजीव (जड़) मानती है। यही कारण था कि आकाश की गणना पंचास्तिकाय में तो की गई किन्तु षट्जीवनिकाय में नहीं । जबकि पृथ्वी, अप, तेज और वायु को षट्जीवनिकाय के अन्तर्गत माना गया । यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि जैन परम्परा ने पृथ्वी, जल आदि के आश्रित जीव रहते हैं- इतना ही न मानकर यह भी माना कि ये स्वयं जीव हैं। अत: जैन धर्म की साधना में और विशेष रूप से जैन मुनि आचार में इनकी हिंसा से बचने के निर्देश दिये गये हैं। जैन आचार में अहिंसा के परिपालन में जो सूक्ष्मता और अतिवादिता आयी है, उसका मूल कारण यह षट्जीवनिकाय की अवधारणा है। यह स्वाभाविक था कि जब पृथ्वी, पानी, वायु आदि को सजीव मान लिया गया तो अहिंसा के परिपालन के लिये इनकी हिंसा से बचना आवश्यक हो गया।
-
यह स्पष्ट है कि षट्जीवनिकाय की अवधारणा जैन दर्शन की प्राचीनतम अवधारणा है। प्राचीन काल से लेकर यह आज तक यथावत रूप से मान्य है । तीसरी शताब्दी से ईसा की दसवीं शताब्दी के मध्य इस अवधारणा में वर्गीकरण सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर अन्य कोई मौलिक परिवर्तन हुआ हो ऐसा कहना कठिन है। इतना स्पष्ट है कि आचारांग के बाद सूत्रकृतांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के जीव सम्बन्धी अवधारणा में कुछ विकास अवश्य हुआ है। पं. दलसुखभाई मालवणिया के अनुसार जीवों की उत्पत्ति किस-किस योनि में होती है, तथा जब वे एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं, तो अपने जन्म स्थान में किस प्रकार आहार ग्रहण करते हैं इसका विवरण सूत्रकृतांग आहार - परिज्ञा नामक द्वितीय श्रुतस्कन्ध में है। यह भी ज्ञातव्य है कि उसमें जीवों के एक प्रकार को 'अनुस्यूत' कहा गया है। सम्भवत: इसी से आगे जैनों में अनन्तकाय और प्रत्येक वनस्पति की अवधारणाओं का विकास हुआ है। दो, तीन और चार इन्द्रिय वाले जीवों में किस वर्ग में कौन से जीव हैं यह भी परवर्ती काल में ही निश्चित हुआ। फिर भी भगवती, जीवाजीवाभिगम, प्रज्ञापना के काल तक अर्थात् ई. की तीसरी
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org