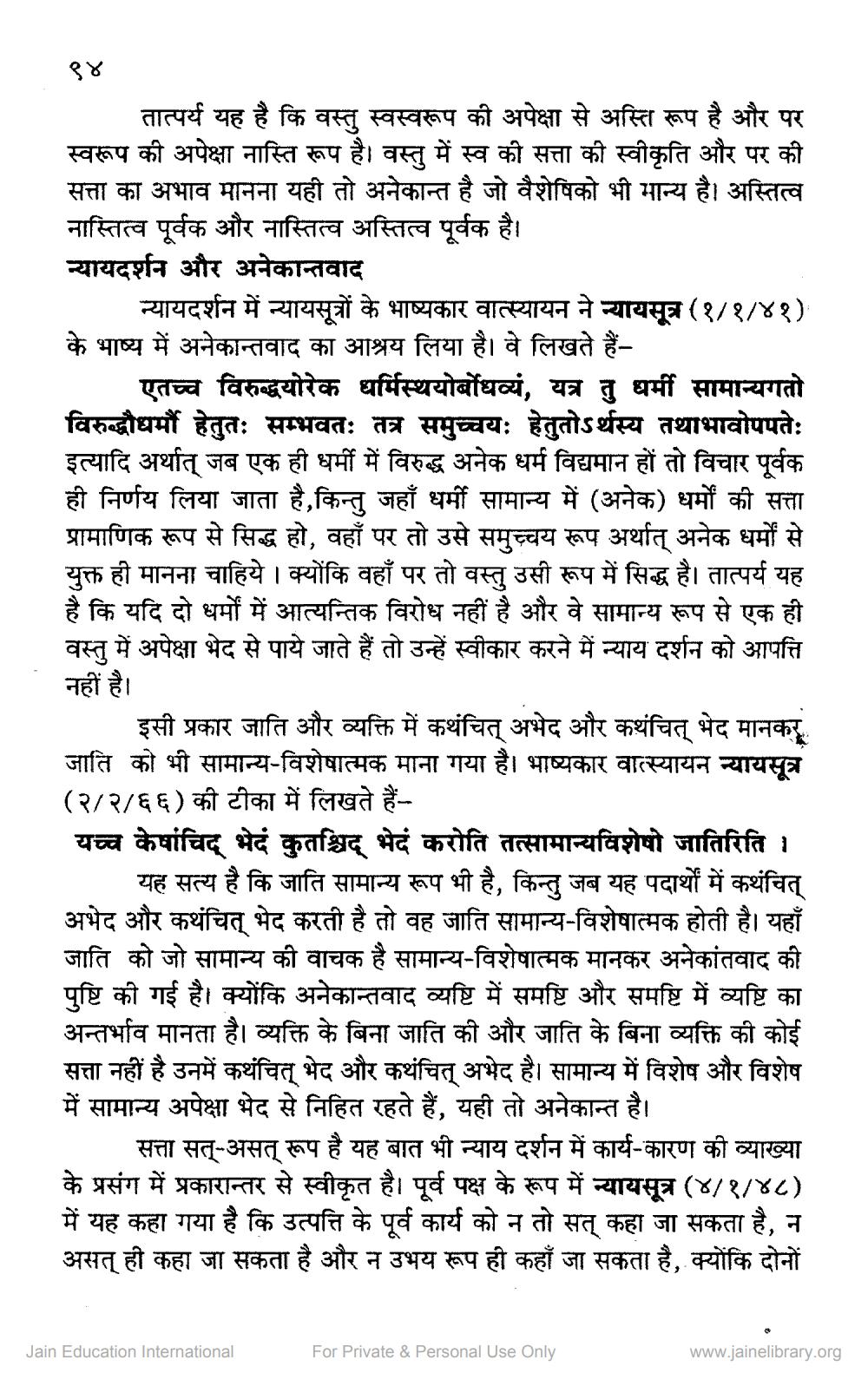________________
९४
तात्पर्य यह है कि वस्तु स्वस्वरूप की अपेक्षा से अस्ति रूप है और पर स्वरूप की अपेक्षा नास्ति रूप है। वस्तु में स्व की सत्ता की स्वीकृति और पर की सत्ता का अभाव मानना यही तो अनेकान्त है जो वैशेषिको भी मान्य है। अस्तित्व नास्तित्व पूर्वक और नास्तित्व अस्तित्व पूर्वक है। न्यायदर्शन और अनेकान्तवाद
न्यायदर्शन में न्यायसूत्रों के भाष्यकार वात्स्यायन ने न्यायसूत्र (१/१/४१) के भाष्य में अनेकान्तवाद का आश्रय लिया है। वे लिखते हैं
एतच्च विरुद्धयोरेक धर्मिस्थयोर्बोधव्यं, यत्र तु धर्मी सामान्यगतो विरुद्धौधौ हेतुतः सम्भवतः तत्र समुच्चयः हेतुतोऽर्थस्य तथाभावोपपतेः इत्यादि अर्थात् जब एक ही धर्मी में विरुद्ध अनेक धर्म विद्यमान हों तो विचार पूर्वक ही निर्णय लिया जाता है, किन्तु जहाँ धर्मी सामान्य में (अनेक) धर्मों की सत्ता प्रामाणिक रूप से सिद्ध हो, वहाँ पर तो उसे समुच्चय रूप अर्थात् अनेक धर्मों से युक्त ही मानना चाहिये । क्योंकि वहाँ पर तो वस्तु उसी रूप में सिद्ध है। तात्पर्य यह है कि यदि दो धर्मों में आत्यन्तिक विरोध नहीं है और वे सामान्य रूप से एक ही वस्तु में अपेक्षा भेद से पाये जाते हैं तो उन्हें स्वीकार करने में न्याय दर्शन को आपत्ति नहीं है।
इसी प्रकार जाति और व्यक्ति में कथंचित् अभेद और कथंचित् भेद मानकर जाति को भी सामान्य-विशेषात्मक माना गया है। भाष्यकार वात्स्यायन न्यायसूत्र (२/२/६६) की टीका में लिखते हैंयच्च केषांचिद् भेदं कुतश्चिद् भेदं करोति तत्सामान्यविशेषो जातिरिति ।
__ यह सत्य है कि जाति सामान्य रूप भी है, किन्तु जब यह पदार्थों में कथंचित् अभेद और कथंचित् भेद करती है तो वह जाति सामान्य-विशेषात्मक होती है। यहाँ जाति को जो सामान्य की वाचक है सामान्य-विशेषात्मक मानकर अनेकांतवाद की पुष्टि की गई है। क्योंकि अनेकान्तवाद व्यष्टि में समष्टि और समष्टि में व्यष्टि का अन्तर्भाव मानता है। व्यक्ति के बिना जाति की और जाति के बिना व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है उनमें कथंचित् भेद और कथंचित् अभेद है। सामान्य में विशेष और विशेष में सामान्य अपेक्षा भेद से निहित रहते हैं, यही तो अनेकान्त है।
सत्ता सत्-असत् रूप है यह बात भी न्याय दर्शन में कार्य-कारण की व्याख्या के प्रसंग में प्रकारान्तर से स्वीकृत है। पूर्व पक्ष के रूप में न्यायसूत्र (४/१/४८) में यह कहा गया है कि उत्पत्ति के पूर्व कार्य को न तो सत् कहा जा सकता है, न असत् ही कहा जा सकता है और न उभय रूप ही कहाँ जा सकता है, क्योंकि दोनों
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org