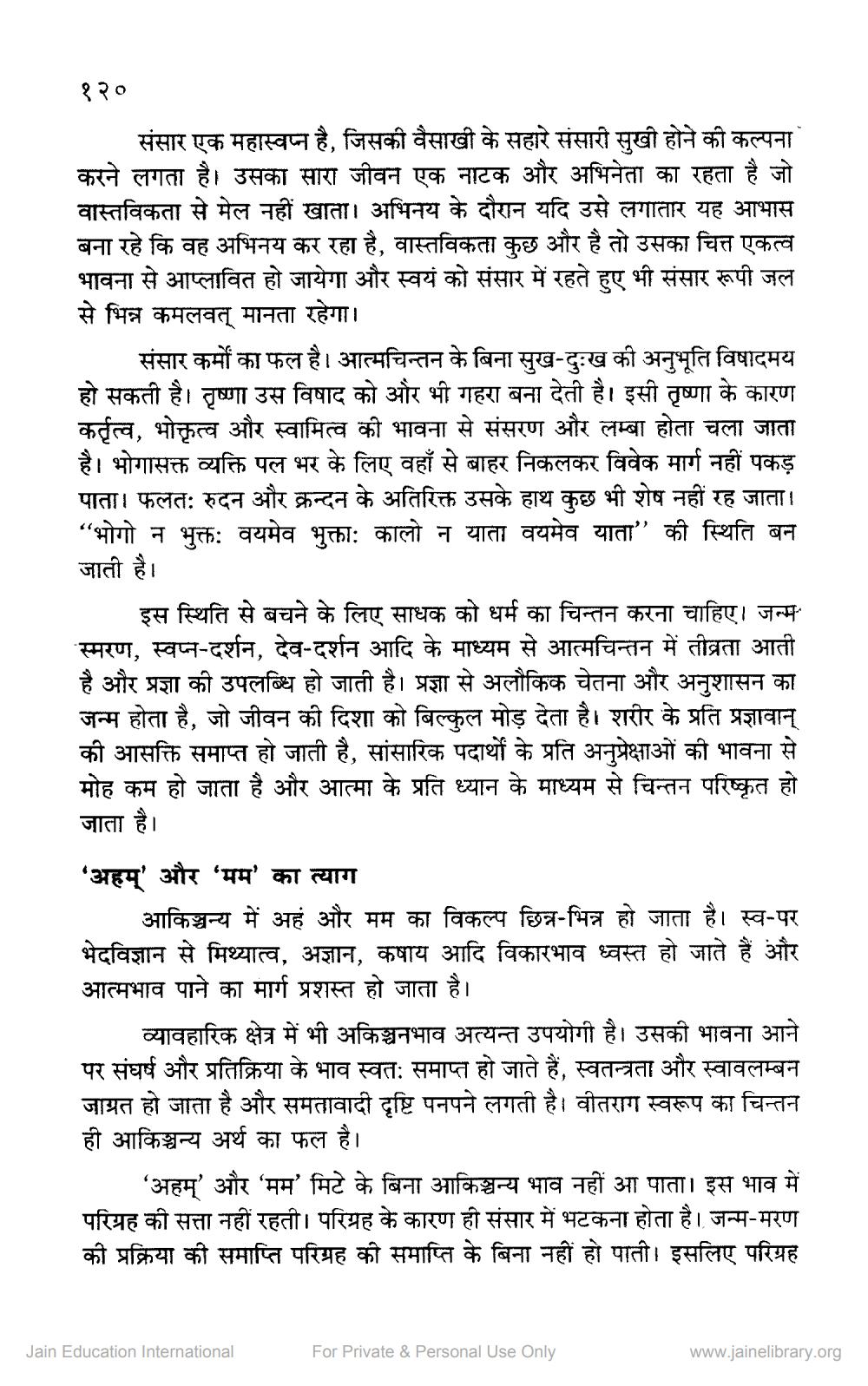________________
१२०
संसार एक महास्वप्न है, जिसकी वैसाखी के सहारे संसारी सुखी होने की कल्पना करने लगता है। उसका सारा जीवन एक नाटक और अभिनेता का रहता है जो वास्तविकता से मेल नहीं खाता। अभिनय के दौरान यदि उसे लगातार यह आभास बना रहे कि वह अभिनय कर रहा है, वास्तविकता कुछ और है तो उसका चित्त एकत्व भावना से आप्लावित हो जायेगा और स्वयं को संसार में रहते हुए भी संसार रूपी जल से भिन्न कमलवत् मानता रहेगा ।
संसार कर्मों का फल है। आत्मचिन्तन के बिना सुख-दुःख की अनुभूति विषादमय हो सकती है। तृष्णा उस विषाद को और भी गहरा बना देती है। इसी तृष्णा के कारण कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व की भावना से संसरण और लम्बा होता चला जाता है । भोगासक्त व्यक्ति पल भर के लिए वहाँ से बाहर निकलकर विवेक मार्ग नहीं पकड़ पाता । फलतः रुदन और क्रन्दन के अतिरिक्त उसके हाथ कुछ भी शेष नहीं रह जाता। " भोगो न भुक्तः वयमेव भुक्ताः कालो न याता वयमेव याता" की स्थिति बन जाती है।
इस स्थिति से बचने के लिए साधक को धर्म का चिन्तन करना चाहिए । जन्म स्मरण, स्वप्न-दर्शन, देव-दर्शन आदि के माध्यम से आत्मचिन्तन में तीव्रता आती है और प्रज्ञा की उपलब्धि हो जाती है। प्रज्ञा से अलौकिक चेतना और अनुशासन का जन्म होता है, जो जीवन की दिशा को बिल्कुल मोड़ देता है । शरीर के प्रति प्रज्ञावान् की आसक्ति समाप्त हो जाती है, सांसारिक पदार्थों के प्रति अनुप्रेक्षाओं की भावना से मोह कम हो जाता है और आत्मा के प्रति ध्यान के माध्यम से चिन्तन परिष्कृत हो जाता है।
'अहम्' और 'मम' का त्याग
आकिञ्चन्य में अहं और मम का विकल्प छिन्न-भिन्न हो जाता है। स्व-पर भेदविज्ञान से मिथ्यात्व, अज्ञान, कषाय आदि विकारभाव ध्वस्त हो जाते हैं और आत्मभाव पाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।
व्यावहारिक क्षेत्र में भी अकिञ्चनभाव अत्यन्त उपयोगी है। उसकी भावना आने पर संघर्ष और प्रतिक्रिया के भाव स्वतः समाप्त हो जाते हैं, स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन जाग्रत हो जाता है और समतावादी दृष्टि पनपने लगती है। वीतराग स्वरूप का चिन्तन ही आकिञ्चन्य अर्थ का फल है ।
'अहम्' और 'मम' मिटे के बिना आकिञ्चन्य भाव नहीं आ पाता । इस भाव में परिग्रह की सत्ता नहीं रहती । परिग्रह के कारण ही संसार में भटकना होता है। जन्म-मरण की प्रक्रिया की समाप्ति परिग्रह की समाप्ति के बिना नहीं हो पाती। इसलिए परिग्रह
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org