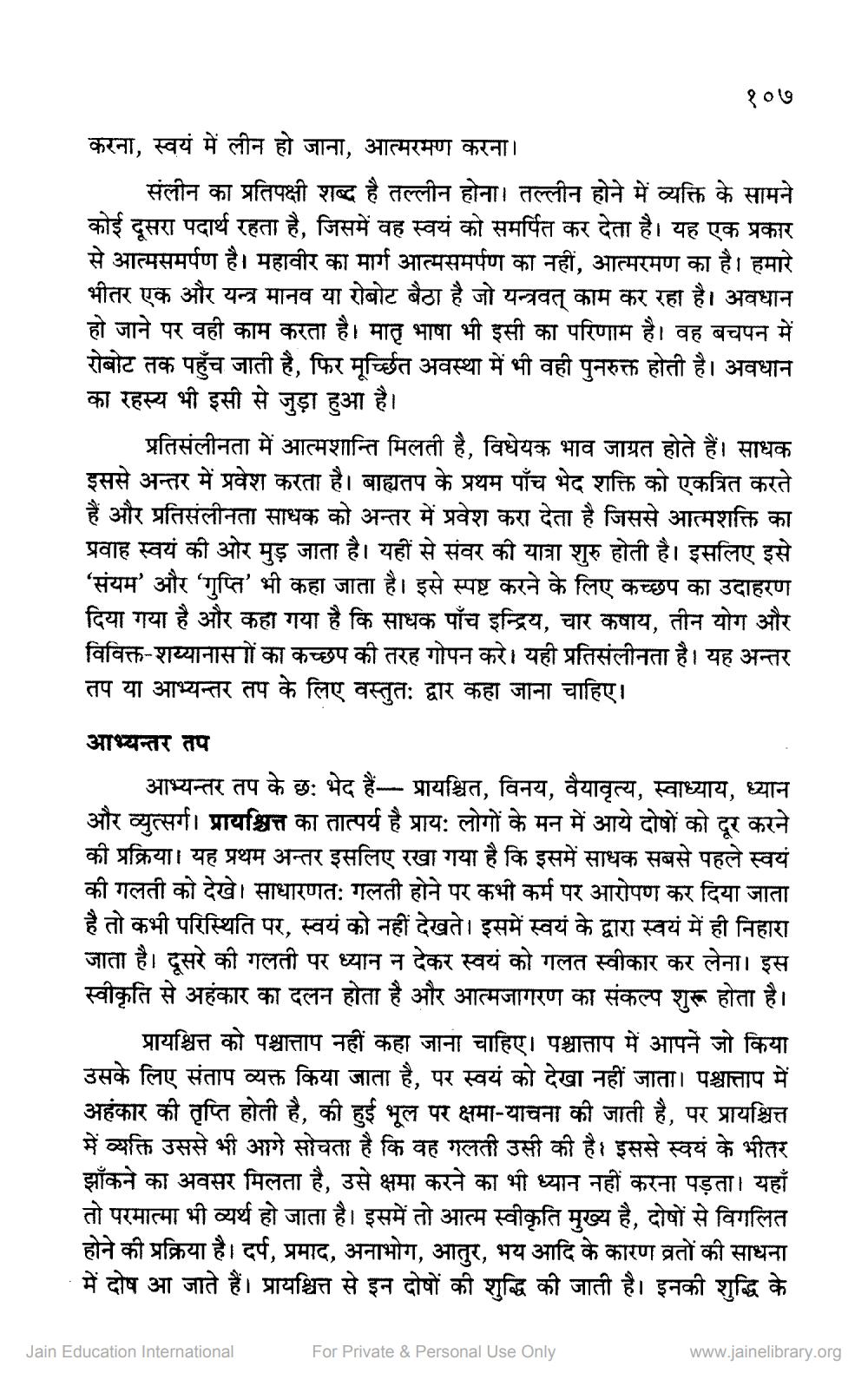________________
१०७
करना, स्वयं में लीन हो जाना, आत्मरमण करना।
संलीन का प्रतिपक्षी शब्द है तल्लीन होना। तल्लीन होने में व्यक्ति के सामने कोई दूसरा पदार्थ रहता है, जिसमें वह स्वयं को समर्पित कर देता है। यह एक प्रकार से आत्मसमर्पण है। महावीर का मार्ग आत्मसमर्पण का नहीं, आत्मरमण का है। हमारे भीतर एक और यन्त्र मानव या रोबोट बैठा है जो यन्त्रवत् काम कर रहा है। अवधान हो जाने पर वही काम करता है। मातृ भाषा भी इसी का परिणाम है। वह बचपन में रोबोट तक पहुँच जाती है, फिर मूर्च्छित अवस्था में भी वही पुनरुक्त होती है। अवधान का रहस्य भी इसी से जुड़ा हुआ है।
प्रतिसंलीनता में आत्मशान्ति मिलती है, विधेयक भाव जाग्रत होते हैं। साधक इससे अन्तर में प्रवेश करता है। बाह्यतप के प्रथम पाँच भेद शक्ति को एकत्रित करते हैं और प्रतिसंलीनता साधक को अन्तर में प्रवेश करा देता है जिससे आत्मशक्ति का प्रवाह स्वयं की ओर मुड़ जाता है। यहीं से संवर की यात्रा शुरु होती है। इसलिए इसे 'संयम' और 'गुप्ति' भी कहा जाता है। इसे स्पष्ट करने के लिए कच्छप का उदाहरण दिया गया है और कहा गया है कि साधक पाँच इन्द्रिय, चार कषाय, तीन योग और विविक्त-शय्यानासों का कच्छप की तरह गोपन करे। यही प्रतिसंलीनता है। यह अन्तर तप या आभ्यन्तर तप के लिए वस्तुत: द्वार कहा जाना चाहिए।
आभ्यन्तर तप
आभ्यन्तर तप के छ: भेद हैं- प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। प्रायश्चित्त का तात्पर्य है प्राय: लोगों के मन में आये दोषों को दूर करने की प्रक्रिया। यह प्रथम अन्तर इसलिए रखा गया है कि इसमें साधक सबसे पहले स्वयं की गलती को देखे। साधारणत: गलती होने पर कभी कर्म पर आरोपण कर दिया जाता है तो कभी परिस्थिति पर, स्वयं को नहीं देखते। इसमें स्वयं के द्वारा स्वयं में ही निहारा जाता है। दूसरे की गलती पर ध्यान न देकर स्वयं को गलत स्वीकार कर लेना। इस स्वीकृति से अहंकार का दलन होता है और आत्मजागरण का संकल्प शुरू होता है।
प्रायश्चित्त को पश्चात्ताप नहीं कहा जाना चाहिए। पश्चाताप में आपने जो किया उसके लिए संताप व्यक्त किया जाता है, पर स्वयं को देखा नहीं जाता। पश्चात्ताप में अहंकार की तृप्ति होती है, की हुई भूल पर क्षमा-याचना की जाती है, पर प्रायश्चित्त में व्यक्ति उससे भी आगे सोचता है कि वह गलती उसी की है। इससे स्वयं के भीतर झाँकने का अवसर मिलता है, उसे क्षमा करने का भी ध्यान नहीं करना पड़ता। यहाँ तो परमात्मा भी व्यर्थ हो जाता है। इसमें तो आत्म स्वीकृति मुख्य है, दोषों से विगलित होने की प्रक्रिया है। दर्प, प्रमाद, अनाभोग, आतुर, भय आदि के कारण व्रतों की साधना में दोष आ जाते हैं। प्रायश्चित्त से इन दोषों की शुद्धि की जाती है। इनकी शुद्धि के
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org