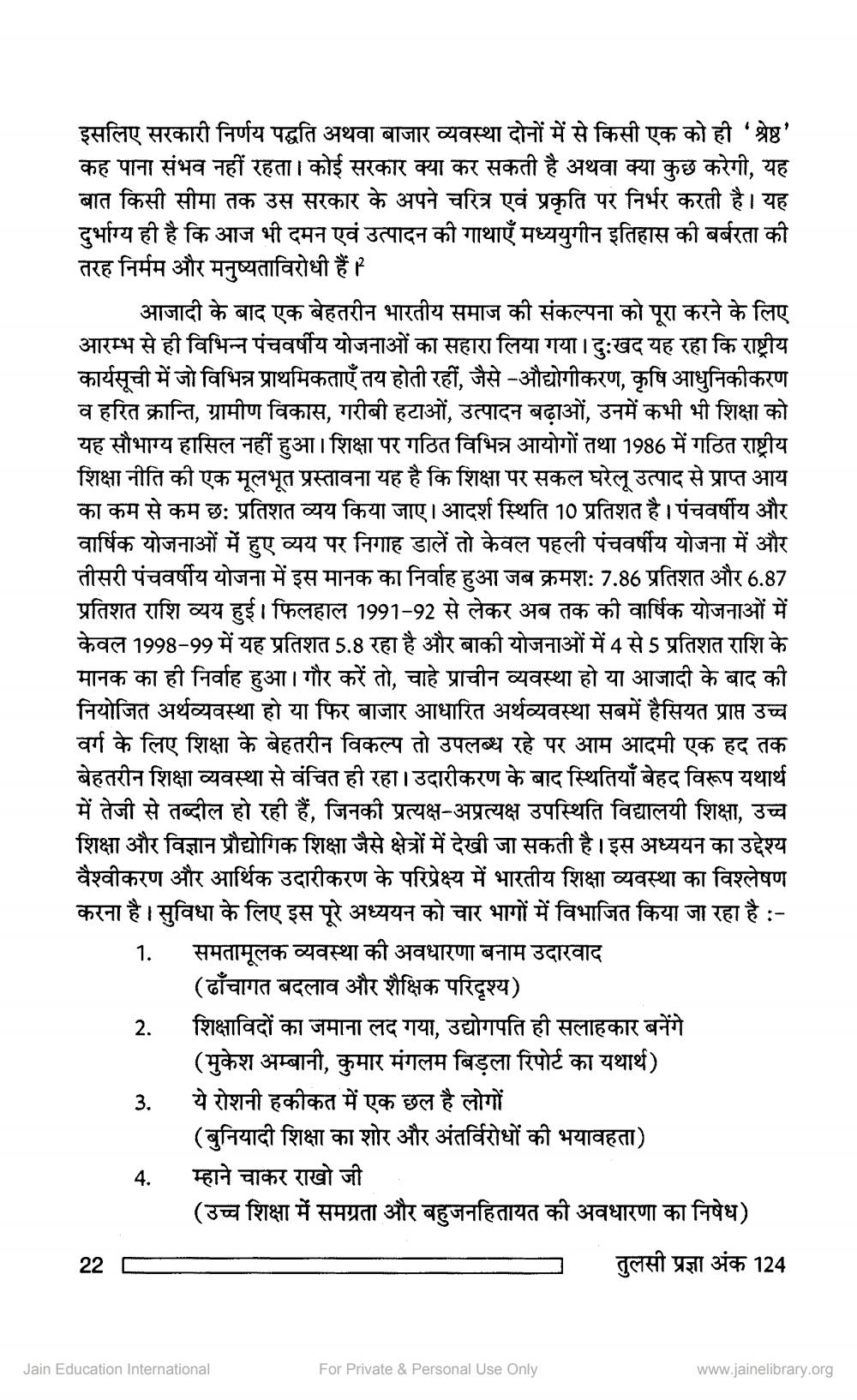________________
इसलिए सरकारी निर्णय पद्धति अथवा बाजार व्यवस्था दोनों में से किसी एक को ही 'श्रेष्ठ' कह पाना संभव नहीं रहता। कोई सरकार क्या कर सकती है अथवा क्या कुछ करेगी, यह बात किसी सीमा तक उस सरकार के अपने चरित्र एवं प्रकृति पर निर्भर करती है। यह दुर्भाग्य ही है कि आज भी दमन एवं उत्पादन की गाथाएँ मध्ययुगीन इतिहास की बर्बरता की तरह निर्मम और मनुष्यताविरोधी हैं।
आजादी के बाद एक बेहतरीन भारतीय समाज की संकल्पना को पूरा करने के लिए आरम्भ से ही विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का सहारा लिया गया। दुःखद यह रहा कि राष्ट्रीय कार्यसूची में जो विभिन्न प्राथमिकताएँ तय होती रहीं, जैसे -औद्योगीकरण, कृषि आधुनिकीकरण व हरित क्रान्ति, ग्रामीण विकास, गरीबी हटाओं, उत्पादन बढ़ाओं, उनमें कभी भी शिक्षा को यह सौभाग्य हासिल नहीं हुआ। शिक्षा पर गठित विभिन्न आयोगों तथा 1986 में गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक मूलभूत प्रस्तावना यह है कि शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद से प्राप्त आय का कम से कम छ: प्रतिशत व्यय किया जाए। आदर्श स्थिति 10 प्रतिशत है। पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाओं में हुए व्यय पर निगाह डालें तो केवल पहली पंचवर्षीय योजना में और तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस मानक का निर्वाह हुआ जब क्रमशः 7.86 प्रतिशत और 6.87 प्रतिशत राशि व्यय हुई। फिलहाल 1991-92 से लेकर अब तक की वार्षिक योजनाओं में केवल 1998-99 में यह प्रतिशत 5.8 रहा है और बाकी योजनाओं में 4 से 5 प्रतिशत राशि के मानक का ही निर्वाह हुआ। गौर करें तो, चाहे प्राचीन व्यवस्था हो या आजादी के बाद की नियोजित अर्थव्यवस्था हो या फिर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था सबमें हैसियत प्राप्त उच्च वर्ग के लिए शिक्षा के बेहतरीन विकल्प तो उपलब्ध रहे पर आम आदमी एक हद तक बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था से वंचित ही रहा। उदारीकरण के बाद स्थितियाँ बेहद विरूप यथार्थ में तेजी से तब्दील हो रही हैं, जिनकी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष उपस्थिति विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा और विज्ञान प्रौद्योगिक शिक्षा जैसे क्षेत्रों में देखी जा सकती है। इस अध्ययन का उद्देश्य वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विश्लेषण करना है। सुविधा के लिए इस पूरे अध्ययन को चार भागों में विभाजित किया जा रहा है :1. समतामूलक व्यवस्था की अवधारणा बनाम उदारवाद
(ढाँचागत बदलाव और शैक्षिक परिदृश्य) 2. शिक्षाविदों का जमाना लद गया, उद्योगपति ही सलाहकार बनेंगे
(मुकेश अम्बानी, कुमार मंगलम बिड़ला रिपोर्ट का यथार्थ) 3. ये रोशनी हकीकत में एक छल है लोगों
(बुनियादी शिक्षा का शोर और अंतर्विरोधों की भयावहता) 4. म्हाने चाकर राखो जी (उच्च शिक्षा में समग्रता और बहुजनहितायत की अवधारणा का निषेध)
- तुलसी प्रज्ञा अंक 124
22
-
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org