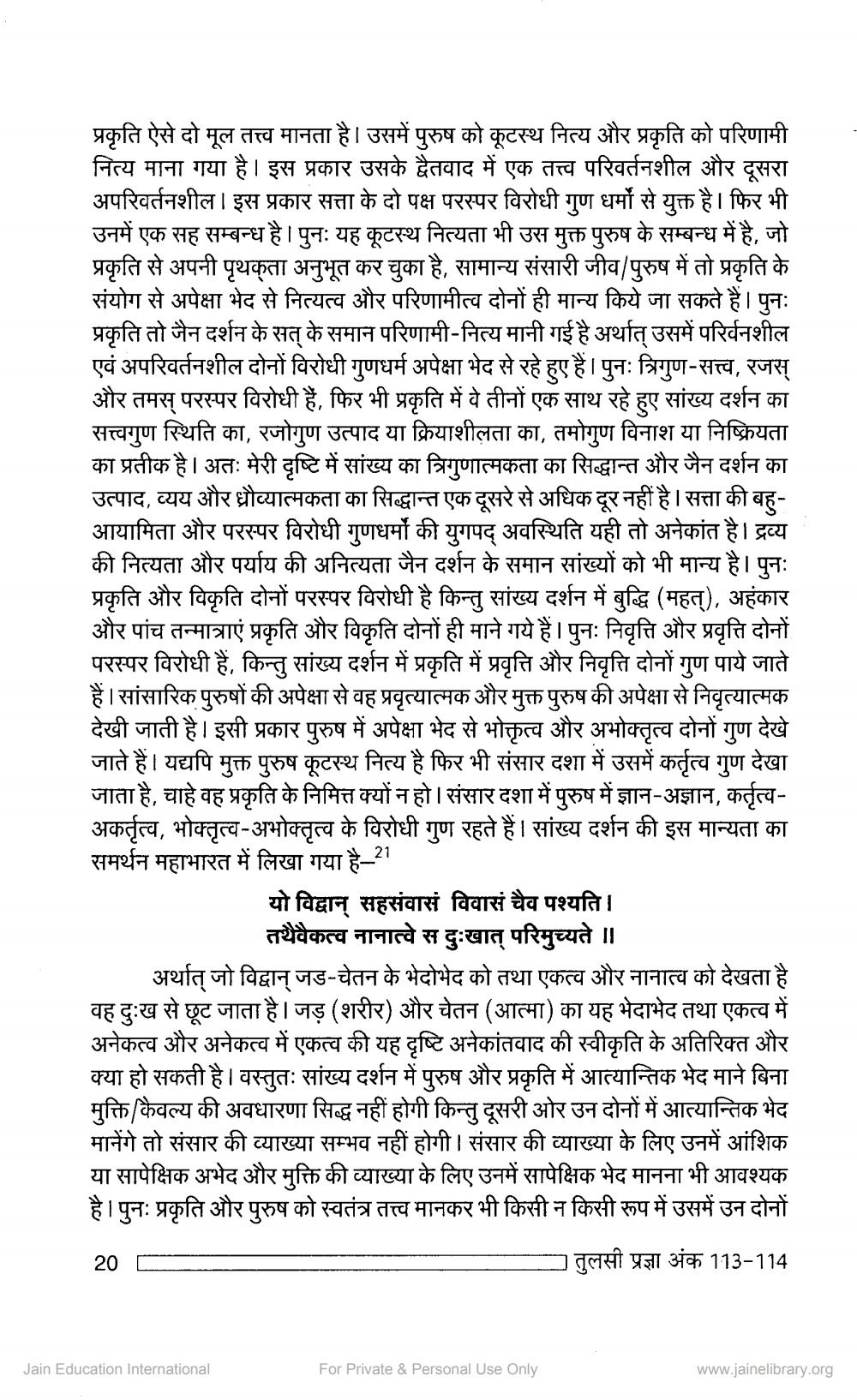________________
प्रकृति ऐसे दो मूल तत्त्व मानता है। उसमें पुरुष को कूटस्थ नित्य और प्रकृति को परिणामी नित्य माना गया है। इस प्रकार उसके द्वैतवाद में एक तत्त्व परिवर्तनशील और दूसरा अपरिवर्तनशील। इस प्रकार सत्ता के दो पक्ष परस्पर विरोधी गुण धर्मों से युक्त है। फिर भी उनमें एक सह सम्बन्ध है। पुनः यह कूटस्थ नित्यता भी उस मुक्त पुरुष के सम्बन्ध में है, जो प्रकृति से अपनी पृथक्ता अनुभूत कर चुका है, सामान्य संसारी जीव/पुरुष में तो प्रकृति के संयोग से अपेक्षा भेद से नित्यत्व और परिणामीत्व दोनों ही मान्य किये जा सकते हैं। पुनः प्रकृति तो जैन दर्शन के सत् के समान परिणामी-नित्य मानी गई है अर्थात् उसमें परिर्वनशील एवं अपरिवर्तनशील दोनों विरोधी गुणधर्म अपेक्षा भेद से रहे हुए हैं। पुनः त्रिगुण-सत्त्व, रजस् और तमस् परस्पर विरोधी हैं, फिर भी प्रकृति में वे तीनों एक साथ रहे हए सांख्य दर्शन का सत्त्वगुण स्थिति का, रजोगुण उत्पाद या क्रियाशीलता का, तमोगुण विनाश या निष्क्रियता का प्रतीक है। अतः मेरी दृष्टि में सांख्य का त्रिगुणात्मकता का सिद्धान्त और जैन दर्शन का उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यात्मकता का सिद्धान्त एक दूसरे से अधिक दूर नहीं है । सत्ता की बहुआयामिता और परस्पर विरोधी गुणधर्मों की युगपद् अवस्थिति यही तो अनेकांत है। द्रव्य की नित्यता और पर्याय की अनित्यता जैन दर्शन के समान सांख्यों को भी मान्य है। पुनः प्रकृति और विकृति दोनों परस्पर विरोधी है किन्तु सांख्य दर्शन में बुद्धि (महत्), अहंकार
और पांच तन्मात्राएं प्रकृति और विकृति दोनों ही माने गये हैं। पुनः निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों परस्पर विरोधी हैं, किन्तु सांख्य दर्शन में प्रकृति में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों गुण पाये जाते हैं। सांसारिक पुरुषों की अपेक्षा से वह प्रवृत्यात्मक और मुक्त पुरुष की अपेक्षा से निवृत्यात्मक देखी जाती है। इसी प्रकार पुरुष में अपेक्षा भेद से भोक्तृत्व और अभोक्तृत्व दोनों गुण देखे जाते हैं। यद्यपि मुक्त पुरुष कूटस्थ नित्य है फिर भी संसार दशा में उसमें कर्तृत्व गुण देखा जाता है, चाहे वह प्रकृति के निमित्त क्यों न हो । संसार दशा में पुरुष में ज्ञान-अज्ञान, कर्तृत्वअकर्तृत्व, भोक्तृत्व-अभोक्तृत्व के विरोधी गुण रहते हैं। सांख्य दर्शन की इस मान्यता का समर्थन महाभारत में लिखा गया है-21
__यो विद्वान् सहसंवासं विवासं चैव पश्यति।
तथैवैकत्व नानात्वे स दुःखात् परिमुच्यते ॥ अर्थात जो विद्वान जड-चेतन के भेदोभेद को तथा एकत्व और नानात्व को देखता है वह दुःख से छूट जाता है। जड़ (शरीर) और चेतन (आत्मा) का यह भेदाभेद तथा एकत्व में अनेकत्व और अनेकत्व में एकत्व की यह दृष्टि अनेकांतवाद की स्वीकृति के अतिरिक्त और क्या हो सकती है। वस्तुतः सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति में आत्यान्तिक भेद माने बिना मुक्ति/कैवल्य की अवधारणा सिद्ध नहीं होगी किन्तु दूसरी ओर उन दोनों में आत्यान्तिक भेद मानेंगे तो संसार की व्याख्या सम्भव नहीं होगी। संसार की व्याख्या के लिए उनमें आंशिक या सापेक्षिक अभेद और मुक्ति की व्याख्या के लिए उनमें सापेक्षिक भेद मानना भी आवश्यक है। पुनः प्रकृति और पुरुष को स्वतंत्र तत्त्व मानकर भी किसी न किसी रूप में उसमें उन दोनों
20
-
तुलसी प्रज्ञा अंक 113-114
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org