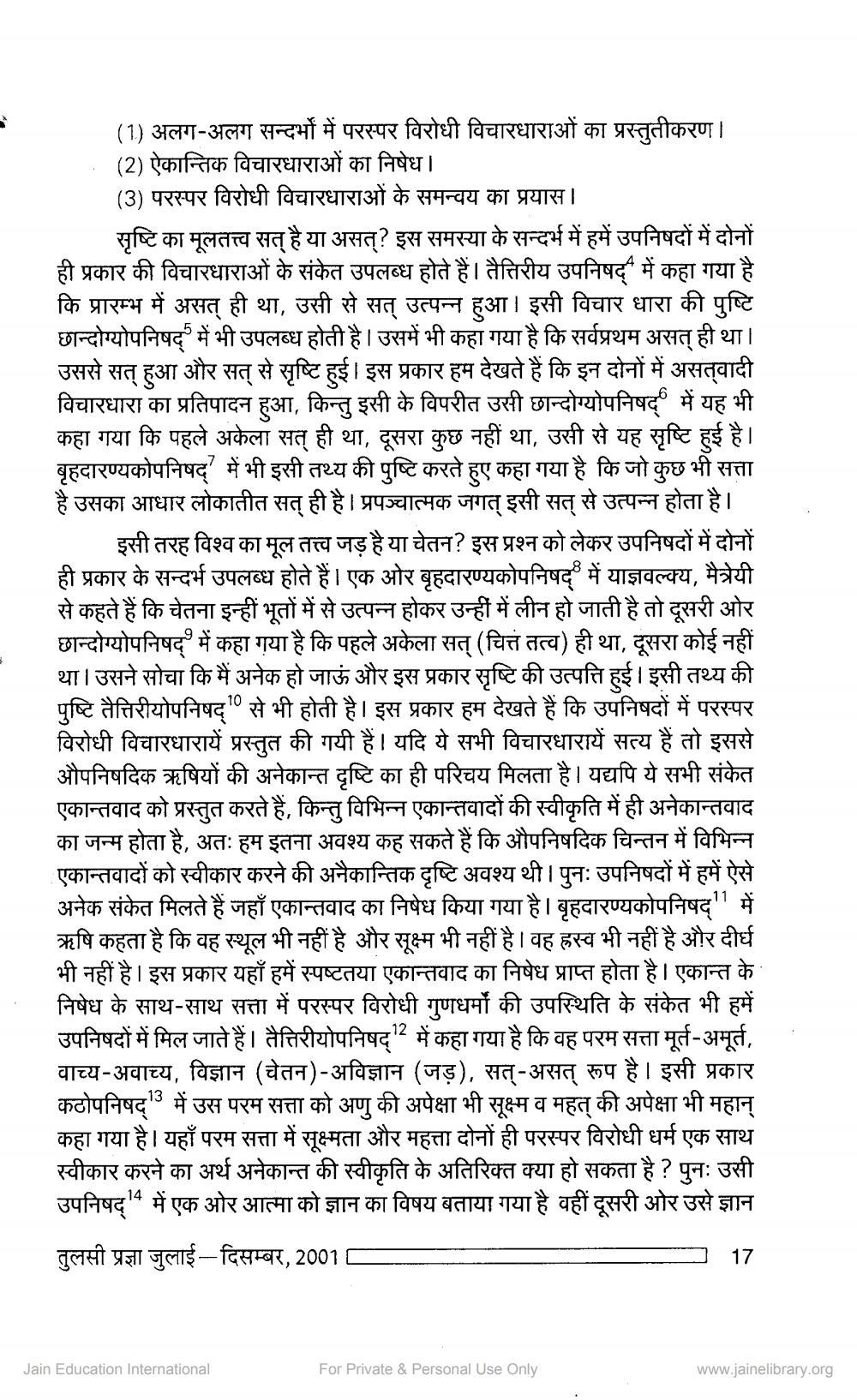________________
(1) अलग-अलग सन्दर्भों में परस्पर विरोधी विचारधाराओं का प्रस्तुतीकरण । (2) ऐकान्तिक विचारधाराओं का निषेध |
(3) परस्पर विरोधी विचारधाराओं के समन्वय का प्रयास ।
सृष्टि का मूलतत्त्व सत् है या असत् ? इस समस्या के सन्दर्भ में हमें उपनिषदों में दोनों ही प्रकार की विचारधाराओं के संकेत उपलब्ध होते हैं । तैत्तिरीय उपनिषद् में कहा गया है कि प्रारम्भ में असत् ही था, उसी से सत् उत्पन्न हुआ । इसी विचार धारा की पुष्टि छान्दोग्योपनिषद्' में भी उपलब्ध होती है। उसमें भी कहा गया है कि सर्वप्रथम असत् ही था ।
उससे सत् हुआ और सत् से सृष्टि हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों में असत्वादी
विचारधारा का प्रतिपादन हुआ, किन्तु इसी के विपरीत उसी छान्दोग्योपनिषद् में यह भी कहा गया कि पहले अकेला सत् ही था, दूसरा कुछ नहीं था, उसी से यह सृष्टि हुई है। बृहदारण्यकोपनिषद्' में भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा गया है कि जो कुछ भी सत्ता है उसका आधार लोकातीत सत् ही है। प्रपञ्चात्मक जगत् इसी सत् से उत्पन्न होता है ।
इसी तरह विश्व का मूल तत्त्व जड़ है या चेतन ? इस प्रश्न को लेकर उपनिषदों में दोनों ही प्रकार के सन्दर्भ उपलब्ध होते हैं। एक ओर बृहदारण्यकोपनिषद् में याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी से कहते हैं कि चेतना इन्हीं भूतों में से उत्पन्न होकर उन्हीं में लीन हो जाती है तो दूसरी ओर छान्दोग्योपनिषद्' में कहा गया है कि पहले अकेला सत् (चित्तं तत्व) ही था, दूसरा कोई नहीं था। उसने सोचा कि मैं अनेक हो जाऊं और इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इसी तथ्य की पुष्टि तैत्तिरीयोपनिषद् " से भी होती है । इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिषदों में परस्पर विरोधी विचारधारायें प्रस्तुत की गयी हैं । यदि ये सभी विचारधारायें सत्य हैं तो इससे औपनिषदिक ऋषियों की अनेकान्त दृष्टि का ही परिचय मिलता है। यद्यपि ये सभी संकेत एकान्तवाद को प्रस्तुत करते हैं, किन्तु विभिन्न एकान्तवादों की स्वीकृति में ही अनेकान्तवाद का जन्म होता है, अतः हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि औपनिषदिक चिन्तन में विभिन्न एकान्तवादों को स्वीकार करने की अनैकान्तिक दृष्टि अवश्य थी । पुनः उपनिषदों में हमें ऐसे अनेक संकेत मिलते हैं जहाँ एकान्तवाद का निषेध किया गया है। बृहदारण्यकोपनिषद् " में ऋषि कहता है कि वह स्थूल भी नहीं है और सूक्ष्म भी नहीं है। वह ह्रस्व भी नहीं है और दीर्घ भी नहीं है । इस प्रकार यहाँ हमें स्पष्टतया एकान्तवाद का निषेध प्राप्त होता है। एकान्त के निषेध के साथ-साथ सत्ता में परस्पर विरोधी गुणधर्मों की उपस्थिति के संकेत भी हमें उपनिषदों में मिल जाते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद् 2 में कहा गया है कि वह परम सत्ता मूर्त-अमूर्त, वाच्य-अवाच्य, विज्ञान (चेतन) - अविज्ञान (जड़), सत्-असत् रूप है। इसी प्रकार कठोपनिषद्'3 में उस परम सत्ता को अणु की अपेक्षा भी सूक्ष्म व महत् की अपेक्षा भी महान् कहा गया है। यहाँ परम सत्ता में सूक्ष्मता और महत्ता दोनों ही परस्पर विरोधी धर्म एक साथ स्वीकार करने का अर्थ अनेकान्त की स्वीकृति के अतिरिक्त क्या हो सकता है ? पुनः उसी उपनिषद् 14 में एक ओर आत्मा को ज्ञान का विषय बताया गया है वहीं दूसरी ओर उसे ज्ञान
तुलसी प्रज्ञा जुलाई - दिसम्बर, 2001
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
17
www.jainelibrary.org