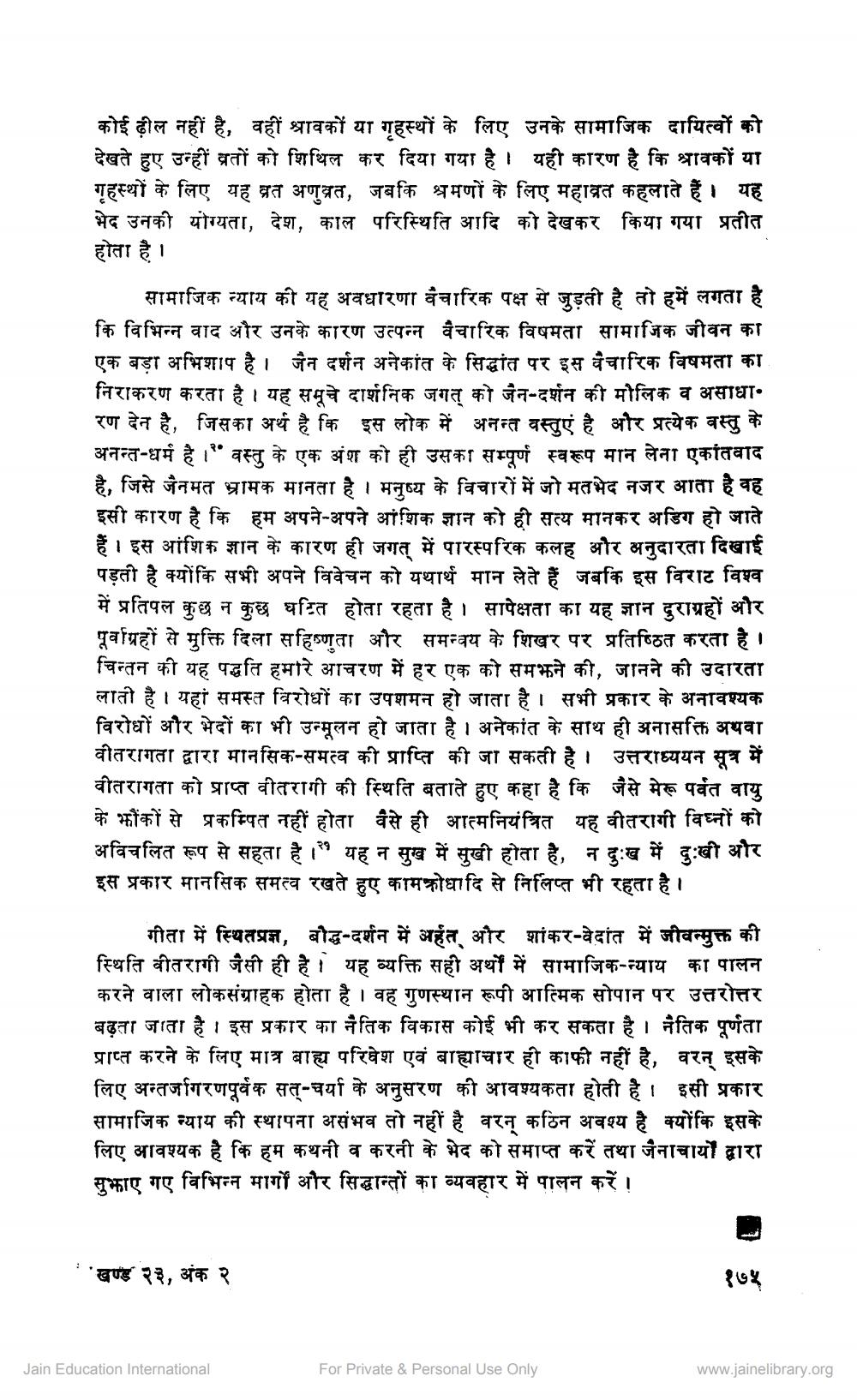________________
कोई ढील नहीं है, वहीं श्रावकों या गृहस्थों के लिए उनके सामाजिक दायित्वों को देखते हुए उन्हीं व्रतों को शिथिल कर दिया गया है। यही कारण है कि श्रावकों या गृहस्थों के लिए यह व्रत अणुव्रत, जबकि श्रमणों के लिए महाव्रत कहलाते हैं। यह भेद उनकी योग्यता, देश, काल परिस्थिति आदि को देखकर किया गया प्रतीत होता है।
सामाजिक न्याय की यह अवधारणा वैचारिक पक्ष से जुड़ती है तो हमें लगता है कि विभिन्न वाद और उनके कारण उत्पन्न वैचारिक विषमता सामाजिक जीवन का एक बड़ा अभिशाप है। जैन दर्शन अनेकांत के सिद्धांत पर इस वैचारिक विषमता का निराकरण करता है । यह समूचे दार्शनिक जगत् को जैन-दर्शन की मौलिक व असाधा. रण देन है, जिसका अर्थ है कि इस लोक में अनन्त वस्तुएं है और प्रत्येक वस्तु के अनन्त-धर्म है।" वस्तु के एक अंश को ही उसका सम्पूर्ण स्वरूप मान लेना एकांतवाद है, जिसे जनमत भ्रामक मानता है । मनुष्य के विचारों में जो मतभेद नजर आता है वह इसी कारण है कि हम अपने-अपने आंशिक ज्ञान को ही सत्य मानकर अडिग हो जाते हैं । इस आंशिक ज्ञान के कारण ही जगत् में पारस्परिक कलह और अनुदारता दिखाई पड़ती है क्योंकि सभी अपने विवेचन को यथार्थ मान लेते हैं जबकि इस विराट विश्व में प्रतिपल कुछ न कुछ घटित होता रहता है। सापेक्षता का यह ज्ञान दुराग्रहों और पूर्वाग्रहों से मुक्ति दिला सहिष्णुता और समन्वय के शिखर पर प्रतिष्ठित करता है । चिन्तन की यह पद्धति हमारे आचरण में हर एक को समझने की, जानने की उदारता लाती है। यहां समस्त विरोधों का उपशमन हो जाता है। सभी प्रकार के अनावश्यक विरोधों और भेदों का भी उन्मूलन हो जाता है । अनेकांत के साथ ही अनासक्ति अथवा वीतरागता द्वारा मानसिक-समत्व की प्राप्ति की जा सकती है। उत्तराध्ययन सूत्र में वीतरागता को प्राप्त वीतरागी की स्थिति बताते हुए कहा है कि जैसे मेरू पर्वत वायु के झौंकों से प्रकम्पित नहीं होता वैसे ही आत्मनियंत्रित यह वीतरागी विघ्नों को अविचलित रूप से सहता है । यह न सुख में सुखी होता है, न दुःख में दुःखी और इस प्रकार मानसिक समत्व रखते हुए कामक्रोधादि से निलिप्त भी रहता है।
गीता में स्थितप्रज, बौद्ध-दर्शन में अर्हत और शांकर-वेदांत में जीवन्मुक्त की स्थिति वीतरागी जैसी ही है। यह व्यक्ति सही अर्थों में सामाजिक-न्याय का पालन करने वाला लोकसंग्राहक होता है । वह गुणस्थान रूपी आत्मिक सोपान पर उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है । इस प्रकार का नैतिक विकास कोई भी कर सकता है। नैतिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए मात्र बाह्य परिवेश एवं बाह्याचार ही काफी नहीं है, वरन् इसके लिए अन्तर्जागरणपूर्वक सत्-चर्या के अनुसरण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सामाजिक न्याय की स्थापना असंभव तो नहीं है वरन् कठिन अवश्य है क्योंकि इसके लिए आवश्यक है कि हम कथनी व करनी के भेद को समाप्त करें तथा जैनाचार्यों द्वारा सुझाए गए विभिन्न मार्गों और सिद्धान्तों का व्यवहार में पालन करें।
• खण्ड २३, अंक २
१७५
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org