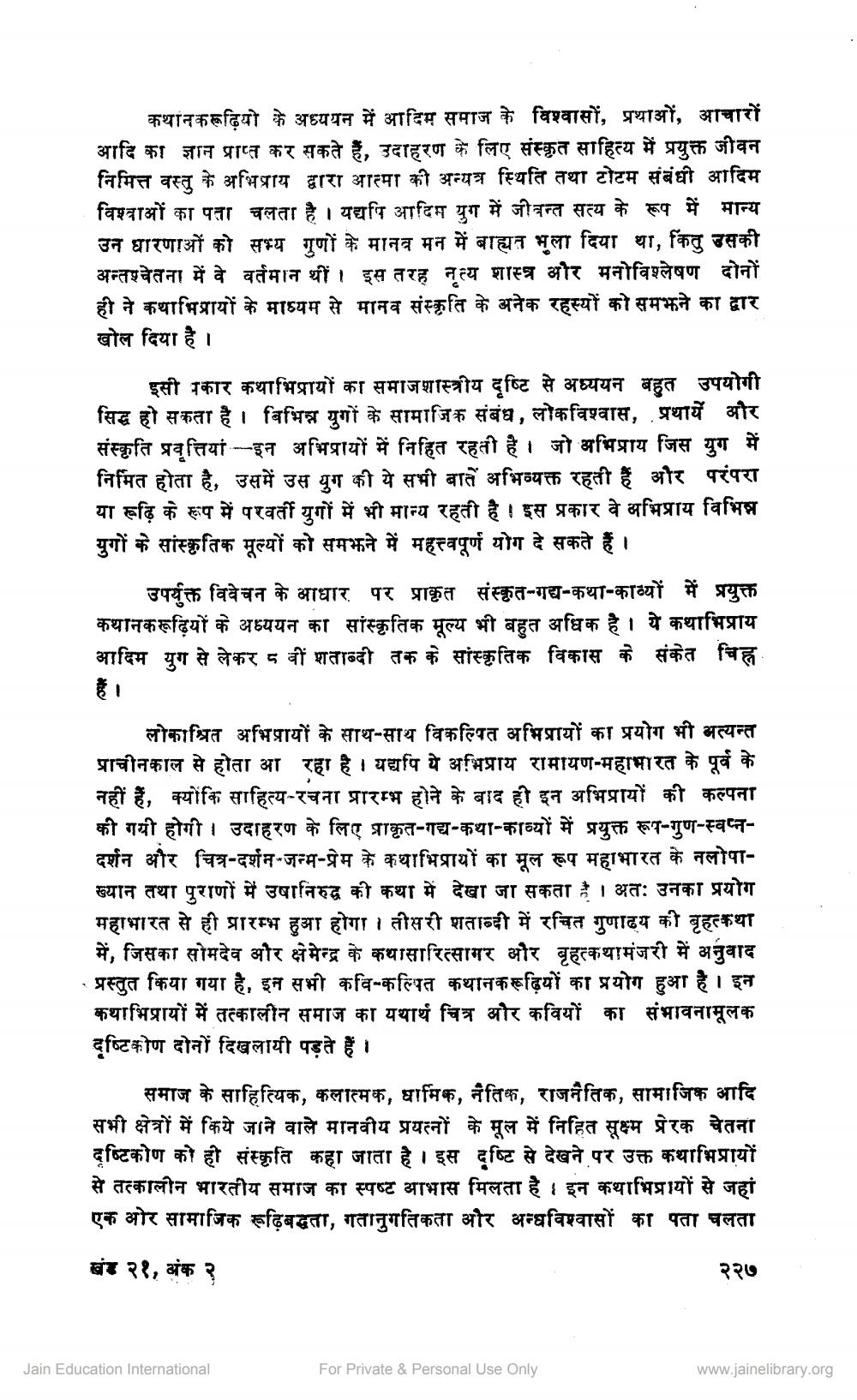________________
कथानकरूढ़ियो के अध्ययन में आदिम समाज के विश्वासों, प्रथाओं, आचारों आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उदाहरण के लिए संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त जीवन निमित्त वस्तु के अभिप्राय द्वारा आत्मा की अन्यत्र स्थिति तथा टोटम संबंधी आदिम विश्वाओं का पता चलता है। यद्यपि आदिम युग में जीवन्त सत्य के रूप में मान्य उन धारणाओं को सभ्य गुणों के मानव मन में बाह्यत भुला दिया था, किंतु उसकी अन्तश्चेतना में वे वर्तमान थीं। इस तरह नृत्य शास्त्र और मनोविश्लेषण दोनों ही ने कथाभिप्रायों के माध्यम से मानव संस्कृति के अनेक रहस्यों को समझने का द्वार खोल दिया है।
इसी प्रकार कथाभिप्रायों का समाजशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है । बिभिन्न युगों के सामाजिक संबंध , लोकविश्वास, प्रथायें और संस्कृति प्रवृत्तियां ---इन अभिप्रायों में निहित रहती है। जो अभिप्राय जिस युग में निर्मित होता है, उसमें उस युग की ये सभी बातें अभिव्यक्त रहती हैं और परंपरा या रूढ़ि के रूप में परवर्ती युगों में भी मान्य रहती है । इस प्रकार वे अभिप्राय विभिन्न युगों के सांस्कृतिक मूल्यों को समझने में महत्त्वपूर्ण योग दे सकते हैं।
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्राकृत संस्कृत-गद्य-कथा-काव्यों में प्रयुक्त कथानकरूढ़ियों के अध्ययन का सांस्कृतिक मूल्य भी बहुत अधिक है। ये कथाभिप्राय आदिम युग से लेकर ८ वीं शताब्दी तक के सांस्कृतिक विकास के संकेत चिह्न
लोकाश्रित अभिप्रायों के साथ-साथ विकल्पित अभिप्रायों का प्रयोग भी अत्यन्त प्राचीनकाल से होता आ रहा है । यद्यपि ये अभिप्राय रामायण-महाभारत के पूर्व के नहीं हैं, क्योंकि साहित्य-रचना प्रारम्भ होने के बाद ही इन अभिप्रायों की कल्पना की गयी होगी। उदाहरण के लिए प्राकृत-गद्य-कथा-काव्यों में प्रयुक्त रूप-गुण-स्वप्नदर्शन और चित्र-दर्शन-जन्म-प्रेम के कथाभिप्रायों का मूल रूप महाभारत के नलोपाख्यान तथा पुराणों में उषानिरुद्ध की कथा में देखा जा सकता है । अतः उनका प्रयोग महाभारत से ही प्रारम्भ हुआ होगा। तीसरी शताब्दी में रचित गुणाढ्य की बृहत्कथा में, जिसका सोमदेव और क्षेमेन्द्र के कथासारित्सागर और बृहत्कथामंजरी में अनुवाद • प्रस्तुत किया गया है, इन सभी कवि-कल्पित कथानकरूढ़ियों का प्रयोग हुआ है । इन कथाभिप्रायों में तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र और कवियों का संभावनामूलक दृष्टिकोण दोनों दिखलायी पड़ते हैं।
समाज के साहित्यिक, कलात्मक, धार्मिक, नैतिक, राजनैतिक, सामाजिक आदि सभी क्षेत्रों में किये जाने वाले मानवीय प्रयत्नों के मूल में निहित सूक्ष्म प्रेरक चेतना दृष्टिकोण को ही संस्कृति कहा जाता है । इस दृष्टि से देखने पर उक्त कथाभिप्रायों से तत्कालीन भारतीय समाज का स्पष्ट आभास मिलता है । इन कथाभिप्रायों से जहां एक ओर सामाजिक रूढिबद्धता, गतानुगतिकता और अन्धविश्वासों का पता चलता बंर २१, अंक २
२२७
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org