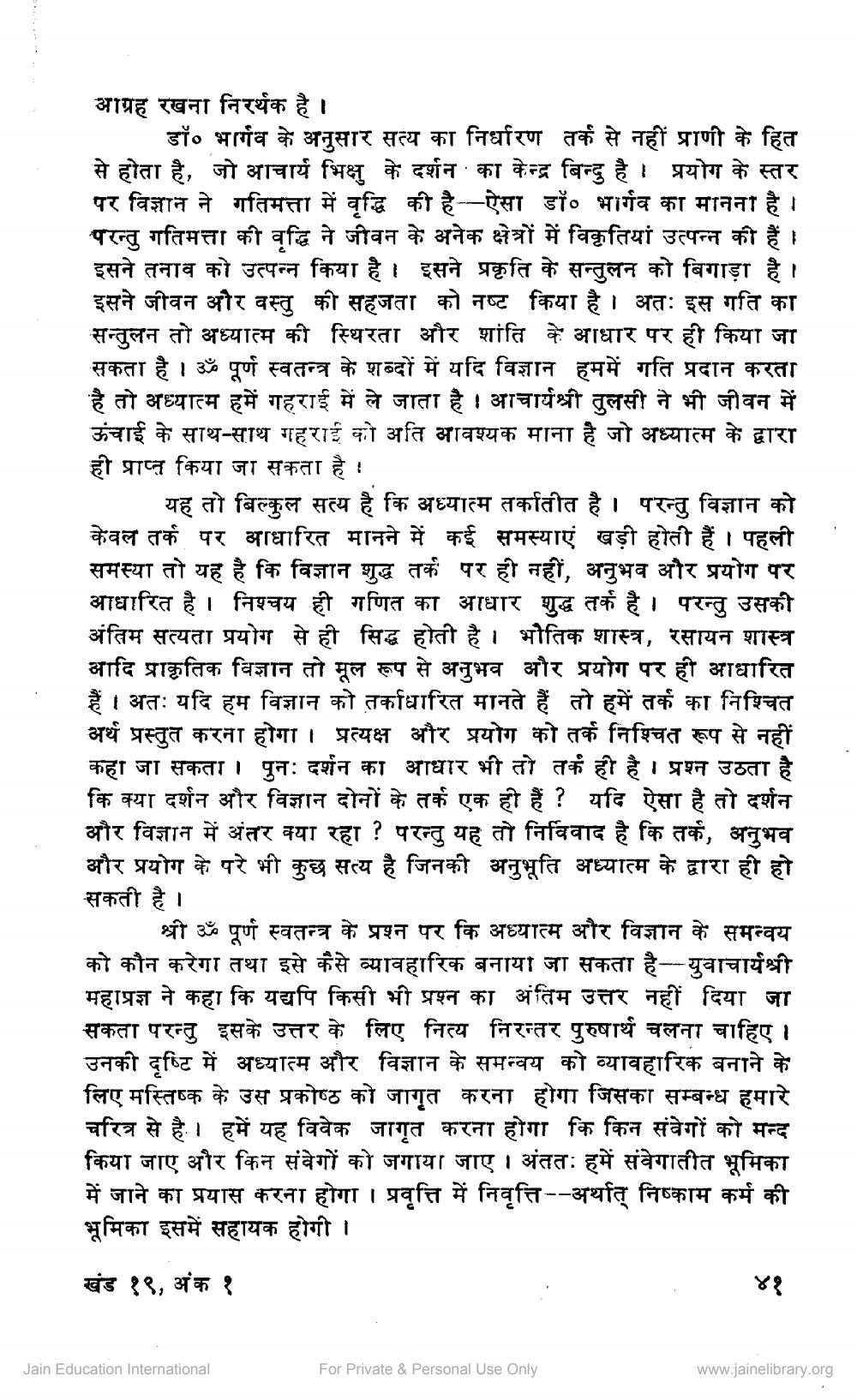________________
आग्रह रखना निरर्थक है।
___डॉ० भार्गव के अनुसार सत्य का निर्धारण तर्क से नहीं प्राणी के हित से होता है, जो आचार्य भिक्षु के दर्शन · का केन्द्र बिन्दु है। प्रयोग के स्तर पर विज्ञान ने गतिमत्ता में वृद्धि की है-ऐसा डॉ० भार्गव का मानना है। परन्तु गतिमत्ता की वृद्धि ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में विकृतियां उत्पन्न की हैं। इसने तनाव को उत्पन्न किया है। इसने प्रकृति के सन्तुलन को बिगाड़ा है। इसने जीवन और वस्तु की सहजता को नष्ट किया है। अतः इस गति का सन्तुलन तो अध्यात्म की स्थिरता और शांति के आधार पर ही किया जा सकता है । ॐ पूर्ण स्वतन्त्र के शब्दों में यदि विज्ञान हममें गति प्रदान करता है तो अध्यात्म हमें गहराई में ले जाता है । आचार्यश्री तुलसी ने भी जीवन में ऊंचाई के साथ-साथ गहराई को अति आवश्यक माना है जो अध्यात्म के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है ।
यह तो बिल्कुल सत्य है कि अध्यात्म तर्कातीत है। परन्तु विज्ञान को केवल तर्क पर आधारित मानने में कई समस्याएं खड़ी होती हैं। पहली समस्या तो यह है कि विज्ञान शुद्ध तर्क पर ही नहीं, अनुभव और प्रयोग पर आधारित है। निश्चय ही गणित का आधार शुद्ध तर्क है। परन्तु उसकी अंतिम सत्यता प्रयोग से ही सिद्ध होती है। भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि प्राकृतिक विज्ञान तो मूल रूप से अनुभव और प्रयोग पर ही आधारित हैं । अतः यदि हम विज्ञान को तर्काधारित मानते हैं तो हमें तर्क का निश्चित अर्थ प्रस्तुत करना होगा। प्रत्यक्ष और प्रयोग को तर्क निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। पुनः दर्शन का आधार भी तो तक ही है। प्रश्न उठता है कि क्या दर्शन और विज्ञान दोनों के तर्क एक ही हैं ? यदि ऐसा है तो दर्शन और विज्ञान में अंतर क्या रहा ? परन्तु यह तो निर्विवाद है कि तर्क, अनुभव और प्रयोग के परे भी कुछ सत्य है जिनकी अनुभूति अध्यात्म के द्वारा ही हो सकती है।
श्री ॐ पूर्ण स्वतन्त्र के प्रश्न पर कि अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय को कौन करेगा तथा इसे कैसे व्यावहारिक बनाया जा सकता है-युवाचार्यश्री महाप्रज्ञ ने कहा कि यद्यपि किसी भी प्रश्न का अंतिम उत्तर नहीं दिया जा सकता परन्तु इसके उत्तर के लिए नित्य निरन्तर पुरुषार्थ चलना चाहिए । उनकी दृष्टि में अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय को व्यावहारिक बनाने के लिए मस्तिष्क के उस प्रकोष्ठ को जागृत करना होगा जिसका सम्बन्ध हमारे चरित्र से है। हमें यह विवेक जागृत करना होगा कि किन संवेगों को मन्द किया जाए और किन संवेगों को जगाया जाए। अंततः हमें संवेगातीत भूमिका में जाने का प्रयास करना होगा । प्रवृत्ति में निवृत्ति--अर्थात् निष्काम कर्म की भूमिका इसमें सहायक होगी।
खंड १९, अंक १
४१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org