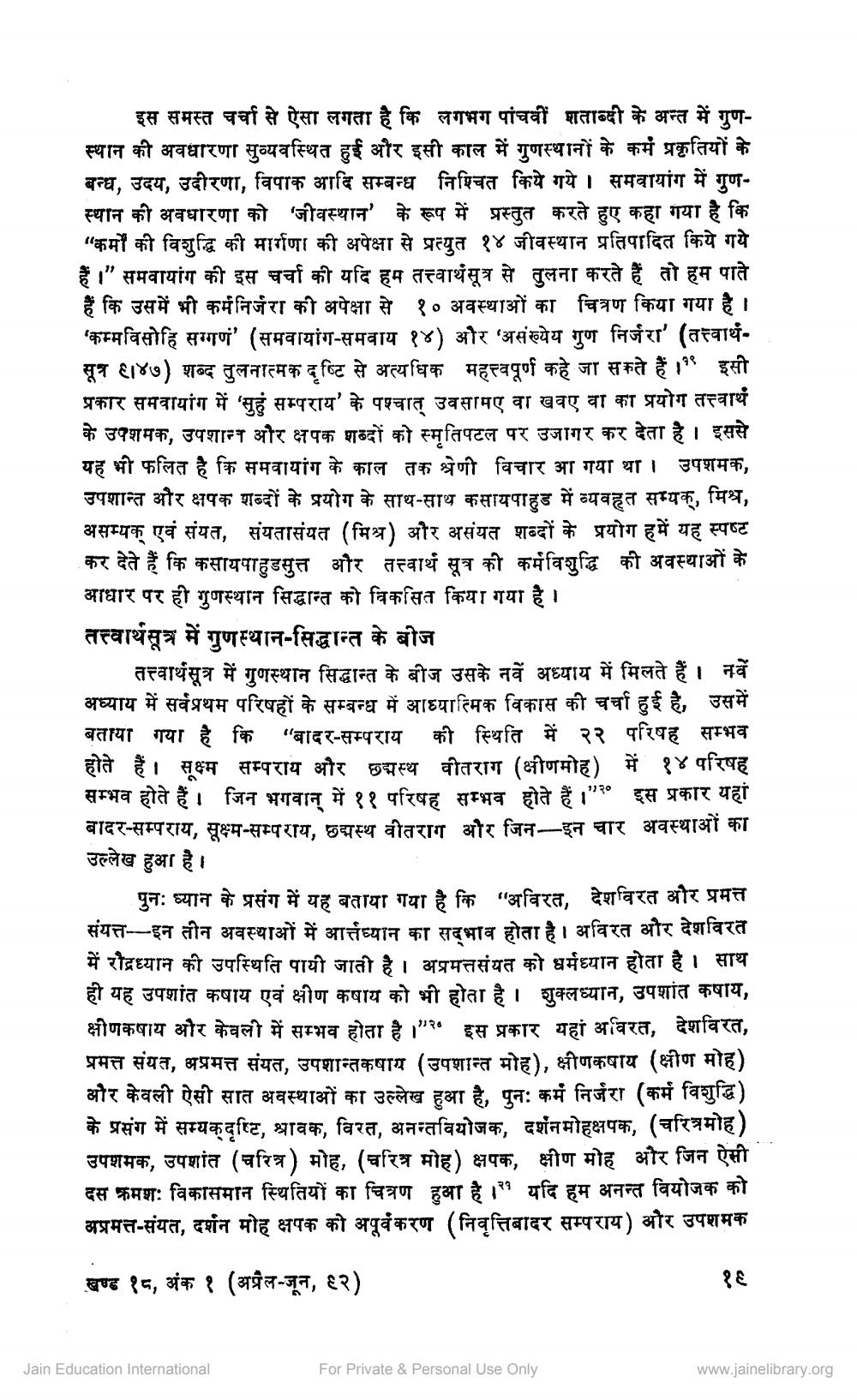________________
इस समस्त चर्चा से ऐसा लगता है कि लगभग पांचवीं शताब्दी के अन्त में गुणस्थान की अवधारणा सुव्यवस्थित हुई और इसी काल में गुणस्थानों के कर्म प्रकृतियों के बन्ध, उदय, उदीरणा, विपाक आदि सम्बन्ध निश्चित किये गये । समवायांग में गुणस्थान की अवधारणा को 'जीवस्थान' के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि "कर्मों की विशुद्धि की मार्गणा की अपेक्षा से प्रत्युत १४ जीवस्थान प्रतिपादित किये गये हैं।" समवायांग की इस चर्चा की यदि हम तत्त्वार्थसूत्र से तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें भी कर्म निर्जरा की अपेक्षा से १० अवस्थाओं का चित्रण किया गया है । 'कम्मविसोहि सग्गणं' (समवायांग-समवाय १४) और 'असंख्येय गुण निर्जरा' (तत्त्वार्थसूत्र ६४७) शब्द तुलनात्मक दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कहे जा सकते हैं ।१९ इसी प्रकार समवायांग में 'सुहं सम्पराय' के पश्चात् उवसामए वा खवए वा का प्रयोग तत्त्वार्थ के उपशमक, उपशान और क्षपक शब्दों को स्मृतिपटल पर उजागर कर देता है। इससे यह भी फलित है कि समवायांग के काल तक श्रेणी विचार आ गया था। उपशमक, उपशान्त और क्षपक शब्दों के प्रयोग के साथ-साथ कसायपाहुड में व्यवहृत सम्यक्, मिश्र, असम्यक एवं संयत, संयतासंयत (मिश्र) और असंयत शब्दों के प्रयोग हमें यह स्पष्ट कर देते हैं कि कसायपाहुडसुत्त और तत्त्वार्थ सूत्र की कर्मविशुद्धि की अवस्थाओं के आधार पर ही गुणस्थान सिद्धान्त को विकसित किया गया है । तत्त्वार्थसूत्र में गुणस्थान-सिद्धान्त के बीज
तत्त्वार्थसूत्र में गुणस्थान सिद्धान्त के बीज उसके नवें अध्याय में मिलते हैं। नवें अध्याय में सर्वप्रथम परिषहों के सम्बन्ध में आध्यात्मिक विकास की चर्चा हुई है, उसमें बताया गया है कि "बादर-सम्पराय की स्थिति में २२ परिषह सम्भव होते हैं। सूक्ष्म सम्पराय और छद्मस्थ वीतराग (क्षीणमोह) में १४ परिषह सम्भव होते हैं। जिन भगवान् में ११ परिषह सम्भव होते हैं ।"२० इस प्रकार यहां बादर-सम्पराय, सूक्ष्म-सम्पराय, छद्मस्थ वीतराग और जिन-इन चार अवस्थाओं का उल्लेख हुआ है।
___पुन: ध्यान के प्रसंग में यह बताया गया है कि "अविरत, देशविरत और प्रमत्त संयत्त-इन तीन अवस्थाओं में आर्तध्यान का सदभाव होता है। अविरत और देशविरत में रोद्रध्यान की उपस्थिति पायी जाती है। अप्रमत्तसंयत को धर्मध्यान होता है। साथ ही यह उपशांत कषाय एवं क्षीण कषाय को भी होता है। शुक्लध्यान, उपशांत कषाय, क्षीणकषाय और केवली में सम्भव होता है ।"२० इस प्रकार यहां अविरत, देशविरत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, उपशान्तकषाय (उपशान्त मोह), क्षीणकषाय (क्षीण मोह) और केवली ऐसी सात अवस्थाओं का उल्लेख हुआ है, पुनः कर्म निर्जरा (कर्म विशुद्धि) के प्रसंग में सम्यक्दृष्टि, श्रावक, विरत, अनन्तवियोजक, दर्शनमोहक्षपक, (चरित्रमोह) उपशमक, उपशांत (चरित्र) मोह, (चरित्र मोह) क्षपक, क्षीण मोह और जिन ऐसी दस क्रमशः विकासमान स्थितियों का चित्रण हुआ है ।२१ यदि हम अनन्त वियोजक को अप्रमत्त-संयत, दर्शन मोह क्षपक को अपूर्वकरण (निवृत्तिबादर सम्पराय) और उपशमक
खण्ड १८, अंक १ (अप्रैल-जून, १२)
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org