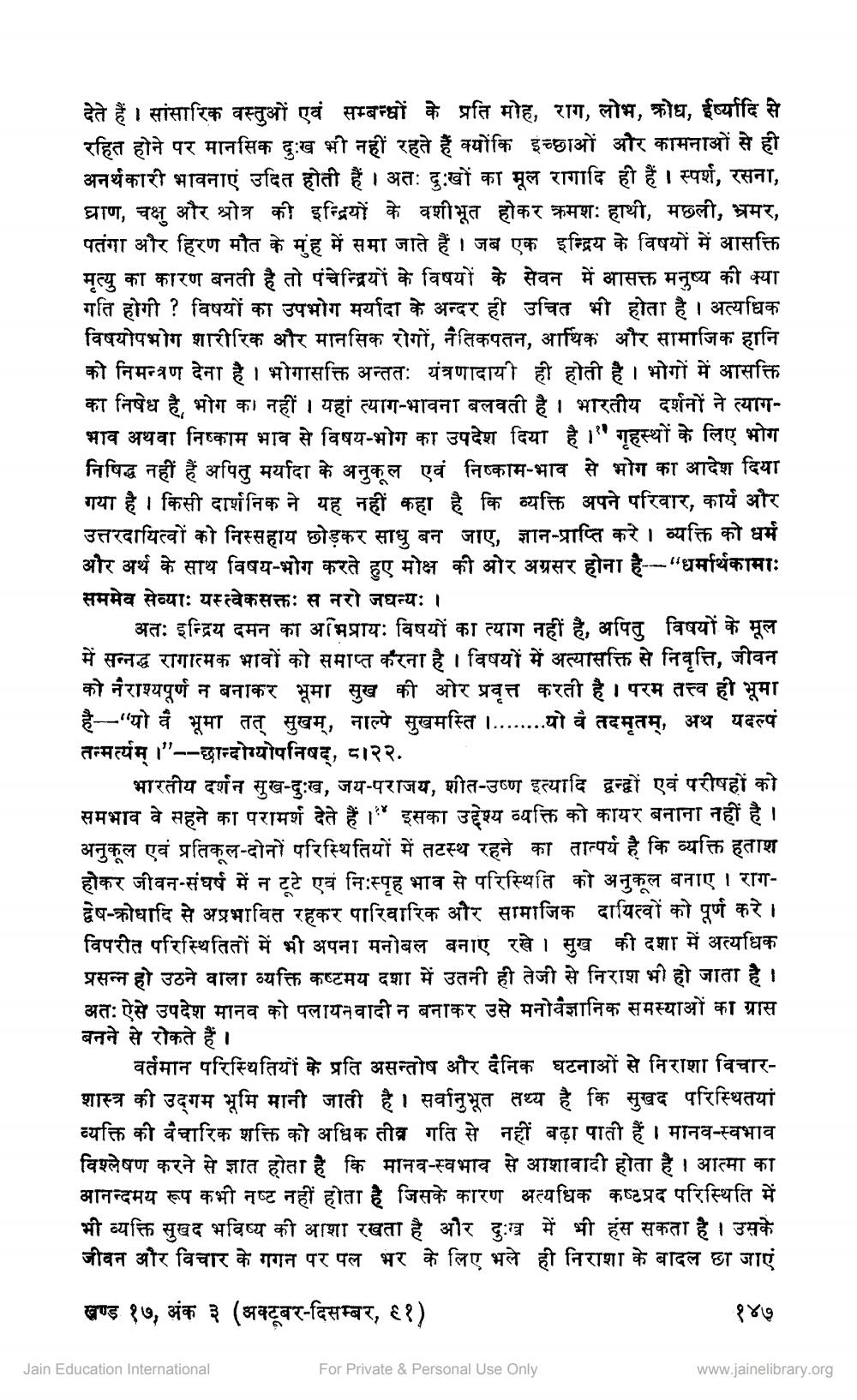________________
देते हैं । सांसारिक वस्तुओं एवं सम्बन्धों के प्रति मोह, राग, लोभ, क्रोध, ईर्ष्यादि से रहित होने पर मानसिक दुःख भी नहीं रहते हैं क्योंकि इच्छाओं और कामनाओं से ही अनर्थकारी भावनाएं उदित होती हैं । अतः दु:खों का मूल रागादि ही हैं । स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र की इन्द्रियों के वशीभूत होकर क्रमशः हाथी, मछली, भ्रमर, पतंगा और हिरण मौत के मुंह में समा जाते हैं। जब एक इन्द्रिय के विषयों में आसक्ति मृत्यु का कारण बनती है तो पंचेन्द्रियों के विषयों के सेवन में आसक्त मनुष्य की क्या गति होगी ? विषयों का उपभोग मर्यादा के अन्दर ही उचित भी होता है । अत्यधिक विषयोपभोग शारीरिक और मानसिक रोगों, नैतिकपतन, आर्थिक और सामाजिक हानि को निमन्त्रण देना है। भोगासक्ति अन्ततः यंत्रणादायी ही होती है । भोगों में आसक्ति का निषेध है, भोग का नहीं । यहां त्याग-भावना बलवती है। भारतीय दर्शनों ने त्यागभाव अथवा निष्काम भाव से विषय-भोग का उपदेश दिया है।" गृहस्थों के लिए भोग निषिद्ध नहीं हैं अपितु मर्यादा के अनुकूल एवं निष्काम-भाव से भोग का आदेश दिया गया है । किसी दार्शनिक ने यह नहीं कहा है कि व्यक्ति अपने परिवार, कार्य और उत्तरदायित्वों को निस्सहाय छोड़कर साधु बन जाए, ज्ञान-प्राप्ति करे। व्यक्ति को धर्म और अर्थ के साथ विषय-भोग करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होना है.---"धर्मार्थकामाः सममेव सेव्याः यस्त्वेकसक्तः स नरो जघन्यः ।
अतः इन्द्रिय दमन का अभिप्रायः विषयों का त्याग नहीं है, अपितु विषयों के मूल में सन्नद्ध रागात्मक भावों को समाप्त करना है । विषयों में अत्यासक्ति से निवृत्ति, जीवन को नैराश्यपूर्ण न बनाकर भूमा सुख की ओर प्रवृत्त करती है । परम तत्त्व ही भूमा है-“यो वै भूमा तत् सुखम्, नाल्पे सुखमस्ति ।........यो वै तदमृतम्, अथ यदल्पं तन्मय॑म् ।"--छान्दोग्योपनिषद्, ८।२२.
___ भारतीय दर्शन सुख-दुःख, जय-पराजय, शीत-उष्ण इत्यादि द्वन्द्वों एवं परीषहों को समभाव वे सहने का परामर्श देते हैं। इसका उद्देश्य व्यक्ति को कायर बनाना नहीं है । अनुकूल एवं प्रतिकूल-दोनों परिस्थितियों में तटस्थ रहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति हताश होकर जीवन-संघर्ष में न टूटे एवं निःस्पृह भाव से परिस्थिति को अनुकूल बनाए । रागद्वेष-क्रोधादि से अप्रभावित रहकर पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करे। विपरीत परिस्थितितों में भी अपना मनोबल बनाए रखे। सुख की दशा में अत्यधिक प्रसन्न हो उठने वाला व्यक्ति कष्टमय दशा में उतनी ही तेजी से निराश भी हो जाता है। अतः ऐसे उपदेश मानव को पलायनवादी न बनाकर उसे मनोवैज्ञानिक समस्याओं का ग्रास बनने से रोकते हैं।
वर्तमान परिस्थितियों के प्रति असन्तोष और दैनिक घटनाओं से निराशा विचारशास्त्र की उद्गम भूमि मानी जाती है। सर्वानुभूत तथ्य है कि सुखद परिस्थितयां व्यक्ति की वैचारिक शक्ति को अधिक तीव्र गति से नहीं बढ़ा पाती हैं । मानव-स्वभाव विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि मानव-स्वभाव से आशावादी होता है । आत्मा का आनन्दमय रूप कभी नष्ट नहीं होता है जिसके कारण अत्यधिक कष्टप्रद परिस्थिति में भी व्यक्ति सुखद भविष्य की आशा रखता है और दुःख में भी हंस सकता है। उसके जीवन और विचार के गगन पर पल भर के लिए भले ही निराशा के बादल छा जाएं
खण्ड १७, अंक ३ (अक्टूबर-दिसम्बर, ६१)
१४७
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org