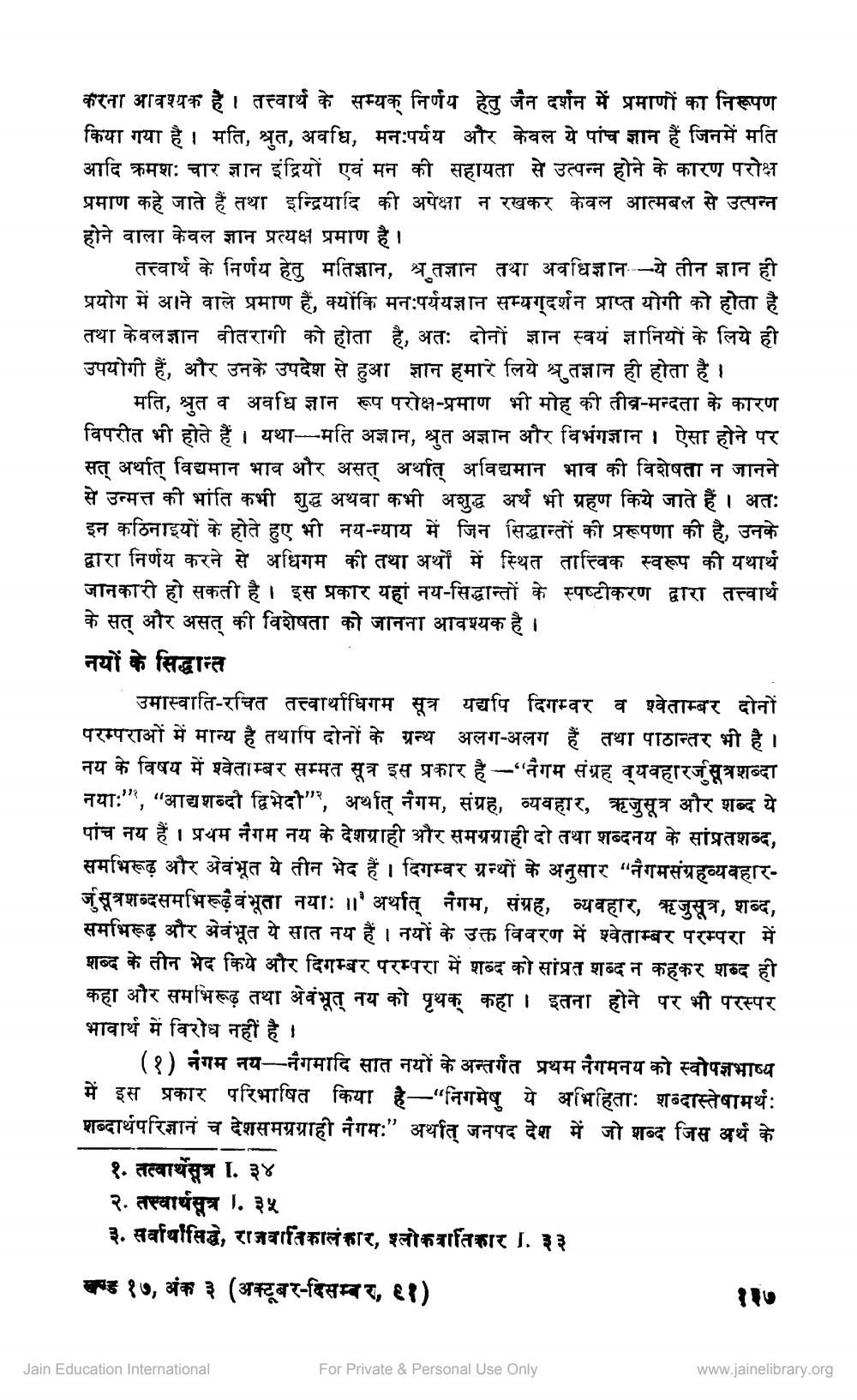________________
करना आवश्यक है । तत्त्वार्थ के सम्यक् निर्णय हेतु जैन दर्शन में प्रमाणों का निरूपण किया गया है । मति, श्रुत, अवधि, मन:पर्यय और केवल ये पांच ज्ञान हैं जिनमें मति आदि क्रमश: चार ज्ञान इंद्रियों एवं मन की सहायता से उत्पन्न होने के कारण परोक्ष प्रमाण कहे जाते हैं तथा इन्द्रियादि की अपेक्षा न रखकर केवल आत्मबल से उत्पन्न होने वाला केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है ।
तत्त्वार्थ के निर्णय हेतु मतिज्ञान, श्रुतज्ञान तथा अवधिज्ञान -- ये तीन ज्ञान ही प्रयोग में आने वाले प्रमाण हैं, क्योंकि मन:पर्ययज्ञान सम्यग्दर्शन प्राप्त योगी को होता है तथा केवलज्ञान वीतरागी को होता है, अतः दोनों ज्ञान स्वयं ज्ञानियों के लिये ही उपयोगी हैं, और उनके उपदेश से हुआ ज्ञान हमारे लिये श्रुतज्ञान ही होता है ।
मति श्रुत व अवधि ज्ञान रूप परोक्ष-प्रमाण भी मोह की तीव्र - मन्दता के कारण विपरीत भी होते हैं । यथा-मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंगज्ञान । ऐसा होने पर सत् अर्थात् विद्यमान भाव और असत् अर्थात् अविद्यमान भाव की विशेषता न जानने से उन्मत्त की भांति कभी शुद्ध अथवा कभी अशुद्ध अर्थ भी ग्रहण किये जाते हैं । अतः इन कठिनाइयों के होते हुए भी नय-न्याय में जिन सिद्धान्तों की प्ररूपणा की है, उनके द्वारा निर्णय करने से अधिगम की तथा अर्थों में स्थित तात्त्विक स्वरूप की यथार्थ जानकारी हो सकती है । इस प्रकार यहां नय-सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण द्वारा तत्त्वार्थ के सत् और असत् की विशेषता को जानना आवश्यक है ।
नयों के सिद्धान्त
उमास्वाति रचित तत्त्वार्थाधिगम सूत्र यद्यपि दिगम्वर व श्वेताम्बर दोनों परम्पराओं में मान्य है तथापि दोनों के ग्रन्थ अलग-अलग हैं तथा पाठान्तर भी है । नय के विषय में श्वेताम्बर सम्मत सूत्र इस प्रकार है - " नैगम संग्रह व्यवहारर्जु सूत्रशब्दा नयाः””, “आद्यशब्दी द्विभेद "", अर्थात् नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र और शब्द ये पांच नय हैं । प्रथम नैगम नय के देशग्राही और समग्रग्राही दो तथा शब्दनय के सांप्रतशब्द, समभिरूढ़ और अवंभूत ये तीन भेद हैं । दिगम्बर ग्रन्थों के अनुसार " नैगमसंग्रहव्यवहारर्जु सूत्रशब्दसमभिरूढ़ें वंभूता नयाः ॥' अर्थात् नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और अवंभूत ये सात नय हैं । नयों के उक्त विवरण में श्वेताम्बर परम्परा में शब्द के तीन भेद किये और दिगम्बर परम्परा में शब्द को सांप्रत शब्द न कहकर शब्द ही कहा और समभिरूढ़ तथा अवंभूत् नय को पृथक् कहा। इतना होने पर भी परस्पर भावार्थ में विरोध नहीं है ।
(१) नंगम नय - नैगमादि सात नयों के अन्तर्गत प्रथम नैगमनय को स्वोपज्ञभाष्य में इस प्रकार परिभाषित किया है- " निगमेषु ये अभिहिताः शब्दास्तेषामर्थ : शब्दार्थपरिज्ञानं च देशसमग्रग्राही नैगमः" अर्थात् जनपद देश में जो शब्द जिस अर्थ के
१. तत्वार्थसूत्र I. ३४
२. तत्वार्थसूत्र . ३५
३. सर्वार्थसिद्धे, राजवातिकालंकार, श्लोकातिकार . ३३
खण्ड १७, अंक ३ (अक्टूबर-दिसम्बर, ९१ )
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
१३७
www.jainelibrary.org