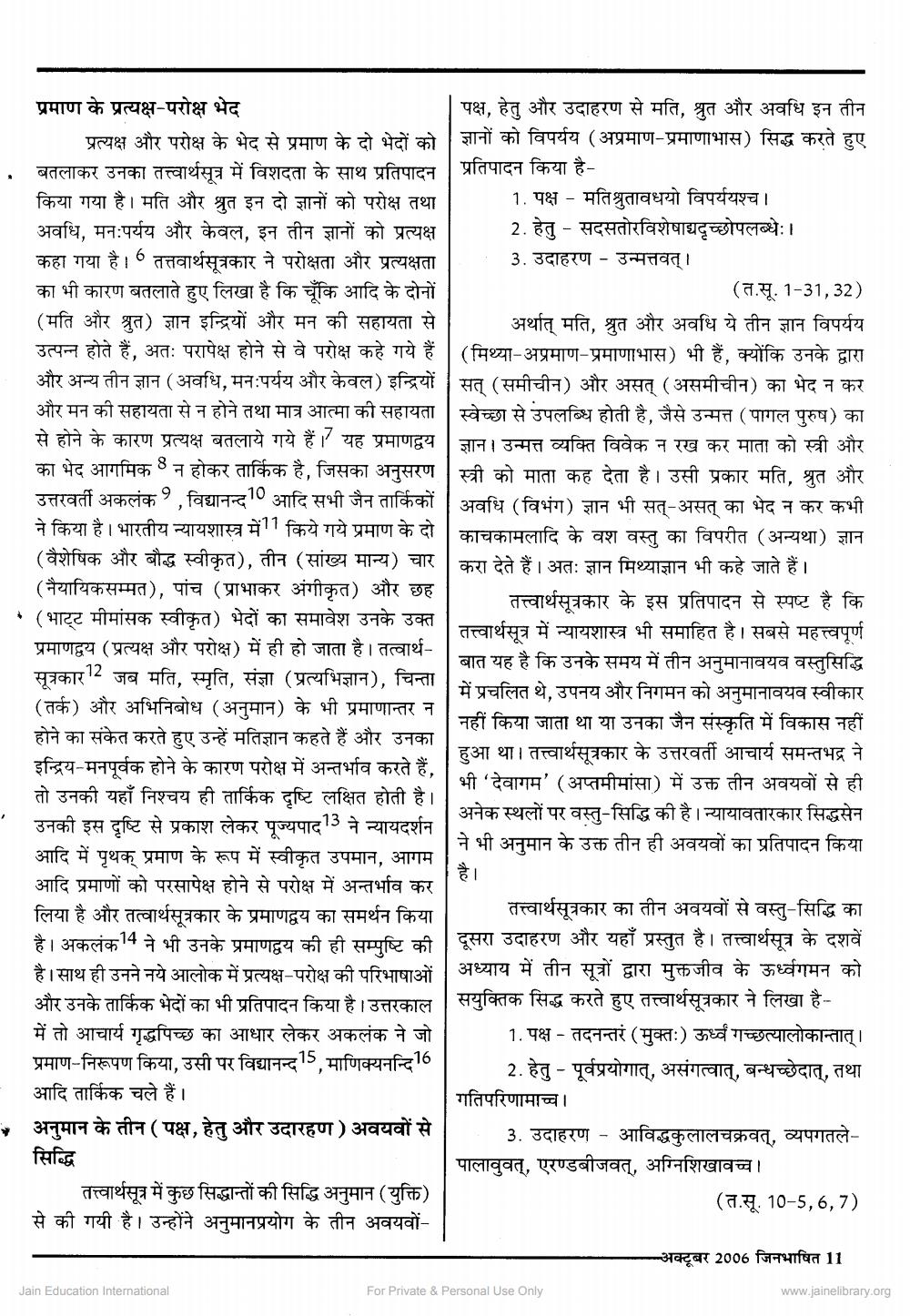________________
·
+
प्रमाण के प्रत्यक्ष-परोक्ष भेद
प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से प्रमाण के दो भेदों को बतलाकर उनका तत्त्वार्थसूत्र में विशदता के साथ प्रतिपादन किया गया है । मति और श्रुत इन दो ज्ञानों को परोक्ष तथा अवधि, मन:पर्यय और केवल इन तीन ज्ञानों को प्रत्यक्ष कहा गया है। 6 तत्तवार्थसूत्रकार ने परोक्षता और प्रत्यक्षता
भी कारण बताते हुए लिखा है कि चूँकि आदि के दोनों (मति और श्रुत) ज्ञान इन्द्रियों और मन की सहायता से उत्पन्न होते अतः परापेक्ष होने से वे परोक्ष कहे गये हैं और अन्य तीन ज्ञान ( अवधि, मन:पर्यय और केवल ) इन्द्रियों और मन की सहायता से न होने तथा मात्र आत्मा की सहायता से होने के कारण प्रत्यक्ष बतलाये गये यह प्रमाणद्वय का भेद आगमिक 8 न होकर तार्किक है, जिसका अनुसरण उत्तरवर्ती अकलंक 9 , विद्यानन्द 10 आदि सभी जैन तार्किकों ने किया है। भारतीय न्यायशास्त्र में 11 किये गये प्रमाण के दो ( वैशेषिक और बौद्ध स्वीकृत), तीन (सांख्य मान्य) चार (नैयायिकसम्मत), पांच (प्राभाकर अंगीकृत) और छह (भाट्ट मीमांसक स्वीकृत) भेदों का समावेश उनके उक्त प्रमाणद्वय (प्रत्यक्ष और परोक्ष) में ही हो जाता है । तत्वार्थसूत्रकार12 जब मति, स्मृति, संज्ञा (प्रत्यभिज्ञान), चिन्ता (तर्क) और अभिनिबोध ( अनुमान) के भी प्रमाणान्तर न होने का संकेत करते हुए उन्हें मतिज्ञान कहते हैं और उनका इन्द्रिय-मनपूर्वक होने के कारण परोक्ष में अन्तर्भाव करते हैं, तो उनकी यहाँ निश्चय ही तार्किक दृष्टि लक्षित होती है। उनकी इस दृष्टि से प्रकाश लेकर पूज्यपाद 13 ने न्यायदर्शन आदि में पृथक् प्रमाण के रूप में स्वीकृत उपमान, आगम आदि प्रमाणों को परसापेक्ष होने से परोक्ष में अन्तर्भाव कर लिया है और तत्वार्थ सूत्रकार के प्रमाणद्वय का समर्थन किया है। अकलंक14 ने भी उनके प्रमाणद्वय की ही सम्पुष्टि की है। साथ ही उनने नये आलोक में प्रत्यक्ष-परोक्ष की परिभाषाओं और उनके तार्किक भेदों का भी प्रतिपादन किया है। उत्तरकाल में तो आचार्य गृद्धपिच्छ का आधार लेकर अकलंक ने जो प्रमाण-निरूपण किया, उसी पर विद्यानन्द 15, माणिक्यनन्दि 16 आदि तार्किक चले हैं ।
के तीन (पक्ष, हेतु और उदारहण) अवयवों से
अनुमान
सिद्धि
तत्त्वार्थसूत्र में कुछ सिद्धान्तों की सिद्धि अनुमान (युक्ति) से की गयी है। उन्होंने अनुमानप्रयोग के तीन अवयवों
Jain Education International
पक्ष, हेतु और उदाहरण से मति, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानों को विपर्यय ( अप्रमाण- प्रमाणाभास) सिद्ध करते हुए प्रतिपादन किया है
1. पक्ष मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च ।
2. हेतु - सदसतोरविशेषाद्यदृच्छोपलब्धेः ।
3. उदाहरण -
उन्मत्तवत् ।
-
(त.सू. 1-31, 32 ) अर्थात् मति, श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान विपर्यय (मिथ्या - अप्रमाण- प्रमाणाभास) भी हैं, क्योंकि उनके द्वारा सत् (समीचीन) और असत् (असमीचीन) का भेद न कर स्वेच्छा से उपलब्धि होती है, जैसे उन्मत्त ( पागल पुरुष ) का ज्ञान । उन्मत्त व्यक्ति विवेक न रख कर माता को स्त्री और स्त्री को माता कह देता है । उसी प्रकार मति, श्रुत और अवधि (विभंग) ज्ञान भी सत्-असत् का भेद न कर कभी काचकामलादि के वश वस्तु का विपरीत (अन्यथा) ज्ञान करा देते हैं । अतः ज्ञान मिथ्याज्ञान भी कहे जाते हैं ।
तत्त्वार्थसूत्रकार के इस प्रतिपादन से स्पष्ट है कि तत्त्वार्थसूत्र में न्यायशास्त्र भी समाहित है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उनके समय में तीन अनुमानावयव वस्तुसिद्धि में प्रचलित थे, उपनय और निगमन को अनुमानावयव स्वीकार नहीं किया जाता था या उनका जैन संस्कृति में विकास नहीं भी 'देवागम' (अप्तमीमांसा) में उक्त तीन अवयवों से ही हुआ था । तत्त्वार्थसूत्रकार के उत्तरवर्ती आचार्य समन्तभद्र ने अनेक स्थलों पर वस्तु-सिद्धि की है। न्यायावतारकार सिद्धसेन ने भी अनुमान के उक्त तीन ही अवयवों का प्रतिपादन किया है ।
तत्त्वार्थसूत्रकार का तीन अवयवों से वस्तु-सिद्धि का दूसरा उदाहरण और यहाँ प्रस्तुत है । तत्त्वार्थसूत्र के दशवें अध्याय में तीन सूत्रों द्वारा मुक्तजीव के ऊर्ध्वगमन को सयुक्तिक सिद्ध करते हुए तत्त्वार्थसूत्रकार ने लिखा है
1. पक्ष - तदनन्तरं (मुक्तः) ऊर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् । 2. हेतु - पूर्वप्रयोगात्, असंगत्वात्, बन्धच्छेदात्, तथा गतिपरिणामाच्च ।
3. उदाहरण
आविद्धकुलालचक्रवत्, व्यपगतलेपालावुवत्, एरण्डबीजवत्, अग्निशिखावच्च ।
(त.सू. 10-5, 6, 7)
For Private & Personal Use Only
-
-अक्टूबर 2006 जिनभाषित 11
www.jainelibrary.org