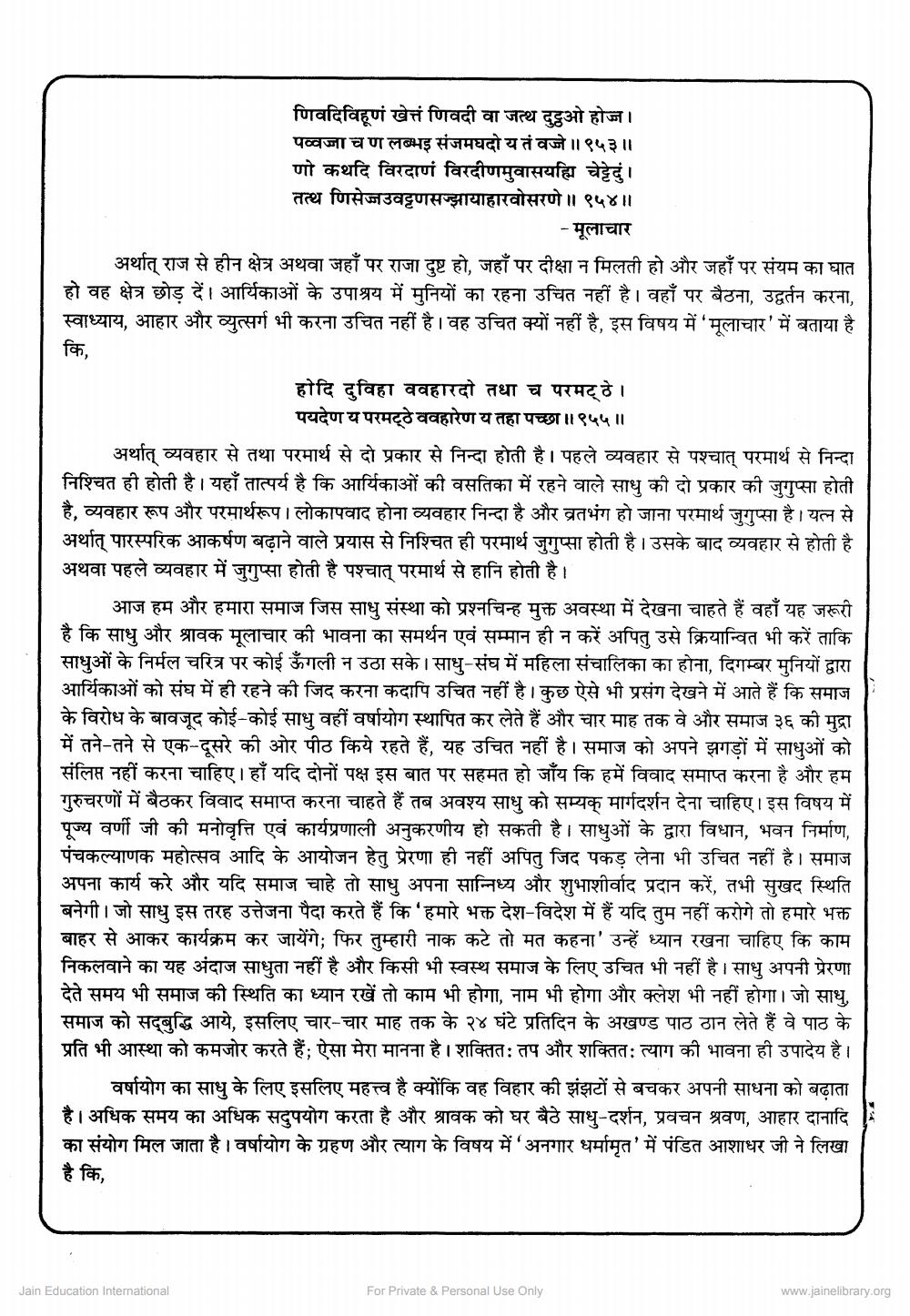________________
णिवदिविहूणं खेत्तं णिवदी वा जत्थ दुट्ठओ होज्ज । पव्वज्जा च ण लब्भइ संजमघदो य तं वज्जे ॥ ९५३ ॥ णो कथदि विरदाणं विरदीणमुवासयह्मि चेट्टेदुं । तत्थ णिसेज्जउवट्टणसज्झायाहारवोसरणे ॥ ९५४॥ मूलाचार
अर्थात् राज से हीन क्षेत्र अथवा जहाँ पर राजा दुष्ट हो, जहाँ पर दीक्षा न मिलती हो और जहाँ पर संयम का घा हो वह क्षेत्र छोड़ दें। आर्यिकाओं के उपाश्रय में मुनियों का रहना उचित नहीं है । वहाँ पर बैठना, उद्वर्तन करना, स्वाध्याय, आहार और व्युत्सर्ग भी करना उचित नहीं है। वह उचित क्यों नहीं है, इस विषय में 'मूलाचार' में बताया है कि,
होदि दुविहा ववहारदो तथा च परमट्ठे । पयदेण य परमट्ठे ववहारेण य तहा पच्छा ।। ९५५ ।।
अर्थात् व्यवहार से तथा परमार्थ से दो प्रकार से निन्दा होती है। पहले व्यवहार से पश्चात् परमार्थ से निन्दा निश्चित ही होती है। यहाँ तात्पर्य है कि आर्यिकाओं की वसतिका में रहने वाले साधु की दो प्रकार की जुगुप्सा होती है, व्यवहार रूप और परमार्थरूप। लोकापवाद होना व्यवहार निन्दा है और व्रतभंग हो जाना परमार्थ जुगुप्सा है। यत्न से अर्थात् पारस्परिक आकर्षण बढ़ाने वाले प्रयास से निश्चित ही परमार्थ जुगुप्सा होती है। उसके बाद व्यवहार से होती है अथवा पहले व्यवहार में जुगुप्सा होती है पश्चात् परमार्थ से हानि होती है।
आज हम और हमारा समाज जिस साधु संस्था को प्रश्नचिन्ह मुक्त अवस्था में देखना चाहते हैं वहाँ यह जरूरी है कि साधु और श्रावक मूलाचार की भावना का समर्थन एवं सम्मान ही न करें अपितु उसे क्रियान्वित भी करें ताकि साधुओं के निर्मल चरित्र पर कोई ऊँगली न उठा सके। साधु-संघ में महिला संचालिका का होना, दिगम्बर मुनियों द्वारा आर्यिकाओं को संघ में ही रहने की जिद करना कदापि उचित नहीं है। कुछ ऐसे भी प्रसंग देखने में आते हैं कि समाज के विरोध के बावजूद कोई-कोई साधु वहीं वर्षायोग स्थापित कर लेते हैं और चार माह तक वे और समाज ३६ की मुद्रा में तने- तने से एक-दूसरे की ओर पीठ किये रहते हैं, यह उचित नहीं है। समाज को अपने झगड़ों में साधुओं को संलिप्त नहीं करना चाहिए। हाँ यदि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो जाँय कि हमें विवाद समाप्त करना है और हम गुरुचरणों में बैठकर विवाद समाप्त करना चाहते हैं तब अवश्य साधु को सम्यक् मार्गदर्शन देना चाहिए । इस विषय में पूज्य वर्णी जी की मनोवृत्ति एवं कार्यप्रणाली अनुकरणीय हो सकती है । साधुओं के द्वारा विधान, भवन निर्माण, पंचकल्याणक महोत्सव आदि के आयोजन हेतु प्रेरणा ही नहीं अपितु जिद पकड़ लेना भी उचित नहीं है। समाज अपना कार्य करे और यदि समाज चाहे तो साधु अपना सान्निध्य और शुभाशीर्वाद प्रदान करें, तभी सुखद स्थिति बनेगी। जो साधु इस तरह उत्तेजना पैदा करते हैं कि 'हमारे भक्त देश-विदेश में हैं यदि तुम नहीं करोगे तो हमारे भक्त बाहर से आकर कार्यक्रम कर जायेंगे; फिर तुम्हारी नाक कटे तो मत कहना' उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि काम निकलवाने का यह अंदाज साधुता नहीं है और किसी भी स्वस्थ समाज के लिए उचित भी नहीं है। साधु अपनी प्रेरणा देते समय भी समाज की स्थिति का ध्यान रखें तो काम भी होगा, नाम भी होगा और क्लेश भी नहीं होगा। जो साधु, समाज को सद्बुद्धि आये, इसलिए चार-चार माह तक के २४ घंटे प्रतिदिन के अखण्ड पाठ ठान लेते हैं वे पाठ के प्रति भी आस्था को कमजोर करते हैं; ऐसा मेरा मानना है। शक्तितः तप और शक्तितः त्याग की भावना ही उपादेय है।
Jain Education International
वर्षायोग का साधु के लिए इसलिए महत्त्व है क्योंकि वह विहार की झंझटों से बचकर अपनी साधना को बढ़ाता है। अधिक समय का अधिक सदुपयोग करता है और श्रावक को घर बैठे साधु-दर्शन, प्रवचन श्रवण, आहार दानादि का संयोग मिल जाता है। वर्षायोग के ग्रहण और त्याग के विषय में 'अनगार धर्मामृत' में पंडित आशाधर जी ने लिखा है कि,
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org