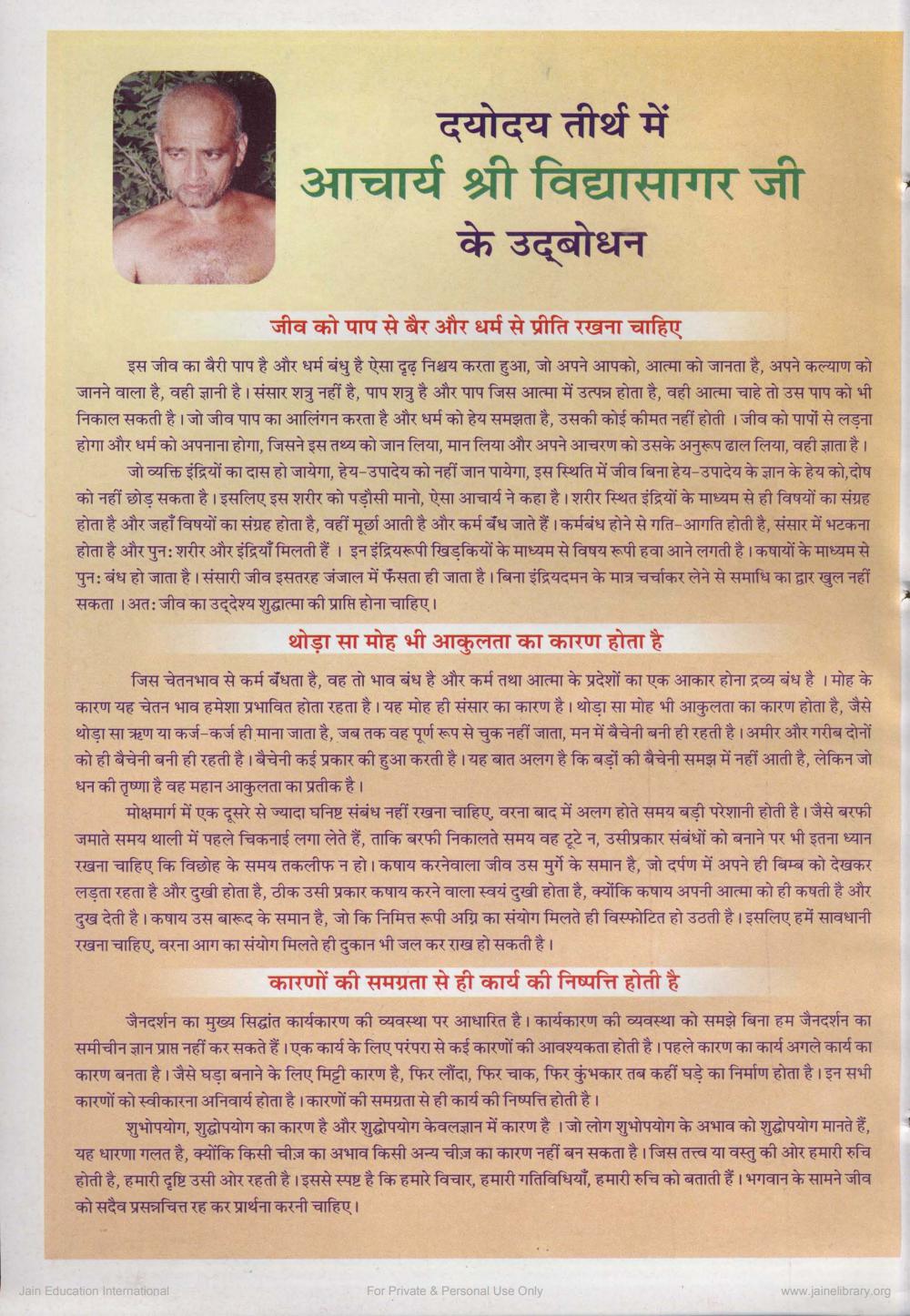________________
दयोदय तीर्थ में आचार्य श्री विद्यासागर जी
के उद्बोधन
जीव को पाप से बैर और धर्म से प्रीति रखना चाहिए
इस जीव का बैरी पाप है और धर्म बंधु है ऐसा दृढ़ निश्चय करता हुआ, जो अपने आपको, आत्मा को जानता है, अपने कल्याण को जानने वाला है, वही ज्ञानी है। संसार शत्रु नहीं है, पाप शत्रु है और पाप जिस आत्मा में उत्पन्न होता है, वही आत्मा चाहे तो उस पाप को भी निकाल सकती है। जो जीव पाप का आलिंगन करता है और धर्म को हेय समझता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती । जीव को पापों से लड़ना होगा और धर्म को अपनाना होगा, जिसने इस तथ्य को जान लिया, मान लिया और अपने आचरण को उसके अनुरूप ढाल लिया, वही ज्ञाता है।
जो व्यक्ति इंद्रियों का दास हो जायेगा, हेय-उपादेय को नहीं जान पायेगा, इस स्थिति में जीव बिना हेय-उपादेय के ज्ञान के हेय को,दोष को नहीं छोड़ सकता है। इसलिए इस शरीर को पड़ौसी मानो, ऐसा आचार्य ने कहा है। शरीर स्थित इंद्रियों के माध्यम से ही विषयों का संग्रह होता है और जहाँ विषयों का संग्रह होता है, वहीं मूर्छा आती है और कर्म बंध जाते हैं। कर्मबंध होने से गति-आगति होती है, संसार में भटकना होता है और पुनः शरीर और इंद्रियाँ मिलती हैं। इन इंद्रियरूपी खिड़कियों के माध्यम से विषय रूपी हवा आने लगती है। कषायों के माध्यम से पुन: बंध हो जाता है। संसारी जीव इसतरह जंजाल में फंसता ही जाता है। बिना इंद्रियदमन के मात्र चर्चाकर लेने से समाधि का द्वार खुल नहीं सकता । अत: जीव का उद्देश्य शुद्धात्मा की प्राप्ति होना चाहिए।
थोड़ा सा मोह भी आकुलता का कारण होता है जिस चेतनभाव से कर्म बँधता है, वह तो भाव बंध है और कर्म तथा आत्मा के प्रदेशों का एक आकार होना द्रव्य बंध है । मोह के कारण यह चेतन भाव हमेशा प्रभावित होता रहता है। यह मोह ही संसार का कारण है। थोड़ा सा मोह भी आकुलता का कारण होता है, जैसे थोड़ा सा ऋण या कर्ज-कर्ज ही माना जाता है, जब तक वह पूर्ण रूप से चुक नहीं जाता, मन में बैचेनी बनी ही रहती है। अमीर और गरीब दोनों को ही बैचेनी बनी ही रहती है। बैचेनी कई प्रकार की हुआ करती है। यह बात अलग है कि बड़ों की बैचेनी समझ में नहीं आती है, लेकिन जो धन की तृष्णा है वह महान आकुलता का प्रतीक है।
_ मोक्षमार्ग में एक दूसरे से ज्यादा घनिष्ट संबंध नहीं रखना चाहिए, वरना बाद में अलग होते समय बड़ी परेशानी होती है। जैसे बरफी जमाते समय थाली में पहले चिकनाई लगा लेते हैं, ताकि बरफी निकालते समय वह टूटे न, उसीप्रकार संबंधों को बनाने पर भी इतना ध्यान रखना चाहिए कि विछोह के समय तकलीफ न हो। कषाय करनेवाला जीव उस मुर्गे के समान है, जो दर्पण में अपने ही बिम्ब को देखकर लड़ता रहता है और दुखी होता है, ठीक उसी प्रकार कषाय करने वाला स्वयं दुखी होता है, क्योंकि कषाय अपनी आत्मा को ही कषती है और दुख देती है। कषाय उस बारूद के समान है, जो कि निमित्त रूपी अग्नि का संयोग मिलते ही विस्फोटित हो उठती है। इसलिए हमें सावधानी रखना चाहिए, वरना आग का संयोग मिलते ही दुकान भी जल कर राख हो सकती है।
कारणों की समग्रता से ही कार्य की निष्पत्ति होती है जैनदर्शन का मुख्य सिद्धांत कार्यकारण की व्यवस्था पर आधारित है। कार्यकारण की व्यवस्था को समझे बिना हम जैनदर्शन का समीचीन ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं । एक कार्य के लिए परंपरा से कई कारणों की आवश्यकता होती है। पहले कारण का कार्य अगले कार्य का कारण बनता है। जैसे घड़ा बनाने के लिए मिट्टी कारण है, फिर लौंदा, फिर चाक, फिर कुंभकार तब कहीं घड़े का निर्माण होता है। इन सभी कारणों को स्वीकारना अनिवार्य होता है। कारणों की समग्रता से ही कार्य की निष्पत्ति होती है।
शुभोपयोग, शुद्धोपयोग का कारण है और शुद्धोपयोग केवलज्ञान में कारण है । जो लोग शुभोपयोग के अभाव को शुद्धोपयोग मानते हैं, यह धारणा गलत है, क्योंकि किसी चीज़ का अभाव किसी अन्य चीज़ का कारण नहीं बन सकता है। जिस तत्त्व या वस्तु की ओर हमारी रुचि होती है, हमारी दृष्टि उसी ओर रहती है। इससे स्पष्ट है कि हमारे विचार, हमारी गतिविधियाँ, हमारी रुचि को बताती हैं। भगवान के सामने जीव को सदैव प्रसन्नचित्त रह कर प्रार्थना करनी चाहिए।
Jain Education International
For Private & Personal use only
www.jainelibrary.org