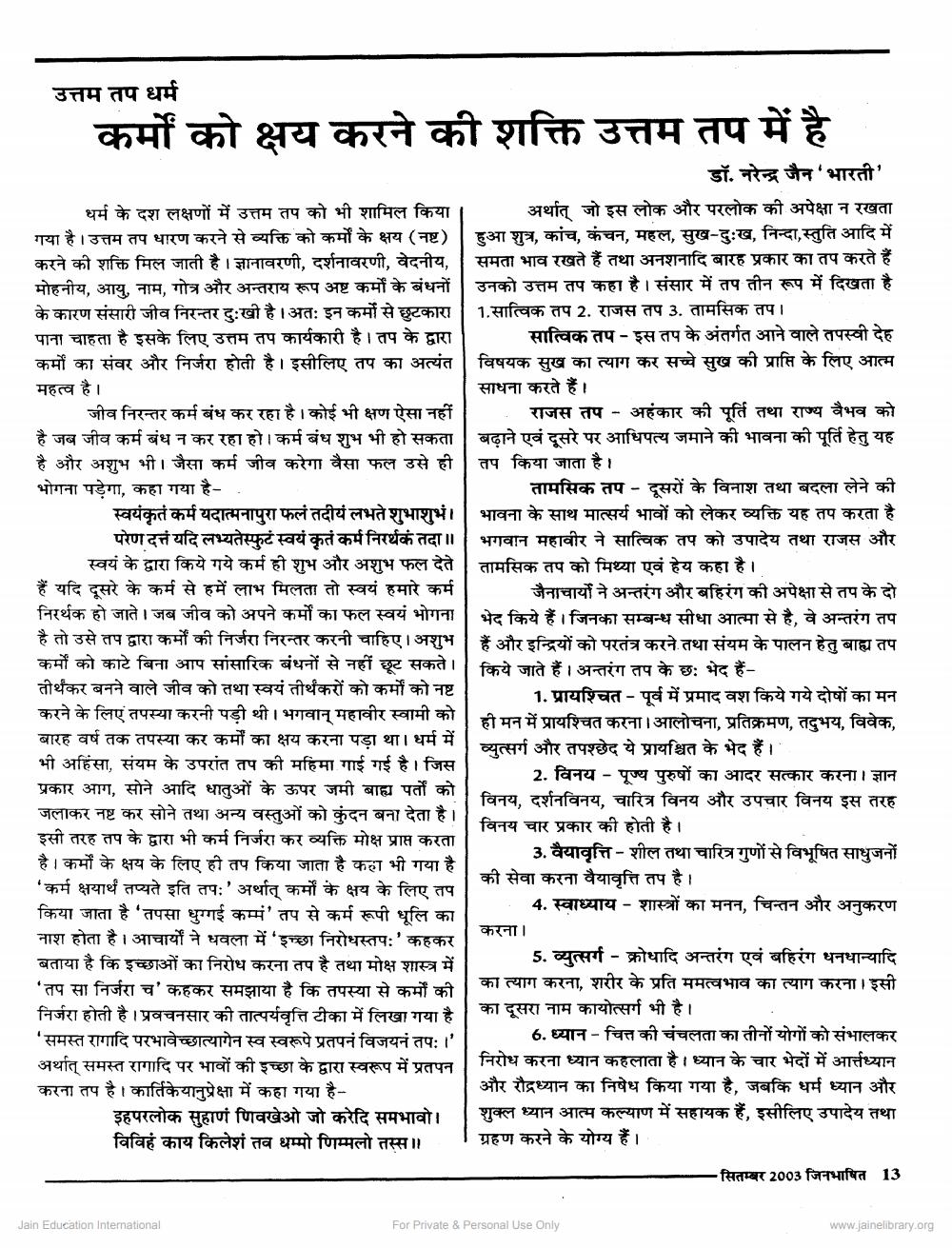________________
उत्तम तप धर्म
कर्मों को क्षय करने की शक्ति उत्तम तप में है
डॉ. नरेन्द्र जैन 'भारती' धर्म के दश लक्षणों में उत्तम तप को भी शामिल किया । अर्थात् जो इस लोक और परलोक की अपेक्षा न रखता गया है। उत्तम तप धारण करने से व्यक्ति को कर्मों के क्षय (नष्ट) | हुआ शुत्र, कांच, कंचन, महल, सुख-दुःख, निन्दा,स्तुति आदि में करने की शक्ति मिल जाती है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, समता भाव रखते हैं तथा अनशनादि बारह प्रकार का तप करते हैं मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय रूप अष्ट कर्मों के बंधनों उनको उत्तम तप कहा है। संसार में तप तीन रूप में दिखता है के कारण संसारी जीव निरन्तर दुःखी है। अत: इन कर्मों से छुटकारा | 1.सात्विक तप 2. राजस तप 3. तामसिक तप। पाना चाहता है इसके लिए उत्तम तप कार्यकारी है। तप के द्वारा | सात्विक तप- इस तप के अंतर्गत आने वाले तपस्वी देह कर्मों का संवर और निर्जरा होती है। इसीलिए तप का अत्यंत | विषयक सुख का त्याग कर सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए आत्म महत्व है।
साधना करते हैं। जीव निरन्तर कर्म बंध कर रहा है। कोई भी क्षण ऐसा नहीं | राजस तप - अहंकार की पूर्ति तथा राज्य वैभव को है जब जीव कर्म बंध न कर रहा हो। कर्म बंध शुभ भी हो सकता | बढ़ाने एवं दूसरे पर आधिपत्य जमाने की भावना की पूर्ति हेतु यह है और अशुभ भी। जैसा कर्म जीव करेगा वैसा फल उसे ही | तप किया जाता है। भोगना पड़ेगा, कहा गया है- . .
तामसिक तप- दूसरों के विनाश तथा बदला लेने की स्वयंकृतं कर्म यदात्मनापुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभं।। भावना के साथ मात्सर्य भावों को लेकर व्यक्ति यह तप करता है
परेण दत्तं यदि लभ्यतेस्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा॥ | भगवान महावीर ने सात्विक तप को उपादेय तथा राजस और
स्वयं के द्वारा किये गये कर्म ही शुभ और अशुभ फल देते | तामसिक तप को मिथ्या एवं हेय कहा है। हैं यदि दूसरे के कर्म से हमें लाभ मिलता तो स्वयं हमारे कर्म जैनाचार्यों ने अन्तरंग और बहिरंग की अपेक्षा से तप के दो निरर्थक हो जाते। जब जीव को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना | भेद किये हैं। जिनका सम्बन्ध सीधा आत्मा से है, वे अन्तरंग तप है तो उसे तप द्वारा कर्मों की निर्जरा निरन्तर करनी चाहिए। अशुभ | हैं और इन्द्रियों को परतंत्र करने तथा संयम के पालन हेतु बाह्य तप कर्मों को काटे बिना आप सांसारिक बंधनों से नहीं छूट सकते। | किये जाते हैं। अन्तरंग तप के छ: भेद हैंतीर्थकर बनने वाले जीव को तथा स्वयं तीर्थंकरों को कर्मों को नष्ट
1.प्रायश्चित- पूर्व में प्रमाद वश किये गये दोषों का मन करने के लिए तपस्या करनी पड़ी थी। भगवान् महावीर स्वामी को
ही मन में प्रायश्चित करना। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, बारह वर्ष तक तपस्या कर कर्मों का क्षय करना पड़ा था। धर्म में
व्युत्सर्ग और तपश्छेद ये प्रायश्चित के भेद हैं। भी अहिंसा, संयम के उपरांत तप की महिमा गाई गई है। जिस
2. विनय - पूज्य पुरुषों का आदर सत्कार करना। ज्ञान प्रकार आग, सोने आदि धातुओं के ऊपर जमी बाह्य पर्तों को
विनय, दर्शनविनय, चारित्र विनय और उपचार विनय इस तरह जलाकर नष्ट कर सोने तथा अन्य वस्तुओं को कुंदन बना देता है। इसी तरह तप के द्वारा भी कर्म निर्जरा कर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता
विनय चार प्रकार की होती है। है। कर्मों के क्षय के लिए ही तप किया जाता है कहा भी गया है
3. वैयावृत्ति- शील तथा चारित्र गुणों से विभूषित साधुजनों 'कर्म क्षयार्थं तप्यते इति तपः' अर्थात् कर्मों के क्षय के लिए तप
की सेवा करना वैयावृत्ति तप है। किया जाता है 'तपसा धुग्गई कम्म' तप से कर्म रूपी धूलि का
4. स्वाध्याय - शास्त्रों का मनन, चिन्तन और अनुकरण नाश होता है। आचार्यों ने धवला में 'इच्छा निरोधस्तपः' कहकर
करना। बताया है कि इच्छाओं का निरोध करना तप है तथा मोक्ष शास्त्र में
5. व्युत्सर्ग - क्रोधादि अन्तरंग एवं बहिरंग धनधान्यादि 'तप सा निर्जरा च' कहकर समझाया है कि तपस्या से कर्मों की
का त्याग करना, शरीर के प्रति ममत्वभाव का त्याग करना। इसी निजरा होती है। प्रवचनसार की तात्पर्यवत्ति टीका में लिखा गया है। का दूसरा नाम कायोत्सर्ग भी है। 'समस्त रागादि परभावेच्छात्यागेन स्व स्वरूपे प्रतपनं विजयनं तपः।'
6. ध्यान- चित्त की चंचलता का तीनों योगों को संभालकर अर्थात् समस्त रागादि पर भावों की इच्छा के द्वारा स्वरूप में प्रतपन |
निरोध करना ध्यान कहलाता है। ध्यान के चार भेदों में आर्तध्यान करना तप है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में कहा गया है
और रौद्रध्यान का निषेध किया गया है, जबकि धर्म ध्यान और इहपरलोक सुहाणं णिवखेओ जो करेदि समभावो। । शुक्ल ध्यान आत्म कल्याण में सहायक हैं, इसीलिए उपादेय तथा विविहं काय किलेशं तव धम्मो णिम्मलो तस्स॥ | ग्रहण करने के योग्य हैं।
-सितम्बर 2003 जिनभाषित 13
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org