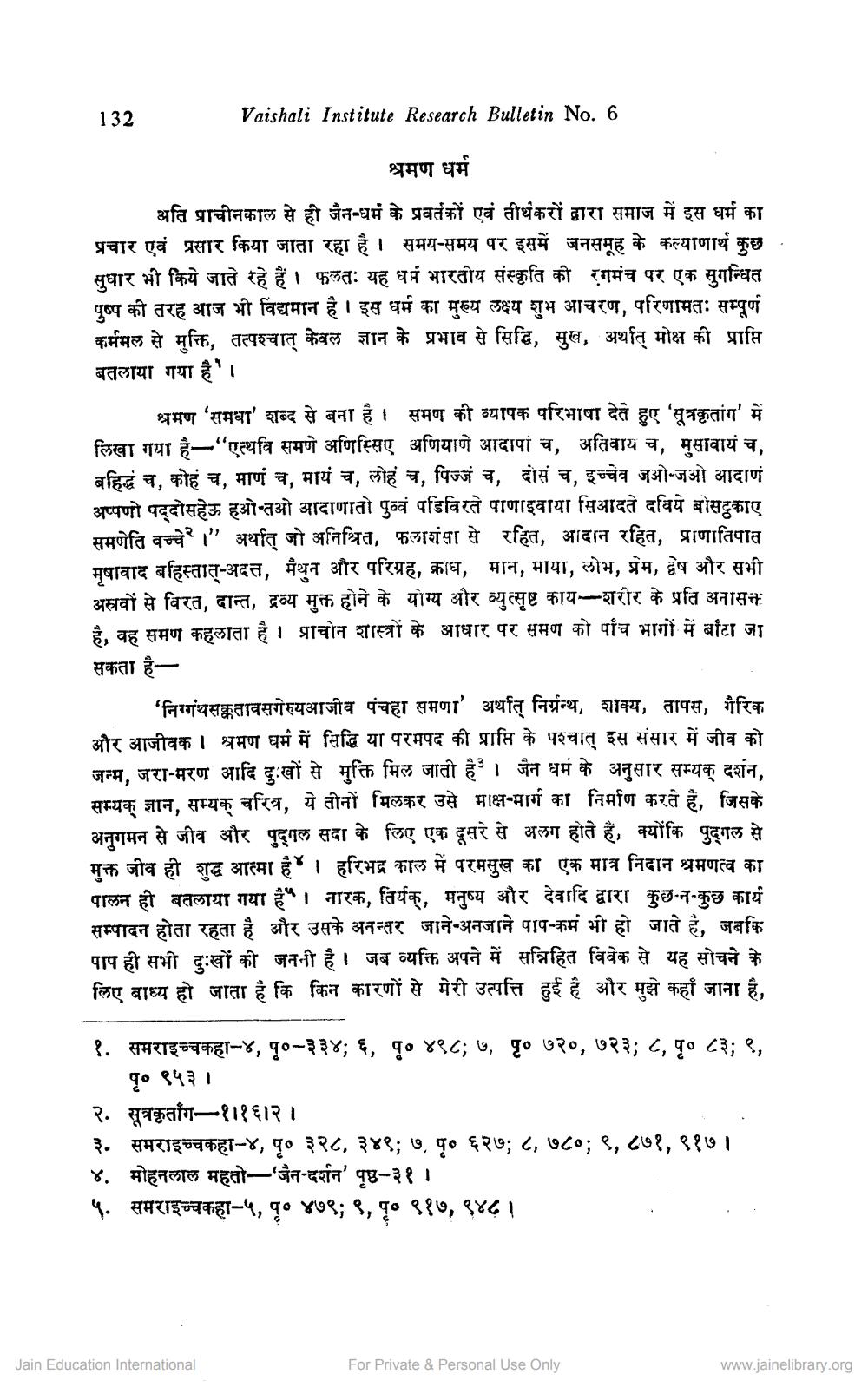________________
Vaishali Institute Research Bulletin No. 6
श्रमण धर्म
अति प्राचीनकाल से ही जैन-धर्म के प्रवर्तकों एवं तीर्थंकरों द्वारा समाज में इस धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया जाता रहा है। समय-समय पर इसमें जनसमूह के कल्याणार्थं कुछ सुधार भी किये जाते रहे हैं । फलतः यह धर्म भारतीय संस्कृति की रंगमंच पर एक सुगन्धित पुष्प की तरह आज भी विद्यमान है। इस धर्म का मुख्य लक्ष्य शुभ आचरण, परिणामतः सम्पूर्ण कर्ममल से मुक्ति, तत्पश्चात् केवल ज्ञान के प्रभाव से सिद्धि, सुख, अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति बतलाया गया है ' ।
132
श्रमण 'समधा' शब्द से बना है । समण की व्यापक परिभाषा देते हुए 'सूत्रकृतांग' में लिखा गया है - " एत्थवि समणे अणिस्सिए अणियाणे आदापां च, अतिवाय च, मुसावायं च, बद्धिं च, कोहं च, माणं च, मायं च, लोहं च, पिज्जं च, दोसं च, इच्चेत्र जओ-जओ आदाणं अप्पणी पद्दो सहेऊ हओ-तओ आदाणातो पुव्वं पडिविरते पाणाइवाया सिआदते दविये बोसटुकाए समणेति वच्चे' ।” अर्थात् जो अनिश्रित फलाशंसा से रहित, आदान रहित, प्राणातिपात मृषावाद बहिस्तात् अदत्त, मैथुन और परिग्रह, क्राध, मान, माया, लोभ, प्रेम, द्वेष और सभी अस्रवों से विरत, दान्त, द्रव्य मुक्त होने के योग्य और व्युत्सृष्ट काय - शरीर के प्रति अनासक्त है, वह समण कहलाता है । प्राचीन शास्त्रों के आधार पर समण को पाँच भागों में बाँटा जा सकता है
'निग्गंथसक्कतावसगेरुयआजीव पंचहा समणा' अर्थात् निर्ग्रन्थ, शाक्य, तापस, गैरिक
इस संसार में जीव को
और आजीवक | श्रमण धर्म में सिद्धि या परमपद की प्राप्ति के पश्चात् जन्म, जरा-मरण आदि दुःखों से मुक्ति मिल जाती है । जैन धर्म के अनुसार सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, सम्यक् चरित्र, ये तीनों मिलकर उसे माक्ष-मार्ग का निर्माण करते हैं, जिसके अनुगमन से जीव और पुद्गल सदा के लिए एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि पुद्गल से मुक्त जीव ही शुद्ध आत्मा हैं । हरिभद्र काल में परमसुख का एक मात्र निदान श्रमणत्व का पालन ही बतलाया गया है" । नारक, तिर्यक्, मनुष्य और देवादि द्वारा कुछ-न-कुछ कार्य सम्पादन होता रहता है और उसके अनन्तर जाने-अनजाने पाप कर्म भी हो जाते है, जबकि पाप ही सभी दुःखों की जननी है । जब व्यक्ति अपने में सन्निहित विवेक से यह सोचने के लिए बाध्य हो जाता है कि किन कारणों से मेरी उत्पत्ति हुई है और मुझे कहाँ जाना है,
१. समराइच्चकहा-४, पृ० - ३३४ ६, पृ० ४९८ ७, पृ० ७२०, ७२३ ८, पृ० ८३, ९, पृ० ९५३ ।
२. सूत्रकृताँग - १।१६।२ ।
३. समराइच्चकहा- ४, पृ० ३२८, ३४९ ७, पृ० ६२७, ८, ७८० ९, ८७१, ९१७ । ४. मोहनलाल महतो - 'जैन दर्शन' पृष्ठ - ३१ ।
५. समराइच्चकहा- ५, पृ० ४७९, ९, पृ० ९१७, ९४८ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org