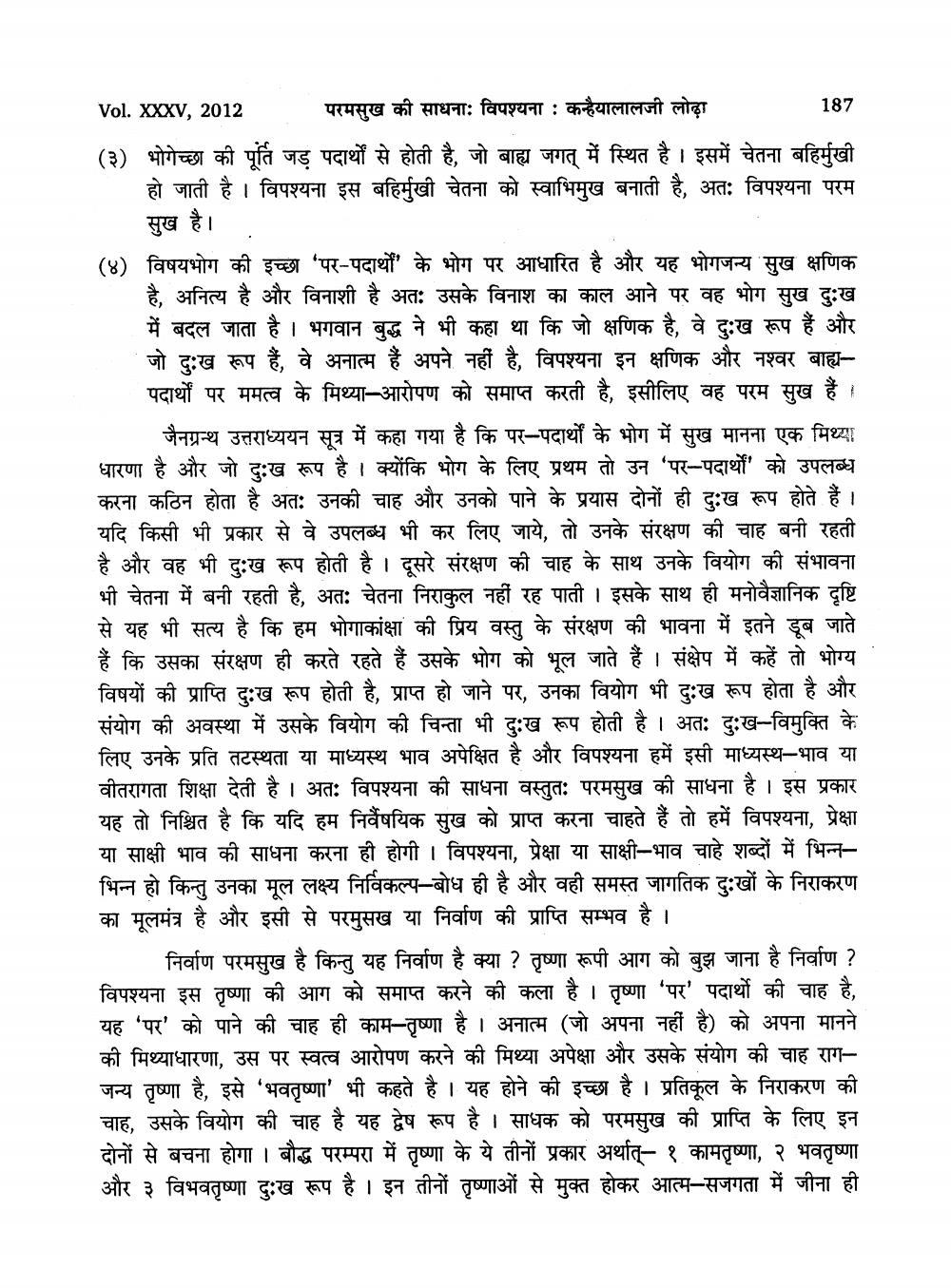________________
Vol. XXXV, 2012 परमसुख की साधनाः विपश्यना : कन्हैयालालजी लोढ़ा
187 (३) भोगेच्छा की पूर्ति जड़ पदार्थों से होती है, जो बाह्य जगत् में स्थित है। इसमें चेतना बहिर्मुखी
हो जाती है । विपश्यना इस बहिर्मुखी चेतना को स्वाभिमुख बनाती है, अत: विपश्यना परम
सुख है। (४) विषयभोग की इच्छा 'पर-पदार्थों' के भोग पर आधारित है और यह भोगजन्य सुख क्षणिक
है, अनित्य है और विनाशी है अतः उसके विनाश का काल आने पर वह भोग सुख दुःख में बदल जाता है। भगवान बुद्ध ने भी कहा था कि जो क्षणिक है, वे दुःख रूप हैं और जो दुःख रूप हैं, वे अनात्म हैं अपने नहीं है, विपश्यना इन क्षणिक और नश्वर बाह्यपदार्थों पर ममत्व के मिथ्या आरोपण को समाप्त करती है, इसीलिए वह परम सुख हैं ।
जैनग्रन्थ उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है कि पर-पदार्थों के भोग में सुख मानना एक मिथ्या धारणा है और जो दुःख रूप है । क्योंकि भोग के लिए प्रथम तो उन 'पर-पदार्थों' को उपलब्ध करना कठिन होता है अतः उनकी चाह और उनको पाने के प्रयास दोनों ही दुःख रूप होते हैं। यदि किसी भी प्रकार से वे उपलब्ध भी कर लिए जाये, तो उनके संरक्षण की चाह बनी रहती है और वह भी दुःख रूप होती है। दूसरे संरक्षण की चाह के साथ उनके वियोग की संभावना भी चेतना में बनी रहती है, अतः चेतना निराकुल नहीं रह पाती । इसके साथ ही मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह भी सत्य है कि हम भोगाकांक्षा की प्रिय वस्तु के संरक्षण की भावना में इतने डूब जाते हैं कि उसका संरक्षण ही करते रहते हैं उसके भोग को भूल जाते हैं । संक्षेप में कहें तो भोग्य
की प्राप्ति दःख रूप होती है. प्राप्त हो जाने पर. उनका वियोग भी दःख रूप होता है और संयोग की अवस्था में उसके वियोग की चिन्ता भी दुःख रूप होती है । अतः दुःख-विमुक्ति के लिए उनके प्रति तटस्थता या माध्यस्थ भाव अपेक्षित है और विपश्यना हमें इसी माध्यस्थ-भाव या वीतरागता शिक्षा देती है । अतः विपश्यना की साधना वस्तुतः परमसुख की साधना है । इस प्रकार यह तो निश्चित है कि यदि हम निर्वैषयिक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें विपश्यना, प्रेक्षा या साक्षी भाव की साधना करना ही होगी। विपश्यना. प्रेक्षा या साक्षी-भाव चाहे शब्दों में भिन्नभिन्न हो किन्तु उनका मूल लक्ष्य निर्विकल्प-बोध ही है और वही समस्त जागतिक दुःखों के निराकरण का मूलमंत्र है और इसी से परमुसख या निर्वाण की प्राप्ति सम्भव है ।
निर्वाण परमसुख है किन्तु यह निर्वाण है क्या ? तृष्णा रूपी आग को बुझ जाना है निर्वाण ? विपश्यना इस तृष्णा की आग को समाप्त करने की कला है । तृष्णा 'पर' पदार्थो की चाह है, यह 'पर' को पाने की चाह ही काम-तृष्णा है । अनात्म (जो अपना नहीं है) को अपना मानने की मिथ्याधारणा, उस पर स्वत्व आरोपण करने की मिथ्या अपेक्षा और उसके संयोग की चाह रागजन्य तृष्णा है, इसे 'भवतृष्णा' भी कहते है । यह होने की इच्छा है । प्रतिकूल के निराकरण की चाह, उसके वियोग की चाह है यह द्वेष रूप है । साधक को परमसुख की प्राप्ति के लिए इन दोनों से बचना होगा । बौद्ध परम्परा में तृष्णा के ये तीनों प्रकार अर्थात्- १ कामतृष्णा, २ भवतृष्णा और ३ विभवतृष्णा दुःख रूप है । इन तीनों तृष्णाओं से मुक्त होकर आत्म-सजगता में जीना ही