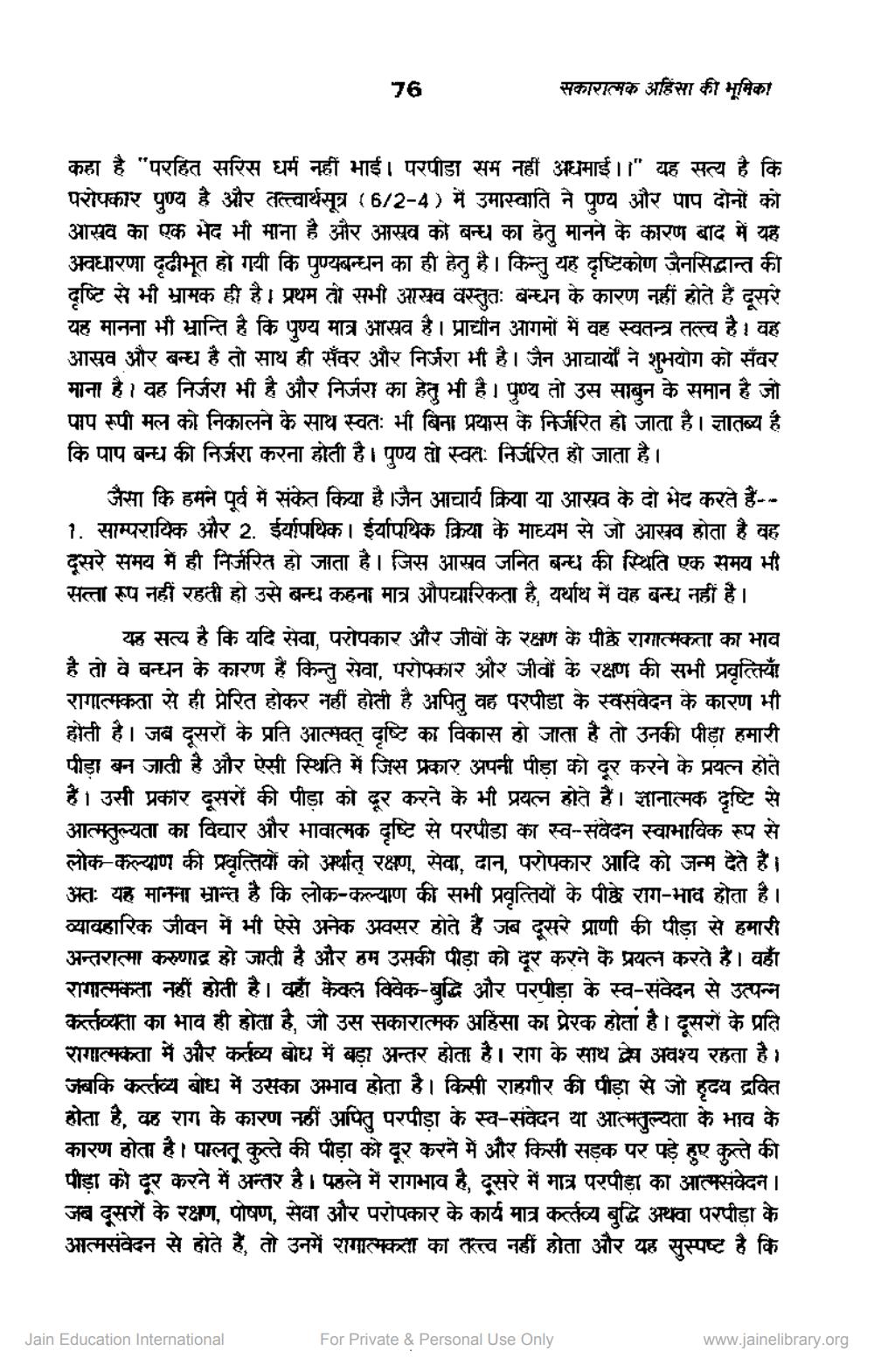________________
76
सकारात्मक अहिंसा की भूमिका
कहा है "परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परपीडा सम नहीं अधमाई।।" यह सत्य है कि परोपकार पुण्य है और तत्त्वार्थसूत्र (6/2-4) में उमास्वाति ने पुण्य और पाप दोनों को आसव का एक भेद भी माना है और आस्रव को बन्ध का हेतु मानने के कारण बाद में यह अवधारणा दृढीभूत हो गयी कि पुण्यबन्धन का ही हेतु है। किन्तु यह दृष्टिकोण जैनसिद्धान्त की दृष्टि से भी भ्रामक ही है। प्रथम तो सभी आसव वस्तुतः बन्धन के कारण नहीं होते हैं दूसरे यह मानना भी भ्रान्ति है कि पुण्य मात्र आस्रव है। प्राचीन आगमों में वह स्वतन्त्र तत्त्व है। वह आसव और बन्ध है तो साथ ही सँवर और निर्जरा भी है। जैन आचार्यों ने शुभयोग को सँवर माना है। वह निर्जरा भी है और निर्जरा का हेतु भी है। पुण्य तो उस साबुन के समान है जो पाप स्पी मल को निकालने के साथ स्वतः भी बिना प्रयास के निर्जरित हो जाता है। ज्ञातव्य है कि पाप बन्ध की निर्जरा करना होती है। पुण्य तो स्वतः निर्जरित हो जाता है।
जैसा कि हमने पूर्व में संकेत किया है।जैन आचार्य क्रिया या आसव के दो भेद करते हैं-- 1. साम्परायिक और 2. ईर्यापथिक। ईर्यापथिक क्रिया के माध्यम से जो आस्रव होता है वह दूसरे समय में ही निर्जरित हो जाता है। जिस आसव जनित बन्ध की स्थिति एक समय भी सत्ता रूप नहीं रहती हो उसे बन्ध कहना मात्र औपचारिकता है, यर्थाथ में वह बन्ध नहीं है।
यह सत्य है कि यदि सेवा, परोपकार और जीवों के रक्षण के पीछे रागात्मकता का भाव है तो वे बन्धन के कारण हैं किन्तु सेवा, परोपकार और जीवों के रक्षण की सभी प्रवृत्तियाँ रागात्मकता से ही प्रेरित होकर नहीं होती है अपितु वह परपीडा के स्वसंवेदन के कारण भी होती है। जब दूसरों के प्रति आत्मवत् दृष्टि का विकास हो जाता है तो उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा बन जाती है और ऐसी स्थिति में जिस प्रकार अपनी पीड़ा को दूर करने के प्रयत्न होते हैं। उसी प्रकार दूसरों की पीड़ा को दूर करने के भी प्रयत्न होते हैं। ज्ञानात्मक दृष्टि से आत्मतुल्यता का विचार और भावात्मक दृष्टि से परपीडा का स्व-संवेदन स्वाभाविक रूप से लोक कल्याण की प्रवृत्तियों को अर्थात् रक्षण, सेवा, दान, परोपकार आदि को जन्म देते है। अतः यह मानना भ्रान्त है कि लोक-कल्याण की सभी प्रवृत्तियों के पीछे राग-भाव होता है। व्यावहारिक जीवन में भी ऐसे अनेक अवसर होते है जब दूसरे प्राणी की पीड़ा से हमारी अन्तरात्मा करुणाद्र हो जाती है और हम उसकी पीड़ा को दूर करने के प्रयत्न करते है। वहाँ रागात्मकता नहीं होती है। वहाँ केवल विवेक-बुद्धि और परपीड़ा के स्व-संवेदन से उत्पन्न कर्त्तव्यता का भाव ही होता है, जो उस सकारात्मक अहिंसा का प्रेरक होता है। दूसरों के प्रति रागात्मकता में और कर्तव्य बोध में बड़ा अन्तर होता है। राग के साथ ले अवश्य रहता है। जबकि कर्तव्य बोध में उसका अभाव होता है। किसी राहगीर की पीड़ा से जो हृदय द्रवित होता है, वह राग के कारण नहीं अपितु परपीड़ा के स्व-संवेदन या आत्मतुल्यता के भाव के कारण होता है। पालतू कुत्ते की पीड़ा को दूर करने में और किसी सड़क पर पड़े हुए कुत्ते की पीड़ा को दूर करने में अन्तर है। पहले में रागभाव है, दूसरे में मात्र परपीड़ा का आत्मसंवेदन । जब दूसरों के रक्षण, पोषण, सेवा और परोपकार के कार्य मात्र कर्तव्य बुद्धि अथवा परपीडा के आत्मसंवेदन से होते हैं, तो उनमें रागात्मकता का तत्त्व नहीं होता और यह सुस्पष्ट है कि
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org