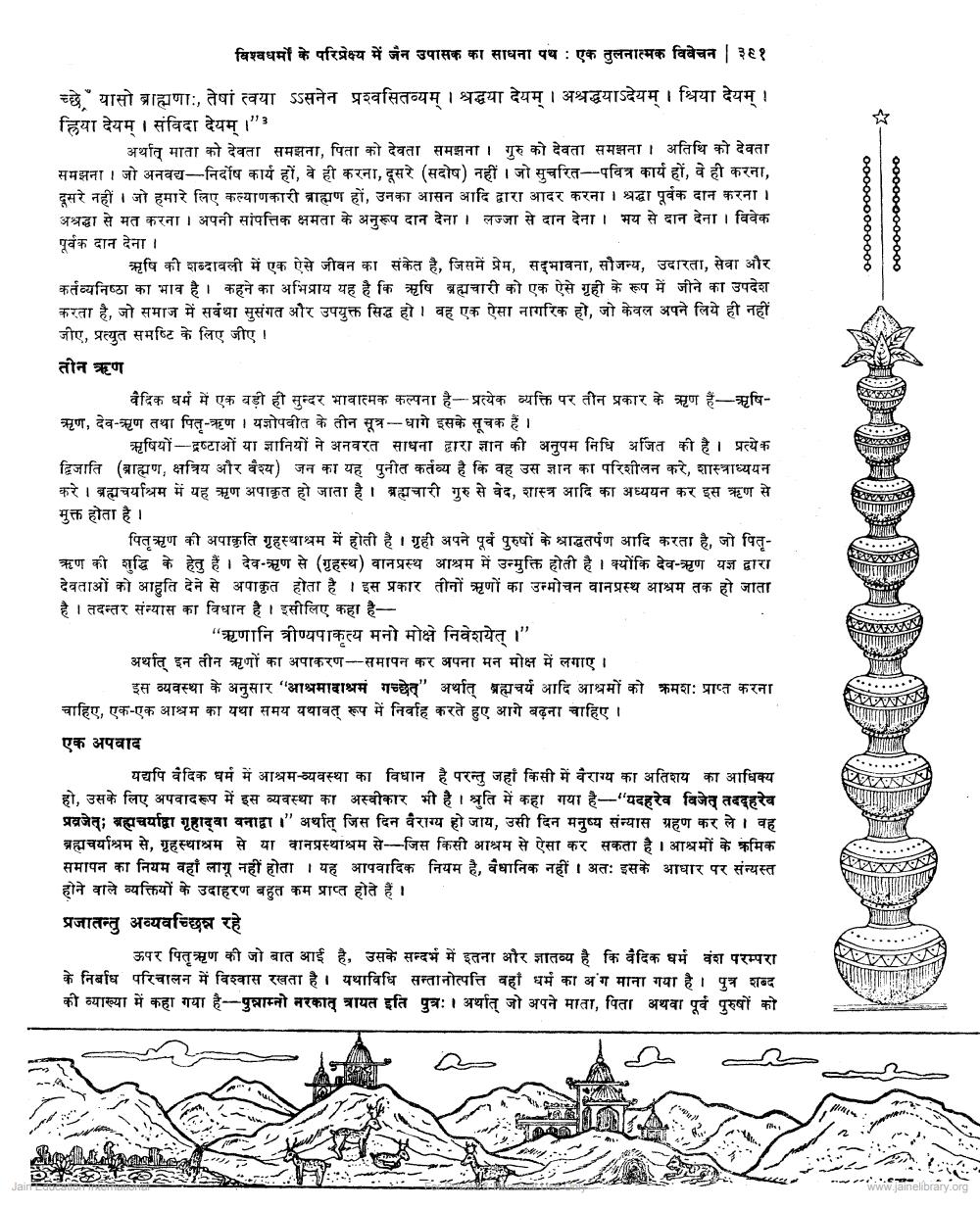________________
विश्वधर्मो के परिप्रेक्ष्य में जैन उपासक का साधना पथ एक तुलनात्मक विवेचन | ३६१
"
च्छे वासो ब्राह्मणाः तेषां त्वया ऽऽसनेन प्रश्वसितव्यम् । श्रद्धया देवम्। अथद्वयाऽदेयम् । धिया देयम् । ह्रिया देयम् । संविदा देयम् ।" 3
Jaira
अर्थात् माता को देवता समझना, पिता को देवता समझना। गुरु को देवता समझना। अतिथि को देवता समझना । जो अनवद्य - निर्दोष कार्य हों, वे ही करना, दूसरे ( सदोष ) नहीं । जो सुचरित -- पवित्र कार्य हों, वे ही करना,
दूसरे नहीं । जो हमारे लिए कल्याणकारी ब्राह्मण हों, उनका आसन आदि द्वारा आदर करना । श्रद्धा पूर्वक दान करना । अश्रद्धा से मत करना। अपनी सांपत्तिक क्षमता के अनुरूप दान देना । लज्जा से दान देना । भय से दान देना । विवेक पूर्वक दान देना ।
ऋषि की शब्दावली में एक ऐसे जीवन का संकेत है, जिसमें प्रेम, सद्भावना, सौजन्य, उदारता, सेवा और कर्तव्यनिष्ठा का भाव है। कहने का अभिप्राय यह है कि ऋषि ब्रह्मचारी को एक ऐसे गृही के रूप में जीने का उपदेश करता है, जो समाज में सर्वथा सुसंगत और उपयुक्त सिद्ध हो। वह एक ऐसा नागरिक हो, जो केवल अपने लिये ही नहीं जीए प्रत्युत समष्टि के लिए जीए ।
तीन ऋण
वैदिक धर्म में एक बड़ी ही सुन्दर भावात्मक कल्पना है- प्रत्येक व्यक्ति पर तीन प्रकार के ऋण हैं-ऋषिऋण देव ऋण तथा पितृ ऋण । यज्ञोपवीत के तीन सूत्र - धागे इसके सूचक हैं ।
ऋषियों-द्रष्टाओं या ज्ञानियों ने अनवरत साधना द्वारा ज्ञान की अनुपम निधि अर्जित की है । प्रत्येक द्विजाति ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ) जन का यह पुनीत कर्तव्य है कि वह उस ज्ञान का परिशीलन करे, शास्त्राध्ययन करे । ब्रह्मचर्याश्रम में यह ऋण अपाकृत हो जाता है । ब्रह्मचारी गुरु से वेद, शास्त्र आदि का अध्ययन कर इस ऋण से मुक्त होता है ।
पितृऋण की अपाकृति गृहस्थाश्रम में होती है । गृही अपने पूर्व पुरुषों के श्राद्धतर्पण आदि करता है, जो पितृऋण की शुद्धि के हेतु हैं । देव ऋण से (गृहस्थ ) वानप्रस्थ आश्रम में उन्मुक्ति होती है । क्योंकि देव ऋण यज्ञ द्वारा देवताओं को आहुति देने से अपाकृत होता है । इस प्रकार तीनों ऋणों का उन्मोचन वानप्रस्थ आश्रम तक हो जाता है । तदन्तर संन्यास का विधान है। इसीलिए कहा है
“ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् ।”
अर्थात् इन तीन ऋणों का अपाकरण- -समापन कर अपना मन मोक्ष में लगाए ।
इस व्यवस्था के अनुसार "आश्रमावाश्रमं गच्छेत्" अर्थात् ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों को क्रमशः प्राप्त करना चाहिए, एक-एक आश्रम का यथा समय यथावत् रूप में निर्वाह करते हुए आगे बढ़ना चाहिए ।
एक अपवाद
यद्यपि वैदिक धर्म में आश्रम व्यवस्था का विधान है परन्तु जहाँ किसी में वैराग्य का अतिशय का आधिक्य हो, उसके लिए अपवादरूप में इस व्यवस्था का अस्वीकार भी है। श्रुति में कहा गया है- " यदहरेव विजेत् तदहरेव प्रव्रजेत्; ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा ।" अर्थात् जिस दिन वैराग्य हो जाय, उसी दिन मनुष्य संन्यास ग्रहण कर ले । वह ब्रह्मचर्याश्रम से, गृहस्थाश्रम से या वानप्रस्थाश्रम से - जिस किसी आश्रम से ऐसा कर सकता है । आश्रमों के क्रमिक समापन का नियम वहाँ लागू नहीं होता । यह आपवादिक नियम है, वैधानिक नहीं । अतः इसके आधार पर संन्यस्त होने वाले व्यक्तियों के उदाहरण बहुत कम प्राप्त होते हैं ।
प्रजातन्तु अव्यवच्छिन्न रहे
ऊपर पितृऋण की जो बात आई है, उसके सन्दर्भ में इतना और ज्ञातव्य है कि वैदिक धर्म वंश परम्परा के निर्बाध परिचालन में विश्वास रखता है । यथाविधि सन्तानोत्पत्ति वहाँ धर्म का अंग माना गया है । पुत्र शब्द की व्याख्या में कहा गया है -- पुन्नाम्नो नरकात् त्रायत इति पुत्रः । अर्थात् जो अपने माता, पिता अथवा पूर्व पुरुषों को
Balas Alg
files
000000000000
pines
000000000000
40000FFCCD
www.jainelibrary.org