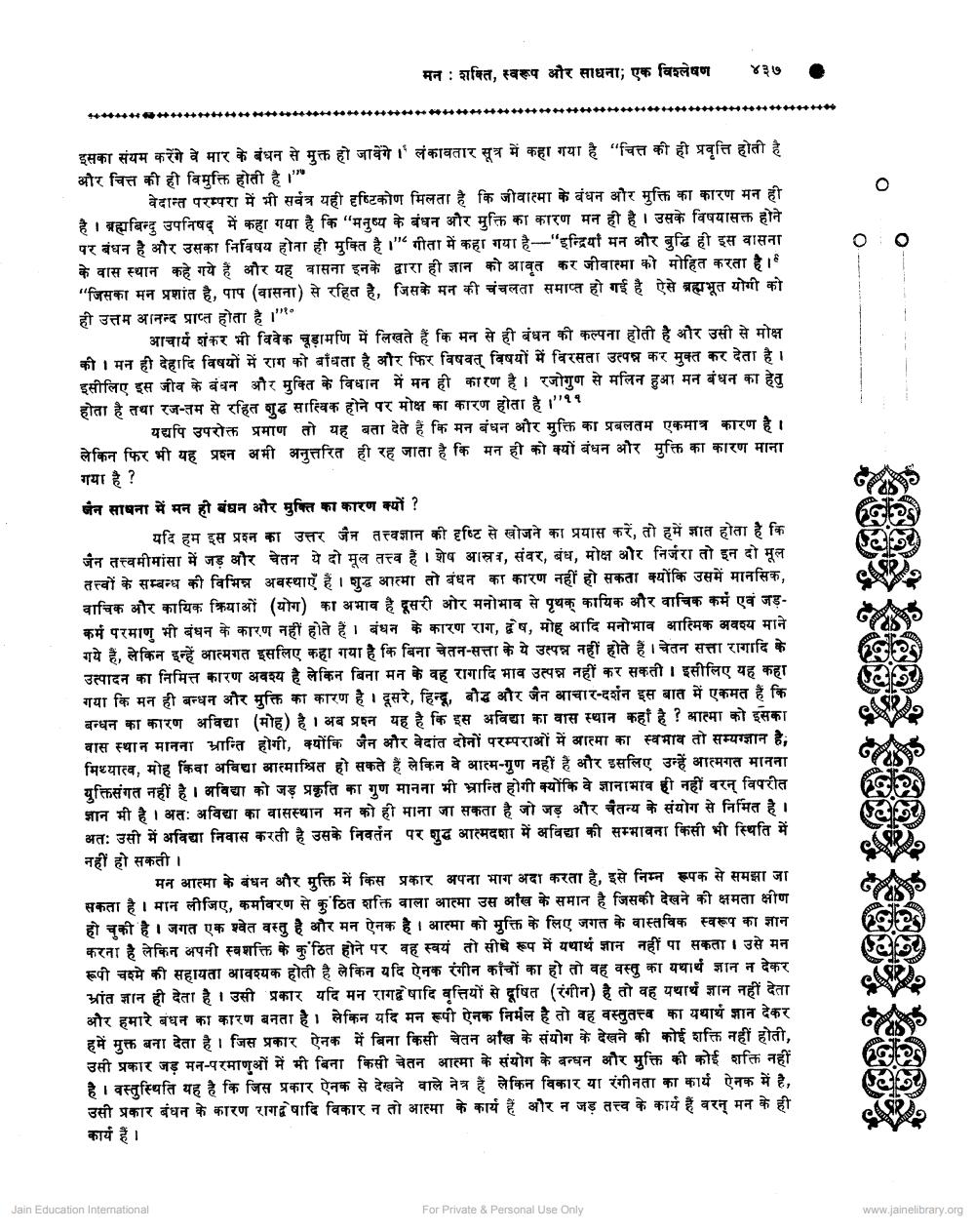________________
+++
मन शक्ति, स्वरूप और साधना; एक विश्लेषण
इसका संयम करेंगे वे मार के बंधन से मुक्त हो जायेंगे ।' लंकावतार सूत्र में कहा गया है "चित्त की ही प्रवृत्ति होती है। और चित्त की ही विमुक्ति होती है ।""
वेदान्त परम्परा में भी सर्वत्र यही दृष्टिकोण मिलता है कि जीवात्मा के बंधन और मुक्ति का कारण मन ही है । ब्रह्मबिन्दु उपनिषद् में कहा गया है कि "मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण मन ही है। उसके विषयासक्त होने पर बंधन है और उसका निर्विषय होता ही मुक्ति है ।"" गीता में कहा गया है - "इन्द्रियां मन और बुद्धि ही इस वासना के वास स्थान कहे गये हैं और यह वासना इनके द्वारा ही ज्ञान को आवृत कर जीवात्मा को मोहित करता है। " जिसका मन प्रशांत है, पाप (वासना) से रहित है, जिसके मन की चंचलता समाप्त हो गई है ऐसे ब्रह्मभूत योगी को ही उत्तम आनन्द प्राप्त होता है ।"
४३७
Jain Education International
आचार्य शंकर भी विवेक चूड़ामणि में की । मन ही देहादि विषयों में राग को बाँधता है इसीलिए इस जीव के बंधन और मुक्ति के विधान होता है तथा रज-तम से रहित शुद्ध सात्विक होने पर मोक्ष का कारण होता है । ११
यद्यपि उपरोक्त प्रमाण तो यह बता देते हैं कि मन बंधन और मुक्ति का प्रबलतम एकमात्र कारण है । लेकिन फिर भी यह प्रश्न अभी अनुत्तरित ही रह जाता है कि मन ही को क्यों बंधन और मुक्ति का कारण माना गया है?
जैन साधना में मन ही बंधन और मुक्ति का कारण क्यों ?
यदि हम इस प्रश्न का उत्तर जैन तत्त्वज्ञान की दृष्टि से खोजने का प्रयास करें, तो हमें ज्ञात होता है कि जैन तत्त्वमीमांसा में जड़ और चेतन ये दो मूल तत्त्व हैं। शेष आस्रत्र, संवर, बंध, मोक्ष और निर्जरा तो इन दो मूल तत्त्वों के सम्बन्ध की विभिन्न अवस्थाएँ हैं । शुद्ध आत्मा तो बंधन का कारण नहीं हो सकता क्योंकि उसमें मानसिक, वाचिक और कायिक क्रियाओं (योग) का अभाव है दूसरी ओर मनोभाव से पृथक् कायिक और वाचिक कर्म एवं जड़कर्म परमाणु भी बंधन के कारण नहीं होते हैं। बंधन के कारण राग, द्वेष, मोह आदि मनोभाव आत्मिक अवश्य माने गये हैं, लेकिन इन्हें आत्मगत इसलिए कहा गया है कि बिना चेतन सत्ता के ये उत्पन्न नहीं होते हैं। चेतन सत्ता रागादि के उत्पादन का निमित्त कारण अवश्य है लेकिन बिना मन के वह रागादि भाव उत्पन्न नहीं कर सकती। इसीलिए यह कहा गया कि मन ही बन्धन और मुक्ति का कारण है। दूसरे, हिन्दू, बौद्ध और जैन आचार-दर्शन इस बात में एकमत हैं कि बन्धन का कारण अविद्या (मोह ) है । अब प्रश्न यह है कि इस अविद्या का वास स्थान कहाँ है ? आत्मा को इसका वास स्थान मानना भ्रान्ति होगी, क्योंकि जैन और वेदांत दोनों परम्पराओं में आत्मा का स्वभाव तो सम्यग्ज्ञान है; मिथ्यात्व, मोह किंवा अविद्या आत्माश्रित हो सकते हैं लेकिन वे आत्म-गुण नहीं हैं और इसलिए उन्हें आत्मगत मानना युक्तिसंगत नहीं है । अविद्या को जड़ प्रकृति का गुण मानना भी भ्रान्ति होगी क्योंकि वे ज्ञानाभाव ही नहीं वरन् विपरीत ज्ञान भी है। अतः अविद्या का वासस्थान मन को ही माना जा सकता है जो जड़ और चेतन्य के संयोग से निर्मित है । अत: उसी में अविद्या निवास करती है उसके निवर्तन पर शुद्ध आत्मदशा में अविद्या की सम्भावना किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती ।
लिखते हैं कि मन से ही बंधन की कल्पना होती है और उसी से मोक्ष और फिर विषवत् विषयों में विरसता उत्पन्न कर मुक्त कर देता है। में मन ही कारण है। रजोगुण से मलिन हुआ मन बंधन का हेतु
मन आत्मा के बंधन और मुक्ति में किस प्रकार अपना भाग अदा करता है, इसे निम्न रूपक से समझा जा सकता है । मान लीजिए, कर्मावरण से कुंठित शक्ति वाला आत्मा उस आंख के समान है जिसकी देखने की क्षमता क्षीण हो चुकी है । जगत एक श्वेत वस्तु है और मन ऐनक है। आत्मा को मुक्ति के लिए जगत के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करना है लेकिन अपनी स्वशक्ति के कुंठित होने पर वह स्वयं तो सीधे रूप में यथार्थ ज्ञान नहीं पा सकता। उसे मन रूपी चश्मे की सहायता आवश्यक होती है लेकिन यदि ऐनक रंगीन काँचों का हो तो वह वस्तु का यथार्थ ज्ञान न देकर भ्रांत ज्ञान ही देता है । उसी प्रकार यदि मन रागद्वेषादि वृत्तियों से दूषित (रंगीन) है तो वह यथार्थ ज्ञान नहीं देता और हमारे बंधन का कारण बनता है। लेकिन यदि मन रूपी ऐनक निर्मल है तो वह वस्तुतत्त्व का यथार्थ ज्ञान देकर हमें मुक्त बना देता है । जिस प्रकार ऐनक में बिना किसी चेतन आँख के संयोग के देखने की कोई शक्ति नहीं होती, उसी प्रकार जड़ मन परमाणुओं में भी बिना किसी चेतन आत्मा के संयोग के बन्धन और मुक्ति की कोई शक्ति नहीं है । वस्तुस्थिति यह है कि जिस प्रकार ऐनक से देखने वाले नेत्र हैं लेकिन विकार या रंगीनता का कार्य ऐनक में है, उसी प्रकार बंधन के कारण रागद्वेषादि विकार न तो आत्मा के कार्य हैं और न जड़ तत्त्व के कार्य हैं वरन् मन के ही कार्य हैं ।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org