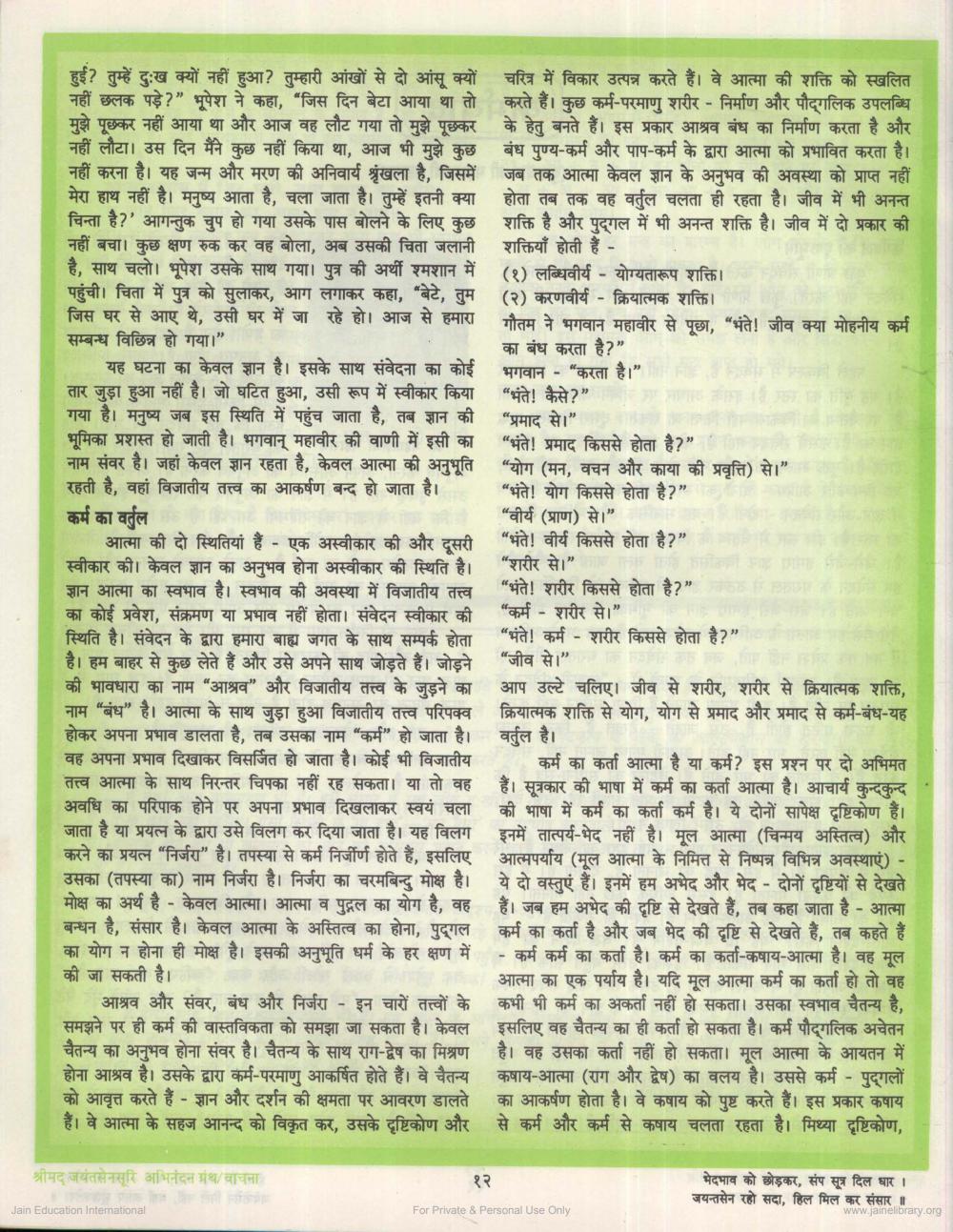________________
हा
हुई? तुम्हें दुःख क्यों नहीं हुआ? तुम्हारी आंखों से दो आंसू क्यों चरित्र में विकार उत्पन्न करते हैं। वे आत्मा की शक्ति को स्खलित नहीं छलक पड़े?" भूपेश ने कहा, "जिस दिन बेटा आया था तो करते हैं। कुछ कर्म-परमाणु शरीर - निर्माण और पौद्गलिक उपलब्धि मुझे पूछकर नहीं आया था और आज वह लौट गया तो मुझे पूछकर के हेतु बनते हैं। इस प्रकार आश्रव बंध का निर्माण करता है और नहीं लौटा। उस दिन मैंने कुछ नहीं किया था, आज भी मुझे कुछ बंध पुण्य-कर्म और पाप-कर्म के द्वारा आत्मा को प्रभावित करता है। नहीं करना है। यह जन्म और मरण की अनिवार्य श्रृंखला है, जिसमें जब तक आत्मा केवल ज्ञान के अनुभव की अवस्था को प्राप्त नहीं मेरा हाथ नहीं है। मनुष्य आता है, चला जाता है। तुम्हें इतनी क्या होता तब तक वह वर्तुल चलता ही रहता है। जीव में भी अनन्त चिन्ता है?' आगन्तुक चुप हो गया उसके पास बोलने के लिए कुछ शक्ति है और पुद्गल में भी अनन्त शक्ति है। जीव में दो प्रकार की नहीं बचा। कुछ क्षण रुक कर वह बोला, अब उसकी चिता जलानी शक्तियाँ होती हैं - है, साथ चलो। भूपेश उसके साथ गया। पुत्र की अर्थी श्मशान में (१) लब्धिवीर्य - योग्यतारूप शक्ति। पहुंची। चिता में पुत्र को सुलाकर, आग लगाकर कहा, “बेटे, तुम (२) करणवीर्य - क्रियात्मक शक्ति। जिस घर से आए थे, उसी घर में जा रहे हो। आज से हमारा
गौतम ने भगवान महावीर से पूछा, “भंते! जीव क्या मोहनीय कर्म सम्बन्ध विछिन्न हो गया।"
का बंध करता है?" यह घटना का केवल ज्ञान है। इसके साथ संवेदना का कोई भगवान - "करता है।" तार जुड़ा हुआ नहीं है। जो घटित हुआ, उसी रूप में स्वीकार किया गया है। मनुष्य जब इस स्थिति में पहुंच जाता है, तब ज्ञान की प्रमाद से।" भूमिका प्रशस्त हो जाती है। भगवान् महावीर की वाणी में इसी का “भंते! प्रमाद किससे होता है?" नाम संवर है। जहां केवल ज्ञान रहता है, केवल आत्मा की अनुभूति ___ “योग (मन, वचन और काया की प्रवृत्ति) से।" रहती है, वहां विजातीय तत्त्व का आकर्षण बन्द हो जाता है। "भंते! योग किससे होता है?" कर्म का वर्तुल
“वीर्य (प्राण) से।" आत्मा की दो स्थितियां हैं - एक अस्वीकार की और दूसरी "भंते! वीर्य किससे होता है?" का स्वीकार की। केवल ज्ञान का अनुभव होना अस्वीकार की स्थिति है। शरीर से। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव की अवस्था में विजातीय तत्त्व "भंते! शरीर किससे होता है?" का कोई प्रवेश, संक्रमण या प्रभाव नहीं होता। संवेदन स्वीकार की “कर्म - शरीर से।" स्थिति है। संवेदन के द्वारा हमारा बाह्य जगत के साथ सम्पर्क होता “भंते! कर्म - शरीर किससे होता है?" है। हम बाहर से कुछ लेते हैं और उसे अपने साथ जोड़ते हैं। जोडने “जीव से।" की भावधारा का नाम “आश्रव” और विजातीय तत्त्व के जुड़ने का आप उल्टे चलिए। जीव से शरीर, शरीर से क्रियात्मक शक्ति, नाम “बंध" है। आत्मा के साथ जुड़ा हुआ विजातीय तत्त्व परिपक्व क्रियात्मक शक्ति से योग, योग से प्रमाद और प्रमाद से कर्म-बंध-यह होकर अपना प्रभाव डालता है, तब उसका नाम “कर्म" हो जाता है। वर्तुल है। वह अपना प्रभाव दिखाकर विसर्जित हो जाता है। कोई भी विजातीय कर्म का कर्ता आत्मा है या कर्म? इस प्रश्न पर दो अभिमत तत्त्व आत्मा के साथ निरन्तर चिपका नहीं रह सकता। या तो वह हैं। सूत्रकार की भाषा में कर्म का कर्ता आत्मा है। आचार्य कुन्दकुन्द अवधि का परिपाक होने पर अपना प्रभाव दिखलाकर स्वयं चला की भाषा में कर्म का कर्ता कर्म है। ये दोनों सापेक्ष दृष्टिकोण हैं। जाता है या प्रयल के द्वारा उसे विलग कर दिया जाता है। यह विलग इनमें तात्पर्य-भेद नहीं है। मूल आत्मा (चिन्मय अस्तित्व) और करने का प्रयत्न “निर्जरा" है। तपस्या से कर्म निर्जीर्ण होते हैं, इसलिए आत्मपर्याय (मूल आत्मा के निमित्त से निष्पन्न विभिन्न अवस्थाएं)उसका (तपस्या का) नाम निर्जरा है। निर्जरा का चरमबिन्दु मोक्ष है। ये दो वस्तुएं हैं। इनमें हम अभेद और भेद - दोनों दृष्टियों से देखते मोक्ष का अर्थ है - केवल आत्मा। आत्मा व पुद्गल का योग है, वह हैं। जब हम अभेद की दृष्टि से देखते हैं, तब कहा जाता है - आत्मा बन्धन है, संसार है। केवल आत्मा के अस्तित्व का होना, पुद्गल कर्म का कर्ता है और जब भेद की दृष्टि से देखते हैं, तब कहते हैं का योग न होना ही मोक्ष है। इसकी अनुभूति धर्म के हर क्षण में - कर्म कर्म का कर्ता है। कर्म का कर्ता-कषाय-आत्मा है। वह मूल की जा सकती है।
आत्मा का एक पर्याय है। यदि मूल आत्मा कर्म का कर्ता हो तो वह आश्रव और संवर, बंध और निर्जरा - इन चारों तत्त्वों के कभी भी कर्म का अकर्ता नहीं हो सकता। उसका स्वभाव चैतन्य है, समझने पर ही कर्म की वास्तविकता को समझा जा सकता है। केवल इसलिए वह चैतन्य का ही कर्ता हो सकता है। कर्म पौद्गलिक अचेतन चैतन्य का अनुभव होना संवर है। चैतन्य के साथ राग-द्वेष का मिश्रण है। वह उसका कर्ता नहीं हो सकता। मूल आत्मा के आयतन में होना आश्रव है। उसके द्वारा कर्म-परमाणु आकर्षित होते हैं। वे चैतन्य कषाय-आत्मा (राग और द्वेष) का वलय है। उससे कर्म - पुद्गलों को आवृत्त करते हैं - ज्ञान और दर्शन की क्षमता पर आवरण डालते का आकर्षण होता है। वे कषाय को पुष्ट करते हैं। इस प्रकार कषाय हैं। वे आत्मा के सहज आनन्द को विकृत कर, उसके दृष्टिकोण और से कर्म और कर्म से कषाय चलता रहता है। मिथ्या दृष्टिकोण,
श्रीमद् जयंतसेनसूरि अभिनंदन मंथ/वाचना
भेदभाव को छोड़कर, संप सूत्र दिल धार । जयन्तसेन रहो सदा, हिल मिल कर संसार ।
www.jainelibrary.org
Jain Education Intemational
For Private & Personal Use Only