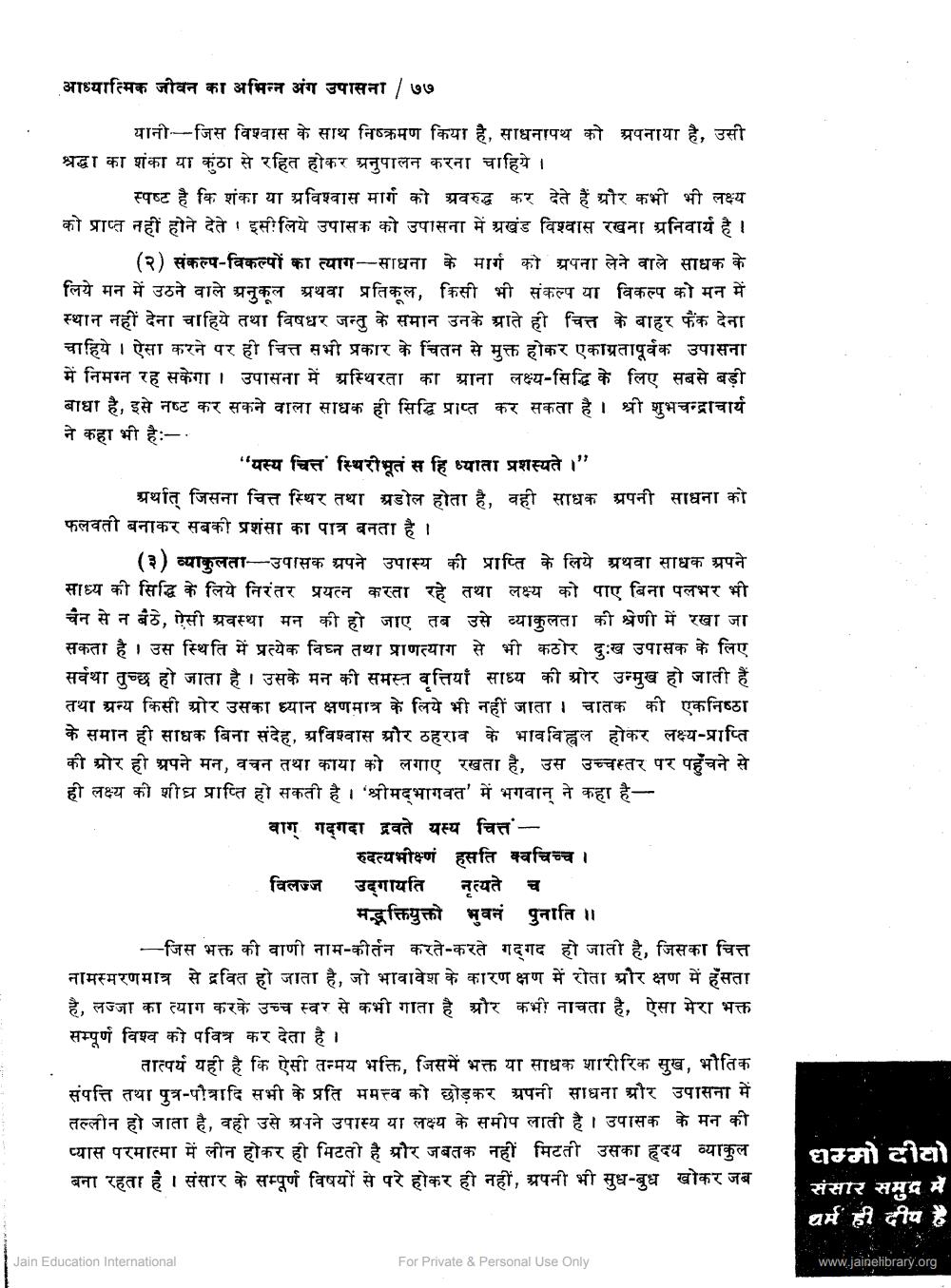________________
आध्यात्मिक जीवन का अभिन्न अंग उपासना / ७७
यानी-जिस विश्वास के साथ निष्क्रमण किया है, साधनापथ को अपनाया है, उसी श्रद्धा का शंका या कुंठा से रहित होकर अनुपालन करना चाहिये।
स्पष्ट है कि शंका या अविश्वास मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं और कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं होने देते । इसीलिये उपासक को उपासना में अखंड विश्वास रखना अनिवार्य है।
(२) संकल्प-विकल्पों का त्याग-साधना के मार्ग को अपना लेने वाले साधक के लिये मन में उठने वाले अनुकल अथवा प्रतिकल, किसी भी संकल्प या विकल्प को मन में स्थान नहीं देना चाहिये तथा विषधर जन्तु के समान उनके पाते ही चित्त के बाहर फेंक देना चाहिये । ऐसा करने पर ही चित्त सभी प्रकार के चिंतन से मुक्त होकर एकाग्रतापूर्वक उपासना में निमग्न रह सकेगा। उपासना में अस्थिरता का आना लक्ष्य-सिद्धि के लिए सबसे बड़ी बाधा है, इसे नष्ट कर सकने वाला साधक ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्री शुभचन्द्राचार्य ने कहा भी है:-.
“यस्य चित्त स्थिरीभूतं स हि ध्याता प्रशस्यते ।" अर्थात् जिसना चित्त स्थिर तथा अडोल होता है, वही साधक अपनी साधना को फलवती बनाकर सबकी प्रशंसा का पात्र बनता है ।
(३) व्याकुलता-उपासक अपने उपास्य की प्राप्ति के लिये अथवा साधक अपने साध्य की सिद्धि के लिये निरंतर प्रयत्न करता रहे तथा लक्ष्य को पाए बिना पलभर भी चैन से न बैठे, ऐसी अवस्था मन की हो जाए तब उसे व्याकुलता की श्रेणी में रखा जा सकता है । उस स्थिति में प्रत्येक विघ्न तथा प्राणत्याग से भी कठोर दुःख उपासक के लिए सर्वथा तुच्छ हो जाता है। उसके मन की समस्त वृत्तियाँ साध्य की ओर उन्मुख हो जाती हैं तथा अन्य किसी ओर उसका ध्यान क्षणमात्र के लिये भी नहीं जाता। चातक की एकनिष्ठा के समान ही साधक बिना संदेह, अविश्वास और ठहराव के भावविह्वल होकर लक्ष्य-प्राप्ति की ओर ही अपने मन, वचन तथा काया को लगाए रखता है, उस उच्चस्तर पर पहुँचने से ही लक्ष्य की शीघ्र प्राप्ति हो सकती है। 'श्रीमद्भागवत' में भगवान ने कहा है
वाग् गद्गदा द्रवते यस्य चित्त
रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च । विलज्ज उद्गायति नृत्यते च
मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति । —जिस भक्त की वाणी नाम-कीर्तन करते-करते गद्गद हो जाती है, जिसका चित्त नामस्मरणमात्र से द्रवित हो जाता है, जो भावावेश के कारण क्षण में रोता और क्षण में हँसता है, लज्जा का त्याग करके उच्च स्वर से कभी गाता है और कभी नाचता है, ऐसा मेरा भक्त सम्पूर्ण विश्व को पवित्र कर देता है।
तात्पर्य यही है कि ऐसी तन्मय भक्ति, जिसमें भक्त या साधक शारीरिक सुख, भौतिक संपत्ति तथा पुत्र-पौत्रादि सभी के प्रति ममत्त्व को छोड़कर अपनी साधना और उपासना में तल्लीन हो जाता है, वही उसे अपने उपास्य या लक्ष्य के समीप लाती है। उपासक के मन की प्यास परमात्मा में लीन होकर ही मिटती है और जबतक नहीं मिटती उसका हृदय व्याकुल बना रहता है । संसार के सम्पूर्ण विषयों से परे होकर ही नहीं, अपनी भी सुध-बुध खोकर जब
धम्मो दीवो संसार समुद्र में धर्म ही दीय है www.jainielibrary.org
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
_