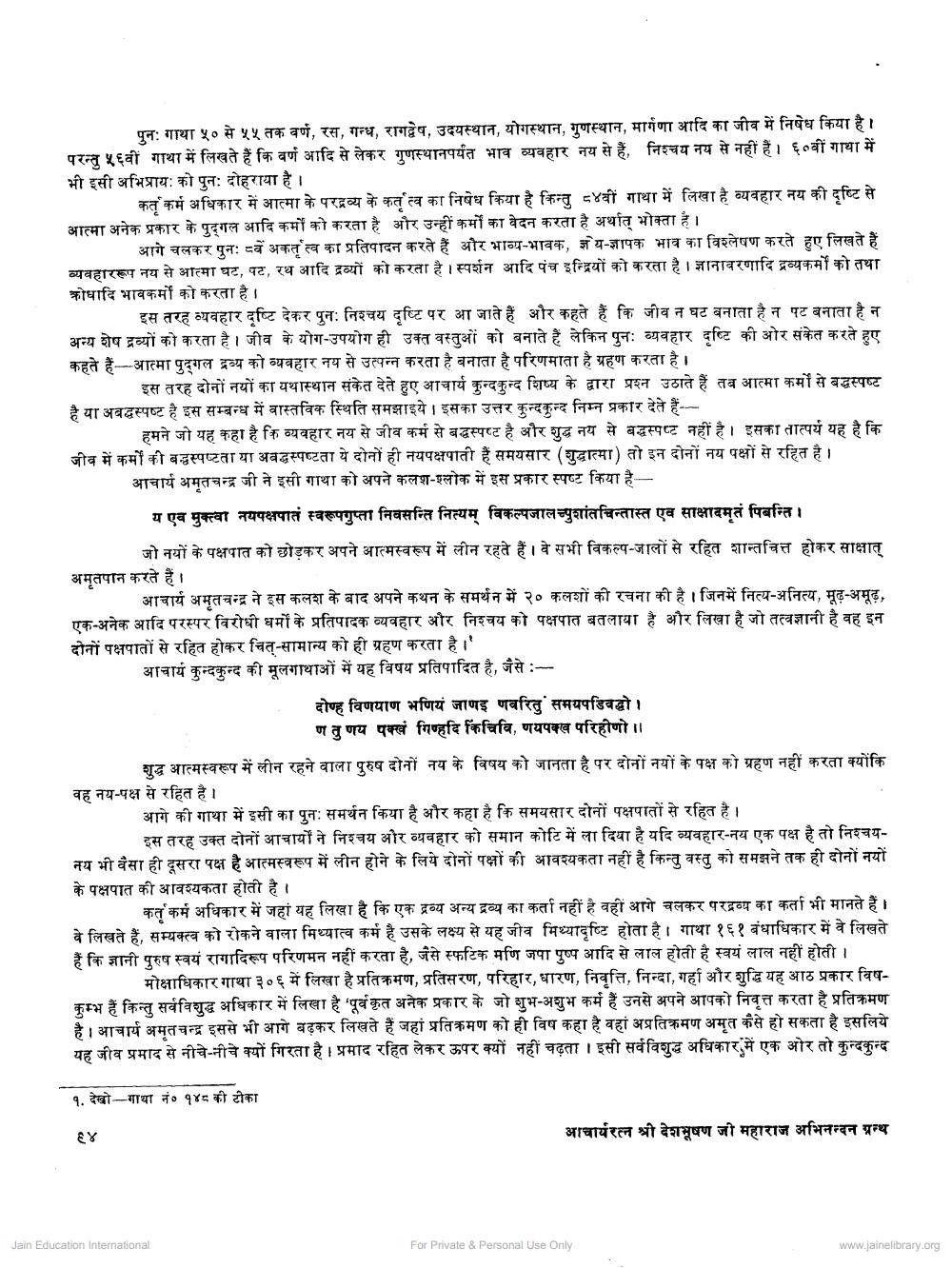________________
पुनः गाथा ५० से ५५ तक वर्ण, रस, गन्ध, रागद्वेष, उदयस्थान, योगस्थान, गुणस्थान, मार्गणा आदि का जीव में निषेध किया है। परन्तु वी माया में लिखते हैं कि वर्ण आदि से लेकर गुणस्थानपर्यंत भाव व्यवहार नय से हैं. निश्चय नय से नहीं है। ६०वीं गाया में ५६वीं भी इसी अभिप्रायः को पुनः दोहराया है।
कर्तृकर्म अधिकार में आत्मा के परद्रव्य के कर्तृत्व का निषेध किया है किन्तु ८४वीं गाथा में लिखा है व्यवहार नय की दृष्टि से आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल आदि कर्मों को करता है और उन्हीं कर्मों का वेदन करता है अर्थात् भोक्ता है।
आगे चलकर पुनः वें अकर्तृत्व का प्रतिपादन करते हैं और भाव्य-भावक, ज्ञेय-ज्ञापक भाव का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं व्यवहाररूप नय से आत्मा घट, पट, रथ आदि द्रव्यों को करता है। स्पर्शन आदि पंच इन्द्रियों को करता है। ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्मों को तथा क्रोधादि भावकर्मों को करता है ।
इस तरह व्यवहार दृष्टि देकर पुनः निश्चय दृष्टि पर आ जाते हैं और कहते हैं कि जीव न घट बनाता है न पट बनाता है न अन्य शेष द्रव्यों को करता है। जीव के योग-उपयोग ही उक्त वस्तुओं को बनाते हैं लेकिन पुनः व्यवहार दृष्टि की ओर संकेत करते हुए कहते हैं- आत्मा पुद्गल द्रव्य को व्यवहार नय से उत्पन्न करता है बनाता है परिणमाता है ग्रहण करता है।
इस तरह दोनों नयों का यथास्थान संकेत देते हुए आचार्य कुन्दकुन्द शिष्य के द्वारा प्रश्न उठाते हैं तब आत्मा कर्मों से बद्धस्पष्ट है या अबद्धस्पष्ट है इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति समझाइये। इसका उत्तर कुन्दकुन्द निम्न प्रकार देते हैं-
हमने जो यह कहा है कि व्यवहार नय से जीव कर्म से बद्धस्पष्ट है और शुद्ध नय से बद्धस्पष्ट नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि जीव में कर्मों की बद्धस्पष्टता या अवद्धस्पष्टता ये दोनों ही नयपक्षपाती हैं समयसार (शुद्धात्मा) तो इन दोनों नय पक्षों से रहित है। आचार्य अमृतचन्द्र जी ने इसी गाथा को अपने कलश-श्लोक में इस प्रकार स्पष्ट किया है
य एवमुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यम् विकल्पजात न्युशांतचिन्तास्त एवं साक्षादमृतं पिबन्ति । जो नयों के पक्षपात को छोड़कर अपने आत्मस्वरूप में लीन रहते हैं। वे सभी विकल्प-जालों से रहित शान्तचित्त होकर साक्षात् अमृतपान करते हैं ।
आचार्य अमृतचन्द्र ने इस कलश के बाद अपने कथन के समर्थन में २० कलशों की रचना की है। जिनमें नित्य अनित्य, मूढ़-अमूढ़, एक-अनेक आदि परस्पर विरोधी धर्मों के प्रतिपादक व्यवहार और निश्चय को पक्षपात बतलाया है और लिखा है जो तत्वज्ञानी है वह इन दोनों पक्षपातों से रहित होकर नि-सामान्य को ही ग्रहण करता है।'
आचार्य कुन्दकुन्द की मूलगाथाओं में यह विषय प्रतिपादित है, जैसे
दोह विणयाण भणियं जाणइ णवरितु समयपडिवद्धो । ण तु णय पक्वं गिण्हदि किचिवि, णयपक्ख परिहीणो ।।
शुद्ध आत्मस्वरूप में लीन रहने वाला पुरुष दोनों नय के विषय को जानता है पर दोनों नयों के पक्ष को ग्रहण नहीं करता क्योंकि
वह नय-पक्ष से रहित है।
आगे की गाथा में इसी का पुनः समर्थन किया है और कहा है कि समयसार दोनों पक्षपातों से रहित है।
इस तरह उक्त दोनों आचार्यों ने निश्चय और व्यवहार को समान कोटि में ला दिया है यदि व्यवहार नय एक पक्ष है तो निश्चयनय भी वैसा ही दूसरा पक्ष है आत्मस्वरूप में लीन होने के लिये दोनों पक्षों की आवश्यकता नहीं है किन्तु वस्तु को समझने तक ही दोनों नयों के पक्षपात की आवश्यकता होती है ।
कर्म अधिकार में जहां यह लिखा है कि एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं है वहीं आगे चलकर परद्रव्य का कर्ता भी मानते हैं । वे लिखते हैं, सम्यक्त्व को रोकने वाला मिथ्यात्व कर्म है उसके लक्ष्य से यह जीव मिथ्यादृष्टि होता है। गाथा १६१ बंधाधिकार में वे लिखते हैं कि ज्ञानी पुरुष स्वयं रागादिरूप परिणमन नहीं करता है, जैसे स्फटिक मणि जपा पुष्प आदि से लाल होती है स्वयं लाल नहीं होती । मोक्षाधिकार गाथा ३०६ में लिखा है प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारण, निवृत्ति, निन्दा, गह और बुद्धि यह आठ प्रकार विषकुम्भ हैं किन्तु सर्वविशुद्ध अधिकार में लिखा है 'पूर्वकृत अनेक प्रकार के जो शुभ-अशुभ कर्म हैं उनसे अपने आपको निवृत्त करता है प्रतिक्रमण है। आचार्य अमृतचन्द्र इससे भी आगे बड़कर लिखते हैं जहां प्रतिक्रमण को ही विष कहा है वहां अतिक्रमण अमृत कैसे हो सकता है इसलिये यह जीव प्रमाद से नीचे-नीचे क्यों गिरता है। प्रमाद रहित लेकर ऊपर क्यों नहीं चढ़ता। इसी सर्वविशुद्ध अधिकार में एक ओर तो कुकुन्द
१. देखो - गाथा नं० १४८ की टीका
૨૪
Jain Education International
आचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज अभिनन्दन ग्रन्थ
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org