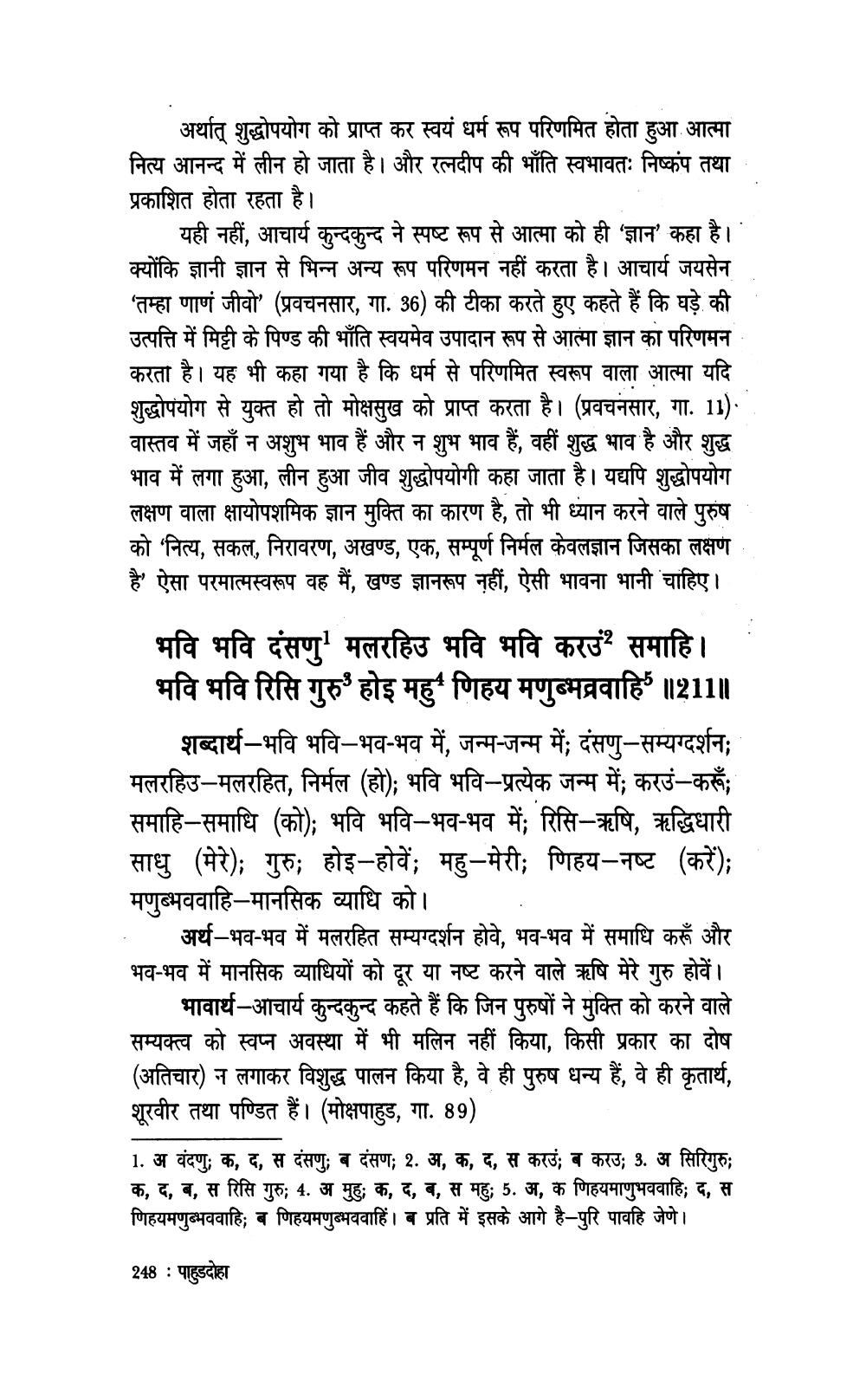________________
अर्थात् शुद्धोपयोग को प्राप्त कर स्वयं धर्म रूप परिणमित होता हुआ आत्मा नित्य आनन्द में लीन हो जाता है। और रत्नदीप की भाँति स्वभावतः निष्कंप तथा प्रकाशित होता रहता है।
यही नहीं, आचार्य कुन्दकुन्द ने स्पष्ट रूप से आत्मा को ही 'ज्ञान' कहा है। क्योंकि ज्ञानी ज्ञान से भिन्न अन्य रूप परिणमन नहीं करता है। आचार्य जयसेन 'तम्हा णाणं जीवो' (प्रवचनसार, गा. 36) की टीका करते हुए कहते हैं कि घड़े की उत्पत्ति में मिट्टी के पिण्ड की भाँति स्वयमेव उपादान रूप से आत्मा ज्ञान का परिणमन करता है। यह भी कहा गया है कि धर्म से परिणमित स्वरूप वाला आत्मा यदि शुद्धोपयोग से युक्त हो तो मोक्षसुख को प्राप्त करता है। (प्रवचनसार, गा. 11). वास्तव में जहाँ न अशुभ भाव हैं और न शुभ भाव हैं, वहीं शुद्ध भाव है और शुद्ध भाव में लगा हुआ, लीन हुआ जीव शुद्धोपयोगी कहा जाता है। यद्यपि शुद्धोपयोग लक्षण वाला क्षायोपशमिक ज्ञान मुक्ति का कारण है, तो भी ध्यान करने वाले पुरुष को 'नित्य, सकल, निरावरण, अखण्ड, एक, सम्पूर्ण निर्मल केवलज्ञान जिसका लक्षण है' ऐसा परमात्मस्वरूप वह मैं, खण्ड ज्ञानरूप नहीं, ऐसी भावना भानी चाहिए।
भवि भवि दंसणु' मलरहिउ भवि भवि करउं समाहि। भवि भवि रिसि गुरु होइ महु णिहय मणुब्भववाहि ॥211॥
शब्दार्थ-भवि भवि-भव-भव में, जन्म-जन्म में; दंसणु-सम्यग्दर्शन; मलरहिउ-मलरहित, निर्मल (हो); भवि भवि-प्रत्येक जन्म में; करउं–करूँ; समाहि-समाधि (को); भवि भवि-भव-भव में; रिसि-ऋषि, ऋद्धिधारी साधु (मेरे); गुरु; होइ-होवें; महु-मेरी; णिहय-नष्ट (करें); मणुब्भववाहि-मानसिक व्याधि को।
अर्थ-भव-भव में मलरहित सम्यग्दर्शन होवे, भव-भव में समाधि करूँ और भव-भव में मानसिक व्याधियों को दूर या नष्ट करने वाले ऋषि मेरे गुरु होवें।
भावार्थ-आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं कि जिन पुरुषों ने मुक्ति को करने वाले सम्यक्त्व को स्वप्न अवस्था में भी मलिन नहीं किया, किसी प्रकार का दोष (अतिचार) न लगाकर विशुद्ध पालन किया है, वे ही पुरुष धन्य हैं, वे ही कृतार्थ, शूरवीर तथा पण्डित हैं। (मोक्षपाहुड, गा. 89)
1. अ वंदणु; क, द, स दंसणु; ब दंसण; 2. अ, क, द, स करउं व करउ; 3. अ सिरिगुरुः क, द, ब, स रिसि गुरु; 4. अ मुहुः क, द, ब, स महु; 5. अ, क णिहयमाणुभववाहि; द, स णिहयमणुब्भववाहि; ब णिहयमणुब्भववाहिं। ब प्रति में इसके आगे है-पुरि पावहि जेणे।
248 : पाहुडदोहा