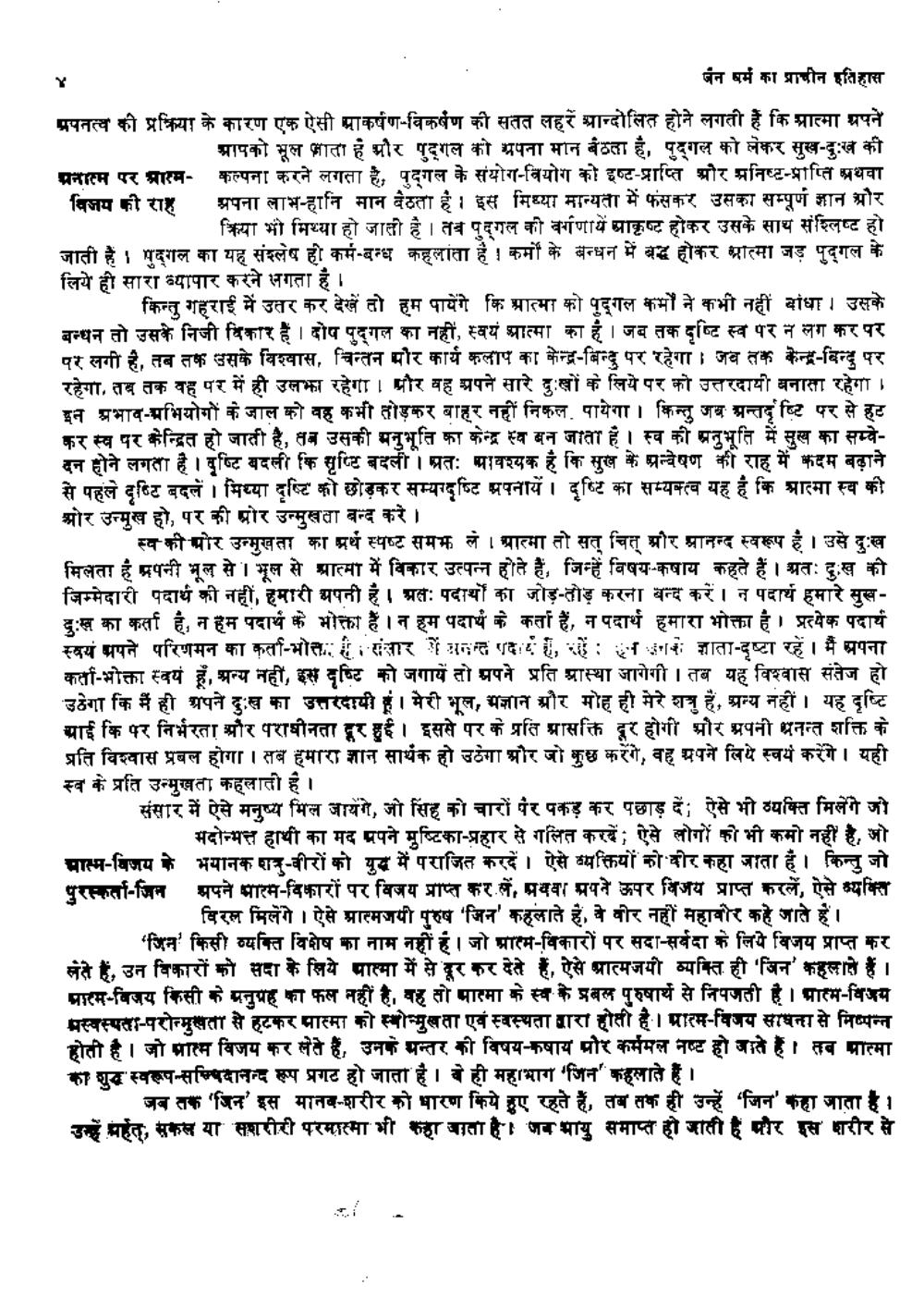________________
जैन धर्म का प्राचीन इतिहास
आपको
प्रपतत्व की प्रक्रिया के कारण एक ऐसी आकर्षण - विकर्षण की सतत लहरें आन्दोलित होने लगती है कि श्रात्मा थपने भूल जाता है और पुद्गल को अपना मान बैठता है, पुद्गल को लेकर सुख-दुःख की अनात्म पर प्रारम- कल्पना करने लगता है, पुद्गल के संयोग-वियोग को इष्ट-प्राप्ति और श्रनिष्ट-प्राप्ति अथवा विजय की राह अपना लाभ-हानि मान बैठता है । इस मिथ्या मान्यता में फंसकर उसका सम्पूर्ण ज्ञान और क्रिया भी मिथ्या हो जाती है। तब पुद्गल की वर्गणायें आकृष्ट होकर उसके साथ संश्लिष्ट हो जाती हैं । मुद्गल का यह संश्लेष ही कर्म-बन्ध कहलाता है । कर्मों के बन्धन में बद्ध होकर ग्रात्मा जड़ पुद्गल लिये ही सारा व्यापार करने लगता है।
के
किन्तु गहराई में उतर कर देखें तो हम पायेंगे कि श्रात्मा को पुद्गल कर्मों ने कभी नहीं बांधा। उसके बन्धन तो उसके निजी विकार । दोष पुद्गल का नहीं, स्वयं आत्मा का है। जब तक दृष्टि स्व पर न लग कर पर पर लगी है, तब तक उसके विश्वास, चिन्तन मौर कार्य कलाप का केन्द्र बिन्दु पर रहेगा। जब तक केन्द्र बिन्दु पर रहेगा, तब तक वह पर में ही उलझा रहेगा । और वह अपने सारे दुःखों के लिये पर को उत्तरदायी बनाता रहेगा । इन अभाव अभियोगों के जाल को वह कभी तोड़कर बाहर नहीं निकल पायेगा । किन्तु जब अन्तर्दृष्टि पर से हट कर स्व पर केन्द्रित हो जाती है, तब उसकी मनुभूति का केन्द्र स्व बन जाता है। स्व की अनुभूति में सुख का सम्वेदन होने लगता है । वृष्टि बदली कि सृष्टि बदली । प्रतः मावश्यक है कि सुख के प्रन्वेषण की राह में कदम बढ़ाने से पहले दृष्टि बदलें । मिथ्या दृष्टि को छोड़कर सम्यग्दृष्टि अपनायें । दृष्टि का सम्यक्त्व यह है कि आत्मा स्व की ओर उन्मुख हो, पर की ओर उन्मुखता बन्द करे ।
Y
पोर उन्मुखता का अर्थ स्पष्ट समझ ले । श्रात्मा तो सत् चित् और श्रानन्द स्वरूप है । उसे दुःख मिलता है अपनी भूल से । भूल से श्रात्मा में विकार उत्पन्न होते हैं, जिन्हें विषय कषाय कहते हैं । अतः दुःख की जिम्मेदारी पदार्थ की नहीं, हमारी अपनी है | अतः पदार्थों का जोड़-तोड़ करना बन्द करें। न पदार्थ हमारे सुखदुःख का कर्ता है, न हम पदार्थ के भोक्ता हैं। न हम पदार्थ के कर्ता हैं, न पदार्थ हमारा भोक्ता है। प्रत्येक पदार्थ स्वयं अपने परिणमन का कर्ता-भोक्ता है। संसार में पदार्थ है, हें उनके ज्ञाता दृष्टा रहें। मैं अपना कर्ता भोक्ता स्वयं हूँ, अन्य नहीं, इस दृष्टि को जगायें तो अपने प्रति श्रास्था जागेगी । तब यह विश्वास संतेज हो उठेगा कि मैं ही अपने दुःख का उत्तरदायी हूं । मेरी भूल, अज्ञान और मोह ही मेरे शत्रु हैं, अन्य नहीं । यह दृष्टि आई कि पर निर्भरता और पराधीनता दूर हुई। इससे पर के प्रति प्रासक्ति दूर होगी और अपनी धनन्त शक्ति के प्रति विश्वास प्रबल होगा । सब हमारा ज्ञान सार्थक हो उठेगा और जो कुछ करेंगे, वह अपने लिये स्वयं करेंगे । यही स्व के प्रति उन्मुखता कहलाती है ।
संसार में ऐसे मनुष्य मिल जायेंगे, जो सिंह को चारों पैर पकड़ कर पछाड़ दें ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे जो मदोन्मत्त हाथी का मद अपने मुष्टिका प्रहार से गलित करदें; ऐसे लोगों को भी कमी नहीं है, जो भयानक शत्रु वीरों को युद्ध में पराजित करदें। ऐसे व्यक्तियों को वीर कहा जाता है। किन्तु जो अपने भात्म-विकारों पर विजय प्राप्त कर लें, प्रववा अपने ऊपर विजय प्राप्त करलें, ऐसे व्यक्ति विरल मिलेंगे । ऐसे प्रात्मजयी पुरुष 'जिन' कहलाते हैं, वे वीर नहीं महावीर कहे जाते हैं । 'जिन' किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं हैं। जो श्रात्म-विकारों पर सदा-सर्वदा के लिये विजय प्राप्त कर लेते हैं, उन विकारों को सदा के लिये मात्मा में से दूर कर देते हैं, ऐसे श्रात्मजयी व्यक्ति ही 'जिन' कहलाते हैं । aren- विजय किसी के अनुग्रह का फल नहीं है, वह तो मारमा के स्व के प्रबल पुरुषार्थं से निपजती है। म्रात्म-विजय स्वस्थता - परोन्मुखता से हटकर मात्मा को स्वोन्मुखता एवं स्वस्थता द्वारा होती है। म्रात्म-विजय साधना से निष्पन्न होती है। जो प्रात्म विजय कर लेते हैं, उनके अन्तर की विषय-कषाय प्रोर कर्ममल नष्ट हो जाते हैं। तब मात्मा का शुद्ध स्वरूप सम्पदानन्द रूप प्रगट हो जाता है। वे ही महाभाग 'जिन' कहलाते हैं ।
जब तक 'जिन' इस मानव शरीर को धारण किये हुए रहते हैं, उन्हें महेत्, सकल या सशरीरी परमात्मा भी कहा जाता है। जब भायु
आत्म-विजय के
पुरस्कर्ता - जिन
तब तक ही उन्हें 'जिन' कहा जाता है। समाप्त हो जाती हैं मौर इस शरीर से