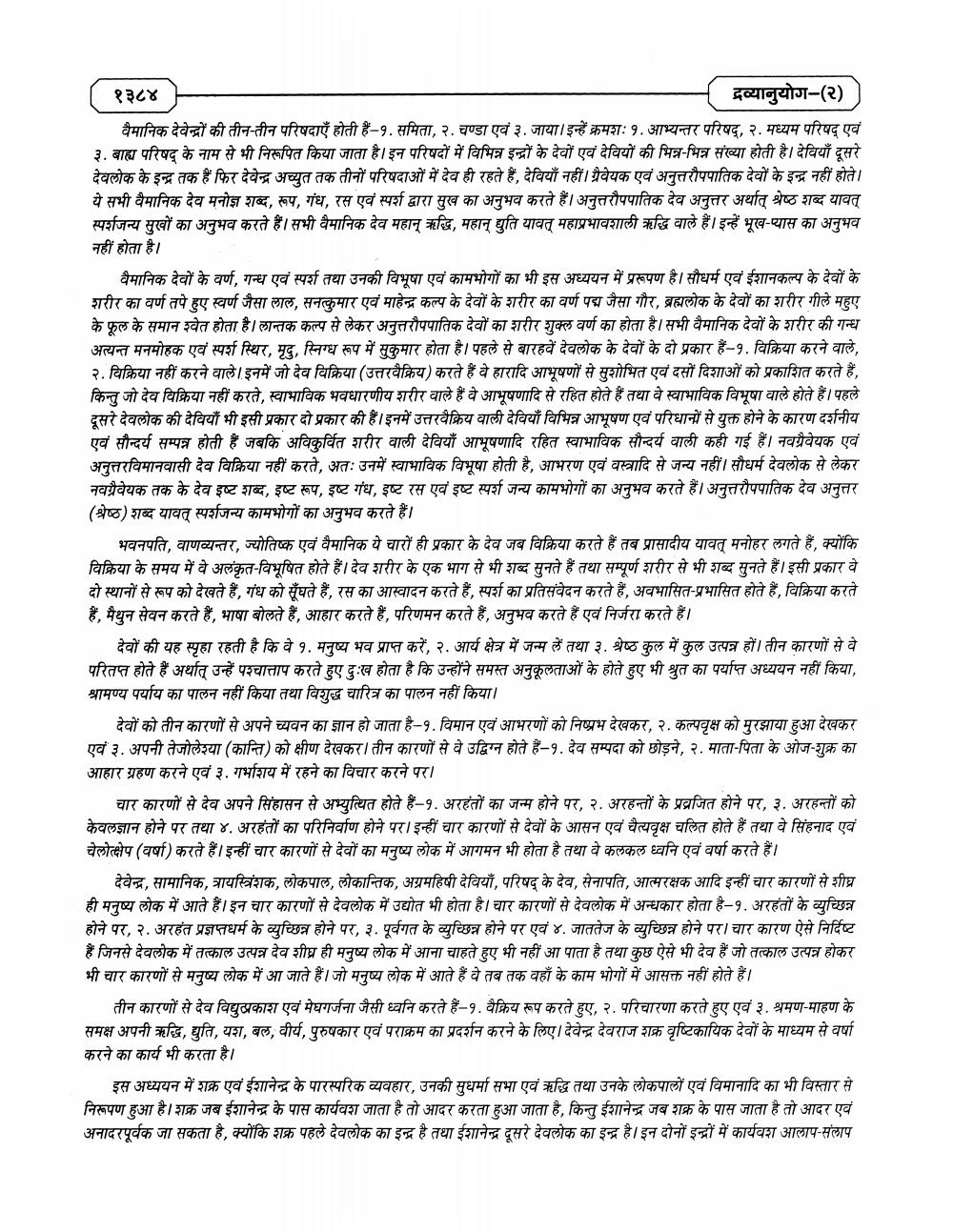________________
१३८४
द्रव्यानुयोग-(२) वैमानिक देवेन्द्रों की तीन-तीन परिषदाएँ होती हैं-१. समिता, २. चण्डा एवं ३. जाया। इन्हें क्रमशः १. आभ्यन्तर परिषद्, २. मध्यम परिषद् एवं ३. बाह्य परिषद् के नाम से भी निरूपित किया जाता है। इन परिषदों में विभिन्न इन्द्रों के देवों एवं देवियों की भिन्न-भिन्न संख्या होती है। देवियाँ दूसरे देवलोक के इन्द्र तक हैं फिर देवेन्द्र अच्युत तक तीनों परिषदाओं में देव ही रहते हैं, देवियाँ नहीं। ग्रैवेयक एवं अनुत्तरौपपातिक देवों के इन्द्र नहीं होते। ये सभी वैमानिक देव मनोज्ञ शब्द, रूप, गंध, रस एवं स्पर्श द्वारा सुख का अनुभव करते हैं। अनुत्तरौपपातिक देव अनुत्तर अर्थात् श्रेष्ठ शब्द यावत् स्पर्शजन्य सुखों का अनुभव करते हैं। सभी वैमानिक देव महान् ऋद्धि, महान् द्युति यावत् महाप्रभावशाली ऋद्धि वाले हैं। इन्हें भूख-प्यास का अनुभव नहीं होता है।
वैमानिक देवों के वर्ण, गन्ध एवं स्पर्श तथा उनकी विभूषा एवं कामभोगों का भी इस अध्ययन में प्ररूपण है। सौधर्म एवं ईशानकल्प के देवों के शरीर का वर्ण तपे हुए स्वर्ण जैसा लाल, सनत्कुमार एवं माहेन्द्र कल्प के देवों के शरीर का वर्ण पद्म जैसा गौर, ब्रह्मलोक के देवों का शरीर गीले महुए के फूल के समान श्वेत होता है। लान्तक कल्प से लेकर अनुत्तरौपपातिक देवों का शरीर शुक्ल वर्ण का होता है। सभी वैमानिक देवों के शरीर की गन्ध अत्यन्त मनमोहक एवं स्पर्श स्थिर, मृदु, स्निग्ध रूप में सुकुमार होता है। पहले से बारहवें देवलोक के देवों के दो प्रकार हैं-१. विक्रिया करने वाले, २. विक्रिया नहीं करने वाले। इनमें जो देव विक्रिया (उत्तरवैक्रिय) करते हैं वे हारादि आभूषणों से सुशोभित एवं दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हैं, किन्तु जो देव विक्रिया नहीं करते, स्वाभाविक भवधारणीय शरीर वाले हैं वे आभूषणादि से रहित होते हैं तथा वे स्वाभाविक विभूषा वाले होते हैं। पहले दूसरे देवलोक की देवियाँ भी इसी प्रकार दो प्रकार की हैं। इनमें उत्तरवैक्रिय वाली देवियाँ विभिन्न आभूषण एवं परिधानों से युक्त होने के कारण दर्शनीय एवं सौन्दर्य सम्पन्न होती हैं जबकि अविकुर्वित शरीर वाली देवियाँ आभूषणादि रहित स्वाभाविक सौन्दर्य वाली कही गई हैं। नवग्रैवेयक एवं अनुत्तरविमानवासी देव विक्रिया नहीं करते, अतः उनमें स्वाभाविक विभूषा होती है, आभरण एवं वस्त्रादि से जन्य नहीं। सौधर्म देवलोक से लेकर नवग्रैवेयक तक के देव इष्ट शब्द, इष्ट रूप, इष्ट गंध, इष्ट रस एवं इष्ट स्पर्श जन्य कामभोगों का अनुभव करते हैं। अनुत्तरौपपातिक देव अनुत्तर (श्रेष्ठ) शब्द यावत् स्पर्शजन्य कामभोगों का अनुभव करते हैं।
भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क एवं वैमानिक ये चारों ही प्रकार के देव जब विक्रिया करते हैं तब प्रासादीय यावत् मनोहर लगते हैं, क्योंकि विक्रिया के समय में वे अलंकृत-विभूषित होते हैं। देव शरीर के एक भाग से भी शब्द सुनते हैं तथा सम्पूर्ण शरीर से भी शब्द सुनते हैं। इसी प्रकार वे दो स्थानों से रूप को देखते हैं, गंध को सूंघते हैं, रस का आस्वादन करते हैं, स्पर्श का प्रतिसंवेदन करते हैं, अवभासित-प्रभासित होते हैं, विक्रिया करते हैं, मैथुन सेवन करते हैं, भाषा बोलते हैं, आहार करते हैं, परिणमन करते हैं, अनुभव करते हैं एवं निर्जरा करते हैं।
देवों की यह स्पृहा रहती है कि वे १. मनुष्य भव प्राप्त करें, २. आर्य क्षेत्र में जन्म लें तथा ३. श्रेष्ठ कुल में कुल उत्पन्न हों। तीन कारणों से वे परितप्त होते हैं अर्थात् उन्हें पश्चात्ताप करते हुए दुःख होता है कि उन्होंने समस्त अनुकूलताओं के होते हुए भी श्रुत का पर्याप्त अध्ययन नहीं किया, श्रामण्य पर्याय का पालन नहीं किया तथा विशुद्ध चारित्र का पालन नहीं किया।
देवों को तीन कारणों से अपने च्यवन का ज्ञान हो जाता है-१. विमान एवं आभरणों को निष्प्रभ देखकर, २. कल्पवृक्ष को मुरझाया हुआ देखकर एवं ३. अपनी तेजोलेश्या (कान्ति) को क्षीण देखकर। तीन कारणों से वे उद्विग्न होते हैं-१. देव सम्पदा को छोड़ने, २. माता-पिता के ओज-शुक्र का आहार ग्रहण करने एवं ३. गर्भाशय में रहने का विचार करने पर।
चार कारणों से देव अपने सिंहासन से अभ्युत्थित होते हैं-१. अरहंतों का जन्म होने पर, २. अरहन्तों के प्रव्रजित होने पर, ३. अरहन्तों को केवलज्ञान होने पर तथा ४. अरहंतों का परिनिर्वाण होने पर। इन्हीं चार कारणों से देवों के आसन एवं चैत्यवृक्ष चलित होते हैं तथा वे सिंहनाद एवं चेलोत्क्षेप (वर्षा) करते हैं। इन्हीं चार कारणों से देवों का मनुष्य लोक में आगमन भी होता है तथा वे कलकल ध्वनि एवं वर्षा करते हैं।
देवेन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंशक, लोकपाल, लोकान्तिक, अग्रमहिषी देवियाँ, परिषद् के देव, सेनापति, आत्मरक्षक आदि इन्हीं चार कारणों से शीघ्र ही मनुष्य लोक में आते हैं। इन चार कारणों से देवलोक में उद्योत भी होता है। चार कारणों से देवलोक में अन्धकार होता है-१. अरहंतों के व्युच्छिन्न होने पर, २. अरहंत प्रज्ञप्तधर्म के व्युच्छिन्न होने पर, ३. पूर्वगत के व्युच्छिन्न होने पर एवं ४. जाततेज के व्युच्छिन्न होने पर। चार कारण ऐसे निर्दिष्ट हैं जिनसे देवलोक में तत्काल उत्पन्न देव शीघ्र ही मनुष्य लोक में आना चाहते हुए भी नहीं आ पाता है तथा कुछ ऐसे भी देव हैं जो तत्काल उत्पन्न होकर भी चार कारणों से मनुष्य लोक में आ जाते हैं। जो मनुष्य लोक में आते हैं वे तब तक वहाँ के काम भोगों में आसक्त नहीं होते हैं।
तीन कारणों से देव विद्युतप्रकाश एवं मेघगर्जना जैसी ध्वनि करते हैं-१. वैक्रिय रूप करते हुए, २. परिचारणा करते हुए एवं ३. श्रमण-माहण के समक्ष अपनी ऋद्धि, द्युति, यश, बल, वीर्य, पुरुषकार एवं पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए। देवेन्द्र देवराज शक्र वृष्टिकायिक देवों के माध्यम से वर्षा करने का कार्य भी करता है।
इस अध्ययन में शक्र एवं ईशानेन्द्र के पारस्परिक व्यवहार, उनकी सुधर्मा सभा एवं ऋद्धि तथा उनके लोकपालों एवं विमानादि का भी विस्तार से निरूपण हुआ है। शक्र जब ईशानेन्द्र के पास कार्यवश जाता है तो आदर करता हुआ जाता है, किन्तु ईशानेन्द्र जब शक्र के पास जाता है तो आदर एवं अनादरपूर्वक जा सकता है, क्योंकि शक्र पहले देवलोक का इन्द्र है तथा ईशानेन्द्र दूसरे देवलोक का इन्द्र है। इन दोनों इन्द्रों में कार्यवश आलाप-संलाप