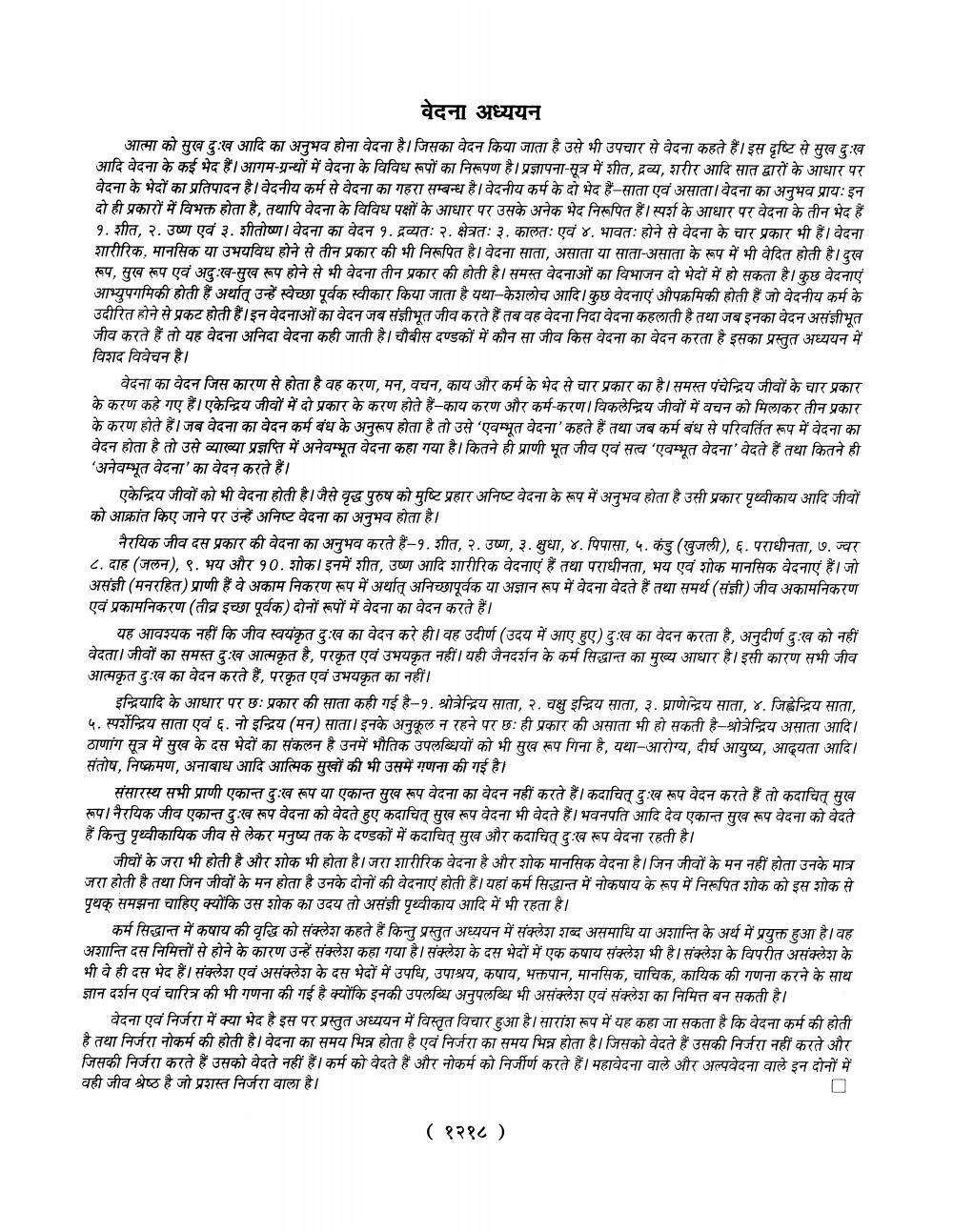________________
वेदना अध्ययन
आत्मा को सुख दुःख आदि का अनुभव होना वेदना है। जिसका वेदन किया जाता है उसे भी उपचार से वेदना कहते हैं। इस दृष्टि से सुख दुःख आदि वेदना के कई भेद हैं। आगम-ग्रन्थों में वेदना के विविध रूपों का निरूपण है। प्रज्ञापना-सूत्र में शीत, द्रव्य, शरीर आदि सात द्वारों के आधार पर वेदना के भेदों का प्रतिपादन है। वेदनीय कर्म से वेदना का गहरा सम्बन्ध है। वेदनीय कर्म के दो भेद हैं-साता एवं असाता। वेदना का अनुभव प्रायः इन दो ही प्रकारों में विभक्त होता है, तथापि वेदना के विविध पक्षों के आधार पर उसके अनेक भेद निरूपित हैं। स्पर्श के आधार पर वेदना के तीन भेद हैं १. शीत, २. उष्ण एवं ३. शीतोष्ण वेदना का वेदन १. द्रव्यतः २. क्षेत्रतः३. कालतः एवं ४. भावतः होने से वेदना के चार प्रकार भी हैं। वेदना शारीरिक, मानसिक या उभयविध होने से तीन प्रकार की भी निरूपित है। वेदना साता, असाता या साता-असाता के रूप में भी वेदित होती है। दुख रूप, सुख रूप एवं अदुःख-सुख रूप होने से भी वेदना तीन प्रकार की होती है। समस्त वेदनाओं का विभाजन दो भेदों में हो सकता है। कुछ वेदनाएं आभ्युपगमिकी होती हैं अर्थात् उन्हें स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया जाता है यथा-केशलोच आदि। कुछ वेदनाएं औपक्रमिकी होती हैं जो वेदनीय कर्म के उदीरित होने से प्रकट होती हैं। इन वेदनाओं का वेदन जब संज्ञीभूत जीव करते हैं तब वह वेदना निदा वेदना कहलाती है तथा जब इनका वेदन असंज्ञीभूत जीव करते हैं तो यह वेदना अनिदा वेदना कही जाती है। चौबीस दण्डकों में कौन सा जीव किस वेदना का वेदन करता है इसका प्रस्तुत अध्ययन में विशद विवेचन है।
वेदना का वेदन जिस कारण से होता है वह करण, मन, वचन, काय और कर्म के भेद से चार प्रकार का है। समस्त पंचेन्द्रिय जीवों के चार प्रकार के करण कहे गए हैं। एकेन्द्रिय जीवों में दो प्रकार के करण होते हैं-काय करण और कर्म-करण। विकलेन्द्रिय जीवों में वचन को मिलाकर तीन प्रकार के करण होते हैं। जब वेदना का वेदन कर्म बंध के अनुरूप होता है तो उसे 'एवम्भूत वेदना' कहते हैं तथा जब कर्म बंध से परिवर्तित रूप में वेदना का वेदन होता है तो उसे व्याख्या प्रज्ञप्ति में अनेवम्भूत वेदना कहा गया है। कितने ही प्राणी भूत जीव एवं सत्व 'एवम्भूत वेदना' वेदते हैं तथा कितने ही 'अनेवम्भूत वेदना' का वेदन करते हैं।
एकेन्द्रिय जीवों को भी वेदना होती है। जैसे वृद्ध पुरुष को मुष्टि प्रहार अनिष्ट वेदना के रूप में अनुभव होता है उसी प्रकार पृथ्वीकाय आदि जीवों को आक्रांत किए जाने पर उन्हें अनिष्ट वेदना का अनुभव होता है।
नैरयिक जीव दस प्रकार की वेदना का अनुभव करते हैं-१. शीत, २. उष्ण, ३. क्षुधा, ४. पिपासा, ५. कंडु (खुजली), ६. पराधीनता, ७. ज्चर ८. दाह (जलन), ९. भय और १०. शोक। इनमें शीत, उष्ण आदि शारीरिक वेदनाएं हैं तथा पराधीनता, भय एवं शोक मानसिक वेदनाएं हैं। जो असंज्ञी (मनरहित) प्राणी हैं वे अकाम निकरण रूप में अर्थात् अनिच्छापूर्वक या अज्ञान रूप में वेदना वेदते हैं तथा समर्थ (संज्ञी) जीव अकामनिकरण एवं प्रकामनिकरण (तीव्र इच्छा पूर्वक) दोनों रूपों में वेदना का वेदन करते हैं।
यह आवश्यक नहीं कि जीव स्वयंकृत दुःख का वेदन करे ही। वह उदीर्ण (उदय में आए हुए) दुःख का वेदन करता है, अनुदीर्ण दुःख को नहीं वेदता। जीवों का समस्त दुःख आत्मकृत है, परकृत एवं उभयकृत नहीं। यही जैनदर्शन के कर्म सिद्धान्त का मुख्य आधार है। इसी कारण सभी जीव आत्मकृत दुःख का वेदन करते हैं, परकृत एवं उभयकृत का नहीं।
इन्द्रियादि के आधार पर छः प्रकार की साता कही गई है-१. श्रोत्रेन्द्रिय साता, २. चक्षु इन्द्रिय साता, ३. घ्राणेन्द्रिय साता, ४. जिह्वेन्द्रिय साता, ५. स्पर्शेन्द्रिय साता एवं ६. नो इन्द्रिय (मन) साता। इनके अनुकूल न रहने पर छः ही प्रकार की असाता भी हो सकती है-श्रोत्रेन्द्रिय असाता आदि। ठाणांग सूत्र में सुख के दस भेदों का संकलन है उनमें भौतिक उपलब्धियों को भी सुख रूप गिना है, यथा-आरोग्य, दीर्घ आयुष्य, आढ्यता आदि। संतोष, निष्क्रमण, अनाबाध आदि आत्मिक सुखों की भी उसमें गणना की गई है।
संसारस्थ सभी प्राणी एकान्त दुःख रूप या एकान्त सुख रूप वेदना का वेदन नहीं करते हैं। कदाचित् दुःख रूप वेदन करते हैं तो कदाचित् सुख रूप। नैरयिक जीव एकान्त दुःख रूप वेदना को वेदते हुए कदाचित् सुख रूप वेदना भी वेदते हैं। भवनपति आदि देव एकान्त सुख रूप वेदना को वेदते हैं किन्तु पृथ्वीकायिक जीव से लेकर मनुष्य तक के दण्डकों में कदाचित् सुख और कदाचित् दुःख रूप वेदना रहती है।
जीवों के जरा भी होती है और शोक भी होता है। जरा शारीरिक वेदना है और शोक मानसिक वेदना है। जिन जीवों के मन नहीं होता उनके मात्र जरा होती है तथा जिन जीवों के मन होता है उनके दोनों की वेदनाएं होती हैं। यहां कर्म सिद्धान्त में नोकषाय के रूप में निरूपित शोक को इस शोक से पृथक् समझना चाहिए क्योंकि उस शोक का उदय तो असंज्ञी पृथ्वीकाय आदि में भी रहता है।
कर्म सिद्धान्त में कषाय की वृद्धि को संक्लेश कहते हैं किन्तु प्रस्तुत अध्ययन में संक्लेश शब्द असमाधि या अशान्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वह अशान्ति दस निमित्तों से होने के कारण उन्हें संक्लेश कहा गया है। संक्लेश के दस भेदों में एक कषाय संक्लेश भी है। संक्लेश के विपरीत असंक्लेश के भी वे ही दस भेद हैं। संक्लेश एवं असंक्लेश के दस भेदों में उपधि, उपाश्रय, कषाय, भक्तपान, मानसिक, चाचिक, कायिक की गणना करने के साथ ज्ञान दर्शन एवं चारित्र की भी गणना की गई है क्योंकि इनकी उपलब्धि अनुपलब्धि भी असंक्लेश एवं संक्लेश का निमित्त बन सकती है।
वेदना एवं निर्जरा में क्या भेद है इस पर प्रस्तुत अध्ययन में विस्तृत विचार हुआ है। सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि वेदना कर्म की होती है तथा निर्जरा नोकर्म की होती है। वेदना का समय भिन्न होता है एवं निर्जरा का समय भिन्न होता है। जिसको वेदते हैं उसकी निर्जरा नहीं करते और जिसकी निर्जरा करते हैं उसको वेदते नहीं हैं। कर्म को वेदते हैं और नोकर्म को निर्जीर्ण करते हैं। महावेदना वाले और अल्पवेदना वाले इन दोनों में वही जीव श्रेष्ठ है जो प्रशस्त निर्जरा वाला है।
( १२१८ )