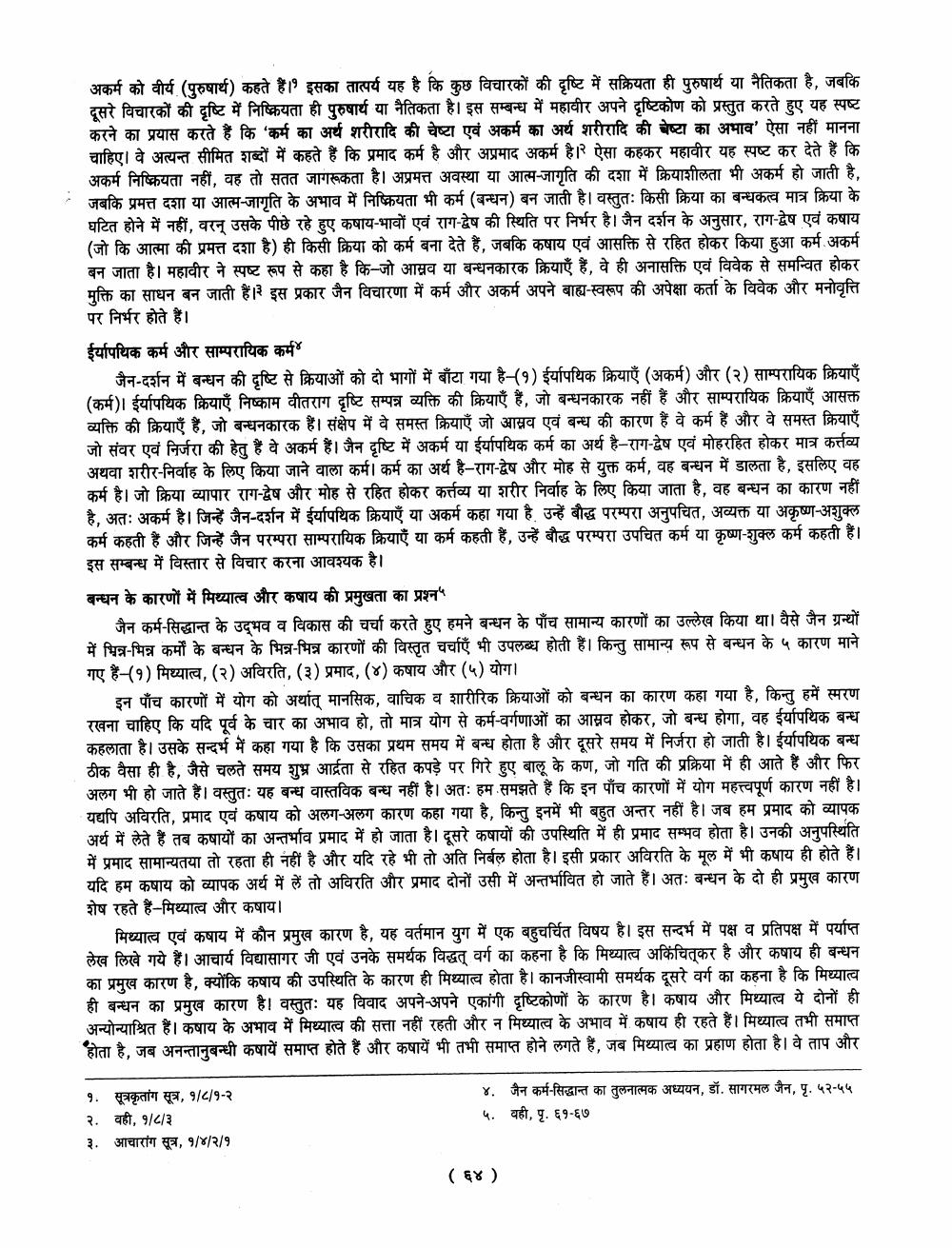________________
अकर्म को वीर्य (पुरुषार्थ) कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कुछ विचारकों की दृष्टि में सक्रियता ही पुरुषार्थ या नैतिकता है, जबकि दूसरे विचारकों की दृष्टि में निष्क्रियता ही पुरुषार्थ या नैतिकता है। इस सम्बन्ध में महावीर अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि 'कर्म का अर्थ शरीरादि की चेष्टा एवं अकर्म का अर्थ शरीरादि की चेष्टा का अभाव' ऐसा नहीं मानना चाहिए। वे अत्यन्त सीमित शब्दों में कहते हैं कि प्रमाद कर्म है और अप्रमाद अकर्म है। ऐसा कहकर महावीर यह स्पष्ट कर देते हैं कि अकर्म निष्क्रियता नहीं, वह तो सतत जागरूकता है। अप्रमत्त अवस्था या आत्म-जागृति की दशा में क्रियाशीलता भी अकर्म हो जाती है, जबकि प्रमत्त दशा या आत्म-जागृति के अभाव में निष्क्रियता भी कर्म (बन्धन) बन जाती है। वस्तुतः किसी क्रिया का बन्धकत्व मात्र क्रिया के घटित होने में नहीं, वरन् उसके पीछे रहे हुए कषाय-भावों एवं राग-द्वेष की स्थिति पर निर्भर है। जैन दर्शन के अनुसार, राग-द्वेष एवं कषाय (जो कि आत्मा की प्रमत्त दशा है) ही किसी क्रिया को कर्म बना देते हैं, जबकि कषाय एवं आसक्ति से रहित होकर किया हुआ कर्म अकर्म बन जाता है। महावीर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि-जो आस्रव या बन्धनकारक क्रियाएँ हैं, वे ही अनासक्ति एवं विवेक से समन्वित होकर मुक्ति का साधन बन जाती हैं। इस प्रकार जैन विचारणा में कर्म और अकर्म अपने बाह्य-स्वरूप की अपेक्षा कर्ता के विवेक और मनोवृत्ति पर निर्भर होते हैं। ईर्यापथिक कर्म और साम्परायिक कर्म
जैन-दर्शन में बन्धन की दृष्टि से क्रियाओं को दो भागों में बाँटा गया है-(१) ईपिथिक क्रियाएँ (अकर्म) और (२) साम्परायिक क्रियाएँ (कर्म)। ईर्यापथिक क्रियाएँ निष्काम वीतराग दृष्टि सम्पन्न व्यक्ति की क्रियाएँ हैं, जो बन्धनकारक नहीं हैं और साम्परायिक क्रियाएँ आसक्त व्यक्ति की क्रियाएँ हैं, जो बन्धनकारक हैं। संक्षेप में वे समस्त क्रियाएँ जो आनव एवं बन्ध की कारण हैं वे कर्म हैं और वे समस्त क्रियाएँ जो संवर एवं निर्जरा की हेतु हैं वे अकर्म हैं। जैन दृष्टि में अकर्म या ईर्यापथिक कर्म का अर्थ है-राग-द्वेष एवं मोहरहित होकर मात्र कर्तव्य अथवा शरीर-निर्वाह के लिए किया जाने वाला कर्म। कर्म का अर्थ है-राग-द्वेष और मोह से युक्त कर्म, वह बन्धन में डालता है, इसलिए वह कर्म है। जो क्रिया व्यापार राग-द्वेष और मोह से रहित होकर कर्तव्य या शरीर निर्वाह के लिए किया जाता है, वह बन्धन का कारण नहीं है, अतः अकर्म है। जिन्हें जैन-दर्शन में ईर्यापथिक क्रियाएँ या अकर्म कहा गया है. उन्हें बौद्ध परम्परा अनुपचित, अव्यक्त या अकृष्ण-अशुक्ल कर्म कहती हैं और जिन्हें जैन परम्परा साम्परायिक क्रियाएँ या कर्म कहती हैं, उन्हें बौद्ध परम्परा उपचित कर्म या कृष्ण-शुक्ल कर्म कहती हैं। इस सम्बन्ध में विस्तार से विचार करना आवश्यक है। बन्धन के कारणों में मिथ्यात्व और कषाय की प्रमुखता का प्रश्न
जैन कर्म-सिद्धान्त के उद्भव व विकास की चर्चा करते हुए हमने बन्धन के पाँच सामान्य कारणों का उल्लेख किया था। वैसे जैन ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न कर्मों के बन्धन के भिन्न-भिन्न कारणों की विस्तृत चर्चाएँ भी उपलब्ध होती हैं। किन्तु सामान्य रूप से बन्धन के ५ कारण माने गए हैं-(१) मिथ्यात्व, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कषाय और (५) योग।
इन पाँच कारणों में योग को अर्थात् मानसिक, वाचिक व शारीरिक क्रियाओं को बन्धन का कारण कहा गया है, किन्तु हमें स्मरण रखना चाहिए कि यदि पूर्व के चार का अभाव हो, तो मात्र योग से कर्म-वर्गणाओं का आनव होकर, जो बन्ध होगा, वह ईर्यापथिक बन्ध कहलाता है। उसके सन्दर्भ में कहा गया है कि उसका प्रथम समय में बन्ध होता है और दूसरे समय में निर्जरा हो जाती है। ईर्यापथिक बन्ध ठीक वैसा ही है, जैसे चलते समय शुभ्र आर्द्रता से रहित कपड़े पर गिरे हुए बालू के कण, जो गति की प्रक्रिया में ही आते हैं और फिर अलग भी हो जाते हैं। वस्तुतः यह बन्ध वास्तविक बन्ध नहीं है। अतः हम समझते हैं कि इन पाँच कारणों में योग महत्त्वपूर्ण कारण नहीं है। यद्यपि अविरति, प्रमाद एवं कषाय को अलग-अलग कारण कहा गया है, किन्तु इनमें भी बहुत अन्तर नहीं है। जब हम प्रमाद को व्यापक अर्थ में लेते हैं तब कषायों का अन्तर्भाव प्रमाद में हो जाता है। दूसरे कषायों की उपस्थिति में ही प्रमाद सम्भव होता है। उनकी अनुपस्थिति में प्रमाद सामान्यतया तो रहता ही नहीं है और यदि रहे भी तो अति निर्बल होता है। इसी प्रकार अविरति के मूल में भी कषाय ही होते हैं। यदि हम कषाय को व्यापक अर्थ में लें तो अविरति और प्रमाद दोनों उसी में अन्तर्भावित हो जाते हैं। अतः बन्धन के दो ही प्रमुख कारण शेष रहते हैं-मिथ्यात्व और कषाय। ___मिथ्यात्व एवं कषाय में कौन प्रमुख कारण है, यह वर्तमान युग में एक बहुचर्चित विषय है। इस सन्दर्भ में पक्ष व प्रतिपक्ष में पर्याप्त लेख लिखे गये हैं। आचार्य विद्यासागर जी एवं उनके समर्थक विद्धत् वर्ग का कहना है कि मिथ्यात्व अकिंचित्कर है और कषाय ही बन्धन का प्रमुख कारण है, क्योंकि कषाय की उपस्थिति के कारण ही मिथ्यात्व होता है। कानजीस्वामी समर्थक दूसरे वर्ग का कहना है कि मिथ्यात्व ही बन्धन का प्रमुख कारण है। वस्तुतः यह विवाद अपने-अपने एकांगी दृष्टिकोणों के कारण है। कषाय और मिथ्यात्व ये दोनों ही अन्योन्याश्रित हैं। कषाय के अभाव में मिथ्यात्व की सत्ता नहीं रहती और न मिथ्यात्व के अभाव में कषाय ही रहते हैं। मिथ्यात्व तभी समाप्त होता है, जब अनन्तानुबन्धी कषायें समाप्त होते हैं और कषायें भी तभी समाप्त होने लगते हैं, जब मिथ्यात्व का प्रहाण होता है। वे ताप और
१. सूत्रकृतांग सूत्र, १/८/१-२ २. वही, १/८/३ ३. आचारांग सूत्र, १/४/२/१
४. जैन कर्म-सिद्धान्त का तुलनात्मक अध्ययन, डॉ. सागरमल जैन, पृ. ५२-५५ ५. वही, पृ.६१-६७
(६४)