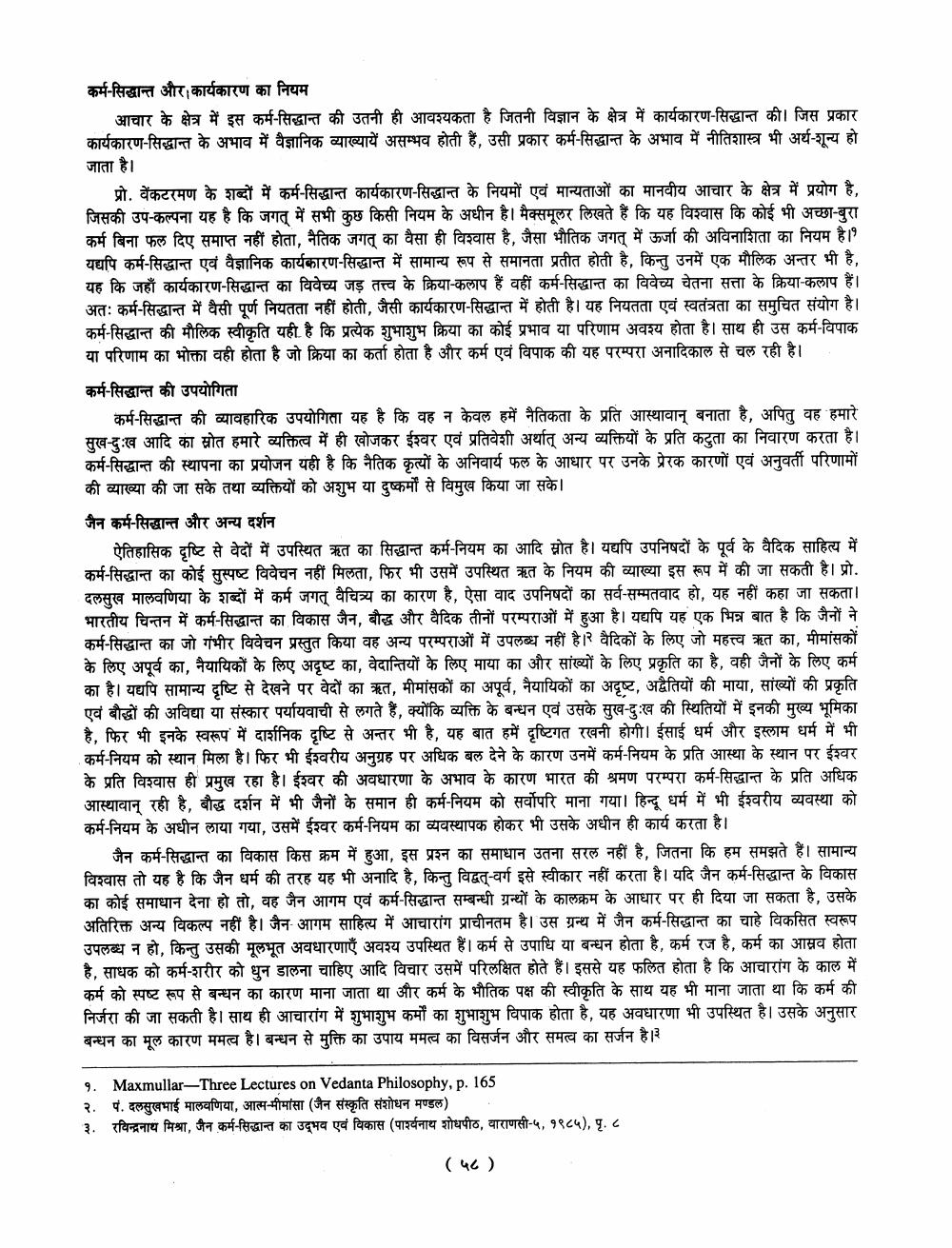________________
कर्म-सिद्धान्त और कार्यकारण का नियम
___ आचार के क्षेत्र में इस कर्म-सिद्धान्त की उतनी ही आवश्यकता है जितनी विज्ञान के क्षेत्र में कार्यकारण-सिद्धान्त की। जिस प्रकार कार्यकारण-सिद्धान्त के अभाव में वैज्ञानिक व्याख्यायें असम्भव होती हैं, उसी प्रकार कर्म-सिद्धान्त के अभाव में नीतिशास्त्र भी अर्थ-शून्य हो जाता है।
प्रो. वेंकटरमण के शब्दों में कर्म-सिद्धान्त कार्यकारण-सिद्धान्त के नियमों एवं मान्यताओं का मानवीय आचार के क्षेत्र में प्रयोग है, जिसकी उप-कल्पना यह है कि जगत् में सभी कुछ किसी नियम के अधीन है। मैक्समूलर लिखते हैं कि यह विश्वास कि कोई भी अच्छा-बुरा कर्म बिना फल दिए समाप्त नहीं होता, नैतिक जगत् का वैसा ही विश्वास है, जैसा भौतिक जगत् में ऊर्जा की अविनाशिता का नियम है।' यद्यपि कर्म-सिद्धान्त एवं वैज्ञानिक कार्यकारण-सिद्धान्त में सामान्य रूप से समानता प्रतीत होती है, किन्तु उनमें एक मौलिक अन्तर भी है, यह कि जहाँ कार्यकारण-सिद्धान्त का विवेच्य जड़ तत्त्व के क्रिया-कलाप हैं वहीं कर्म-सिद्धान्त का विवेच्य चेतना सत्ता के क्रिया-कलाप हैं। अतः कर्म-सिद्धान्त में वैसी पूर्ण नियतता नहीं होती, जैसी कार्यकारण-सिद्धान्त में होती है। यह नियतता एवं स्वतंत्रता का समुचित संयोग है। कर्म-सिद्धान्त की मौलिक स्वीकृति यही है कि प्रत्येक शुभाशुभ क्रिया का कोई प्रभाव या परिणाम अवश्य होता है। साथ ही उस कर्म-विपाक या परिणाम का भोक्ता वही होता है जो क्रिया का कर्ता होता है और कर्म एवं विपाक की यह परम्परा अनादिकाल से चल रही है। कर्म-सिद्धान्त की उपयोगिता
कर्म-सिद्धान्त की व्यावहारिक उपयोगिता यह है कि वह न केवल हमें नैतिकता के प्रति आस्थावान् बनाता है, अपितु वह हमारे सुख-दुःख आदि का स्रोत हमारे व्यक्तित्व में ही खोजकर ईश्वर एवं प्रतिवेशी अर्थात् अन्य व्यक्तियों के प्रति कटुता का निवारण करता है। कर्म-सिद्धान्त की स्थापना का प्रयोजन यही है कि नैतिक कृत्यों के अनिवार्य फल के आधार पर उनके प्रेरक कारणों एवं अनुवर्ती परिणामों की व्याख्या की जा सके तथा व्यक्तियों को अशुभ या दुष्कर्मों से विमुख किया जा सके। जैन कर्म-सिद्धान्त और अन्य दर्शन
ऐतिहासिक दृष्टि से वेदों में उपस्थित ऋत का सिद्धान्त कर्म-नियम का आदि मोत है। यद्यपि उपनिषदों के पूर्व के वैदिक साहित्य में कर्म-सिद्धान्त का कोई सुस्पष्ट विवेचन नहीं मिलता, फिर भी उसमें उपस्थित ऋत के नियम की व्याख्या इस रूप में की जा सकती है। प्रो. दलसुख मालवणिया के शब्दों में कर्म जगत् वैचित्र्य का कारण है, ऐसा वाद उपनिषदों का सर्व-सम्मतवाद हो, यह नहीं कहा जा सकता। भारतीय चिन्तन में कर्म-सिद्धान्त का विकास जैन, बौद्ध और वैदिक तीनों परम्पराओं में हुआ है। यद्यपि यह एक भिन्न बात है कि जैनों ने कर्म-सिद्धान्त का जो गंभीर विवेचन प्रस्तुत किया वह अन्य परम्पराओं में उपलब्ध नहीं है। वैदिकों के लिए जो महत्त्व ऋत का, मीमांसकों के लिए अपूर्व का, नैयायिकों के लिए अदृष्ट का, वेदान्तियों के लिए माया का और सांख्यों के लिए प्रकृति का है, वही जैनों के लिए कर्म का है। यद्यपि सामान्य दृष्टि से देखने पर वेदों का ऋत, मीमांसकों का अपूर्व, नैयायिकों का अदृष्ट, अद्वैतियों की माया, सांख्यों की प्रकृति एवं बौद्धों की अविद्या या संस्कार पर्यायवाची से लगते हैं, क्योंकि व्यक्ति के बन्धन एवं उसके सुख-दुःख की स्थितियों में इनकी मुख्य भूमिका है, फिर भी इनके स्वरूप में दार्शनिक दृष्टि से अन्तर भी है, यह बात हमें दृष्टिगत रखनी होगी। ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में भी कर्म-नियम को स्थान मिला है। फिर भी ईश्वरीय अनग्रह पर अधिक बल देने के कारण उनमें कर्म-नियम के प्रति आस्था के स्थान पर ईश्वर के प्रति विश्वास ही प्रमुख रहा है। ईश्वर की अवधारणा के अभाव के कारण भारत की श्रमण परम्परा कर्म-सिद्धान्त के प्रति अधिक आस्थावान् रही है, बौद्ध दर्शन में भी जैनों के समान ही कर्म-नियम को सर्वोपरि माना गया। हिन्दू धर्म में भी ईश्वरीय व्यवस्था को कर्म-नियम के अधीन लाया गया, उसमें ईश्वर कर्म-नियम का व्यवस्थापक होकर भी उसके अधीन ही कार्य करता है।
जैन कर्म-सिद्धान्त का विकास किस क्रम में हुआ, इस प्रश्न का समाधान उतना सरल नहीं है, जितना कि हम समझते हैं। सामान्य विश्वास तो यह है कि जैन धर्म की तरह यह भी अनादि है, किन्तु विद्वत्-वर्ग इसे स्वीकार नहीं करता है। यदि जैन कर्म-सिद्धान्त के विकास का कोई समाधान देना हो तो, वह जैन आगम एवं कर्म-सिद्धान्त सम्बन्धी ग्रन्थों के कालक्रम के आधार पर ही दिया जा सकता है, उसके अतिरिक्त अन्य विकल्प नहीं है। जैन आगम साहित्य में आचारांग प्राचीनतम है। उस ग्रन्थ में जैन कर्म-सिद्धान्त का चाहे विकसित स्वरूप उपलब्ध न हो, किन्तु उसकी मूलभूत अवधारणाएँ अवश्य उपस्थित हैं। कर्म से उपाधि या बन्धन होता है, कर्म रज है, कर्म का आस्रव होता है, साधक को कर्म-शरीर को धुन डालना चाहिए आदि विचार उसमें परिलक्षित होते हैं। इससे यह फलित होता है कि आचारांग के काल में कर्म को स्पष्ट रूप से बन्धन का कारण माना जाता था और कर्म के भौतिक पक्ष की स्वीकृति के साथ यह भी माना जाता था कि कर्म की निर्जरा की जा सकती है। साथ ही आचारांग में शुभाशुभ कर्मों का शुभाशुभ विपाक होता है, यह अवधारणा भी उपस्थित है। उसके अनुसार बन्धन का मूल कारण ममत्व है। बन्धन से मुक्ति का उपाय ममत्व का विसर्जन और समत्व का सर्जन है।३
9. Maxmullar-Three Lectures on Vedanta Philosophy, p. 165 २. पं. दलसुखभाई मालवणिया, आत्म-मीमांसा (जैन संस्कृति संशोधन मण्डल) ३. रविन्द्रनाथ मिश्रा, जैन कर्म-सिद्धान्त का उद्भव एवं विकास (पार्श्वनाथ शोधपीठ, वाराणसी-५, १९८५), पृ.८
(५८)