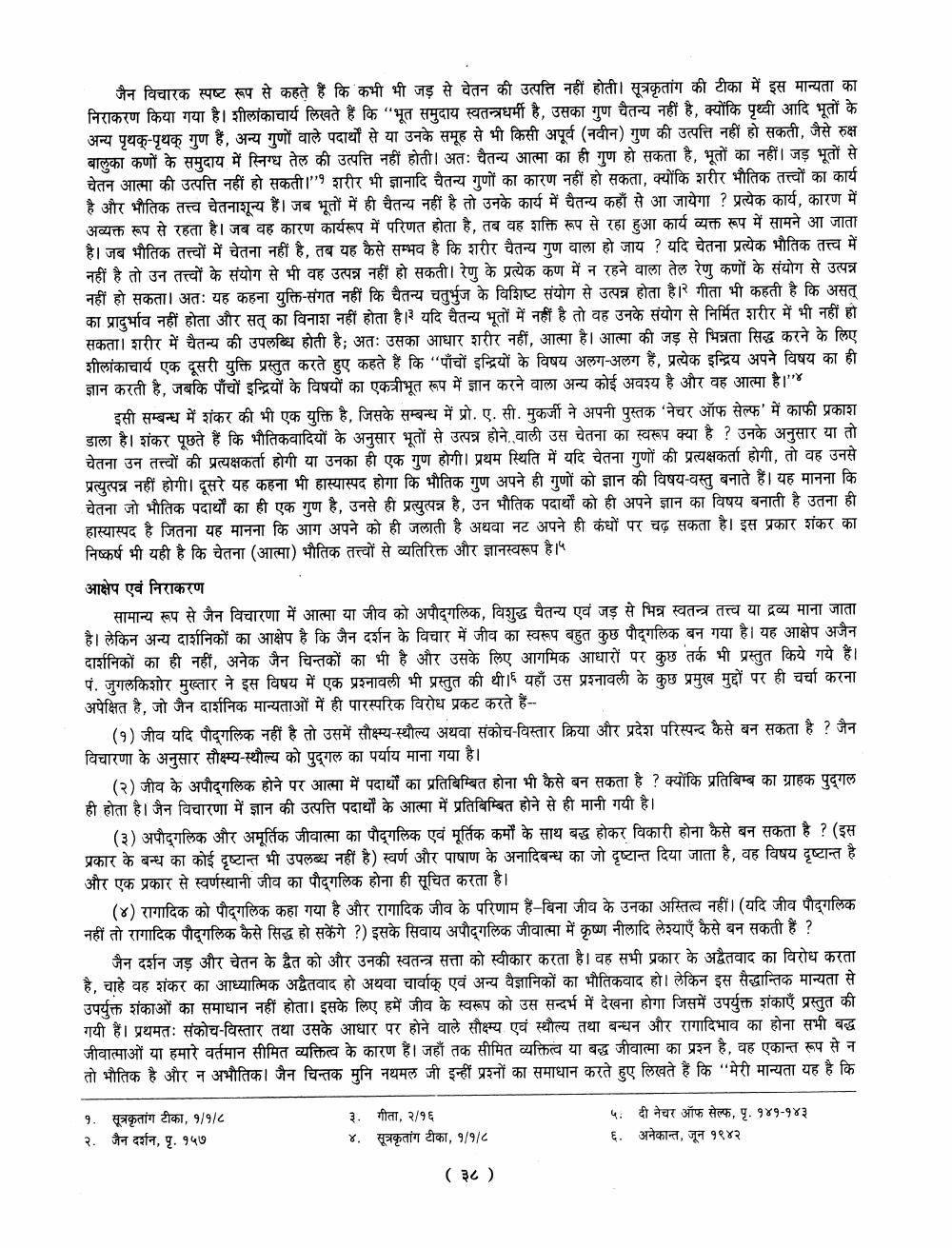________________
जैन विचारक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कभी भी जड़ से वेतन की उत्पत्ति नहीं होती। सूत्रकृतांग की टीका में इस मान्यता का निराकरण किया गया है। शीलांकाचार्य लिखते हैं कि "भूत समुदाय स्वतन्त्रधर्मी है, उसका गुण चैतन्य नहीं है, क्योंकि पृथ्वी आदि भूतों के अन्य पृथक्-पृथक् गुण हैं, अन्य गुणों वाले पदार्थों से या उनके समूह से भी किसी अपूर्व (नवीन) गुण की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जैसे रुक्ष बालुका कणों के समुदाय में स्निग्ध तेल की उत्पत्ति नहीं होती। अतः चैतन्य आत्मा का ही गुण हो सकता है, भूतों का नहीं। जड़ भूतों से चेतन आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती।"१ शरीर भी ज्ञानादि चैतन्य गुणों का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर भौतिक तत्त्वों का कार्य है और भौतिक तत्त्व चेतनाशून्य हैं। जब भूतों में ही चैतन्य नहीं है तो उनके कार्य में चैतन्य कहाँ से आ जायेगा ? प्रत्येक कार्य, कारण में अव्यक्त रूप से रहता है। जब वह कारण कार्यरूप में परिणत होता है, तब वह शक्ति रूप से रहा हुआ कार्य व्यक्त रूप में सामने आ जाता है। जब भौतिक तत्त्वों में चेतना नहीं है, तब यह कैसे सम्भव है कि शरीर चैतन्य गुण वाला हो जाय ? यदि चेतना प्रत्येक भौतिक तत्त्व में नहीं है तो उन तत्त्वों के संयोग से भी वह उत्पन्न नहीं हो सकती। रेणु के प्रत्येक कण में न रहने वाला तेल रेणु कणों के संयोग से उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः यह कहना युक्ति-संगत नहीं कि चैतन्य चतुर्भुज के विशिष्ट संयोग से उत्पन्न होता है। गीता भी कहती है कि असत् का प्रादुर्भाव नहीं होता और सत् का विनाश नहीं होता है। यदि चैतन्य भूतों में नहीं है तो वह उनके संयोग से निर्मित शरीर में भी नहीं हो सकता। शरीर में चैतन्य की उपलब्धि होती है; अतः उसका आधार शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा की जड़ से भिन्नता सिद्ध करने के लिए शीलांकाचार्य एक दूसरी युक्ति प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि “पाँचों इन्द्रियों के विषय अलग-अलग हैं, प्रत्येक इन्द्रिय अपने विषय का ही ज्ञान करती है, जबकि पाँचों इन्द्रियों के विषयों का एकत्रीभूत रूप में ज्ञान करने वाला अन्य कोई अवश्य है और वह आत्मा है।"४ ___इसी सम्बन्ध में शंकर की भी एक युक्ति है, जिसके सम्बन्ध में प्रो. ए. सी. मुकर्जी ने अपनी पुस्तक 'नेचर ऑफ सेल्फ' में काफी प्रकाश डाला है। शंकर पूछते हैं कि भौतिकवादियों के अनुसार भूतों से उत्पन्न होने वाली उस चेतना का स्वरूप क्या है ? उनके अनुसार या तो चेतना उन तत्त्वों की प्रत्यक्षकर्ता होगी या उनका ही एक गुण होगी। प्रथम स्थिति में यदि चेतना गुणों की प्रत्यक्षकर्ता होगी, तो वह उनसे प्रत्युत्पन्न नहीं होगी। दूसरे यह कहना भी हास्यास्पद होगा कि भौतिक गुण अपने ही गुणों को ज्ञान की विषय-वस्तु बनाते हैं। यह मानना कि चेतना जो भौतिक पदार्थों का ही एक गुण है, उनसे ही प्रत्युत्पन्न है, उन भौतिक पदार्थों को ही अपने ज्ञान का विषय बनाती है उतना ही हास्यास्पद है जितना यह मानना कि आग अपने को ही जलाती है अथवा नट अपने ही कंधों पर चढ़ सकता है। इस प्रकार शंकर का निष्कर्ष भी यही है कि चेतना (आत्मा) भौतिक तत्त्वों से व्यतिरिक्त और ज्ञानस्वरूप है। आक्षेप एवं निराकरण
सामान्य रूप से जैन विचारणा में आत्मा या जीव को अपौद्गलिक, विशुद्ध चैतन्य एवं जड़ से भिन्न स्वतन्त्र तत्त्व या द्रव्य माना जाता है। लेकिन अन्य दार्शनिकों का आक्षेप है कि जैन दर्शन के विचार में जीव का स्वरूप बहुत कुछ पौद्गलिक बन गया है। यह आक्षेप अजैन दार्शनिकों का ही नहीं, अनेक जैन चिन्तकों का भी है और उसके लिए आगमिक आधारों पर कुछ तर्क भी प्रस्तुत किये गये हैं। पं. जुगलकिशोर मुख्तार ने इस विषय में एक प्रश्नावली भी प्रस्तुत की थी। यहाँ उस प्रश्नावली के कुछ प्रमुख मुद्दों पर ही चर्चा करना अपेक्षित है, जो जैन दार्शनिक मान्यताओं में ही पारस्परिक विरोध प्रकट करते हैं--
(१) जीव यदि पौद्गलिक नहीं है तो उसमें सौक्ष्म्य-स्थौल्य अथवा संकोच-विस्तार क्रिया और प्रदेश परिस्पन्द कैसे बन सकता है ? जैन विचारणा के अनुसार सौक्ष्य-स्थौल्य को पुद्गल का पर्याय माना गया है।
(२) जीव के अपौद्गलिक होने पर आत्मा में पदार्थों का प्रतिबिम्बित होना भी कैसे बन सकता है ? क्योंकि प्रतिबिम्ब का ग्राहक पुद्गल ही होता है। जैन विचारणा में ज्ञान की उत्पत्ति पदार्थों के आत्मा में प्रतिबिम्बित होने से ही मानी गयी है।
(३) अपौद्गलिक और अमूर्तिक जीवात्मा का पौद्गलिक एवं मूर्तिक कर्मों के साथ बद्ध होकर विकारी होना कैसे बन सकता है ? (इस प्रकार के बन्ध का कोई दृष्टान्त भी उपलब्ध नहीं है) स्वर्ण और पाषाण के अनादिबन्ध का जो दृष्टान्त दिया जाता है, वह विषय दृष्टान्त है और एक प्रकार से स्वर्णस्थानी जीव का पौद्गलिक होना ही सूचित करता है।
(४) रागादिक को पौद्गलिक कहा गया है और रागादिक जीव के परिणाम हैं-बिना जीव के उनका अस्तित्व नहीं। (यदि जीव पौद्गलिक नहीं तो रागादिक पौद्गलिक कैसे सिद्ध हो सकेंगे ?) इसके सिवाय अपौद्गलिक जीवात्मा में कृष्ण नीलादि लेश्याएँ कैसे बन सकती हैं ?
जैन दर्शन जड़ और चेतन के द्वैत को और उनकी स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार करता है। वह सभी प्रकार के अद्वैतवाद का विरोध करता है, चाहे वह शंकर का आध्यात्मिक अद्वैतवाद हो अथवा चार्वाक् एवं अन्य वैज्ञानिकों का भौतिकवाद हो। लेकिन इस सैद्धान्तिक मान्यता से उपर्युक्त शंकाओं का समाधान नहीं होता। इसके लिए हमें जीव के स्वरूप को उस सन्दर्भ में देखना होगा जिसमें उपर्युक्त शंकाएँ प्रस्तुत की गयी हैं। प्रथमतः संकोच-विस्तार तथा उसके आधार पर होने वाले सौक्ष्य एवं स्थौल्य तथा बन्धन और रागादिभाव का होना सभी बद्ध जीवात्माओं या हमारे वर्तमान सीमित व्यक्तित्व के कारण हैं। जहाँ तक सीमित व्यक्तित्व या बद्ध जीवात्मा का प्रश्न है, वह एकान्त रूप से न तो भौतिक है और न अभौतिक। जैन चिन्तक मुनि नथमल जी इन्हीं प्रश्नों का समाधान करते हुए लिखते हैं कि “मेरी मान्यता यह है कि
१. २.
सूत्रकृतांग टीका, १/9/८ जैन दर्शन, पृ. १५७
३. ४.
गीता, २/१६ सूत्रकृतांग टीका, १/9/८
५. दी नेचर ऑफ सेल्फ, पृ. १४१-१४३ ६. अनेकान्त, जून १९४२
(३८)