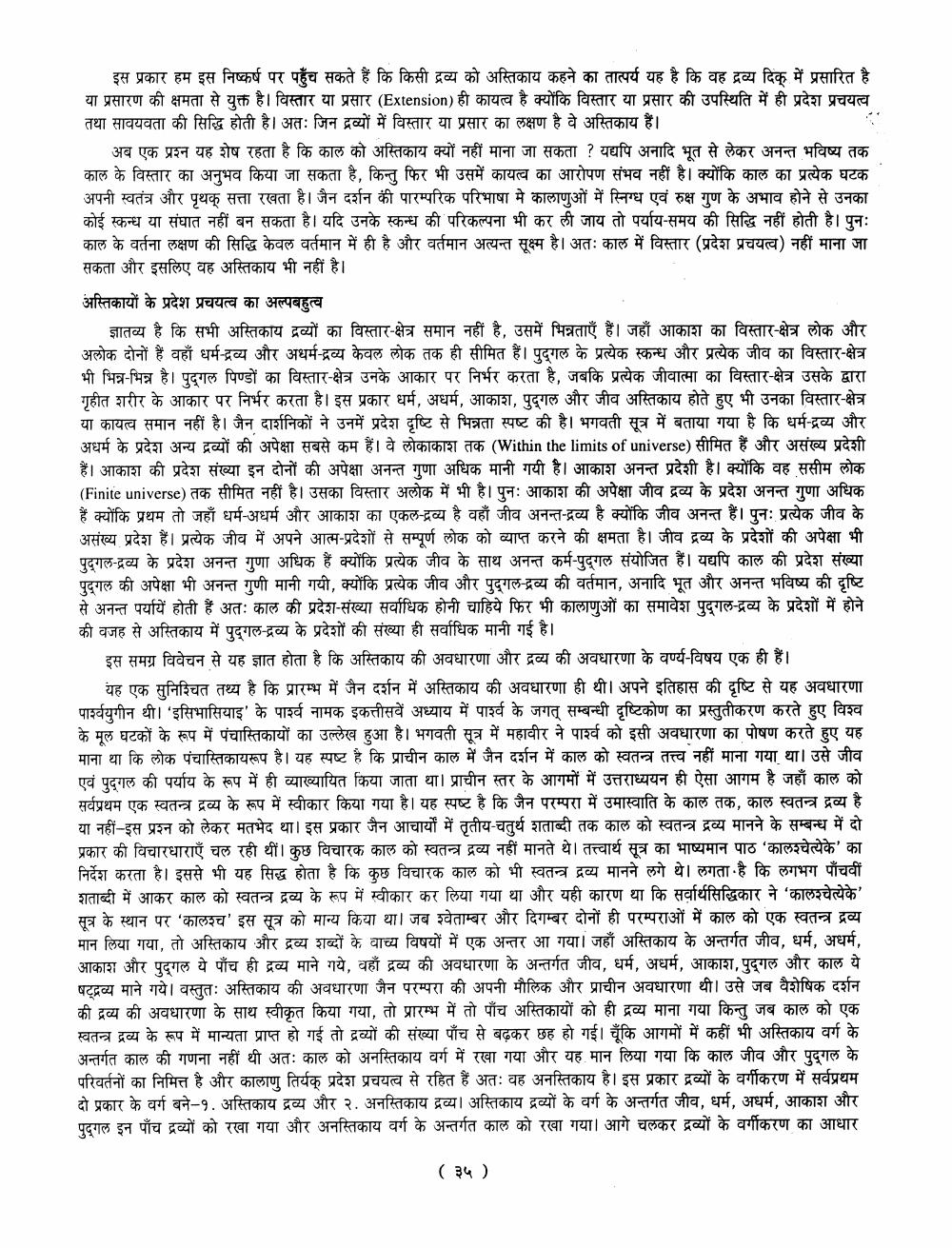________________
इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि किसी द्रव्य को अस्तिकाय कहने का तात्पर्य यह है कि वह द्रव्य दिन में प्रसारित है या प्रसारण की क्षमता से युक्त है। विस्तार या प्रसार (Extension) ही कायत्व है क्योंकि विस्तार या प्रसार की उपस्थिति में ही प्रदेश प्रचयत्व तथा सावयवता की सिद्धि होती है। अतः जिन द्रव्यों में विस्तार या प्रसार का लक्षण है वे अस्तिकाय हैं।
अब एक प्रश्न यह शेष रहता है कि काल को अस्तिकाय क्यों नहीं माना जा सकता ? यद्यपि अनादि भूत से लेकर अनन्त भविष्य तक काल के विस्तार का अनुभव किया जा सकता है, किन्तु फिर भी उसमें कायत्व का आरोपण संभव नहीं है। क्योंकि काल का प्रत्येक घटक अपनी स्वतंत्र और पृथक् सत्ता रखता है। जैन दर्शन की पारम्परिक परिभाषा मे कालाणुओं में स्निग्ध एवं रुक्ष गुण के अभाव होने से उनका कोई स्कन्ध या संघात नहीं बन सकता है। यदि उनके स्कन्ध की परिकल्पना भी कर ली जाय तो पर्याय-समय की सिद्धि नहीं होती है। पुनः काल के वर्तना लक्षण की सिद्धि केवल वर्तमान में ही है और वर्तमान अत्यन्त सूक्ष्म है। अतः काल में विस्तार (प्रदेश प्रचयत्व) नहीं माना जा सकता और इसलिए वह अस्तिकाय भी नहीं है। अस्तिकायों के प्रदेश प्रचयत्व का अल्पबहुत्व ___ ज्ञातव्य है कि सभी अस्तिकाय द्रव्यों का विस्तार-क्षेत्र समान नहीं है, उसमें भिन्नताएँ हैं। जहाँ आकाश का विस्तार-क्षेत्र लोक और अलोक दोनों हैं वहाँ धर्म-द्रव्य और अधर्म-द्रव्य केवल लोक तक ही सीमित हैं। पुद्गल के प्रत्येक स्कन्ध और प्रत्येक जीव का विस्तार-क्षेत्र भी भिन्न-भिन्न है। पुद्गल पिण्डों का विस्तार-क्षेत्र उनके आकार पर निर्भर करता है, जबकि प्रत्येक जीवात्मा का विस्तार-क्षेत्र उसके द्वारा गृहीत शरीर के आकार पर निर्भर करता है। इस प्रकार धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और जीव अस्तिकाय होते हुए भी उनका विस्तार-क्षेत्र या कायत्व समान नहीं है। जैन दार्शनिकों ने उनमें प्रदेश दृष्टि से भिन्नता स्पष्ट की है। भगवती सूत्र में बताया गया है कि धर्म-द्रव्य और अधर्म के प्रदेश अन्य द्रव्यों की अपेक्षा सबसे कम हैं। वे लोकाकाश तक (Within the limits of universe) सीमित हैं और असंख्य प्रदेशी हैं। आकाश की प्रदेश संख्या इन दोनों की अपेक्षा अनन्त गुणा अधिक मानी गयी है। आकाश अनन्त प्रदेशी है। क्योंकि वह ससीम लोक (Finite universe) तक सीमित नहीं है। उसका विस्तार अलोक में भी है। पुनः आकाश की अपेक्षा जीव द्रव्य के प्रदेश अनन्त गुणा अधिक हैं क्योंकि प्रथम तो जहाँ धर्म-अधर्म और आकाश का एकल-द्रव्य है वहाँ जीव अनन्त-द्रव्य है क्योंकि जीव अनन्त हैं। पुनः प्रत्येक जीव के असंख्य प्रदेश हैं। प्रत्येक जीव में अपने आत्म-प्रदेशों से सम्पूर्ण लोक को व्याप्त करने की क्षमता है। जीव द्रव्य के प्रदेशों की अपेक्षा भी पुद्गल-द्रव्य के प्रदेश अनन्त गुणा अधिक हैं क्योंकि प्रत्येक जीव के साथ अनन्त कर्म-पुद्गल संयोजित हैं। यद्यपि काल की प्रदेश संख्या पुद्गल की अपेक्षा भी अनन्त गुणी मानी गयी, क्योंकि प्रत्येक जीव और पुद्गल-द्रव्य की वर्तमान, अनादि भूत और अनन्त भविष्य की दृष्टि से अनन्त पर्यायें होती हैं अतः काल की प्रदेश-संख्या सर्वाधिक होनी चाहिये फिर भी कालाणुओं का समावेश पुद्गल-द्रव्य के प्रदेशों में होने की वजह से अस्तिकाय में पुद्गल-द्रव्य के प्रदेशों की संख्या ही सर्वाधिक मानी गई है।
इस समग्र विवेचन से यह ज्ञात होता है कि अस्तिकाय की अवधारणा और द्रव्य की अवधारणा के वर्ण्य-विषय एक ही हैं।
यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि प्रारम्भ में जैन दर्शन में अस्तिकाय की अवधारणा ही थी। अपने इतिहास की दृष्टि से यह अवधारणा पार्श्वयुगीन थी। ‘इसिभासियाइ' के पार्श्व नामक इकत्तीसवें अध्याय में पार्श्व के जगत् सम्बन्धी दृष्टिकोण का प्रस्तुतीकरण करते हुए विश्व के मूल घटकों के रूप में पंचास्तिकायों का उल्लेख हुआ है। भगवती सूत्र में महावीर ने पार्श्व को इसी अवधारणा का पोषण करते हुए यह माना था कि लोक पंचास्तिकायरूप है। यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल में जैन दर्शन में काल को स्वतन्त्र तत्त्व नहीं माना गया था। उसे जीव एवं पुद्गल की पर्याय के रूप में ही व्याख्यायित किया जाता था। प्राचीन स्तर के आगमों में उत्तराध्ययन ही ऐसा आगम है जहाँ काल को सर्वप्रथम एक स्वतन्त्र द्रव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। यह स्पष्ट है कि जैन परम्परा में उमास्वाति के काल तक, काल स्वतन्त्र द्रव्य है या नहीं इस प्रश्न को लेकर मतभेद था। इस प्रकार जैन आचार्यों में तृतीय-चतुर्थ शताब्दी तक काल को स्वतन्त्र द्रव्य मानने के सम्बन्ध में दो प्रकार की विचारधाराएँ चल रही थीं। कुछ विचारक काल को स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानते थे। तत्त्वार्थ सूत्र का भाष्यमान पाठ 'कालश्चेत्येके' का निर्देश करता है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि कुछ विचारक काल को भी स्वतन्त्र द्रव्य मानने लगे थे। लगता है कि लगभग पाँचवीं शताब्दी में आकर काल को स्वतन्त्र द्रव्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था और यही कारण था कि सर्वार्थसिद्धिकार ने 'कालश्चेत्येके' सूत्र के स्थान पर 'कालश्च' इस सूत्र को मान्य किया था। जब श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं में काल को एक स्वतन्त्र द्रव्य मान लिया गया, तो अस्तिकाय और द्रव्य शब्दों के वाच्य विषयों में एक अन्तर आ गया। जहाँ अस्तिकाय के अन्तर्गत जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये पाँच ही द्रव्य माने गये, वहाँ द्रव्य की अवधारणा के अन्तर्गत जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और काल ये षद्रव्य माने गये। वस्तुतः अस्तिकाय की अवधारणा जैन परम्परा की अपनी मौलिक और प्राचीन अवधारणा थी। उसे जब वैशेषिक दर्शन की द्रव्य की अवधारणा के साथ स्वीकृत किया गया, तो प्रारम्भ में तो पाँच अस्तिकायों को ही द्रव्य माना गया किन्तु जब काल को एक स्वतन्त्र द्रव्य के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई तो द्रव्यों की संख्या पाँच से बढ़कर छह हो गई। चूँकि आगमों में कहीं भी अस्तिकाय वर्ग के अन्तर्गत काल की गणना नहीं थी अतः काल को अनस्तिकाय वर्ग में रखा गया और यह मान लिया गया कि काल जीव और पुद्गल के परिवर्तनों का निमित्त है और कालाणु तिर्यक् प्रदेश प्रचयत्व से रहित हैं अतः वह अनस्तिकाय है। इस प्रकार द्रव्यों के वर्गीकरण में सर्वप्रथम दो प्रकार के वर्ग बने-१. अस्तिकाय द्रव्य और २. अनस्तिकाय द्रव्य। अस्तिकाय द्रव्यों के वर्ग के अन्तर्गत जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल इन पाँच द्रव्यों को रखा गया और अनस्तिकाय वर्ग के अन्तर्गत काल को रखा गया। आगे चलकर द्रव्यों के वर्गीकरण का आधार
( ३५ )