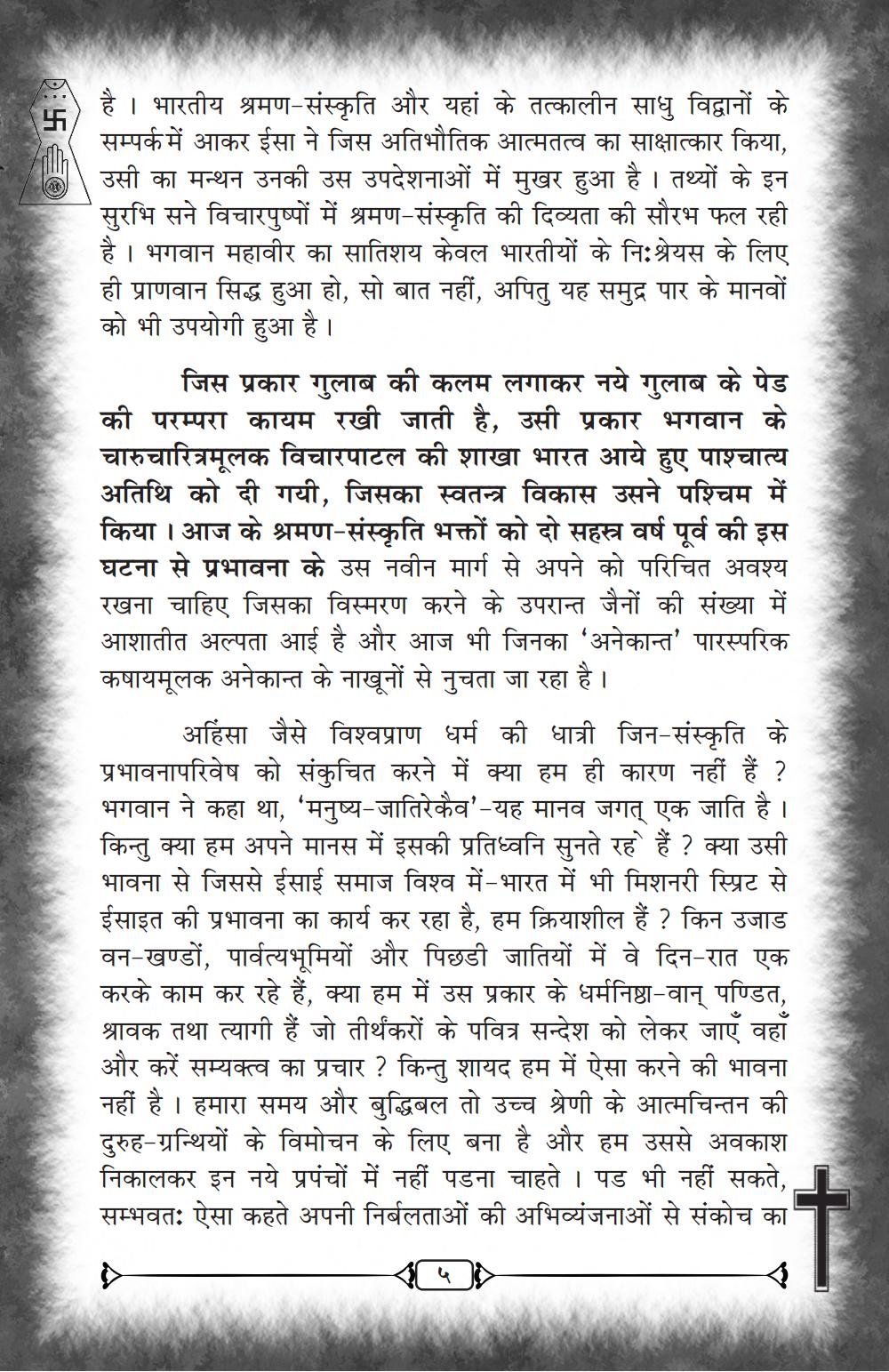________________
है । भारतीय श्रमण- - संस्कृति और यहां के तत्कालीन साधु विद्वानों के सम्पर्क में आकर ईसा ने जिस अतिभौतिक आत्मतत्व का साक्षात्कार किया, उसी का मन्थन उनकी उस उपदेशनाओं में मुखर हुआ है। तथ्यों के इन सुरभि सने विचारपुष्पों में श्रमण-संस्कृति की दिव्यता की सौरभ फल रही है । भगवान महावीर का सातिशय केवल भारतीयों के निःश्रेयस के लिए ही प्राणवान सिद्ध हुआ हो, सो बात नहीं, अपितु यह समुद्र पार के मानवों को भी उपयोगी हुआ है I
जिस प्रकार गुलाब की कलम लगाकर नये गुलाब के पेड की परम्परा कायम रखी जाती है, उसी प्रकार भगवान के चारुचारित्रमूलक विचारपाटल की शाखा भारत आये हुए पाश्चात्य अतिथि को दी गयी, जिसका स्वतन्त्र विकास उसने पश्चिम में किया । आज के श्रमण-संस्कृति भक्तों को दो सहस्त्र वर्ष पूर्व की इस घटना से प्रभावना के उस नवीन मार्ग से अपने को परिचित अवश्य रखना चाहिए जिसका विस्मरण करने के उपरान्त जैनों की संख्या में आशातीत अल्पता आई है और आज भी जिनका 'अनेकान्त' पारस्परिक कषायमूलक अनेकान्त के नाखूनों से नुचता जा रहा है ।
अहिंसा जैसे विश्वप्राण धर्म की धात्री जिन-संस्कृति के प्रभावनापरिवेष को संकुचित करने में क्या हम ही कारण नहीं हैं ? भगवान ने कहा था, ‘मनुष्य-जातिरेकैव' - यह मानव जगत् एक जाति है । किन्तु क्या हम अपने मानस में इसकी प्रतिध्वनि सुनते रह े हैं ? क्या उसी भावना से जिससे ईसाई समाज विश्व में भारत में भी मिशनरी स्प्रिंट से ईसाइत की प्रभावना का कार्य कर रहा है, हम क्रियाशील हैं ? किन उजाड वन-खण्डों, पार्वत्यभूमियों और पिछडी जातियों में वे दिन-रात एक करके काम कर रहे हैं, क्या हम में उस प्रकार के धर्मनिष्ठा-वान् पण्डित, श्रावक तथा त्यागी हैं जो तीर्थंकरों के पवित्र सन्देश को लेकर जाएँ वहाँ और करें सम्यक्त्व का प्रचार ? किन्तु शायद हम में ऐसा करने की भावना नहीं है । हमारा समय और बुद्धिबल तो उच्च श्रेणी के आत्मचिन्तन की दुरुह -ग्रन्थियों के विमोचन के लिए बना है और हम उससे अवकाश निकालकर इन नये प्रपंचों में नहीं पडना चाहते । पड भी नहीं सकते,, सम्भवतः ऐसा कहते अपनी निर्बलताओं की अभिव्यंजनाओं से संकोच का
t
>
५