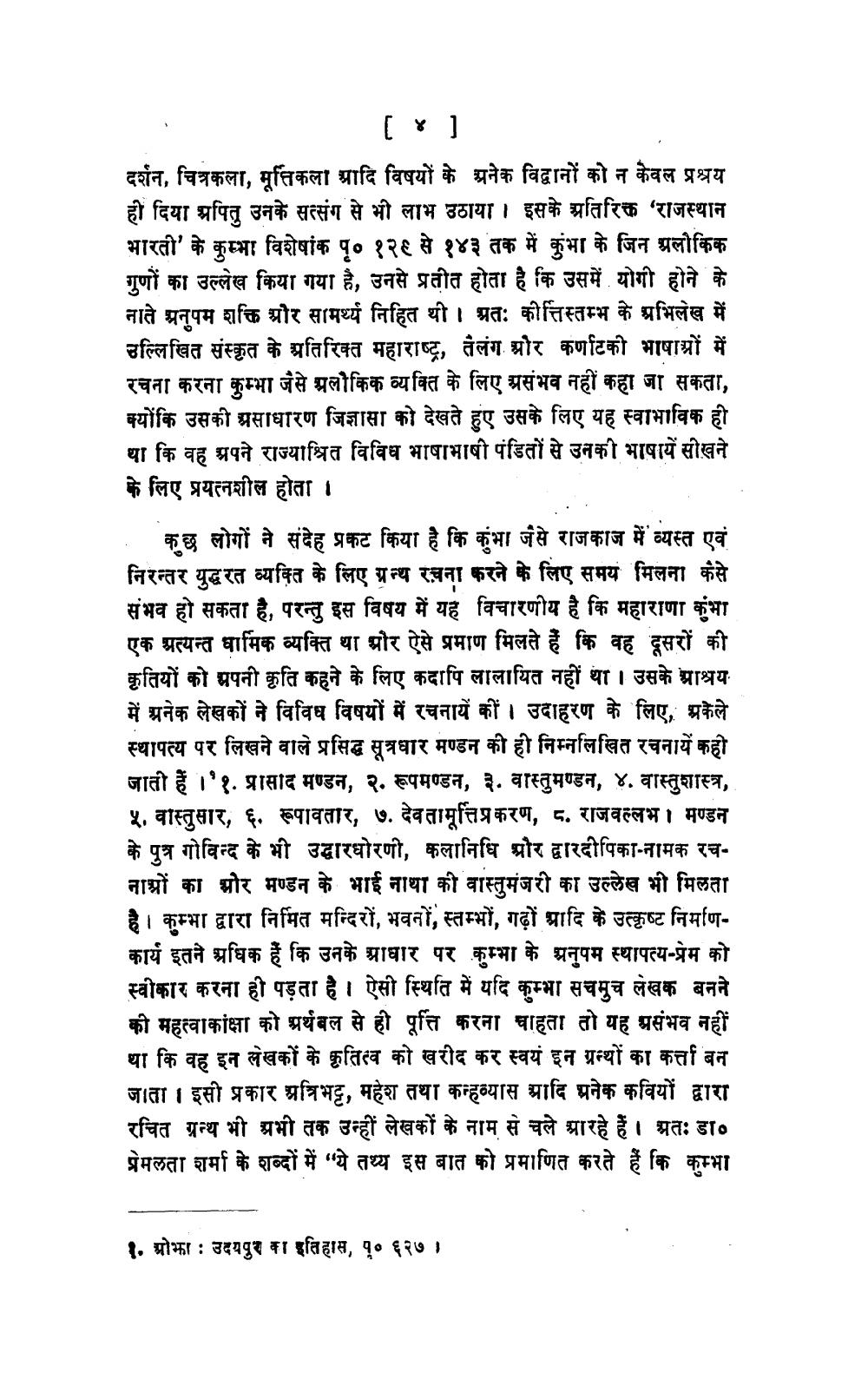________________
[ ४ ]
दर्शन, चित्रकला, मूर्तिकला आदि विषयों के अनेक विद्वानों को न केवल प्रश्रय ही दिया अपितु उनके सत्संग से भी लाभ उठाया। इसके अतिरिक्त ' राजस्थान भारती' के कुम्भा विशेषांक पृ० १२६ से १४३ तक में कुंभा के जिन अलोकिक गुणों का उल्लेख किया गया है, उनसे प्रतीत होता है कि उसमें योगी होने के नाते अनुपम शक्ति और सामर्थ्य निहित थी । श्रतः कीर्तिस्तम्भ के अभिलेख में उल्लिखित संस्कृत के अतिरिक्त महाराष्ट्र, तैलंग और कर्णाटकी भाषात्रों में रचना करना कुम्भा जैसे अलौकिक व्यक्ति के लिए असंभव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसकी असाधारण जिज्ञासा को देखते हुए उसके लिए यह स्वाभाविक ही
कि वह अपने राज्याश्रित विविध भाषाभाषी पंडितों से उनकी भाषायें सीखने के लिए प्रयत्नशील होता ।
कुछ लोगों ने संदेह प्रकट किया है कि कुंभा जैसे राजकाज में व्यस्त एवं निरन्तर युद्धरत व्यक्ति के लिए ग्रन्थ रचना करने के लिए समय मिलना कैसे संभव हो सकता है, परन्तु इस विषय में यह विचारणीय है कि महाराणा कुंभा एक अत्यन्त धार्मिक व्यक्ति था और ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि वह दूसरों की कृतियों को अपनी कृति कहने के लिए कदापि लालायित नहीं था । उसके प्राश्रय में अनेक लेखकों ने विविध विषयों में रचनायें कीं । उदाहरण के लिए, अकेले स्थापत्य पर लिखने वाले प्रसिद्ध सूत्रधार मण्डन की ही निम्नलिखित रचनायें कही जाती हैं । १. प्रासाद मण्डन, २. रूपमण्डन, ३. वास्तुमण्डन, ४. वास्तुशास्त्र, ५. वास्तुसार, ६. रूपावतार, ७. देवतामूर्तिप्रकरण, ८. राजवल्लभ । मण्डन के पुत्र गोविन्द के भी उद्धारधोरणी, कलानिधि श्रौर द्वारदीपिका- नामक रचनानों का और मण्डन के भाई नाथा की वास्तुमंजरी का उल्लेख भी मिलता है । कुम्भा द्वारा निर्मित मन्दिरों, भवनों, स्तम्भों, गढ़ों श्रादि के उत्कृष्ट निर्माणकार्य इतने अधिक हैं कि उनके आधार पर कुम्भा के अनुपम स्थापत्य प्रेम को स्वीकार करना ही पड़ता है । ऐसी स्थिति में यदि कुम्भा सचमुच लेखक बनने की महत्वाकांक्षा को अर्थबल से ही पूर्ति करना चाहता तो यह असंभव नहीं था कि वह इन लेखकों के कृतित्व को खरीद कर स्वयं इन ग्रन्थों का कर्त्ता बन जाता । इसी प्रकार अत्रिभट्ट, महेश तथा कन्हव्यास आदि अनेक कवियों द्वारा रचित ग्रन्थ भी अभी तक उन्हीं लेखकों के नाम से चले आ रहे हैं । अतः डा० प्रेमलता शर्मा के शब्दों में "ये तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कुम्भा
१. प्रोझा : उदयपुर का इतिहास, पू० ६२७ ।