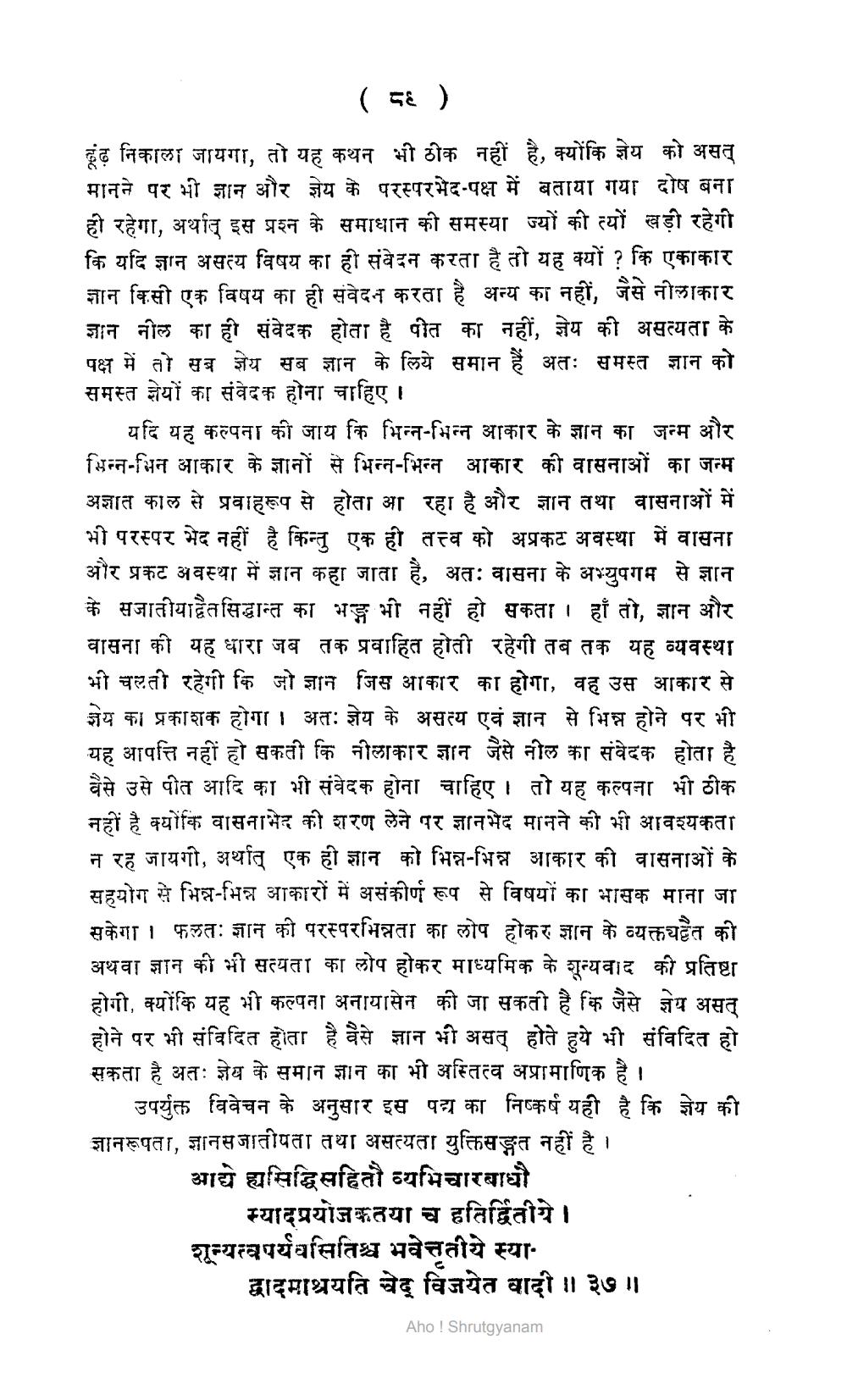________________
(
८८
)
ढूंढ़ निकाला जायगा, तो यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञेय को असत् मानने पर भी ज्ञान और ज्ञेय के परस्परभेद-पक्ष में बताया गया दोष बना ही रहेगा, अर्थात् इस प्रश्न के समाधान की समस्या ज्यों की त्यों खड़ी रहेगी कि यदि ज्ञान असत्य विषय का ही संवेदन करता है तो यह क्यों ? कि एकाकार ज्ञान किसी एक विषय का ही संवेदन करता है अन्य का नहीं, जैसे नीलाकार ज्ञान नील का ही संवेदक होता है पीत का नहीं, ज्ञेय की असत्यता के पक्ष में तो सब ज्ञेय सब ज्ञान के लिये समान हैं अतः समस्त ज्ञान को समस्त ज्ञेयों का संवेदक होना चाहिए।
यदि यह कल्पना की जाय कि भिन्न-भिन्न आकार के ज्ञान का जन्म और भिन्न-भिन आकार के ज्ञानों से भिन्न-भिन्न आकार की वासनाओं का जन्म अज्ञात काल से प्रवाहरूप से होता आ रहा है और ज्ञान तथा वासनाओं में भी परस्पर भेद नहीं है किन्तु एक ही तत्त्व को अप्रकट अवस्था में वासना और प्रकट अवस्था में ज्ञान कहा जाता है, अतः वासना के अभ्युपगम से ज्ञान के सजातीयाद्वैत सिद्धान्त का भङ्ग भी नहीं हो सकता। हाँ तो, ज्ञान और वासना की यह धारा जब तक प्रवाहित होती रहेगी तब तक यह व्यवस्था भी चलती रहेगी कि जो ज्ञान जिस आकार का होगा, वह उस आकार से ज्ञेय का प्रकाशक होगा। अतः ज्ञेय के असत्य एवं ज्ञान से भिन्न होने पर भी यह आपत्ति नहीं हो सकती कि नीलाकार ज्ञान जैसे नील का संवेदक होता है वैसे उसे पीत आदि का भी संवेदक होना चाहिए। तो यह कल्पना भी ठीक नहीं है क्योंकि वासनाभेद की शरण लेने पर ज्ञानभेद मानने की भी आवश्यकता न रह जायगी, अर्थात् एक ही ज्ञान को भिन्न-भिन्न आकार की वासनाओं के सहयोग से भिन्न-भिन्न आकारों में असंकीर्ण रूप से विषयों का भासक माना जा सकेगा। फलतः ज्ञान की परस्परभिन्नता का लोप होकर ज्ञान के व्यक्तयद्वैत की अथवा ज्ञान की भी सत्यता का लोप होकर माध्यमिक के शून्यवाद की प्रतिष्टा होगी, क्योंकि यह भी कल्पना अनायासेन की जा सकती है कि जैसे ज्ञेय असत् होने पर भी संविदित होता है वैसे ज्ञान भी असत् होते हुये भी संविदित हो सकता है अतः ज्ञेय के समान ज्ञान का भी अस्तित्व अप्रामाणिक है।
उपर्युक्त विवेचन के अनुसार इस पद्य का निष्कर्ष यही है कि ज्ञेय की ज्ञानरूपता, ज्ञानस जातीयता तथा असत्यता युक्तिसङ्गत नहीं है ।
आद्ये ह्यसिद्धिसहितौ व्यभिचारबाधौ
स्यादप्रयोजकतया च हतिर्द्वितीये। शून्यत्वपर्यवसितिश्च भवेत्ततीये स्या.
द्वादमाश्रयति चेद् विजयेत वादी ॥ ३७॥
Aho! Shrutgyanam