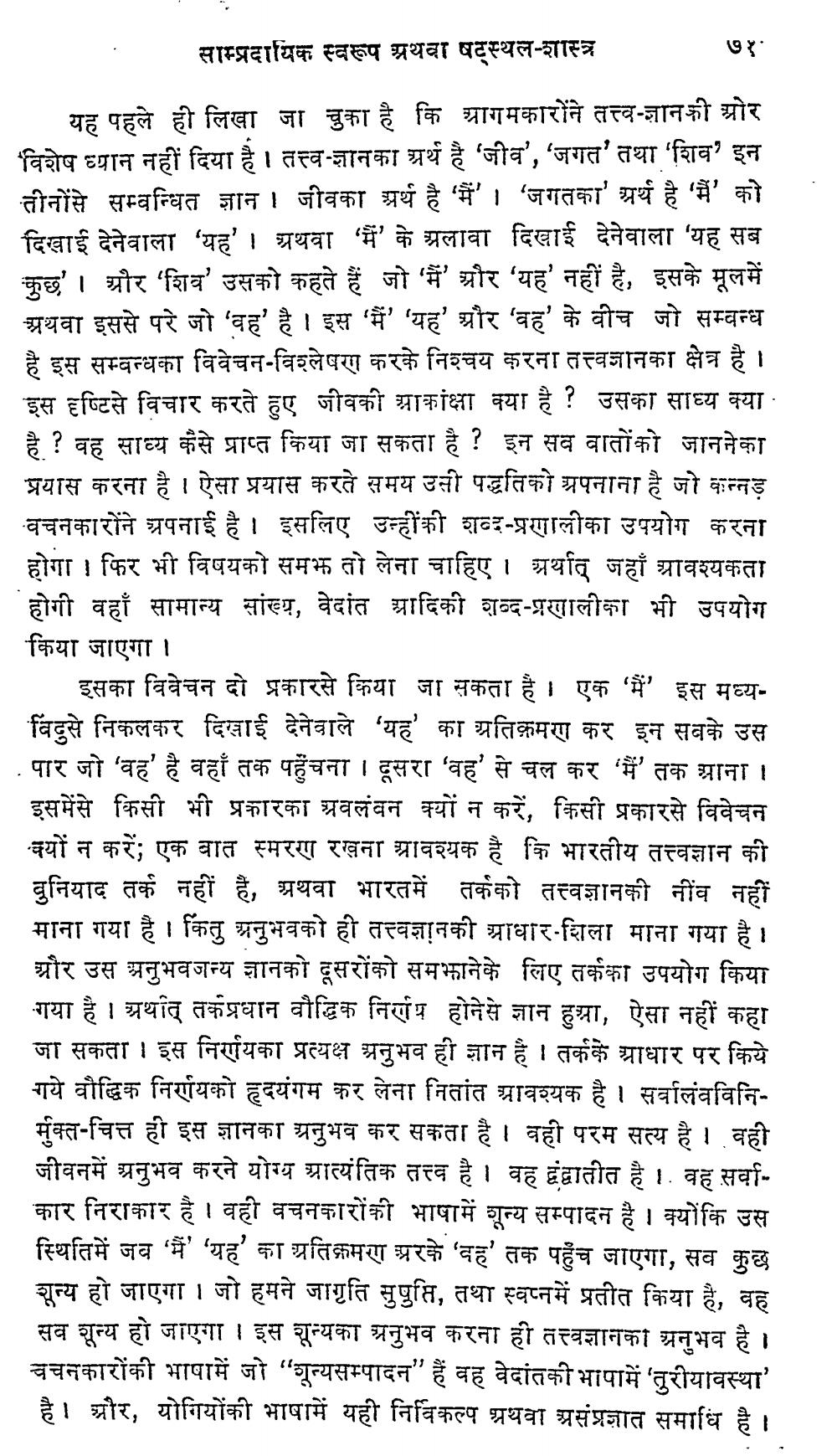________________
साम्प्रदायिक स्वरूप अथवा षट्स्थल - शास्त्र
यह पहले ही लिखा जा चुका है कि ग्रागमकारोंने तत्त्व-ज्ञानकी प्रोर 'विशेष ध्यान नहीं दिया है । तत्त्व-ज्ञानका अर्थ है 'जीव', 'जगत' तथा 'शिव' इन तीनोंसे सम्बन्धित ज्ञान । जीवका अर्थ है 'मैं' | 'जगतका' अर्थ है 'मैं' को दिखाई देनेवाला 'यह' । अथवा 'मैं' के अलावा दिखाई देनेवाला 'यह सब 'कुछ' | और 'शिव' उसको कहते हैं जो 'मैं' और 'यह' नहीं है, इसके मूलमें अथवा इससे परे जो 'वह' है । इस 'मैं' 'यह' और 'वह' के वीच जो सम्बन्ध है इस सम्बन्धका विवेचन-विश्लेषण करके निश्चय करना तत्त्वज्ञानका क्षेत्र है । इस दृष्टि से विचार करते हुए जीवकी प्राकांक्षा क्या है ? उसका साध्य क्या है ? वह साध्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? इन सब वातोंको जाननेका प्रयास करना है । ऐसा प्रयास करते समय उत्ती पद्धतिको अपनाना है जो कन्नड़ वचनकारोंने अपनाई है । इसलिए उन्हीं की शब्द- प्रणालीका उपयोग करना होगा । फिर भी विषयको समझ तो लेना चाहिए । अर्थात् जहाँ ग्रावश्यकता होगी वहाँ सामान्य सांख्य, वेदांत ग्रादिकी शब्द- प्रणालीका भी उपयोग किया जाएगा ।
इसका विवेचन दो प्रकारसे किया जा सकता है । एक 'मैं' इस मध्यबिंदुसे निकलकर दिखाई देनेवाले 'यह' का प्रतिक्रमण कर इन सबके उस पार जो 'वह' है वहाँ तक पहुँचना । दूसरा 'वह' से चल कर 'मैं' तक ग्राना । इसमें से किसी भी प्रकारका अवलंबन क्यों न करें, किसी प्रकार से विवेचन क्यों न करें; एक बात स्मरण रखना आवश्यक है कि भारतीय तत्त्वज्ञान की बुनियाद तर्क नहीं हैं, अथवा भारत में तर्कको तत्त्वज्ञानकी नींव नहीं माना गया है। किंतु अनुभवको ही तत्त्वज्ञानकी श्राधार- शिला माना गया है । नौर उस अनुभवजन्य ज्ञानको दूसरोंको समझाने के लिए तर्कका उपयोग किया गया है । अर्थात् तर्कप्रधान वौद्धिक निर्णय होनेसे ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं कहा जा सकता । इस निर्णयका प्रत्यक्ष अनुभव ही ज्ञान है । तर्कके ग्राधार पर किये गये वौद्धिक निर्णयको हृदयंगम कर लेना नितांत आवश्यक है । सर्वालंवविनिमुक्त-चित्त ही इस ज्ञानका अनुभव कर सकता है । वही परम सत्य है । वही जीवनमें अनुभव करने योग्य प्रात्यंतिक तत्त्व है । वह द्वंद्वातीत है । वह सर्वाकार निराकार है | वही वचनकारों की भाषा में शून्य सम्पादन है । क्योंकि उस स्थिति में जब 'मैं' 'यह' का प्रतिक्रमण अरके 'दह' तक पहुँच जाएगा, सव कुछ शून्य हो जाएगा । जो हमने जागृति सुषुप्ति, तथा स्वप्न में प्रतीत किया है, वह सव शून्य हो जाएगा । इस शून्यका अनुभव करना ही तत्त्वज्ञानका अनुभव है । वचनकारोंकी भाषामें जो " शून्यसम्पादन " हैं वह वेदांत की भाषा में 'तुरीयावस्था' है । और, योगियोंकी भाषामें यही निर्विकल्प श्रथवा असंप्रज्ञात समाधि है ।
७१
.