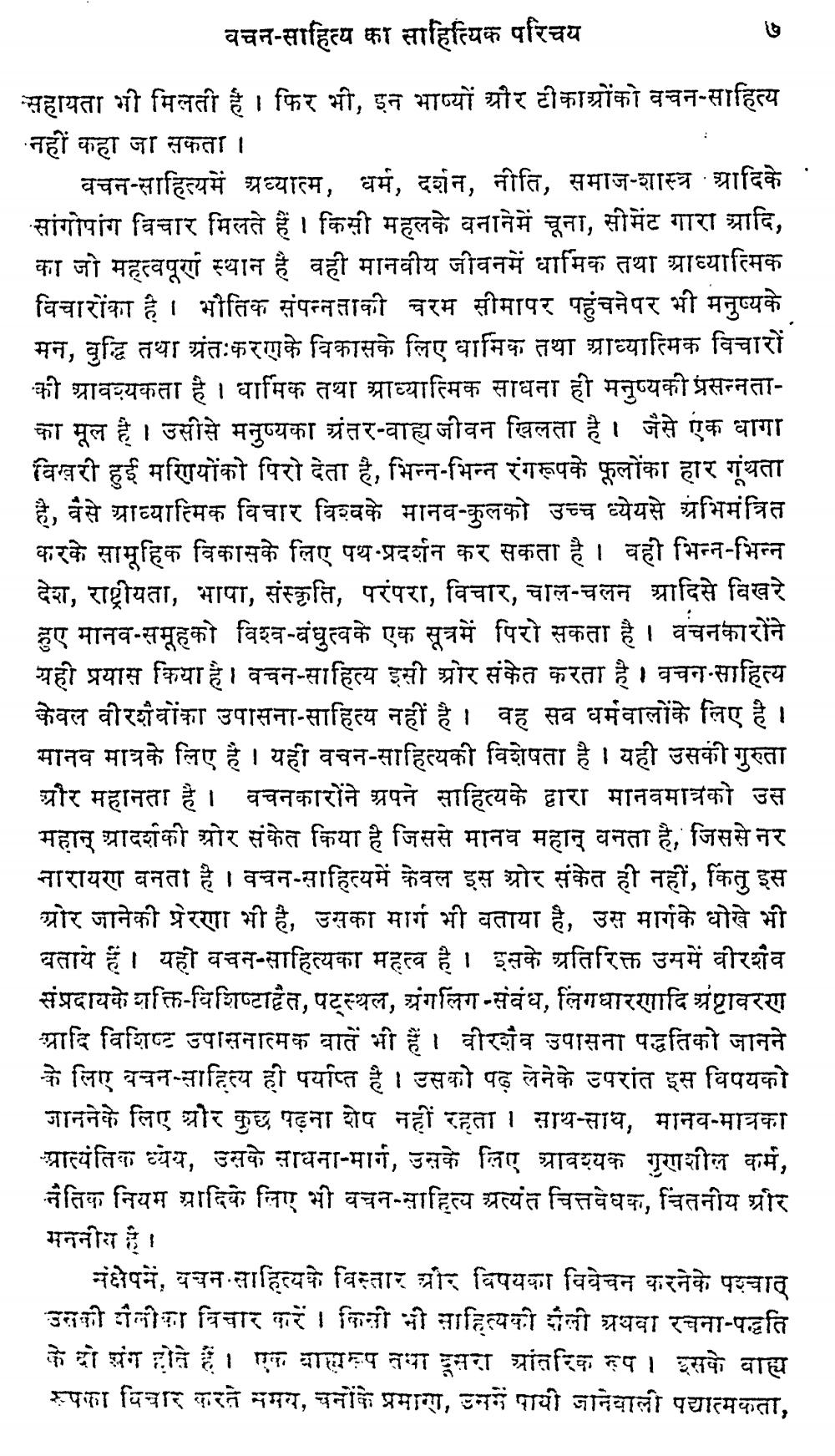________________
वचन-साहित्य का साहित्यिक परिचय सहायता भी मिलती है । फिर भी, इन भाष्यों और टीकाओंको वचन-साहित्य नहीं कहा जा सकता।
वचन-साहित्यमें अध्यात्म, धर्म, दर्शन, नीति, समाज-शास्त्र आदिके । सांगोपांग विचार मिलते हैं । किसी महलके बनानेमें चूना, सीमेंट गारा आदि, का जो महत्वपूर्ण स्थान है वही मानवीय जीवनमें धार्मिक तथा आध्यात्मिक विचारोंका है । भौतिक संपन्नताकी चरम सीमापर पहुंचने पर भी मनुष्यके मन, बुद्धि तथा अंतःकरणके विकासके लिए धार्मिक तथा प्राध्यात्मिक विचारों की आवश्यकता है । धार्मिक तथा आध्यात्मिक साधना ही मनुष्यकी प्रसन्नताका मूल है । उसीसे मनुष्यका अंतर-वाह्य जीवन खिलता है। जैसे एक धागा विखरी हुई मणियोंको पिरो देता है, भिन्न-भिन्न रंगरूपके फूलोंका हार गूंथता है, वैसे आध्यात्मिक विचार विश्वके मानव-कुलको उच्च ध्येयसे अभिमंत्रित करके सामूहिक विकासके लिए पथ-प्रदर्शन कर सकता है । वही भिन्न-भिन्न देश, राष्ट्रीयता, भाषा, संस्कृति, परंपरा, विचार, चाल-चलन आदिसे विखरे हुए मानव-समूहको विश्व-बंधुत्व के एक सूत्रमें पिरो सकता है । वचनकारोंने यही प्रयास किया है। वचन-साहित्य इसी ओर संकेत करता है । बचन साहित्य केवल वीरशैवोंका उपासना-साहित्य नहीं है। वह सब धर्मवालोंके लिए है। मानव मात्रके लिए है। यही वचन-साहित्यकी विशेषता है । यही उसकी गुरुता
और महानता है। वचनकारोंने अपने साहित्यके द्वारा मानवमात्रको उस महान् अादर्शकी ओर संकेत किया है जिससे मानव महान् बनता है, जिससे नर नारायण बनता है । वचन-साहित्यमें केवल इस ओर संकेत ही नहीं, किंतु इस
ओर जानेकी प्रेरणा भी है, उसका मार्ग भी बताया है, उस मार्गके धोखे भी बताये हैं। यही वचन-साहित्यका महत्व है। इसके अतिरिक्त उसमें वीरशैव संप्रदायके शक्ति-विशिष्टाद्वैत, पट्स्थल, अंगलिंग-संबंध, लिंगधारणादि अंटावरण आदि विशिष्ट उपासनात्मक बातें भी हैं। वीरशैव उपासना पद्धतिको जानने के लिए बचन-साहित्य ही पर्याप्त है । उसको पढ़ लेनेके उपरांत इस विषयको जाननेके लिए और कुछ पढ़ना शेष नहीं रहता । साथ-साथ, मानव-मात्रका प्रात्यंतिक ध्येय, उसके साधना-मार्ग, उसके लिए आवश्यक गुणशील कर्म, नैतिक नियम ग्रादिके लिए भी वचन-साहित्य अत्यंत चित्तवेधक, चिंतनीय और मननीय है।
नक्षेपमें, बचन साहित्य के विस्तार और विषयका विवेचन करने के पश्चात् उसकी शैलीका विचार करें। किसी भी साहित्यको शैली अथवा रचना-पद्धति के दो अंग होते हैं। एक बाहाम्प तथा दूसरा प्रांतरिक रूप। इसके बाह्य रुपका विचार करते समय, चनों के प्रमाग, उनमें पायी जानेवाली पद्यात्मकता,