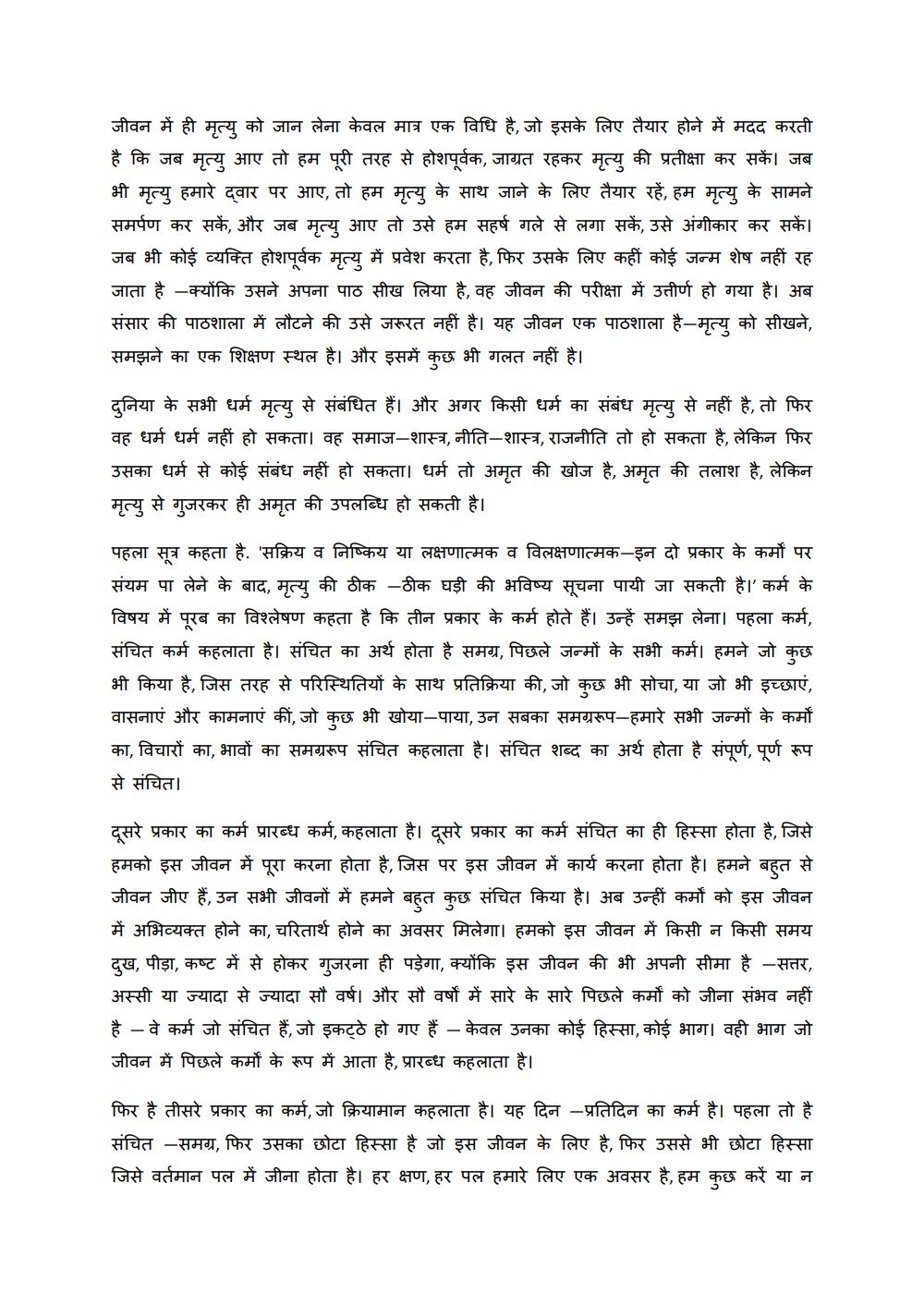________________ जीवन में ही मृत्यु को जान लेना केवल मात्र एक विधि है, जो इसके लिए तैयार होने में मदद करती है कि जब मृत्यु आए तो हम पूरी तरह से होशपूर्वक, जाग्रत रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकें। जब भी मृत्यु हमारे द्वार पर आए, तो हम मृत्यु के साथ जाने के लिए तैयार रहें, हम मृत्यु के सामने समर्पण कर सकें, और जब मृत्यू आए तो उसे हम सहर्ष गले से लगा सकें, उसे अंगीकार कर सकें। जब भी कोई व्यक्ति होशपूर्वक मृत्य में प्रवेश करता है, फिर उसके लिए कहीं कोई जन्म शेष नहीं जाता है -क्योंकि उसने अपना पाठ सीख लिया है, वह जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है। अब संसार की पाठशाला में लौटने की उसे जरूरत नहीं है। यह जीवन एक पाठशाला है-मृत्यु को सीखने, समझने का एक शिक्षण स्थल है। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दुनिया के सभी धर्म मृत्यु से संबंधित हैं। और अगर किसी धर्म का संबंध मृत्यु से नहीं है, तो फिर वह धर्म धर्म नहीं हो सकता। वह समाज-शास्त्र, नीति-शास्त्र, राजनीति तो हो सकता है, लेकिन फिर उसका धर्म से कोई संबंध नहीं हो सकता। धर्म तो अमृत की खोज है, अमृत की तलाश है, लेकिन मृत्यु से गुजरकर ही अमृत की उपलब्धि हो सकती है। पहला सूत्र कहता है. 'सक्रिय व निष्किय या लक्षणात्मक व विलक्षणात्मक-इन दो प्रकार के कर्मों पर संयम पा लेने के बाद, मृत्यु की ठीक -ठीक घड़ी की भविष्य सूचना पायी जा सकती है।' कर्म के विषय में परब का विश्लेषण कहता है कि तीन प्रकार के कर्म होते हैं। उन्हें समझ लेना। पहला कर्म, संचित कर्म कहलाता है। संचित का अर्थ होता है समग्र, पिछले जन्मों के सभी कर्म। हमने जो कुछ भी किया है, जिस तरह से परिस्थितियों के साथ प्रतिक्रिया की, जो कुछ भी सोचा, या जो भी इच्छाएं, वासनाएं और कामनाएं की, जो कुछ भी खोया-पाया, उन सबका समग्ररूप-हमारे सभी जन्मों के कर्मों का, विचारों का, भावों का समग्ररूप संचित कहलाता है। संचित शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण, पूर्ण रूप से संचित। दूसरे प्रकार का कर्म प्रारब्ध कर्म, कहलाता है। दूसरे प्रकार का कर्म संचित का ही हिस्सा होता है, जिसे हमको इस जीवन में पूरा करना होता है, जिस पर इस जीवन में कार्य करना होता है। हमने बहुत से जीवन जीए हैं, उन सभी जीवनों में हमने छ संचित किया है। अब उन्हीं कर्मों को इस जीवन में अभिव्यक्त होने का, चरितार्थ होने का अवसर मिलेगा। हमको इस जीवन में किसी न किसी समय दुख, पीड़ा, कष्ट में से होकर गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि इस जीवन की भी अपनी सीमा है -सत्तर, अस्सी या ज्यादा से ज्यादा सौ वर्ष। और सौ वर्षों में सारे के सारे पिछले कर्मों को जीना संभव नहीं है - वे कर्म जो संचित हैं, जो इकट्ठे हो गए हैं - केवल उनका कोई हिस्सा, कोई भाग। वही भाग जो जीवन में पिछले कर्मों के रूप में आता है, प्रारब्ध कहलाता है। फिर है तीसरे प्रकार का कर्म, जो क्रियामान कहलाता है। यह दिन -प्रतिदिन का कर्म है। पहला तो है संचित –समग्र, फिर उसका छोटा हिस्सा है जो इस जीवन के लिए है, फिर उससे भी छोटा हिस्सा जिसे वर्तमान पल में जीना होता है। हर क्षण, हर पल हमारे लिए एक अवसर है, हम कुछ करें या न