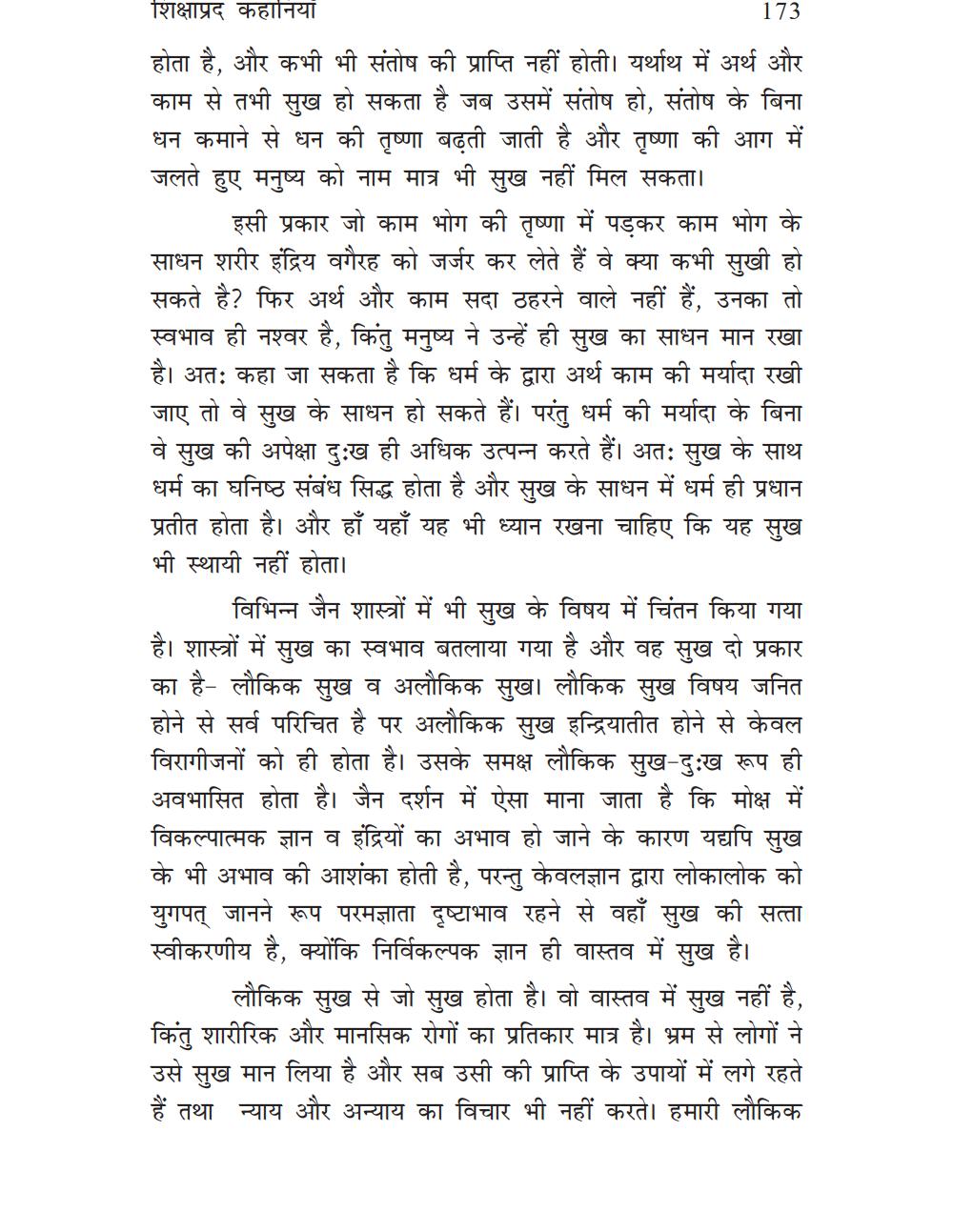________________
शिक्षाप्रद कहानिया
173 होता है, और कभी भी संतोष की प्राप्ति नहीं होती। यर्थाथ में अर्थ और काम से तभी सुख हो सकता है जब उसमें संतोष हो, संतोष के बिना धन कमाने से धन की तृष्णा बढ़ती जाती है और तृष्णा की आग में जलते हुए मनुष्य को नाम मात्र भी सुख नहीं मिल सकता।
इसी प्रकार जो काम भोग की तृष्णा में पड़कर काम भोग के साधन शरीर इंद्रिय वगैरह को जर्जर कर लेते हैं वे क्या कभी सुखी हो सकते है? फिर अर्थ और काम सदा ठहरने वाले नहीं हैं, उनका तो स्वभाव ही नश्वर है, किंतु मनुष्य ने उन्हें ही सुख का साधन मान रखा है। अतः कहा जा सकता है कि धर्म के द्वारा अर्थ काम की मर्यादा रखी जाए तो वे सुख के साधन हो सकते हैं। परंतु धर्म की मर्यादा के बिना वे सुख की अपेक्षा दुःख ही अधिक उत्पन्न करते हैं। अतः सुख के साथ धर्म का घनिष्ठ संबंध सिद्ध होता है और सुख के साधन में धर्म ही प्रधान प्रतीत होता है। और हाँ यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह सुख भी स्थायी नहीं होता।
विभिन्न जैन शास्त्रों में भी सुख के विषय में चिंतन किया गया है। शास्त्रों में सुख का स्वभाव बतलाया गया है और वह सुख दो प्रकार का है- लौकिक सुख व अलौकिक सुख। लौकिक सुख विषय जनित होने से सर्व परिचित है पर अलौकिक सुख इन्द्रियातीत होने से केवल विरागीजनों को ही होता है। उसके समक्ष लौकिक सुख-दु:ख रूप ही अवभासित होता है। जैन दर्शन में ऐसा माना जाता है कि मोक्ष में विकल्पात्मक ज्ञान व इंद्रियों का अभाव हो जाने के कारण यद्यपि सुख के भी अभाव की आशंका होती है, परन्तु केवलज्ञान द्वारा लोकालोक को युगपत् जानने रूप परमज्ञाता दृष्टाभाव रहने से वहाँ सुख की सत्ता स्वीकरणीय है, क्योंकि निर्विकल्पक ज्ञान ही वास्तव में सुख है।
लौकिक सुख से जो सुख होता है। वो वास्तव में सुख नहीं है, किंतु शारीरिक और मानसिक रोगों का प्रतिकार मात्र है। भ्रम से लोगों ने उसे सुख मान लिया है और सब उसी की प्राप्ति के उपायों में लगे रहते हैं तथा न्याय और अन्याय का विचार भी नहीं करते। हमारी लौकिक