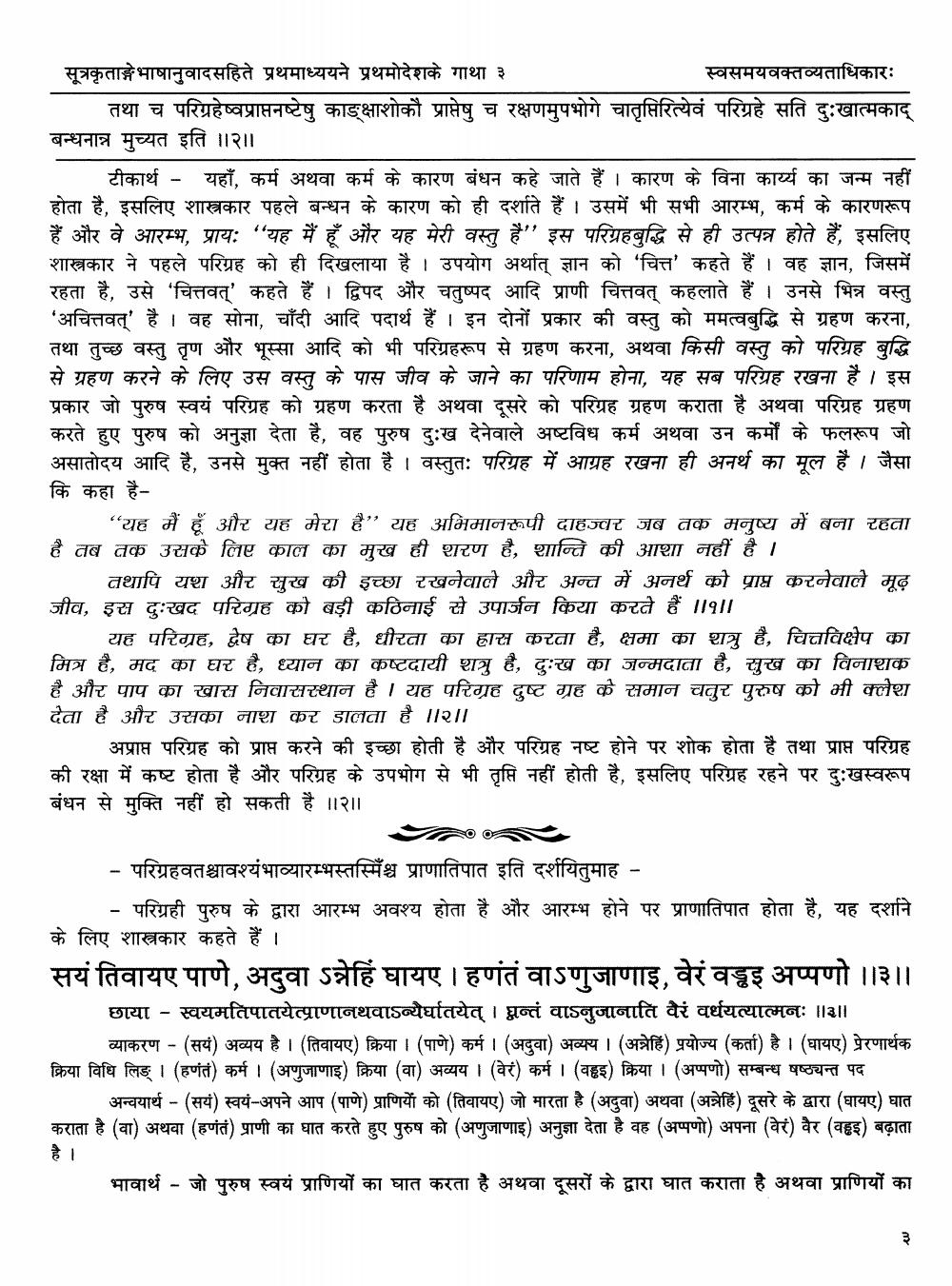________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते प्रथमाध्ययने प्रथमोदेशके गाथा ३
स्वसमयवक्तव्यताधिकारः
तथा च परिग्रहेष्वप्राप्तनष्टेषु काङ्क्षाशोकौ प्राप्तेषु च रक्षणमुपभोगे चातृप्तिरित्येवं परिग्रहे सति दुःखात्मकाद् बन्धनान्न मुच्यत इति ॥२॥
टीकार्थ यहाँ, कर्म अथवा कर्म के कारण बंधन कहे जाते हैं । कारण के विना कार्य्य का जन्म नहीं होता है, इसलिए शास्त्रकार पहले बन्धन के कारण को ही दर्शाते हैं । उसमें भी सभी आरम्भ, कर्म के कारणरूप हैं और वे आरम्भ, प्रायः " यह मैं हूँ और यह मेरी वस्तु है" इस परिग्रहबुद्धि से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए शास्त्रकार ने पहले परिग्रह को ही दिखलाया है । उपयोग अर्थात् ज्ञान को 'चित्त' कहते हैं । वह ज्ञान, जिसमें रहता है, उसे 'चित्तवत्' कहते हैं । द्विपद और चतुष्पद आदि प्राणी चित्तवत् कहलाते हैं। उनसे भिन्न वस्तु 'अचित्तवत्' है । वह सोना, चाँदी आदि पदार्थ हैं । इन दोनों प्रकार की वस्तु को ममत्वबुद्धि से ग्रहण करना, तथा तुच्छ वस्तु तृण और भूस्सा आदि को भी परिग्रहरूप से ग्रहण करना, अथवा किसी वस्तु को परिग्रह बुद्धि से ग्रहण करने के लिए उस वस्तु के पास जीव के जाने का परिणाम होना, यह सब परिग्रह रखना / इस प्रकार जो पुरुष स्वयं परिग्रह को ग्रहण करता है अथवा दूसरे को परिग्रह ग्रहण कराता है अथवा परिग्रह ग्रहण करते हुए पुरुष को अनुज्ञा देता है, वह पुरुष दुःख देनेवाले अष्टविध कर्म अथवा उन कर्मों के फलरूप जो असातोदय आदि है, उनसे मुक्त नहीं होता है । वस्तुतः परिग्रह में आग्रह रखना ही अनर्थ का मूल है। जैसा कि कहा है
-
"यह मैं हूँ और यह मेरा है" यह अभिमानरूपी दाहज्वर जब तक मनुष्य में बना रहता है तब तक उसके लिए काल का मुख ही शरण है, शान्ति की आशा नहीं है ।
तथापि यश और सुख की इच्छा रखनेवाले और अन्त में अनर्थ को प्राप्त करनेवाले मूढ़ जीव, इस दुःखद परिग्रह को बड़ी कठिनाई से उपार्जन किया करते हैं ||१||
यह परिग्रह, द्वेष का घर है, धीरता का ह्रास करता है, क्षमा का शत्रु है, चित्तविक्षेप का मित्र है, मद का घर है, ध्यान का कष्टदायी शत्रु है, दुःख का जन्मदाता है, सुख का विनाशक है और पाप का खास निवासस्थान है । यह परिग्रह दुष्ट ग्रह के समान चतुर पुरुष को भी क्लेश देता है और उसका नाश कर डालता है ॥२॥
अप्राप्त परिग्रह को प्राप्त करने की इच्छा होती है और परिग्रह नष्ट होने पर शोक होता है तथा प्राप्त परिग्रह की रक्षा में कष्ट होता है और परिग्रह के उपभोग से भी तृप्ति नहीं होती है, इसलिए परिग्रह रहने पर दुःखस्वरूप बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती है ॥२॥
परिग्रहवतश्चावश्यंभाव्यारम्भस्तस्मिँश्च प्राणातिपात इति दर्शयितुमाह
परिग्रही पुरुष के द्वारा आरम्भ अवश्य होता है और आरम्भ होने पर प्राणातिपात होता है, यह दर्शाने के लिए शास्त्रकार कहते हैं ।
सयं तिवायए पाणे, अदुवा ऽन्नेहिं घायए । हणंतं वाऽणुजाणाइ, वेरं वड्ढइ अप्पणी ||३||
छाया - स्वयमतिपातयेत्प्राणानथवाऽन्यैर्घातयेत् । घ्नन्तं वाऽनुजानाति वैरं वर्धयत्यात्मनः ||३||
व्याकरण - (सयं) अव्यय है । (तिवायए) क्रिया । (पाणे) कर्म । (अदुवा) अव्यय । (अनेहिं) प्रयोज्य (कर्ता) है । ( घायए) प्रेरणार्थक क्रिया विधि लिङ् । (हणंतं) कर्म । (अणुजाणाइ) क्रिया (वा) अव्यय । (वेरं) कर्म । (वड्डइ) क्रिया । (अप्पणो) सम्बन्ध षष्ठ्यन्त पद
-
अन्वयार्थ – (सयं) स्वयं-अपने आप (पाणे) प्राणियों को (तिवायए) जो मारता है (अदुवा) अथवा (अन्नेहिं) दूसरे के द्वारा (घायए) घात कराता है (वा) अथवा (हणंतं) प्राणी का घात करते हुए पुरुष को (अणुजाणाइ) अनुज्ञा देता है वह (अप्पणो ) अपना (वेरं) वैर (वडइ) बढ़ाता
है ।
भावार्थ जो पुरुष स्वयं प्राणियों का घात करता है अथवा दूसरों के द्वारा घात कराता है अथवा प्राणियों का
३