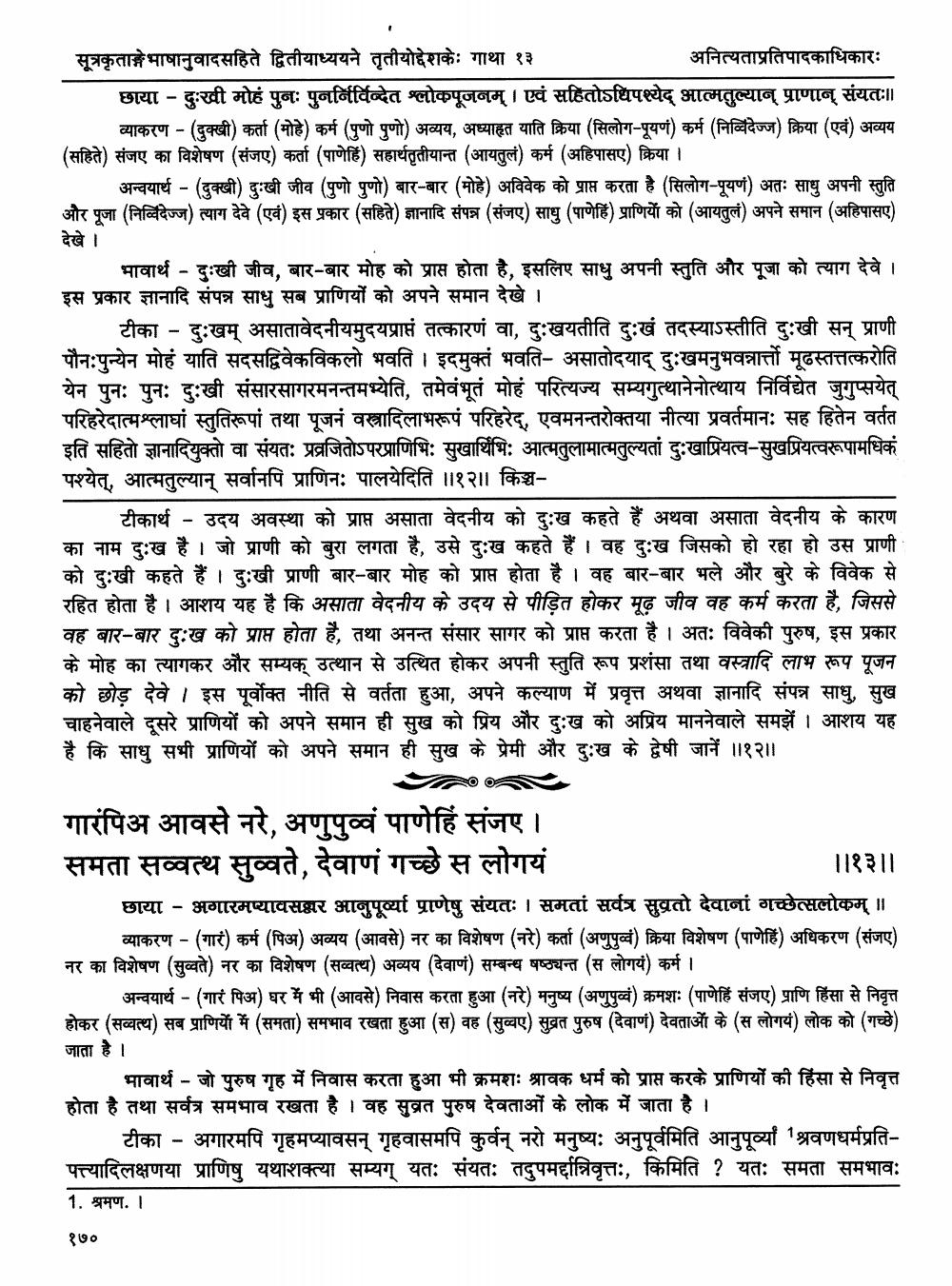________________
सूत्रकृताङ्गेभाषानुवादसहिते द्वितीयाध्ययने तृतीयोद्देशकः गाथा १३
अनित्यताप्रतिपादकाधिकारः ____ छाया - दुःखी मोहं पुनः पुनर्निर्विव्देत श्लोकपूजनम् । एवं सहितोऽधिपश्येद् आत्मतुल्यान् प्राणान् संयतः।।
व्याकरण - (दुक्खी) कर्ता (मोहे) कर्म (पुणो पुणो) अव्यय, अध्याहृत याति क्रिया (सिलोग-पूयणं) कर्म (निविंदेज्ज) क्रिया (एवं) अव्यय (सहिते) संजए का विशेषण (संजए) कर्ता (पाणेहि) सहार्थतृतीयान्त (आयतुलं) कर्म (अहिपासए) क्रिया ।
अन्वयार्थ - (दुक्खी) दुःखी जीव (पुणो पुणो) बार-बार (मोहे) अविवेक को प्राप्त करता है (सिलोग-पूयणं) अतः साधु अपनी स्तुति और पूजा (निविंदेज्ज) त्याग देवे (एवं) इस प्रकार (सहिते) ज्ञानादि संपन्न (संजए) साधु (पाणेहिं) प्राणियों को (आयतुलं) अपने समान (अहिपासए) देखे।
भावार्थ - दुःखी जीव, बार-बार मोह को प्राप्त होता है, इसलिए साधु अपनी स्तुति और पूजा को त्याग देवे । इस प्रकार ज्ञानादि संपन्न साधु सब प्राणियों को अपने समान देखे ।
टीका - दुःखम् असातावेदनीयमुदयप्राप्तं तत्कारणं वा, दुःखयतीति दुःखं तदस्याऽस्तीति दुःखी सन् प्राणी पौनःपुन्येन मोहं याति सदसद्विवेकविकलो भवति । इदमुक्तं भवति- असातोदयाद् दुःखमनुभवन्नार्को मूढस्तत्तत्करोति येन पुनः पुनः दुःखी संसारसागरमनन्तमभ्येति, तमेवंभूतं मोहं परित्यज्य सम्यगुत्थानेनोत्थाय निर्विद्येत परिहरेदात्मश्लाघां स्तुतिरूपां तथा पूजनं वस्त्रादिलाभरूपं परिहरेद्, एवमनन्तरोक्तया नीत्या प्रवर्तमानः सह हितेन वर्तत इति सहितो ज्ञानादियुक्तो वा संयतः प्रव्रजितोऽपरप्राणिभिः सुखार्थिभिः आत्मतुलामात्मतुल्यतां दुःखाप्रियत्व-सुखप्रियत्वरूपामधिकं पश्येत्, आत्मतुल्यान् सर्वानपि प्राणिनः पालयेदिति ।।१२।। किञ्च
टीकार्थ - उदय अवस्था को प्राप्त असाता वेदनीय को दुःख कहते हैं अथवा असाता वेदनीय के कारण का नाम दुःख है । जो प्राणी को बुरा लगता है, उसे दुःख कहते हैं । वह दुःख जिसको हो रहा हो उस प्राणी को दुःखी कहते हैं । दुःखी प्राणी बार-बार मोह को प्राप्त होता है । वह बार-बार भले और बुरे के विवेक से रहित होता है । आशय यह है कि असाता वेदनीय के उदय से पीड़ित होकर मूढ़ जीव वह कर्म करता है, जिससे वह बार-बार दुःख को प्राप्त होता है, तथा अनन्त संसार सागर को प्राप्त करता है । अतः विवेकी पुरुष, इस प्रकार के मोह का त्यागकर और सम्यक् उत्थान से उत्थित होकर अपनी स्तुति रूप प्रशंसा तथा वस्त्रादि लाभ रूप पूजन को छोड़ दे पूर्वाक्त नीति से वतेता हुआ, अपने कल्याण में प्रवृत्त अथवा ज्ञानादि संपन्न साधु, सुख चाहनेवाले दूसरे प्राणियों को अपने समान ही सुख को प्रिय और दुःख को अप्रिय माननेवाले समझें । आशय यह है कि साधु सभी प्राणियों को अपने समान ही सुख के प्रेमी और दुःख के द्वेषी जानें ॥१२॥
गारंपिअ आवसे नरे, अणुपुव्वं पाणेहिं संजए । समता सव्वत्थ सुव्वते, देवाणं गच्छे स लोगयं
॥१३॥ छाया - अगारमप्यावसकर आनुपूर्ध्या प्राणेषु संयतः । समतां सर्वत्र सुव्रतो देवानां गच्छेत्सलोकम् ॥
व्याकरण - (गार) कर्म (पिअ) अव्यय (आवसे) नर का विशेषण (नरे) कर्ता (अणुपुव्वं) क्रिया विशेषण (पाणेहिं) अधिकरण (संजए) नर का विशेषण (सुब्बते) नर का विशेषण (सव्वत्थ) अव्यय (देवाणं) सम्बन्ध षष्ठ्यन्त (स लोगयं) कर्म ।
अन्वयार्थ - (गार पिअ) घर में भी (आवसे) निवास करता हुआ (नरे) मनुष्य (अणुपुव्वं) क्रमशः (पाणेहिं संजए) प्राणि हिंसा से निवृत्त होकर (सव्वत्थ) सब प्राणियों में (समता) समभाव रखता हुआ (स) वह (सुब्बए) सुव्रत पुरुष (देवाणं) देवताओं के (स लोगय) लोक को (गच्छे) जाता है।
भावार्थ - जो पुरुष गृह में निवास करता हुआ भी क्रमशः श्रावक धर्म को प्राप्त करके प्राणियों की हिंसा से निवृत्त होता है तथा सर्वत्र समभाव रखता है । वह सुव्रत पुरुष देवताओं के लोक में जाता है ।
टीका अगारमपि गृहमप्यावसन् गृहवासमपि कुर्वन् नरो मनुष्यः अनुपूर्वमिति आनुपूर्त्या 'श्रवणधर्मप्रतिपत्त्यादिलक्षणया प्राणिषु यथाशक्त्या सम्यग् यतः संयतः तदुपमर्दानिवृत्तः, किमिति ? यतः समता समभावः 1. श्रमण.।
१७०