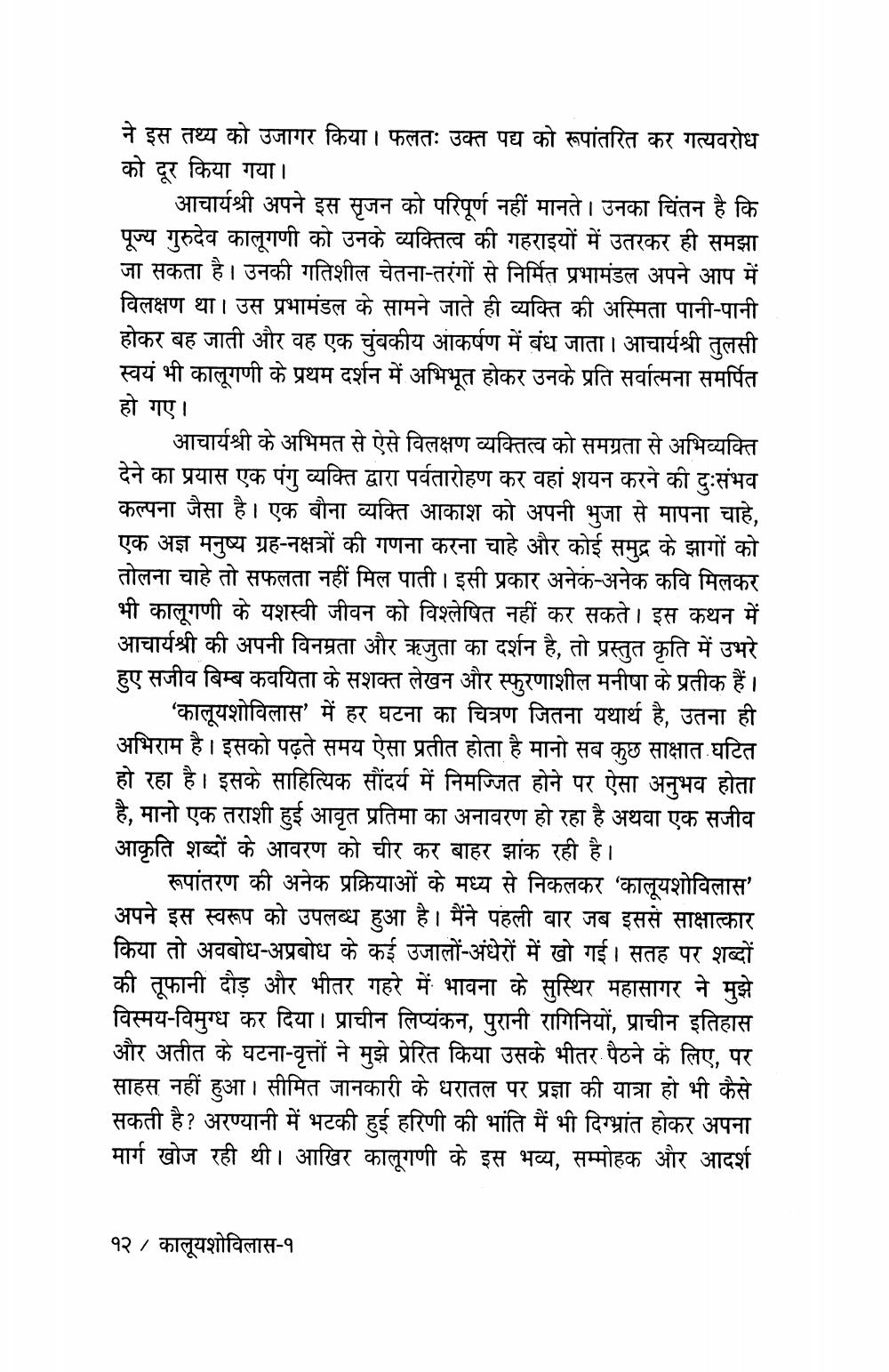________________
ने इस तथ्य को उजागर किया। फलतः उक्त पद्य को रूपांतरित कर गत्यवरोध को दूर किया गया।
आचार्यश्री अपने इस सृजन को परिपूर्ण नहीं मानते। उनका चिंतन है कि पूज्य गुरुदेव कालूगणी को उनके व्यक्तित्व की गहराइयों में उतरकर ही समझा जा सकता है। उनकी गतिशील चेतना-तरंगों से निर्मित प्रभामंडल अपने आप में विलक्षण था। उस प्रभामंडल के सामने जाते ही व्यक्ति की अस्मिता पानी-पानी होकर बह जाती और वह एक चुंबकीय आकर्षण में बंध जाता। आचार्यश्री तुलसी स्वयं भी कालूगणी के प्रथम दर्शन में अभिभूत होकर उनके प्रति सर्वात्मना समर्पित हो गए।
आचार्यश्री के अभिमत से ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व को समग्रता से अभिव्यक्ति देने का प्रयास एक पंगु व्यक्ति द्वारा पर्वतारोहण कर वहां शयन करने की दुःसंभव कल्पना जैसा है। एक बौना व्यक्ति आकाश को अपनी भुजा से मापना चाहे, एक अज्ञ मनुष्य ग्रह-नक्षत्रों की गणना करना चाहे और कोई समुद्र के झागों को तोलना चाहे तो सफलता नहीं मिल पाती। इसी प्रकार अनेक-अनेक कवि मिलकर भी कालूगणी के यशस्वी जीवन को विश्लेषित नहीं कर सकते। इस कथन में आचार्यश्री की अपनी विनम्रता और ऋजुता का दर्शन है, तो प्रस्तुत कृति में उभरे हुए सजीव बिम्ब कवयिता के सशक्त लेखन और स्फुरणाशील मनीषा के प्रतीक हैं। _ 'कालूयशोविलास' में हर घटना का चित्रण जितना यथार्थ है, उतना ही अभिराम है। इसको पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता है मानो सब कुछ साक्षात घटित हो रहा है। इसके साहित्यिक सौंदर्य में निमज्जित होने पर ऐसा अनुभव होता है, मानो एक तराशी हुई आवृत प्रतिमा का अनावरण हो रहा है अथवा एक सजीव आकृति शब्दों के आवरण को चीर कर बाहर झांक रही है।
रूपांतरण की अनेक प्रक्रियाओं के मध्य से निकलकर 'कालूयशोविलास' अपने इस स्वरूप को उपलब्ध हुआ है। मैंने पहली बार जब इससे साक्षात्कार किया तो अवबोध-अप्रबोध के कई उजालों-अंधेरों में खो गई। सतह पर शब्दों की तूफानी दौड़ और भीतर गहरे में भावना के सुस्थिर महासागर ने मुझे विस्मय-विमुग्ध कर दिया। प्राचीन लिप्यंकन, पुरानी रागिनियों, प्राचीन इतिहास
और अतीत के घटना-वृत्तों ने मुझे प्रेरित किया उसके भीतर पैठने के लिए, पर साहस नहीं हुआ। सीमित जानकारी के धरातल पर प्रज्ञा की यात्रा हो भी कैसे सकती है? अरण्यानी में भटकी हुई हरिणी की भांति मैं भी दिग्भ्रांत होकर अपना मार्ग खोज रही थी। आखिर कालूगणी के इस भव्य, सम्मोहक और आदर्श
१२ / कालूयशोविलास-१