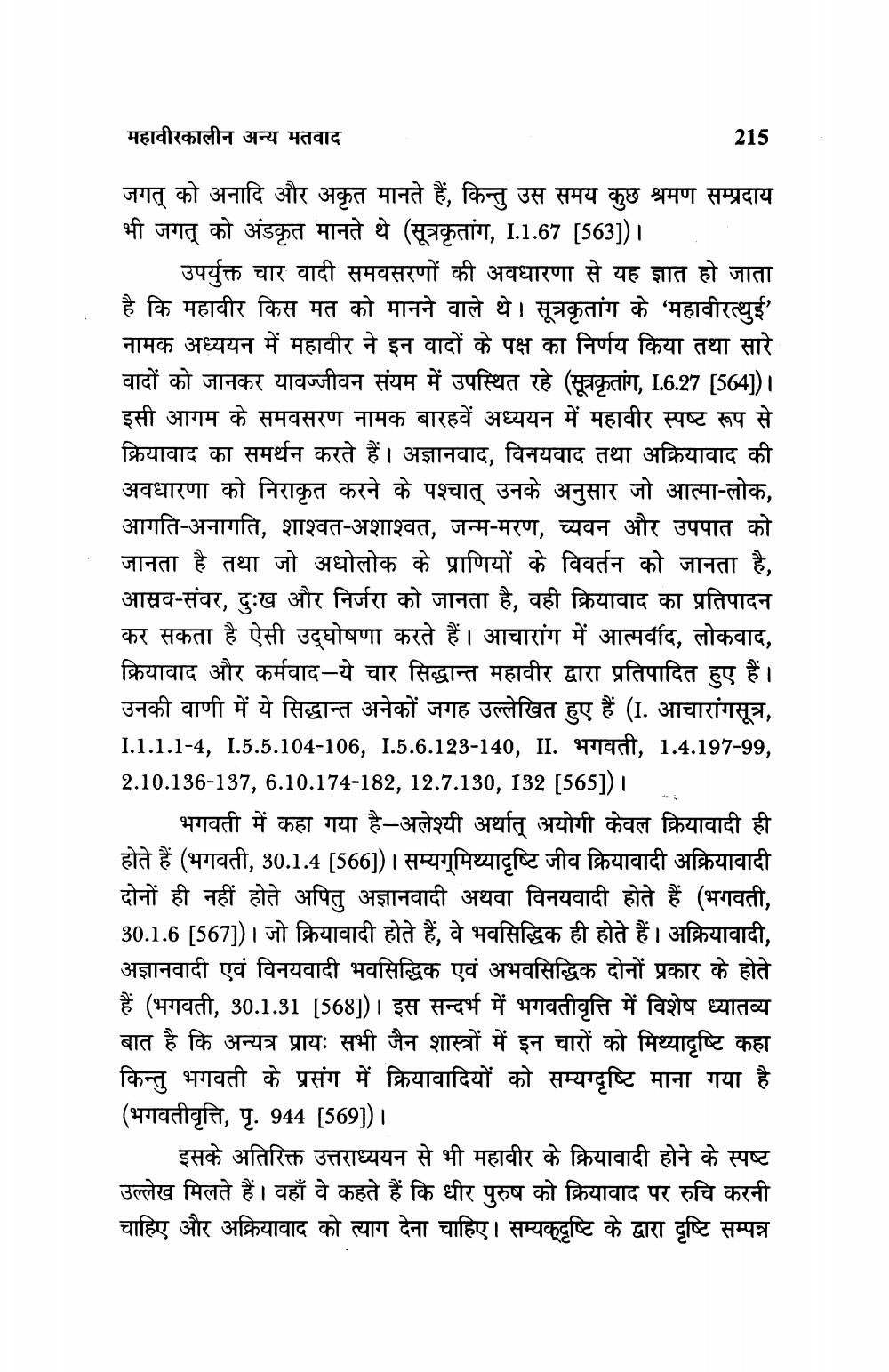________________
महावीरकालीन अन्य मतवाद
215
जगत् को अनादि और अकृत मानते हैं, किन्तु उस समय कुछ श्रमण सम्प्रदाय भी जगत् को अंडकृत मानते थे (सूत्रकृतांग, I.1.67 [563])।
उपर्युक्त चार वादी समवसरणों की अवधारणा से यह ज्ञात हो जाता है कि महावीर किस मत को मानने वाले थे। सूत्रकृतांग के ‘महावीरत्थुई' नामक अध्ययन में महावीर ने इन वादों के पक्ष का निर्णय किया तथा सारे वादों को जानकर यावज्जीवन संयम में उपस्थित रहे (सूत्रकृतांग, I.6.27 [564))। इसी आगम के समवसरण नामक बारहवें अध्ययन में महावीर स्पष्ट रूप से क्रियावाद का समर्थन करते हैं। अज्ञानवाद, विनयवाद तथा अक्रियावाद की अवधारणा को निराकृत करने के पश्चात् उनके अनुसार जो आत्मा-लोक, आगति-अनागति, शाश्वत-अशाश्वत, जन्म-मरण, च्यवन और उपपात को जानता है तथा जो अधोलोक के प्राणियों के विवर्तन को जानता है, आम्रव-संवर, दुःख और निर्जरा को जानता है, वही क्रियावाद का प्रतिपादन कर सकता है ऐसी उद्घोषणा करते हैं। आचारांग में आत्मदि, लोकवाद, क्रियावाद और कर्मवाद-ये चार सिद्धान्त महावीर द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। उनकी वाणी में ये सिद्धान्त अनेकों जगह उल्लेखित हुए हैं (I. आचारांगसूत्र, I.1.1.1-4, I.5.5.104-106, I.5.6.123-140, II. भगवती, 1.4.197-99, 2.10.136-137, 6.10.174-182, 12.7.130, 132 [565])।
__भगवती में कहा गया है-अलेश्यी अर्थात् अयोगी केवल क्रियावादी ही होते हैं (भगवती, 30.1.4 [566])। सम्यमिथ्यादृष्टि जीव क्रियावादी अक्रियावादी दोनों ही नहीं होते अपितु अज्ञानवादी अथवा विनयवादी होते हैं (भगवती, 30.1.6 [567])। जो क्रियावादी होते हैं, वे भवसिद्धिक ही होते हैं। अक्रियावादी, अज्ञानवादी एवं विनयवादी भवसिद्धिक एवं अभवसिद्धिक दोनों प्रकार के होते हैं (भगवती, 30.1.31 [568])। इस सन्दर्भ में भगवतीवृत्ति में विशेष ध्यातव्य बात है कि अन्यत्र प्रायः सभी जैन शास्त्रों में इन चारों को मिथ्यादृष्टि कहा किन्तु भगवती के प्रसंग में क्रियावादियों को सम्यग्दृष्टि माना गया है (भगवतीवृत्ति, पृ. 944 [569])।
इसके अतिरिक्त उत्तराध्ययन से भी महावीर के क्रियावादी होने के स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। वहाँ वे कहते हैं कि धीर पुरुष को क्रियावाद पर रुचि करनी चाहिए और अक्रियावाद को त्याग देना चाहिए। सम्यकदृष्टि के द्वारा दृष्टि सम्पन्न