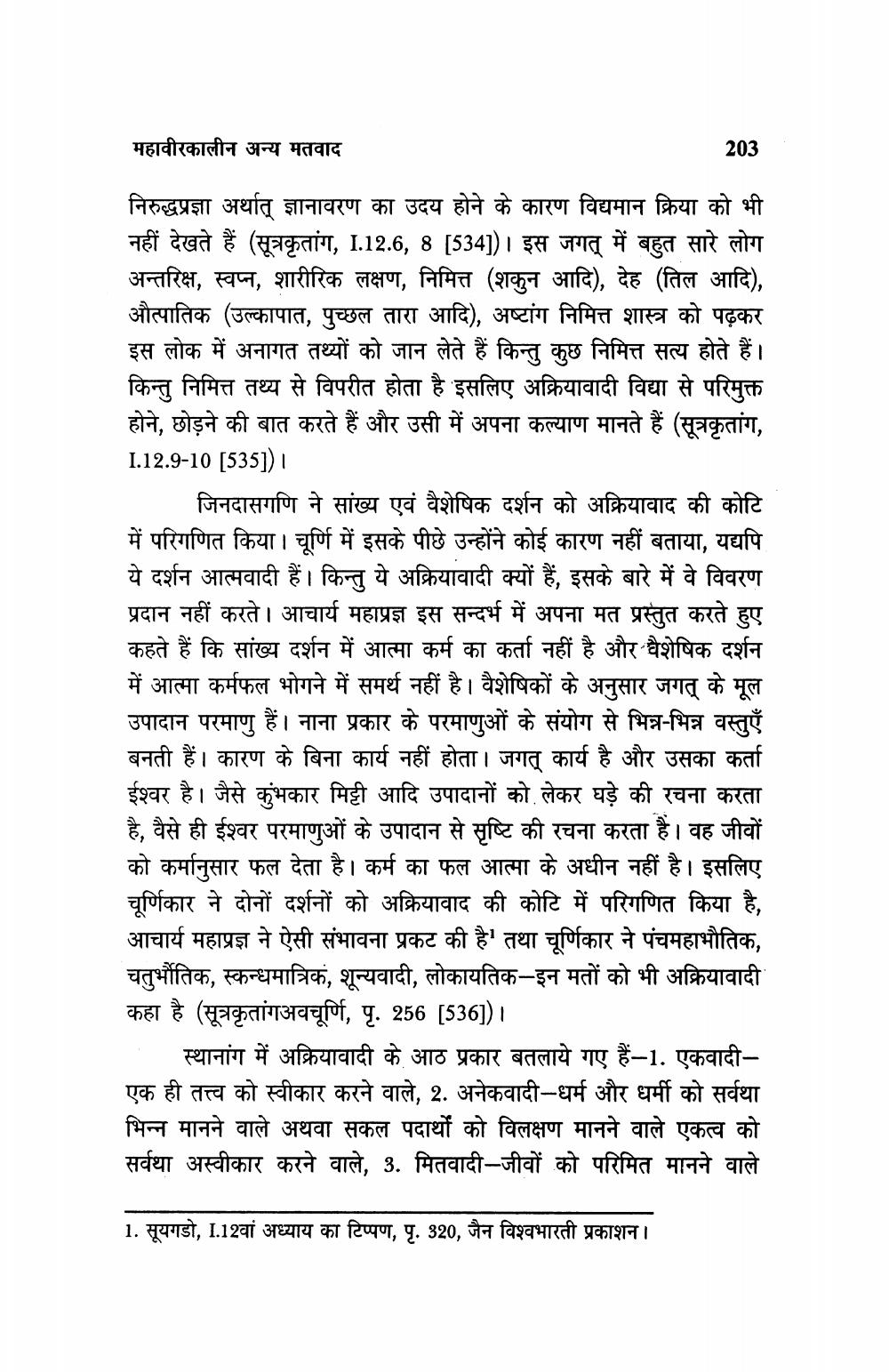________________
महावीरकालीन अन्य मतवाद
203
निरुद्धप्रज्ञा अर्थात् ज्ञानावरण का उदय होने के कारण विद्यमान क्रिया को भी नहीं देखते हैं (सूत्रकृतांग, I.12.6, 8 [534])। इस जगत् में बहुत सारे लोग अन्तरिक्ष, स्वप्न, शारीरिक लक्षण, निमित्त (शकुन आदि), देह (तिल आदि),
औत्पातिक (उल्कापात, पुच्छल तारा आदि), अष्टांग निमित्त शास्त्र को पढ़कर इस लोक में अनागत तथ्यों को जान लेते हैं किन्तु कुछ निमित्त सत्य होते हैं। किन्तु निमित्त तथ्य से विपरीत होता है इसलिए अक्रियावादी विद्या से परिमुक्त होने, छोड़ने की बात करते हैं और उसी में अपना कल्याण मानते हैं (सूत्रकृतांग, I.12.9-10 [535])।
जिनदासगणि ने सांख्य एवं वैशेषिक दर्शन को अक्रियावाद की कोटि में परिगणित किया। चूर्णि में इसके पीछे उन्होंने कोई कारण नहीं बताया, यद्यपि ये दर्शन आत्मवादी हैं। किन्तु ये अक्रियावादी क्यों हैं, इसके बारे में वे विवरण प्रदान नहीं करते। आचार्य महाप्रज्ञ इस सन्दर्भ में अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि सांख्य दर्शन में आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है और वैशेषिक दर्शन में आत्मा कर्मफल भोगने में समर्थ नहीं है। वैशेषिकों के अनुसार जगत् के मूल उपादान परमाणु हैं। नाना प्रकार के परमाणुओं के संयोग से भिन्न-भिन्न वस्तुएँ बनती हैं। कारण के बिना कार्य नहीं होता। जगत् कार्य है और उसका कर्ता ईश्वर है। जैसे कुंभकार मिट्टी आदि उपादानों को लेकर घड़े की रचना करता है, वैसे ही ईश्वर परमाणुओं के उपादान से सृष्टि की रचना करता है। वह जीवों को कर्मानुसार फल देता है। कर्म का फल आत्मा के अधीन नहीं है। इसलिए चूर्णिकार ने दोनों दर्शनों को अक्रियावाद की कोटि में परिगणित किया है, आचार्य महाप्रज्ञ ने ऐसी संभावना प्रकट की है तथा चूर्णिकार ने पंचमहाभौतिक, चतुर्भोतिक, स्कन्धमात्रिक, शून्यवादी, लोकायतिक-इन मतों को भी अक्रियावादी कहा है (सूत्रकृतांगअवचूर्णि, पृ. 256 [536])।
स्थानांग में अक्रियावादी के आठ प्रकार बतलाये गए हैं-1. एकवादीएक ही तत्त्व को स्वीकार करने वाले, 2. अनेकवादी-धर्म और धर्मी को सर्वथा भिन्न मानने वाले अथवा सकल पदार्थों को विलक्षण मानने वाले एकत्व को सर्वथा अस्वीकार करने वाले, 3. मितवादी-जीवों को परिमित मानने वाले
1. सूयगडो, I.12वां अध्याय का टिप्पण, पृ. 320, जैन विश्वभारती प्रकाशन।